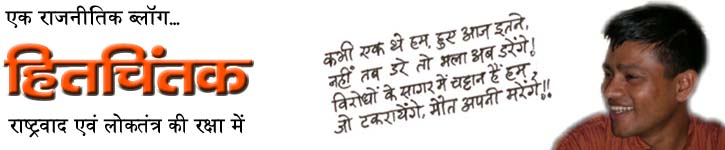आजादी की पहली लड़ाई
-संजीव कुमार सिन्हा
सन् 1857 का स्वतंत्रता-संग्राम अंग्रेजी हुकूमत पर वह पहला करारा प्रहार था, जिसकी परिणति 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के रूप में हुई। वास्तव में, यह स्वतंत्रता संग्राम कई मायनों में भारतीय इतिहास का सुनहरा अध्याय है। इसे आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अंग्रेजों की गुलामी के विरुध्द बगावत के स्वर नहीं उठे, निश्चित रुप से फिरंगियों को भारतवासियों की ओर से छिटपुट प्रतिरोध तो अवश्य झेलना पड़ता था, लेकिन पहली बार, 1857 में गुलामी की जंजीर को तोड़ फेंकने के लिए पूरा समाज एकजुट हो गया। इस विद्रोह के प्रमुख कर्णधार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब, अमर सिंह, तात्या टोपे, बहादुरशाह जफर, मौलवी अहमद शाह, राव तुलाराम, आदि थे। एक तरफ, आधुनिक शस्त्रों से लैस अंग्रेजों की सेना, सब तरह की सुविधाएं, उनकी 'फूट डालो-राज करो' की नीति। दूसरी तरफ, आम आदमी अपने ही बलबूते आधुनिक हथियारों के अभाव में भी, भाला, तीर-धनुष, लाठी और देशी बन्दूक लेकर अंग्रेजों के विरूध्द रणक्षेत्र में। भारतीयों ने उस महाशक्ति से लोहा लिया, जिसकी विश्व भर में तूती बोलती थी और उस समय ऐसा माना जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद से टकराना, तबाही को आमंत्रण देने के बराबर था। इस संघर्ष में दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अवधा आदि स्थानों में अंग्रेजों से खुले मुठभेड़ हुए, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। प्रमुख रुप से उत्तर भारत- उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मधय प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में यह संग्राम फैला, जबकि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में लोग बगावत के लिए मैदान में आए। इस क्रांति के परिप्रेक्ष्य में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्थिक साधनों के घोर अभाव के बावजूद लोगों ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया।
क्रांति की चिनगारी
अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया था कि जब तक भारतीय अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, तब तक भारत पर पूर्णरुपेण आधिपत्य नहीं जमाया जा सकता, क्योंकि भारतीय समाज की एकता का मुख्य आधार राजनीतिक न होकर धर्म और संस्कृति हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी परम्परागत ''फूट डालो और राज करो'' नीति के तहत सभी भारतवासियों को ईसाई बनाने की कुटिल चाल चली और हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की।
कलकत्ता में अंग्रेजी शासकों ने 1 जनवरी, 1857 को सेना में 'एनफील्ड राइफल्स' इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इस बन्दूक में प्रयोग होने वाले कारतूस की छर्रे गाय या सूअर की चर्बी से लिपटे रहते थे। बन्दूक में कारतूस भरने के पूर्व इसके छर्रों को मुंह से काटना होता था। इसको लेकर हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों में असंतोष के स्वर उभरने लगे। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इसकी अवहेलना करने वाले सैनिक को कोर्ट मार्शल करने का निर्देश दिया। अवहेलना करने वाले कई सैनिकों से वर्दी और हथियार वापस लेकर उन्हें अपमानित किया गया।
बरहामपुर के 19 एन.आई. के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इसके फलस्वरुप अनुशासनहीनता के आरोप में पूरी कम्पनी को भंग कर दिया गया। इसे लेकर सैनिकों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का वातावरण बनने लगा। इनमें से ही मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने इस तुगलकी फैसले के खिलाफ खुलकर विरोधा किया और अंग्रेजों को सबक सिखाने का ठान लिया। 29 मार्च, 1857 ई को पांडे ने अपनी कम्पनी के दो अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। इसके बाद कई अंग्रेज सैनिक उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, उन पर भी उसने गोली चला दी। उन्होंने जमकर अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया लेकिन अन्तत: वे पकड़ लिए गए और 8 अप्रैल, 1857 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। साथ ही 34वीं कम्पनी भी भंग कर दी गयी। इस कम्पनी के सैनिक मंगल पांडे की बहादुरी और शहादत के बारे में अपने क्षेत्रों की जनता के बीच चर्चा करने लगे। इसी तरह की घटना लखनऊ में भी घटी। 2 मई को 7वीं अवधा रेजीमेंट के सैनिकों ने भी ऐसे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इस आरोप में कम्पनी भंग कर दी गई। मंगल पांडे ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर देशधार्म की रक्षा की। उनकी शहादत रंग लाई। इससे प्रेरणा पाकर सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। उसकी प्रतिधवनि तुरन्त मेरठ में गूंजी।
6 मई, 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में 3 एल.सी. (घुड़सवार सैनिक टुकड़ी) की परेड में 90 भारतीय घुड़सवारों को चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग का आदेश हुआ। 5 को छोड़कर 85 ने दांत से कारतूसों को काटने से इनकार कर दिया। आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था पर धार्म का उतना ही पालन। आदेश के उल्लंघन में इन 85 सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल भेजने से पूर्व 9 मई को परेड ग्राउण्ड पर शेष सैनिकों को चेतावनी देने के लिए बुलाया गया। उनके समक्ष उन देश-धार्मभक्तों को पूरे अपमान के साथ हथकड़ियां पहनाकर जेल भेजा गया। 9 मई की ही रात में 10 मई के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया गया। 3 एल.सी. के कमांडर लेटी, गफ को यह भनक मिल गई कि 10 मई को रविवार है, ईसाइयों का गिररिजाघरों में प्रार्थना का दिन। विद्रोह पैदल सैनिकों द्वारा प्रारंभ होगा फिर घुड़सवार सैनिक उनसे मिल जायेंगे। 10 मई, 1857 को मेरठ में सचमुच क्रांति का सूत्रपात हो गया। बंदी सैनिकों को मुक्त करा लिया गया। हथियार लूट लिए गए। मेरठ में अंग्रेज सेना थोड़ी थी। मेरठ आजाद हो गया।
आग की लपटों की तरह फैल गई क्रांति
मेरठ के विप्लवियों के दिल्ली प्रवेश के साथ यहां के सैनिक नागरिक भी उनसे मिल गए। 82 वर्षीय बहादुरशाह जफर को हिन्दुस्तान का सम्राट घोषित किया गया और उसके नाम पर अंग्रेजों से घमासान शुरू हो गया। पहले दौर में क्रांतिकारियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया परन्तु अंग्रेज दिल्ली को वापस लेने पर कटिबध्द हो गए। सितम्बर, 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया।
आगरा नगर में ऊपरी शांति रही पर उससे सटे क्षेत्रों से विप्लवी लपटें पश्चिमी संयुक्त प्रांत के रूहेलखण्ड इलाके में, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी आदि जनपदों को छूने लगी। इन इलाकों की मुक्ति होती जा रही थी, लखनऊ में 3 मई को क्रांति का धामाका हुआ फिर वहीं से वह मई के अंत में अवधा रियासत को अपने प्रभाव में ले लेती है। नवाब वाजिदअली शाह के कलकत्ता निर्वाचन के बावजूद अवधा के सभी वर्ग के लोगों ने क्रांति में भाग लिया- जनक्रांति का नजारा था।
प्रशासक जान लारेंस की पक्की पहरेदारी के बावजूद पंजाब में विप्लव की घुसपैठ हो गई, विशेष रूप से उन छावनियों में जहां सिक्ख सैनिकों की संख्या कम थी या जहां पुरविया पलटने थीं यथा पेशावर, फिरोजपुर, रमदान, जालंधार, अजनाला आदि।
पंजाब की तुलना में आज के हरियाणा के ग्रामीण अंचल के किसानों ने क्रांति में बढ़चढ़ कर भाग लिया। इनमें रिबाड़ी के जमींदार राव तुलाराम व राव कृष्ण गोपाल ,मेवाती सरदार अली हसन, समद खां, झझर के नवाब अब्दुर्रहमान, वल्लभगढ़ के नाहर सिंह, फरूखनगर के नवाब फौजदार खां ने छिटपुट विद्रोह किया।
क्रांति की अग्निशिखा दक्षिण भारत में निजाम के हैदराबाद रियासत तक पहुंची, इधार के बड़े नवाब और राजा बाहरी तौर पर सरकार के प्रति वफादार रहे पर अंदर से भी उनमें साहस की कमी थी। फिर भी देशी पलटन और जनता ने युध्द में भाग लिया। हैदराबाद के जोतपुर, कोल्हापुर, सतारा, नागपुर, धार, जबलपुर, खानदेश, पूना, बाम्बे आदि में स्वाधीनता युध्द ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई।
इस क्रांति की मशाल बिहार में भी जली। यहां संघर्ष को नेतृत्व दिया जगदीशपुर रियासत के कुंवरसिंह और उनके भाई अमर सिंह ने। संघर्ष में जनता की भागीदारी ने हुकूमत को परेशानी में डाल दिया था। स्मरणीय है कि युध्द के दौरान अनेक क्षेत्रों रियासतों में ब्रिटिश राज का शामियाना उखड़ गया था। एक बार तो दिल्ली से बनारस तक ग्रेडट्रंक रोड़ आजाद था।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सितम्बर-अक्टूबर 1857 में झांसी पर अपना पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन उनका कब्जा महज छह महिने तक रहा। आखिरी विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर इलाके में दबा दिया। 8 जुलाई 1858 को एक शांति संधि हुई और यह विद्रोह अंतिम रुप से खत्म हो गया।
क्रांति की उपलब्धियां
कुछ ब्रिटीश और वामपंथी इतिहासकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को मात्र 'सिपाही विद्रोह' कहकर इसकी आलोचना करते है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह सही है कि सैनिकों ने इस लड़ाई का बिगुल बजाया लेकिन इसके साथ-साथ किसान, मजदूर, आदिवासी भी संगठित होकर रणभूमि में कूद पड़े थे। 1857 का युध्द राष्ट्रीय था। इसका राष्ट्रीयता की दृष्टि से सबसे सुखद परिणाम सामने आया कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। मराठों ने बहादुरशाह को सम्राट और मुसलमानों ने नानासाहब को पेशवा की मान्यता दी।
सन् 1908 ई. में प्रख्यात क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी चिंतक विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की शौर्य-गाथा को 'वार ऑफ इंडिपेंडेंस' नामक ग्रंथ में लिखकर इसे स्वाधीनता युध्द की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रस्तुत किया। उनका भी मानना था, '1857 ई. का विद्रोह केवल सैनिकों का बलवा नहीं था, अपितु यह भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रथम प्रयास था।' सावरकर की इस पुस्तक ने क्रांतिकारियों को राष्ट्र की खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी।