लेखक -वेदप्रताप वैदिक
नंदीग्राम मार्क्सवाद का बंदीग्राम बन गया है। स्तालिन और माओ ने कार्ल मार्क्स को कठघरे में वैसे कभी खड़ा नहीं किया, जैसे हमारे मार्क्सवादियों ने कर दिया है। स्तालिन और माओं ने सर्वहारा की ओर से कुलकों और सामंतों पर प्रहार किया, लेकिन हमारे मार्क्सवादियों ने सर्वहाराओं के बीच ही गृह-युध्द छिड़वा दिया है। सर्वहारा ही सर्वहारा का खून बहाए, क्या यह मार्क्सवाद की उलट-पराकाष्ठा नहीं है? नंदीग्राम में मारे गए दर्जनों लोग कौन हैं? क्या वे पूंजीपति हैं, सामंत हैं, बुर्जुग हैं, शोषक हैं? वे चाहे माकपा के लोग हों, माओवादी हों, भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के स्वयंसेवक हों, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, पुलिस वाले हों - उनमें से कोई भी शोषक वर्ग का सदस्य नहीं है। इन शोषितों का खून बहाकर हमारे मार्क्सवादियों ने आज की राजनीति में कार्ल मार्क्स को कितने माक्र्स दिलवाए हैं? आज मार्क्स को शून्य 'मार्क्स' मिल रहे हैं। महान विचारक मार्क्स की ऐसी दुर्गति करने वाले हमारे मार्क्सवादी क्या अब खुद बच जाएंगे। उन्हें कल्पना नहीं है कि उनकी कितनी दुर्गति होगी।
तीन दशक में पहली बार बंगाल से मार्क्सवादियों के उच्छेद का बिगुल बज गया है। चुनाव में जब उच्छेद होगा, तब होगा, लेकिन अभी ही ऐसी स्थिति बन गई है कि केंद्र में भाजपा-गठबंधन होता तो कोलकाता की सरकार बर्खास्त हो जाती। राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को दो-दो बार खुला हस्तक्षेप करना पड़ा, यह मामूली बात नहीं है। स्वयं मार्क्सवादी गठबंधन के घटक बगावत की मुद्रा में है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री क्षिति गोस्वामी ने इस्तीफे की पेशकश की है। भाकपा और फारवर्ड ब्लॉक के नेता भी नंदीग्राम की हिंसा की निंदा कर रहे हैं। अनेक मार्क्सवादी नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टियों के रवैए पर मौन जरूर हैं, लेकिन अत्यंत क्षुब्ध हैं। अगर बंगाल में कोई सशक्त विकल्प होता तो बंगाल के सत्तारूढ़ दलों का आज दिवाला पिट जाता, लेकिन जहां तक बंगाल की जनता का सवाल है, उसकी नजर में मार्क्सवादियों की कीमत बहुत गिर चुकी है, वरना क्या अड़तालीस घंटे का बंद वैसा सफल होता, जैसा कि अभी हुआ है?
मई 2006 के विधानसभा चुनाव में 294 में से 235 सीटें जीतने वाले बुध्ददेव भट्टाचार्य इतनी जल्दी फीकें क्यों पड़ गए हैं? वे इतने असहाय और निरूपाय क्यों दिखाई पड़ रहे है? बुरी तरह चुनाव हारने वाली तृणमूल नेता ममता बनर्जी अचानक बंगाली जनमत पर हावी क्यों होती जा रही हैं? शेर की तरह दहाड़ने वाले माकपा के केंद्रीय नेता अब मेमनों की तरह क्यों मिमिया रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ है कि परमाणु सौदे पर हमारे मार्क्सवादी शीर्षासन की मुद्रा में आ गए हैं? आखिर क्या वजह है कि उन्होंने केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से बात करने की ढील दे दी है?
इस ढील का मूल कारण वह शिकंजा है, जो नंदीग्राम ने मार्क्सवादियों के गले पर अचानक कस दिया है। यह कांग्रेस की मेहरबानी है कि वह भट्टाचार्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर रही है। अगर वह बर्खास्त कर दे और इस समय चुनाव हो जाएं तो माक्र्सवादियों को पता है कि बंगाल की जनता उन्हें नंदीग्राम में बंद कर देगी। कोलकाता छोड़कर उन्हें नंदीग्राम में बंद कर देगी। कोलकाता छोड़ कर उन्हें नंदीग्राम के बंदीग्राम में निवास करना पड़ेगा। अब तक चुनाव का डर केवल कांग्रेस को था, अब उसकी दहशत मार्क्सवादियों के दिल में भी बैठ गई है। इसीलिए अब दोनों एक-दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। दोनों जुबान जरूर चलाएंगे, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर गठबंधन का रथ भी हांकते रहेंगे। अब कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा।
इस अधार के लटकाव का ज्यादा नुकसान भाकपा को भुगतना होगा, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही गिड़गिड़ा रहीं थी, लेकिन मार्क्सवादी निरंतर गुर्राते रहे थे। अब वे बंगाल में ही नहीं, सारे भारत में मसखरों की तरह दिखाई पड़ेंगे। सत्ता का गणित शेर को कैसे भेड़ बना देता है, इस कहावत को मार्क्सवादी चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। उन्होंने बता दिया है कि उनमें उतना ही और वैसा ही क्षीण नैतिक साहस है, जैसा कि अन्य बुर्जुआ पार्टियों में है। नंदीग्राम ने मार्क्सवादी पार्टियों के नाम पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। वे अपने आपको बंगाल की क्षेत्रीय पार्टियां घोषित क्यों नहीं कर देतीं? अपने सत्ता-सुख के लिए वे मार्क्सवाद को चूना क्यों लगा रही हैं?
इस तरह के असुविधाजनक सवाल मार्क्सवादियों से कांग्रेस क्यों करेगी? कांग्रेस को कोई लाग-लपेट नहीं है। वह पूरी तरह सत्तावादी और सुविधावादी पार्टी है। नंदीग्राम उसके लिए अचानक आसमान से फरिश्ते की तरह उतरा है। वह गदगद है। वह अब तृणमूल से भी हाथ मिला लेगी। वह इसलिए भी गदगद है कि नंदीग्राम, भारत के 'सबसे बड़े भक्त' जॉर्ज बुश की मनोकामना भी पूरी करेगा। अगर परमाणु सौदे पर हमारे कॉमरेड मौन साधा लें तो क्या पता वाइट हाउस में बुश नंदी-पूजा ही शुरू करवा दें। किसे पता था कि नंदीग्राम जैसा एक स्थानीय मसला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इतना महत्वपूर्ण निणार्यक तत्व बन जाएगा।
अगर सिंगुर और नंदीग्राम के हादसे नहीं होते तो दुनिया को यह भी शायद ही पता चलता है कि हमारे छोटे मियां तो बड़े मियां से भी आगे चल रहे हैं। साम्यवाद के सबसे बड़े मियां आजकल चीन ही है। जैसे औद्योगीकरण के खातिर चीनी कॉमरेडों ने शंघाई और शेन-जेन की पुरानी बस्तियों को एक ही झटके में उखाड़ दिया, वैसे ही हमारे कॉमरेड भी भारतीय और इंडोनेशियाई पूंजीपतियों की खातिर बंगाली किसानों को अपनी जमीन से बेदखल करना चाहते थे। वे चीनियों से भी आगे निकल रहे थे, क्योंकि चीनी कॉमरेड यही काम चीनी राज्य के लिए कर रहे थे। लेकिन हमारे कॉमरेड यही काम देसी और विदेशी पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा चीन विस्थापितों के लिए समुचित वैकल्पिक सुविधा और उचित मुआवजे की व्यवस्था करता है जबकि हमारे यहां शोषितों के जीवन-मरण का यह प्रश्न अभी तक कोरी बहस का मुद्दा बना हुआ है।
माकपा की सराहना तो तब होती जब वह इस समस्या का कोई आदर्श हल सबके सामने लाती। अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करते। तब तो माना जाता कि शोषितों-पीड़ितों के लिए मार्क्सवादियों के दिल में कुछ दर्द है। अब सारी योजना को वापस लेने का क्या फायदा? उसने यही सिध्द किया कि आपने जन-आक्रोश के आगे घुटने टेक दिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि मार्क्सवादियों को यह भी ध्यान नहीं रहा कि वे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंग है। वे किसी चीनी या सोवियत व्यवस्था में सरकार नहीं चला रहे हैं।
लोकशाही और पार्टीशाही में कितना फर्क है, इस तथ्य को मार्क्सवादी अब भली-भांति समझ गए होंगे। इस तथ्य का एक आनुषंगिक निष्कर्ष यह भी है कि भारत का सौभाग्य है कि माक्र्सवादियों का राज्य केवल बंगाल और केरल जैसे प्रदेशों में ही कायम हुआ, सारे भारत में नहीं हुआ। अगर हो जाता तो क्या होता, इसकी कल्पना की जा सकती है।
मार्क्सवादियों ने अपने आचरण से कई बुनियादी सवाल भी खड़े कर दिए। जैसे, क्या राज्य और पार्टी में कोई फर्क नहीं है? क्या दोनों एक-दूसरे के पर्याय है? नंदीग्राम के मकानों और भूखंडों से माकपा कार्यकर्ताओं को बेदखल करके अगर विरोधियों ने उन पर कब्जा कर लिया था तो राजधर्म क्या कहता है? अत्याचार ग्रस्त लोगों को न्याय दिलाइए। कोई फर्क मत कीजिए। वे चाहे किसी भी पार्टी या जाति या मजहब के हों। सरकार को निष्पक्ष रह कर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया? आंख मींच ली और पार्टी काडर को इशारा कर दिया। माकपा कार्यकर्ता नंदीग्राम पर टूट पड़े। हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने हत्या की, लूटपाट मचाई, बलात्कार किया और कब्जे किए। पुलिस खड़ी-खड़ी देखती रही।
केंद्र ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस भिजवाई, लेकिन बहुत देर से। नंदीग्राम पहुंची हुई पुलिस बाहर ही खड़ी कर दी गई ताकि वह माकपा कार्यकर्ताओं के जन-युध्द में बाधा न पहुंचाए। अब ज्योति बसु और बुध्ददेव भट्टाचार्य संतुष्ट है कि नंदीग्राम में शांति लौट रही है। कैसी घृणित जुगलबंदी है, संप्रदायवाद और सेकुलरवाद में? इससे बढ़कर गैर-जिम्मेदाराना बयान कोई मुख्यमंत्री क्या दे सकता है कि नंदीग्राम के लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से मिला है। यह तो राजधर्म के पूर्ण तिरोधान की घोषणा ही है। लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि आप पहले सरकार और पार्टी को एकमेक कर दें और फिर यह मान बैठें कि पार्टी ही जनता है। बुध्ददेव भट्टाचार्य कृपया यह बताएं कि वे पूरे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ माकपा के हैं? इसमें शक नहीं कि नंदीग्राम के पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को अकर्मण्यता का नकाब पहनने के लिए मजबूर किया हो, लेकिन क्या चुनी हुई सरकार को खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आखिर वह किसके प्रति जवाबदेह है? उसका सर्वोच्च स्वामी कौन है? पार्टी कार्यकर्ता या जनता? जनता को नाराज करके नेता कहां जाएंगे? आखिर चुनाव की अग्नि परीक्षा में तो उन्हें उतरना ही पड़ेगा।
प्रदेश के कुल निवासियों के पंद्रह-बीस प्रतिशत वोट ही काफी होते हैं, चुनाव जीतने के लिए। सिर्फ वोटों की संख्या तय नहीं करती कि आप लोकतांत्रिक हैं। लोकतांत्रिक नैतिकता लोगों की संख्या से परे की चीज है। उसका निवास लोकमत में है, लोक-कल्याण में है, लोकप्रियता में है। क्या माकपा इस कसौटी पर खरी उतर रही है?
इस कसौटी पर मार्क्सवादी खोटे सिध्द हो रहे हैं। दलबंदी से अलग रहने वाली आम जनता के गुस्से की बात जाने दें, जो विद्वान, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार लोग वामपंथी या उनके सहयात्री माने जाते हैं। आज उनकी राय क्या है? महाश्वेता देवी, अपर्णा सेन, ऋतुपर्ण घोष जैसे लोग किसी दक्षिणपंथी पार्टी के स्वयंसेवक नहीं हैं। मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश और जनेवि के आचार्यगण किसी पार्टी या नेता के पिछलग्गू नहीं है। आखिर ये सब लोग खफा क्यों हैं? जनेवि के छात्र संघ के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टियों को आखिर मुंह की क्यों खानी पड़ी? सारा खबरतंत्र माकपा की खबर लेने पर उतारू क्यों है? बंगाल के बाहर रहने वाले बंगाली नंदीग्राम पर लज्जित क्यों हो रहे हैं? मार्क्सवादियों ने अपने कारनामों से मार्क्स पर ही नहीं, बंगाल के स्वर्णिम नाम पर भी बट्टा लगा दिया है। नंदीग्राम को अपने गले का पत्थर बना लिया है।
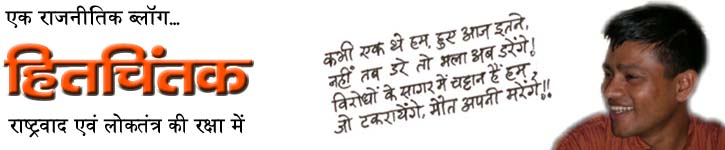
No comments:
Post a Comment