लेखक- नरेन्द्र मोहन
हिन्दुत्व एक ऐसी भू-सांस्कृतिक अवधारणा है, जिसमें सभी के लिए आदर है, स्थान है और सह-अस्तित्व का भाव भी। इस सह-अस्तित्व प्रधान सांस्कृतिक चेतना ने उसे अत्यंत उदार, सहिष्णु और लचीला भी बनाया। बात तब बिगड़ी जब विदेशी आक्रमणकारियों की संस्कृतियों ने इस अति सहिष्णु संस्कृति की उदारता का लाभ उठा कर इसकी जड़ें ही काटनी प्रारंभ कर दीं। हिन्दुत्व की इस अति-सहिष्णुता को उसकी कायरता माना गया तथा उसके जो भी मूल तत्व थे उन्हें नष्ट-भ्रष्ट करने की हर संभव चेष्टा की गई। अभी भी इस हेतु तरह-तरह के षडयंत्र रचे जा रहे हैं।
आक्रमणकारियों के समक्ष पलायन करने की नीति का सह-अस्तित्व, सहिष्णुता के दर्शन और सिध्दांत से कुछ भी लेना देना नहीं है। सह-अस्तित्व व सहिष्णुता और 'आत्मवत्' दर्शन के जो भी शत्रु हैं उनसे मोर्चा लेने, युध्द करने तथा उन्हें पराजित करने का कर्त्तव्य-कर्म तो हिन्दुत्व का आधारस्तंभ अनादि काल से रहा है और रहेगा। जब-जब आक्रमणकारी शत्रुओं से युध्द करने में हिन्दुत्व से चूक हुई तब-तब न केवल अपमान सहना पड़ा है, बल्कि पराधीनता में भी रहना पड़ा है।
आज हिन्दुत्व को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। उसे एक राजनीतिक अथवा साम्प्रदायिक अवधारणा कह कर लांछित और अपमानित किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि यह लांछन अभारतीय तो लगा ही रहे हैं, पर हम भारतवासी भी स्वयं लगा रहे हैं। स्वाधीनता के पहले हिन्दुत्व के प्रति अपमानजनक भाव रखने वालों की संख्या कम थी और केवल दुराग्रही व आक्रमणकारी संस्कृतियों के प्रति तुष्टिकरण का भाव रखने वाले ही 'हिन्दू' शब्द को साम्प्रदायिक बताते थे पर स्वाधीनता के बाद तो 'हिन्दुत्व' को गाली देना और उसका अपमान करना एक बौध्दिक फैशन बन गया और विडंबना यह है कि अपमान, लांछन व तिरस्कार के इस विष को बिना किसी प्रतिकार के 'प्रगतिवाद' के नाम पर सहन किया जा रहा है।
लगभग दो हजार वर्षों की दासता ने यही सिखाया है कि विदेशी संस्कृतियां हमारा सहयोग नहीं करना चाहतीं, वे हमें तोड़ कर तथा धवस्त करके हम पर शासन करना चाहती है। विदेशी संस्कृतियां चाहती हैं कि भारत अपनी अस्मिता भुला दे, उसे छोड़ दें, अत: हमें विदेशी प्रचार के उनके प्रलोभनों के प्रति सावधान रहना होगा।
भारत की मूर्छा धीरे-धीरे टूट रही है और यह एक शुभ लक्षण है। 'हिन्दुत्व' के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किए गए हैं उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक ने नकार दिया है। भारत के कुछ राजनीतिक दल अज्ञानवश आज भी हिन्दुत्व के प्रति शंकालु हैं। उन्हें हिन्दुत्व की ऊर्जा, उसका तप और उसका सर्वकल्याणकारी भाव ही नहीं दिखाई देता। ऐसे राजनीतिज्ञों से न तो डरने की आवश्यकता होती है और न ही चिन्तित होने की। हाल के वर्षों में वोट बैंक की राजनीति के दुष्प्रभाव में आकर हिन्दुत्व पर जितने अपमानजनक प्रहार किए गए हैं, वे चिंताजनक हैं। इन प्रहारों से भारत का आत्मविश्वास तो टूट ही रहा है, साथ ही नई पीढ़ी के भ्रमित होने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। नई पीढ़ी को भ्रमित करने में पश्चिम से आये सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का भी बहुत बड़ा हाथ है। यद्यपि पहले की तरह आज का विश्व राजनीति उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद से पीड़ित नहीं है, पर आने वाली शताब्दी में आर्थिक, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की समस्याओं से मानवता को जूझना ही होगा। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की तीन धाराएं इस समय विश्व में प्रबलता से चल रही हैं-पहली धारा ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित, पोषित और समर्थित, दूसरी, इस्लामी रूढ़िवादिता से संचालित, पोषित और समर्थित। इस्लाम के अनेक पक्षधार अत्यधिक आक्रामक व दुराग्रही हो चुके हैं। वे इतने अधिक असहिष्णुता-प्रधान हैं कि समस्त विश्व का इस्लामीकरण करने के लिए प्रतिबध्द हैं। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की तीसरी धारा 'साम्यवादी विचारधारा' अर्थात् वामपंथी विचारधारा है। यह चुनौती प्रत्यक्ष कम प्रच्छन्न अधिक है।
राष्ट्रीय अज्ञान व विभ्रम की यह स्थिति आज हर स्तर पर है और सर्वाधिक उस वर्ग में है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति से जुड़ा यह वर्ग भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्तवों से न केवल अनभिज्ञ है वरन वह भारत के सांस्कृतिक व्यक्तित्व को पश्चिमी विचारकों की ही दृष्टि से देखना चाहता है। निस्संदेह भारतीय संस्कृति के संदर्भ में सर्वाधिक विभ्रम अंग्रेज इतिहासकारों ने फैलाया है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे भारतीय जनमानस हमेशा-हमेशा के लिए अंग्रेजियत की दासता स्वीकार कर ले तथा भारत पर अंग्रेजी सत्ता का प्रभुत्व बना रह सके। भारतीय एकता और अखंडता को सबसे बड़ा खतरा उस अंग्रेजियत से है जिसका एकमात्र लक्ष्य भारतीय संस्कृति को लांछित करना और भारत को मानसिक स्तर पर विभाजित रखना रहा। यद्यपि रानाडे, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, महर्षि अरविंद, डा0 केशवराम बलिराम हेडगेवार और महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने अंग्रेजों की कुटिलता की कड़ी से कड़ी भर्त्सना की पर कुल मिलाकर भारतीय राजनीति का मन संशयग्रस्त ही रहा और रह-रह कर यह विचार ज्वार-भाटे की तरह उठता और गिरता रहा कि भारत की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है भी या नहीं। भारत की अपनी एक संस्कृति है, इसका सबसे प्रबल विरोध उस समय प्रारंभ हुआ जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गयी। उन्नीसवीं व बीसवीं शताब्दी के भारतीय राजनीतिज्ञों से सबसे बड़ी भूल यह हुई कि उन्होंने 'हिन्दू' के संदर्भ में उस परिभाषा को ग्रहण कर लिया जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। 'हिन्दू' शब्द एक भू-सांस्कृतिक अवधारणा की उपज है, यह यथार्थ पता नहीं कैसे भारत में निरन्तर उपेक्षित होता चला गया और यह मान्यता प्रगाढ़ता से भारतीय मन पर छा गई कि 'हिन्दू' एक वैसा ही मजहब है जैसे कि इस्लाम या ईसाइयत।
आश्चर्य की बात यह है कि जो भूल इस्लामी आक्रमणकारियों ने भ्रमवश की थी और जिस भूल को अपनी निहित स्वार्थों के कारण अंग्रेजों ने सैध्दांतिक व वैचारिक जामा पहना दिया उसे हम भारतीयों ने भी धीरे-धीरे बिना प्रतिरोध के स्वीकार कर लिया और परिणामत: सांस्कृतिक स्तर पर नए विभ्रम को जन्म दिया।
अंग्रेजी दासता के दौरान भारतीय संस्कृति की इतनी अधिक दुर्दशा कर दी गई कि उसकी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक शब्दावली तक को भ्रष्ट किया गया और इस शब्दावली के राजनीतिक अर्थ निकाले गए। उदाहरणस्वरूप 'धर्म' शब्द का जैसा मनमाना अर्थ अंग्रेजों ने किया उसके पीछे उनके स्वयं के निहित स्वार्थ थे। उन दिनों यह भी स्थापित करने का प्रयास किया गया कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, वह तो अंग्रेजों ने आकर इसे राजनीतिक एकता प्रदान कर दी। प्राचीन भारत की साहित्यिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों को पश्चिम का उच्छिष्ट सिध्द करने के प्रयत्न किए गए और समूचे भारतीय जीवन को आत्मगौरव शून्य एवं आत्मविस्मृत बनाने की दुरभिसंधि रची गयी। एक राष्ट्र के नाते हमारे पहचान के जितने तत्व हो सकते थे अंग्रेज उन्हें पूर्णत: नष्ट या विकृत करने का प्रयत्न करते रहे।
मजेदार मामला यह है कि जब भारत का संविधान रचा गया तब न तो भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों की ओर ही गंभीरता से निहारा गया और न भारतीय मूल्यों, आदर्शों व श्रेष्ठ परंपराओं तथा भारतीय मन की अभिलाषाओं को ही समझने का प्रयास किया गया। भारतीय संविधान को बनाया गया तो भारत की जनता के लिए, लेकिन भारत की जनता के मन में क्या है, कहां बसती है, उसकी आस्थाएं किस पर हैं, उसका विश्वास क्या रहा है, किन मूल्यों की रक्षा के लिए लगभग डेढ़ हजार वर्षों तक उसने विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष किया, यह सब जानने की चेष्टा ही नहीं की गई।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थायित्व प्रदान करने के निमित्त मैकाले ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक के सहयोग से संस्कृति पर प्रहार करने में जो सफलता प्राप्त कर ली उस आघात से भारत आज भी नहीं उबर पा रहा है। जीवन की विश्वात्म धारणा को प्रतिपादित करने वाला भारत, जिसका कभी विश्वास रहा, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' पर वह दुष्प्रचार का शिकार होकर स्वयं ही अपने मूल्य छोड़ बैठा और सांस्कृतिक रूप से बिखर गया। यह सांस्कृतिक बिखराव आज भी राजनीति में हर स्तर पर हमें दिखाई दे रहा है।
ऐसा नहीं है कि भारत की संविधान सभा में भारतीय संस्कृति एकात्म भाव तथा राष्ट्रीयता के पक्षधार नहीं थे, पर वे कुल मिला कर मौन ही रहे। जब 7 और 8 दिसम्बर, 1948 को संस्कृति से जुड़े अनुच्छेद पर संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तब केवल लोकनाथ मिश्र ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता देने का सुझाव दिया था पर उसका उग्र विरोध मुस्लिम सदस्यों द्वारा हुआ और अंतत: 'भारत एक सांस्कृतिक इकाई है तथा उसे अपनी सांस्कृतिक धारोहर की रक्षा करनी है', यह भाव इस विरोधा के कारण भारतीय संविधान का अंग न बन सका।
प्राकृतिक अनेकता में मानसिक एकता के जो सूत्र विद्यमान रहते हैं उनसे ही राष्ट्र का और उसकी संस्कृति का निर्माण होता है। इस मानसिक एकता से ही अंतत: राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी होता है और इस राष्ट्रीय चरित्र में विभिन्न मूलवंशों के लोग सहभागी और सहयोगी होते हैं। इस सामूहिक अस्मिता के अभाव में राष्ट्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। इस सामूहिक अस्मिता का जन्म भारत में कहां से हुआ? यह अस्मिता किन प्रतीकों व आदर्शों से जुड़ी है? कौन हैं इस सामूहिक अस्मिता के प्रेरणास्रोत आज इस प्रश्नों पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए और भी महत्वपूर्ण तथा तात्कालिक हो चुकी है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद उन्तीस में यह प्रतिपादित करके कि हर व्यक्ति को अपनी एक पृथक वैयक्तिक संस्कृति है-एक प्रकार से बिखराव व बिखंडन के बीज बो दिए गए हैं। सिध्दांतत: किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। हर नागरिक को अंतत: राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोच्चता प्रदान करनी होगी।
अपने राष्ट्र की संस्कृति के रहस्य को भारत के राजनीतिज्ञ इसलिए नहीं समझ सके, क्योंकि वैयक्तिक स्तर पर वे न तो अज्ञात में छलांग लगाने के लिए तैयार थे और न अपने उन राजनीतिक स्वार्थों व पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए तैयार थे जो उन्होंने यूरोपीय प्रभाव के कारण प्राप्त किए थे। स्वतंत्रता के उपरांत भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आया हो, यह नहीं कहा जा सकता। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय यदि पं. नेहरू चाहते तो भारतीय संस्कृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते थे और भारत की जो गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा है उसकी रक्षा भी कर सकते थे, पर वे स्वयं के राजनीतिक स्वार्थों और यूरोपीय प्रभाव से इतने अधिक जुड़े रहे कि अगर यह कहा जाए कि इसके दुष्प्रभाव से भटक गए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
यह बात एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिए कि भारत एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति है। अगर भारत के राजनीतिज्ञ इस सत्य का साक्षात्कार करने से इंकार करेंगे तो राष्ट्र की प्रभुसत्ता और अखंडता संकट में पड़ सकती है। संकट में इसलिए पड़ सकती है क्योंकि फिर वे समस्त तत्वहीन और श्रीहीन हो जाएंगे जिन पर इस राष्ट्र का एकत्व आश्रित होता है। राजनीति का पहला कर्त्तव्य यह है कि वह राष्ट्रीय एकत्व के प्रति समर्पित हो। यदि राजनीति राष्ट्रीय एकत्व के प्रति समर्पित नहीं है और उसे राष्ट्र की प्रभुसत्ता और अखंडता की चिंता नहीं है तब फिर ऐसी राजनीति कलह को ही जन्म देगी। भारत की सांस्कृतिक एकता का अर्थ यह नहीं है कि भारत में अनेक संस्कृतियां हैं बल्कि इसका अर्थ यह है कि इस राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति है और यह एक ऐसी संस्कृति है जो अनेकता को प्रश्रय देती है।
अंग्रेजों ने इस झूठ को सौ बार दोहराया कि मजहब के आधार पर देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बनाया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजों ने अपने देश में ऐसा नहीं किया। इंग्लैण्ड में तो ईसाइयों के अनेक पंथ है, लेकिन विभिन्न पंथों को मानने वाले अंग्रजों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच विभाजित नहीं किया गया। सच बात तो यह है कि राष्ट्रीयता का संबंध उपासना पध्दति की विभिन्नता से नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीयता उपासना पध्दति से कहीं अधिक विशाल, उदात्त और श्रेष्ठ है। हिन्दुत्व पंथ नहीं है, मजहब नहीं है, वह पंथ या मजहब हो ही नहीं सकता। मजहब या पंथ के उसमें कोई गुण ही नहीं हैं। जिसमें अनंत जीवन दर्शन, अनंत पंथ, अनंत जीवन-शैलियां, अनंत उपासना-पध्दतियां समाहित हो, उसे कोई किसी एक परिभाषा से कैसे बांधोगा? हिन्दुत्व का सारा प्रयास सामंजस्य एवं एकरसता प्राप्त करना है, सभी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी की समृध्दि हो, सभी में मित्रता हो, सभी एक दूसरे के सहयोगी बनें, कोई किसी से द्वेष न करे। ये सारे प्रयास हमें वर्तमान में ही करने होंगे।
हिन्दुत्व वर्तमान में
सत्य का साक्षात्कार ही हिन्दुत्व का प्राणतत्व है और यह साक्षात्कार हमें वर्तमान में करना होता है। अतीत के गुण गाकर हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अतीत में क्या था, यह तो इतिहास की बात हो गई, पर क्या होना चाहते हैं, किनकी नकल करना चाहते हैं यह हुई कल्पना की बात। कोई भी समाज इतिहास के कल्पना लोक में जीकर विश्व को नेतृत्व नहीं दे सकता और भविष्य की कोरी कल्पनाओं के आधार पर भी किसी भी समाज ने उन्नति नहीं की है। हिन्दुत्व का आधार है 'चरैवेति'। हिन्दुत्व में ठहराव नहीं है। यह ठीक है कि किन्हीं कारणों से हिन्दुत्व नीचे गहरी खाई में जा गिरा है और यह संभवत: इसलिए हुआ होगा क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन अब यह कालचक्र उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। उचित यह होगा कि भारतीय समाज यह समीक्षा करें कि उसके उत्कर्ष में क्या सहायक है और क्या अवरोधक?
हिन्दुत्व किन्हीं कारणों से जो भटकावग्रस्त हुआ है, उससे समाज में कलह बढ़ी है, विघटन बढ़ा है, विद्वेष बढ़ा है और दुष्कर्म बढ़ा है तथा उत्कर्ष के स्थान पर पतन हुआ है। हिन्दुत्व का सनातन प्रवाह, जो हमारी राष्ट्रीय चेतना की मुख्यधारा है, उसे शक्तिवान बनाने के स्थान पर यदि कोई उसे प्रदूषित कर रहा है अथवा किसी कारणवश वह प्रवाह प्रदूषणग्रस्त होता चला जा रहा है, तो हमें प्रदूषण की इस सत्यता को स्वीकार करना ही होगा। कपोतवृति अपनाकर हम यथार्थ की उपेक्षा तो कर सकते हैं पर यथार्थ के सत्य को नष्ट नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज ने जिसे आज 'हिन्दू समाज' कहकर संबोधिात किया जाता है उसने समय-समय पर स्वयं की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए संघर्ष नहीं किया। समाज सुधारकों का भी जन्म हुआ, पर जो भी आज तक हुआ है, वह बहुत ही आधार अधूरा है। न तो हमने अंधाविश्वास पर पूर्णत: विजय पाकर बुध्दि व विवेक की सत्ता पुन: स्थापित की है और न पाखंड का ही पूर्ण परित्याग कर अपनी कथनी-करनी के भेद को ही मिटाया है। जाति-प्रथा व वर्ण व्यवस्था में आज सर्वाधिक सहारा मनुस्मृति का लिया जाता है और यह जाने समझे बिना कि मनुस्मृति के नाम जो ग्रंथ बाजारों में बिकता है, वास्तव में क्या है। यह निर्विवादित रूप से सिध्द हो चुका है कि आज जिस ग्रंथ को 'मनुस्मृति' के रूप में जाना जाता है, वह किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, इस ग्रंथ को एक कालखंड में भी नहीं लिखा गया और समय-समय पर स्वयं के स्वार्थों की रक्षा के लिए इसमें ऐसे विचारों को भी जोड़ दिया गया जो परस्पर विरोधी है। क्या यह स्वयं में एक क्रूर व्यंग्य नहीं है कि जिस 'मनुस्मृति' का आधार लेकर आज जन्म आधारित जाति व वर्णव्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है, उसी व्यवस्था का विधान है कि कर्म के बदलते ही वर्ण भी बदल जाता है।
हिन्दुत्व की इस दुर्बलता को कैसे सुधारा जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अब यदि भारत का पूरा का पूरा मन नहीं बदलता तो उसके जीवन-दर्शन में जो भारी गिरावट आ गई है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। पर राष्ट्र एवं समाज का मन बदलने के लिए जैसे प्रयास होने चाहिए, उस ओर ध्यान देने की चेष्टा नहीं की जा रही है। भारतीय जीवन दर्शन के मन में जो दुर्बलताएं आ गयी हैं उन्हें दूर करने का काम समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर करना होगा। केवल कानून बना देने से भारतीय समाज स्वयं को पतन के गर्त से बाहर नहीं निकाल सकेगा।
(लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक थे)
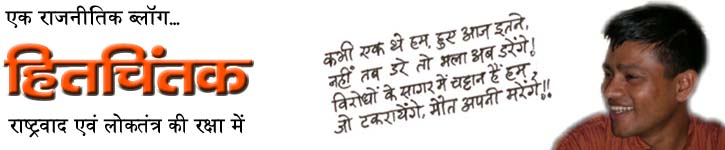
No comments:
Post a Comment