लेखक- पं0 दीनदयाल उपाध्याय
भारत में एक ही संस्कृति रह सकती है; एक से अधिक संस्कृतियों का नारा देश के टुकड़े-टुकड़े कर हमारे जीवन का विनाश कर देगा।
मनुष्य अनेक जन्मजात प्रवृत्तियों के समान, देशभक्ति की भावना भी स्वभाव से ही प्राप्त करता है। केवल परिस्थितियों एवं वातावरण के दवाब से किसी व्यक्ति में ये प्रवृत्ति सुप्त होकर विलीनप्राय हो जाती है। इस प्रकार विकसित देश-प्रेम के व्यक्ति, अपनी कार्य-कलापों की प्रेरणा अस्पष्ट एवं क्षीण भावना से नहीं वरन् अपने स्वप्नों के अनुसार अपने देश का निर्माण करने की प्रबल ध्येयवादिता से पाते हैं। भारत में भी प्रत्येक देशभक्त के सम्मुख इस प्रकार का ध्येय-पथ है तथा वह समझता है कि अपने पथ पर चलकर ही वह देश को समुन्नत बना सकेगा। यह धयेय-पथ यदि एक ही होता तथा सब देश-भक्तों के लिये आदर्श भारत का स्वरूप भी एक ही होता तब तो किसी भी प्रकार के विवाद या संघर्ष का प्रश्न नहीं था, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि आज भिन्न-भिन्न मार्गों से लोग देश को आगे ले जाना चाहते हैं तथा प्रत्येक का विश्वास है कि उसी का मार्ग सही मार्ग है। अत: हमको इन मार्गों का विश्लेषण करना होगा और तब ही हम प्रत्येक की वास्तविकता को भी समझ सकेंगे।
चार प्रमुख मार्ग
इन मार्गों को देखते हुए हमें चार प्रधान वर्ग दिखाई देते हैं, अर्थवादी, राजनीतिवादी, मतवादी तथा संस्कृतिवादी।
अर्थवादी
प्रथम वर्ग अर्थवादी, सम्पत्ति को ही सर्वस्व समझता है तथा उसके स्वामित्व एवं वितरण दोषों को सब प्रकार की दुर्व्यवस्था को जड़ मान कर उसमें सुधार करना ही अपना एकमेव कर्तव्य समझता है। उसका एकमेव लक्ष्य 'अर्थ' है। साम्यवादी एवं समाजवादी इसी वर्ग के लोग हैं। इनके अनुसार भारत की राजनीति का निधार्रण अर्थ-नीति के आधार पर होना चाहिये तथा संस्कृति एवं मत (Religion) को वे गौण समझकर अधिक महत्व देने को तैयार नहीं हैं।
राजनीतिवादी
राजनीतिवादी दूसरा वर्ग है। यह जीवन का सम्पूर्ण महत्व राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने में ही समझता है तथा राजनीतिक दृष्टि से ही संस्कृति, मज़हब तथा अर्थनीति की व्याख्या करता है। अर्थवादी यदि एकदम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अथवा बिना मुआविजा दिये जमींदारी-उन्मूलन चाहता है तो राजनीतिवादी अपने राजनीतिक कारणों से ऐसा करने में असमर्थ है। इस प्रकार उसके लिए संस्कृति एवं मज़हब का भी मूल्य अपनी राजनीति के लिए ही है, अन्यथा नहीं। इस वर्ग के अधिकांश लोग कांग्रेस में हैं जो आज भारत की राजनीतिक बागडोर संभाले हुए है।
मतवादी
तीसरा वर्ग मज़हब-परस्त या मतवादी है। इसे धर्मनिष्ठ कहना ठीक न होगा; क्योंकि धर्म; मज़हब या मत से बड़ा तथा विशाल है। यह वर्ग अपने-अपनी मज़हब के सिध्दान्तों के अनुसार ही देश की राजनीति अथवा अर्थनीति को चलाना चाहता है। इस प्रकार का वर्ग मुल्ला-मौलवियों तथा रूढ़िवादी कट्टरपंथियों के रूप में अब भी विद्यमान है, यद्यपि आजकल उसका बहुत प्रभाव नहीं रह गया है।
संस्कृतिवादी
चौथा वर्ग संस्कृतिवादी है। इसका विश्वास है कि भारत की आत्मा का स्वरूप प्रमुखतया संस्कृति ही है। अत: अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास ही हमारा कर्तव्य होना चाहिये। यदि हमारा सांस्कृतिक ह्रास हो गया तथा हमने पश्चिम के अर्थ-प्रधान अथवा भोग-प्रधान जीवन को अपना लिया तो हम निश्चित ही समाप्त हो जायेंगे। यह वर्ग भारत में बहुत बड़ा है। इसके लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तथा कुछ अंशों में कांग्रेस में भी हैं। कांग्रेस के ऐसे लोग राजनीति को केवल संस्कृति का पोषक मात्र ही मानते हैं, संस्कृति का निर्णायक नहीं। हिन्दीवादी सब लोग इसी वर्ग के हैं।
मार्गों की प्राचीनता
उपर्युक्त चार वर्गों की विवेचना में यद्यपि हमने आधुनिक शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु प्राचीन काल में भी ये चार प्रवृत्तियां उपस्थित थीं तथा इनमें एक एक प्रवृत्ति को ही अपनाकर हमने अपने जीवन के आदर्श का मानदण्ड बनाया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही चार प्रवृत्तियां हैं। धर्म संस्कृति का, अर्थ नैतिक वैभव का, काम राजनैतिक आकांक्षाओं का तथा मोक्ष पारलौकिक उन्नति का द्योतक था। इनमें से हमने धार्म को ही अपनी जीवन का आधार बनाया है, क्योंकि उसके द्वारा ही हमने शेष सबको सधाते हुए देखा है। इसीलिये जब महाभारत काल में धार्म की अवहेलना होनी प्रारम्भ हुई, तब महर्षि व्यास ने कहा :-
''उधर्वबाहुर्विरोम्पयेष न च कश्चिच्छृणेति मे।
धर्मादर्थश्य कामख्य स धर्म: किं न सेव्येत॥''
अर्थ और काम की ही नहीं, मोक्ष की भी प्राप्ति धार्म से होती है; इसलिये धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि ''यतोऽभ्युदय नि:श्रेयस् सिध्दि: स धर्म:।'' जिससे ऐहिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त हो वही धर्म है। यह धर्म निश्चित ही अंग्रेजी का रिलीजन नहीं है। रिलीजन के लिये तो हमने मत शब्द का प्रयोग किया है, जो प्रत्येक के लिये भिन्न होता था तथा मोक्ष-निर्वाण अथवा परमानन्द-प्राप्ति का साधान होता था, जबकि धर्म के द्वारा सम्पूर्ण समाज की धारणा तथा उसके अंगों का पालन होता था। इसलिये धर्म की भी व्याख्या की गई है :-
''धारणाध्दर्मभित्याहु धर्मो धारयते प्रजा:।''
धर्मप्रधान भारतीय जीवन
भारतीय जीवन को धर्म-प्रधान बनाने का प्रमुख कारण यह था कि इसी में जीवन का विकास सबसे अधिक निश्चित है। आर्थिक दृष्टिकोण वाले लोग यद्यपि आर्थिक समानता के पक्षपाती हैं, किन्तु वे व्यक्ति की राजनीतिक एवं आत्मिक सत्ता को पूर्णत: समाप्त कर देते हैं। राजनीतिवादी प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार देकर उसके राजनैतिक व्यक्तित्व की रक्षा तो अवश्य करते हैं किन्तु आर्थिक एवं आत्मिक दृष्टि से वे भी अधिक विचार नहीं करते। अर्थवादी यदि जीवन को भोग-प्रधान बनाते हैं तो राजनीतिवादी उसको अधिकार-प्रधान बना देते हैं। मतवादी बहुत कुछ अव्यावहारिक, गतिहीन एवं संकुचित हो जाते हैं। किसी-किसी व्यक्ति विशेष अथवा पुस्तक विशेष के विचारों के वे इतने गुलाम हो जाते हैं कि समय के साथ वे अपने आपको नहीं रख पाते तथा इस प्रकार पूर्णत: नष्ट हो जाते हैं। इन सबके विपरीत संस्कृति-प्रधान जीवन की यह विशेषता है कि इसमें जीवन के केवल मौलिक तत्तवों पर तो जोर दिया जाता है पर शेष बाह्य बातों के संबंधा में प्रत्येक को स्वतंत्रता रहती है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता है। संस्कृति किसी काल विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के बन्धन से जकड़ी हुई नहीं है, अपितु यह तो स्वतंत्र एवं विकासशील जीवन की मौलिक प्रवृत्ति है। इस संस्कृति को ही हमने धर्म कहा है। अत: जब कहा जाता है कि भारतवर्ष धर्म-प्रधान देश है तो इसका अर्थ मज़हब, मत या रिलीजन नहीं, किन्तु यह संस्कृति ही होता है।
भारत की विश्व को देन
हमने देखा है कि भारत की आत्मा को समझना है तो उसे राजनीति अथवा अर्थ-नीति के चश्मे से न देखकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही देखना होगा। भारतीयता की अभिव्यक्ति राजनीति के द्वारा न होकर उसकी संस्कृति के द्वारा ही होगी। विश्व को भी यदि हम कुछ सिखा सकते हैं तो उसे अपनी सांस्कृतिक सहिष्णुता एवं कर्त्तव्य-प्रधान जीवन की भावना की ही शिक्षा दे सकते हैं, राजनीति अथवा अर्थनीति की नहीं। उसमें तो शायद हमको उनसे ही उल्टे कुछ सीखना पड़े। अर्थ, काम और मोक्ष के विपरीत धर्म की प्रमुख भावना ने भोग के स्थान पर त्याग, अधिकार के स्थान पर कर्त्तव्य तथा संकुचित असहिष्णुता के स्थान पर विशाल एकात्मता प्रकट की है। इनके साथ ही हम विश्व में गौरव के साथ खड़े हो सकते हैं।
संघर्ष का आधार
भारतीय जीवन का प्रमुख तत्व उसकी संस्कृति अथवा धर्म होने के कारण उसके इतिहास में भी जो संघर्ष हुये हैं, वे अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए ही हुए हैं। तथा इसी के द्वारा हमने विश्व में ख्याति भी प्राप्त की है। हमने बड़े-बड़े साम्राज्यों के निर्माण को महत्व न देकर अपने सांस्कृतिक जीवन को पराभूत नहीं होने दिया। यदि हम अपने मध्ययुग का इतिहास देखें तो हमारा वास्तविक युध्द अपनी संस्कृति के रक्षार्थ ही हुआ है। उसका राजनीतिक स्वरूप यदि कभी प्रकट भी हुआ तो उस संस्कृति की रक्षा के निमित्त ही।
राणा प्रताप तथा राजपूतों का युध्द केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था किन्तु धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही था। छत्रपति शिवाजी ने अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना गौ-ब्राह्मण प्रतिपालन के लिए ही की। सिक्ख-गुरुओं ने समस्त युध्द-कर्म धर्म की रक्षा के लिए ही किए। इन सबका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि राजनीति का कोई महत्व नहीं था और राजनीतिक गुलामी हमने सहर्ष स्वीकार कर ली; किन्तु तात्पर्य यह है कि राजनीति को हमने जीवन में केवल सुख का कारण-मात्र माना है, जब कि संस्कृति जीवन ही है।
संस्कृतियों का संघर्ष
आज भी भारत में प्रमुख समस्या सांस्कृतिक ही है वह भी आज दो प्रकार से उपस्थित है, प्रथम तो संस्कृति को ही भारतीय जीवन का प्रथम तत्त्व मानना तथा दूसरा इसे मान लेने पर उस संस्कृति का रूप कौन सा हो? विचार के लिए यद्यपि यह समस्या दो प्रकार की मालूम होती है, किन्तु वास्तव में है एक ही। क्योंकि एक बार संस्कृति को जीवन का प्रमुख एवं आवश्यक तत्त्व मान लेने पर उसके स्वरूप के सम्बन्धा में झगड़ा नहीं रहता, न उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का मतभेद ही उत्पन्न होता है। यह मतभेद तो तब उत्पन्न होता है जब अन्य तत्वों को प्रधानता देकर संस्कृति को उसके अनुरूप उन ढांचों में ढंकने का प्रयत्न किया जाता है।
इस दृष्टि से देखें तो आज भारत में एक-संस्कृतिवाद, द्वि-संस्कृतिवाद तथा बहु-संस्कृतिवाद के नाम से तीन वर्ग दिखाई देते हैं। एक-संस्कृतिवाद के पुरस्कर्ता भारत में विकसित एक ही भारतीय संस्कृति का अस्तित्तव मानते हैं तथा अन्य संस्कृतियों के लिए, जो विदेशों से भारत में आयी हैं, आवश्यक समझते हैं कि वह भारतीय संस्कृति में विलीन हो जाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी एक-संस्कृतिवाद के पोषक तथा कांग्रेस में श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जैसे व्यक्ति इसी वाद के पोषक रहे हैं।
द्वि-संस्कृतिवादी
द्वि-संस्कृतिवादी दो प्रकार के हैं। एक तो स्पष्ट तथा दूसरे प्रच्छन्न। एक वर्ग भारत में स्पष्टतया दो संस्कृतियों का अस्तित्तव मानता है तथा उनको बनाये रखने की मांग करता है। मुस्लिम लीगी इसी मत के हैं। वे हिन्दू और मुस्लिम दो संस्कृतियों को मानते हैं तथा उनका आग्रह है कि मुसलमान अपनी संस्कृति की रक्षा अवश्य करेगा। दो संस्कृतियों के आधार पर ही उन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्वान्त सामने रखा, जिसके परिणाम को हम पिछले वर्षों में भली-भांति अनुभव कर चुके हैं। प्रच्छन्न द्वि-संस्कृतिवादी वे लोग हैं जो स्पष्टतया तो दो संस्कृतियों का अस्तित्व नहीं मानते, मूल से एक संस्कृति एवं एक राष्ट्र का ही राग अलापते हैं, किन्तु व्यवहार में दो संस्कृतियों को मानकर उनका समन्वय करने का असफल प्रयत्न करते हैं। वे यह तो मान लेते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो संस्कृतियां हैं, किन्तु उनको मिलाकर एक नवीन हिन्दुस्तानी संस्कृति बनाना चाहते हैं। अत: हिन्दी-उर्दू का प्रश्न वे हिन्दुतानी बनाकर हल करना चाहते हैं तथा अकबर को राष्ट्र-पुरुष मानकर अपने राष्ट्र के महापुरुषों के प्रश्न को हल करना चाहते हैं। 'नमस्ते' और 'सलामालेकुल' का काम ये 'आदाब-अर्ज' से चला लेना चाहते हैं। यह वर्ग कांग्रेस में बहुमत में है। दो संस्कृतियों के मिलाने के अब तक असफल प्रयत्न हुए हैं किन्तु परिणाम विघातक ही रहा है। मुख्य कारण यह है कि जिसको मुस्लिम संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है वह किसी मजहब की संस्कृति न होकर अनेक अभारतीय संस्कृतियों का समुच्चय मात्र है। फलत: उसमें विदेशीपन है, जिसका मेल भारतीयत्व से बैठना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है। इसलिए यदि भारत में एक संस्कृति एवं एक राष्ट्र को मानना है तो वह भारतीय संस्कृति एवं भारतीय हिन्दू राष्ट्र, जिसके अन्तर्गत मुसलमान भी आ जाते हैं, के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता।
बहु-संस्कृतिवादी
बहु-संस्कृतिवादी वे लोग हैं जो प्रान्त को निजी संस्कृति मानते हैं तथा उस प्रान्त को उस आधार पर आत्म-निर्णय का अधिकार देकर बहुत कुछ अंशों में स्वतंत्र ही मान लेते हैं। साम्यवादी एवं भाषानुसार प्रान्तवादी लोग इस वर्ग के हैं। वे भारत में सभी प्रान्तों में भारतीय संस्कृति की अखण्ड धारा का दर्शन नहीं कर पाते।
संस्कृति से भिन्न जीवन का आधार
उपरोक्त तीनों प्रकार के वर्गों का प्रमुख कारण यह है कि उनके सम्मुख संस्कृति-प्रधान जीवन न होकर मज़हब, राजनीति अथवा अर्थनीति-प्रधान जीवन ही है। मुस्लिम लीग ने अपनी अमूर्त तत्तव का आधार मुस्लिम मज़हब समझकर ही भिन्न मुस्लिम संस्कृति एवं राष्ट्र का नारा लगाया तथा उसके आधार पर ही अपनी सब नीति निधार्रित कीं। कांग्रेस का जीवन एवं लक्ष्य राजनीति-प्रधान होने के कारण उसने अंग्रेजों को मुकाबला करने के लिए तथा शासन चलाने के लिए सब वर्गों को मिलाकर खड़ा करने का विचार किया, जिसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से यह भी द्वि-संस्कृतिवाद का शिकार बन गई। बहु-संस्कृतिवादी जीवन को अर्थ-प्रधान मानते हैं, अत: वे आर्थिक एकता की चिन्ता करते हुए सांस्कृतिक एकता की ओर से उदासीन रह सकते हैं।
एक राष्ट्र और एक संस्कृति
केवल एक-संस्कृतिवादी लोग ही ऐसे हैं जिनके समक्ष और कोई ध्येय नहीं है तथा जैसा कि हमने देखा, संस्कृति ही भारत की आत्मा होने के कारण वे भारतीयता की रक्षा एवं विकास कर सकते हैं। शेष सब तो पश्चिम का अनुकरण करके या तो पूंजीवाद अथवा रूस की तरह आर्थिक प्रजातन्त्र तथा राजनैतिक पूंजीवाद का निर्माण करना चाहते हैं। अत: उनमें सब प्रकार की सद्भावना होते हुए भी इस बात की सम्भावना कम नहीं है कि उसके द्वारा भी भारतीय आत्मा का तथा भारतीयत्व का विनाश हो जाय। अत: आज की प्रमुख आवश्यकता तो यह है कि एक-संस्कृतिवादियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाय। तभी हम गौरव और वैभव से खड़े हो सकेंगे तथा राष्ट्र-विघटन जैसी भावी दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे।
(भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रह चुके दीनदयाल जी मौलिक चिंतक थे)
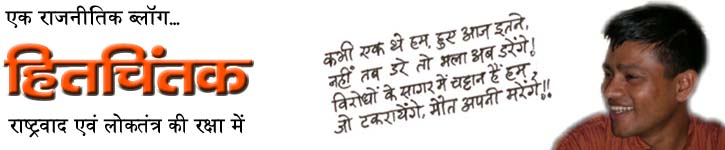
1 comment:
चलिए आपको स्व. दीनदयाल जी की याद तो आई . उनकी विचारधारा को तो भाजपा कब की भूल गयी है . एकात्म मानववाद , अन्तोदय आदि को तो आप लोग उस अलमारी मे बंद कर वह जगह भी भूल गए है जहाँ वह अलमारी रखी गई है .
स्व. दीनदयाल जैसे महत्मा का आपने वाही किया जो कांग्रेस ने गांधीजी का किया . इतने दिन सत्ता मे रहकर भी पंडित जी की हत्या की गुत्थी भी नहीं सुलझवा पाए .
Post a Comment