लेखक- शंकर शरण
अभी किसी संगोष्ठी में एक जाने-माने हिंदी मार्क्सवादी ने कहा कि दुनिया में हर जगह सबसे बड़े राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट ही हुए हैं। यह भी कि हर राजनीतिक प्रणाली तानाशाही होती है अत: कम्युनिस्ट शासनों को अलग से तानाशाही कहना ठीक नहीं। उनके अनुसार मार्क्सवाद का लक्ष्य वही था जो पहले भारतीय शास्त्रों में सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया:... के रूप में कहा गया। उन्होंने दस मिनट के अंदर ऐसी अनेक बेजोड़ बातें कहीं। इससे पता चलता है कि आखिर हिंदी वाले मार्क्सवादी कैसे बिना किसी शंका-शर्म के मार्क्सवाद का बिल्ला आज भी लहराते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता भयंकर अंधविश्वास और घोर अज्ञान में डूबी है। वे मार्क्सीय विचार का म नहीं जानते, मगर प्रतिष्टिंत मार्क्सवादी हैं! इनके ही भरोसे हिंदी के विद्यार्थी मार्क्सवादी या उसके हमदर्द बनते रहे। इस तरह यह अज्ञानी संप्रदाय हिंदी समाज को डुबा रहा है।
-- यह बड़ी मोटी सी बात है कि इस्लाम की तरह मार्क्सीय विचार में भी अंतर्राष्ट्रीयतावाद एक मूल सिध्दांत है। इसमें भी राष्ट्रवाद को सदैव एक दोष या भटकाव माना गया। इसीलिए कम्युनिस्टों की आपसी बहस में राष्ट्रवादी कहलाना गाली जैसा रहा है। कार्ल मार्क्स के शब्दों में, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। जब देश ही नहीं, तो देशभक्ति कैसी। लेनिन ने द्वितीय इंटरनेशनल को खारिज कर 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इसीलिए बनाया था क्योंकि उनके ख्याल में यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियां राष्ट्रवादी हो गई थीं। पश्चिमी में अपने देश के खिलाफ सोवियत संघ के लिए जासूसी करने वाले अधिकांश लोग संबंधित देशों के कम्युनिस्ट ही थे। भारत में भी, कम्युनिस्टों ने 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन से द्रोह एवं अंग्रेजों से सहयोग सोवियत संघ को मदद पहुँचाने की चाह से किया। फिर 1943 में (मुस्लिम आत्मनिर्णय का अधिकार कह कर) भारत के विभाजन का मौलिक सिध्दांत कम्युनिस्ट पार्टी ने ही दिया था। उसके लिए गढ़ी गई विस्तृत अधिकारी थीसिस क्या राष्ट्रवाद का दस्तावेज था। उस एक थीसिस ने भारत को जितना तबाह किया, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं, किंतु हिंदी मार्क्सवादी इस घोर-सांप्रदायिक अतीत के बावजूद धर्म-निरपेक्ष हैं! भारतीय कम्युनिस्टों के लिए 1942 और 1943 कोई पहला या अंतिम राष्ट्र-विरोधी कारनामा नहीं था। उससे पहले भी उनकी नीतियाँ कोमिंटर्न या स्तालिन के कहने पर तय होती थीं।
-- राष्ट्रीय नेताओं या कांग्रेस का चरित्र हमारे कम्युनिस्ट अपनी अक्ल से नहीं, अपने रूसी या ब्रिटिश कामरेडों की बुध्दि से तय करते रहे। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही कम्युनिस्ट भी काम करते थे। उससे वे निकाले क्यों गए। इसलिए कि कोमिंटर्न की लाइन के अनुरूप वे छल से कांग्रेस का नेतृत्व हड़पने के लिए उद्योग कर रहे थे, न कि राष्ट्रीय आंदोलन को मदद देने के लिए। इसी तरह 1962 में चीनी आक्रमण का बचाव करने के लिए ही कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुई। जो लोग अलग होकर माकपा (सीपीएम) बने, उन्होंने कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयता के नशे में नेहरू सरकार को ही दोषी बताया। यह न मानने के कारण ही भाकपा (सीपीआई) को राष्ट्रवादी भटकाव की शिकार दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी कहकर दो दशक तक निंदित किया गया। वस्तुत: पूरे एशिया में कम्युनिस्ट आंदोलन का ग्राफ दिखाता है कि राष्ट्रवादी भावनाओं से दूर होने के कारण ही वह लोगों की सहानुभूति खोता गया। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपने देश के राष्ट्रवादियों के साथ केवल एक छोटी अवधि तक ही रहीं। वह भी कोमिंटर्न के इशारे पर ही। इसी दौर में उन्हें कुछ लोकप्रियता भी मिली। लेकिन चूँकि राष्ट्रवाद उनकी निष्ठा नहीं थी, इसलिए जैसे-जैसे यह साफ होता गया, लोग उनसे दूर होते गए।
-- कम्युनिस्टों को देश से कभी मतलब न था, उन्हें हर हाल में केवल विश्व में साम्यवादी सत्ता के लिए जोड़-तोड़ षडयंत्र करना था। इसीलिए वे देश की चिंता से कभी एकाकार नहीं हुए। अंतर्राष्ट्रीयतावादी फिक्र में उनका मुख्य शत्रु अमेरिका और एकमात्र पितृभूमि सोवियत संघ या लाल चीन था। अपना देश उनकी गिनती में हमेशा बाद में आता था। सोवियत संघ के समीकरणों से उनकी नीतियाँ बनती थीं, न कि अपने देश-हित के लिए। जब बार-बार अनुभव से जनता ने यह समझ लिया, तब से लोकतांत्रिक देशों में कम्युनिस्टों की स्थिति एक सीमित संप्रदाय की हो गई। जिस पर देश-हित के लिए कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। केवल भारतीय कम्युनिस्टों ने मुस्लिम आत्मनिर्णय के नाम पर देश को नहीं तोड़ा। जर्मनी, कोरिया और यमन में भी उन्होंने अपने-अपने देशों का विखंडन किया। स्पष्टंत: उनके लिए वर्ग-संघर्ष के समक्ष राष्ट्रीय एकता, अखंडता या सहमति का कोई अर्थ न था। मगर सैध्दांतिक, व्यावहारिक तथ्यों, अनुभवों से अनजान हिंदी का मार्क्सवादी कम्युनिस्टों को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मान उनका भक्त बना हुआ है! उसके लिए सबका कल्याण ही मार्क्सवाद है। उसके लिए निजी संपत्ति का खात्मा, पूँजीपति वर्ग का विनाश, वर्ग-युध्द, क्रांतिकारी हिंसा आदि संकल्पनाओं का अस्तित्व नहीं। कितनी हैरत की बात है कि जो सिध्दांत डंके की चोट पर मानवता के एक हिस्से को खूँरेजी से मिटाने की बात करता है उसे कोई सबका कल्याण चाहने वाला बताए! 1989 में पूर्वी यूरोप में जनता ने तमाम कम्युनिस्ट तानाशाहियों को रातो-रात गद्दी से खींच उतारा। उनसे लोगों को कितनी घृणा थी, इसके रोचक दृश्य सारी दुनिया ने टेलीविजन पर देखे, मगर हिंदी मार्क्सवादी के लिए सभी शासन तानाशाही हैं।
-- हिंदी मार्क्सवादी के लिए सभा-संगठन की आजादी, मुक्त प्रेस, स्वतंत्र न्यायालय, वयस्क मताधिकार आदि के होने या न होने में कोई अंतर नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में मार्क्सवादी मंडली हर कहीं, हर विषय पर अनर्गल प्रवचन देती दिखती है। उसे किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं। बस उसके बारे में कुछ-न-कुछ मान लेने की जरूरत है। कुछ न जानकर भी सर्व-ज्ञानी होने का अंदाज- ऐसा विचित्र दृश्य हिंदी मार्क्सवादी जगत के सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने अपनी सदिच्छाओं को मार्क्सवादी पर आरोपित कर उसे बाजार में चलाया, लेकिन जैसा कि निर्मल वर्मा ने कहीं लिखा है कि जिन्होंने मार्क्स, लेनिन आदि के लेखन को सचमुच पढ़ने-समझने का कष्टं किया, वे निश्चित रूप से मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन से दूर होते गए। हिंदी बौध्दिकता में आज भी मार्क्सवाद की प्रतिष्ठा का रहस्य इसी टिप्पणी में छिपा हुआ है।
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।
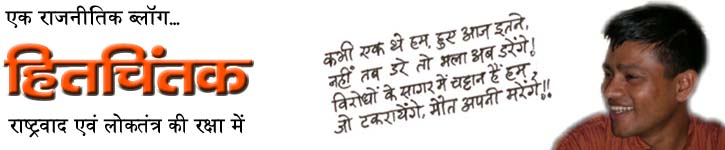
No comments:
Post a Comment