
लेखक : बनवारी
गत 12 जुलाई को जनसत्ता में सुप्रसिद्ध स्तंभकार श्री बनवारी का वर्तमान भारतीय राजनीति में मार्क्सवादियों की भूमिका पर केद्रिंत लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख की व्यापक चर्चा हुई है। मार्क्सवादियों की मनोदशा को समझने में यह लेख सहायक होगा, इसी मकसद से हम इसे यहां भी प्रकाशित कर रहे है-
हरकिशन सिंह सुरजीत ने अपने राजनीतिक कौशल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में पहुंचा दिया था। प्रकाश कारत ने उसे फिर किनारे बैठा दिया है। करात को उम्मीद थी कि वे भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौते को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को गिरा देंगे। इस मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा। कांग्रेस अलग-थलग पड़ जाएगी, इससे जो राजनीतिक संकट पैदा होगा उसमें मार्क्सवादियों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा।
दुनिया भर के साम्यवादियों का एक घोषित उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवाद को शिकस्त देना है। भले ही चीन और रूस के साम्यवादी नेताओं तक ने बदलती परिस्थितियों में उसी अमेरिकी साम्राज्यवाद से सहयोग करना लाभदायक समझा हो। भारतीय मार्क्सवादी दिखा देंगे कि वे अपनी सीमित शक्ति के बावजूद अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं और भारत को अमेरिका का सहयोगी बनने से रोक सकते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी बिरादरी में उनका यश बढ़ेगा। इस तरह से वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी कीर्ति फैला सकेंगे। इस कीर्ति से उन्हें अपने साम्यवादी आंदोलन के लिए नए सिपाही मिलेंगे। उनके बल पर अगले चुनाव में वे और बड़ी शक्ति होंगे, उनकी और बड़ी भूमिका होगी और देर-सबेर सत्ता उनकी पकड़ में आ जाएगी।
लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां किसी किताबी सिध्दांत के चश्मे से जितनी सरल दिखाई देती हैं, वास्तव में उतनी सरल होती नहीं हैं। इसलिए कुछ दिन पहले तक जो कांग्रेस सरकार वामपंथियों की बैसाखी पर अनिवार्य रूप से टिकी दिखाई देती थी, उसने अपने टिके रहने के और सहारे ढूढ़ लिए। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री न बनने देने से मुलायम सिंह यादव के प्रति पैदा हुई अपनी चिढ़ छोड़ दी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने और परमाणु समझौते का समर्थन करने का रास्ता बना।
भाजपा खेमे की कई पार्टियों तक को भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौते में राष्ट्रीय सुरक्षा दिखाई दी और मनमोहन सिंह सरकार का बने रहना सुनिश्चित हो गया। कांग्रेस, जिसे मार्क्सवादी इस मुद्दे पर देश की राजनीति में अलग-थलग कर देना चाहते थे, मुख्यधारा में बनी रही, मार्क्सवादी खुद अलग-थलग पड़ गए। जो संकट वे कांग्रेस के लिए पैदा करना चाहते थे, वह अब उन्हीं के गले में पड़ गया है।
मार्क्सवादी अपने संसदीय शक्ति के सबसे बड़े स्रोत पश्चिम बंगाल में मुश्किल में हैं। बिगड़ती हुई आर्थिक परिस्थितियों का जो गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ फूटना चाहिए था वह पश्चिम बंगाल में उन्हीं के खिलाफ फूट रहा है। पिछले इकतीस साल में राज्य की सत्ता में खूंटा गाड़े बैठी माकपा को इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। मई में हुए पंचायत चुनावों में पहली बार उसे राज्य की ग्रामीण आबादी अपने खिलाफ होती दिखाई दी थी। जून के अंत में हुए नगरपालिका चुनाव में उसकी और भी बुरी हार हुई। मई में वह चार जिला परिषदें, अनेक पंचायत समितियां और लगभग आधी ग्राम पंचायतें हार गई थी। जून में हुए नगरपालिका चुनावों में वह तेरह में से आठ नगरपालिकाएं हार गई। बाकी पांच में भी सिर्फ तीन उसे मिली हैं और दो सहयोगियों को।
लोग कहने लगे हैं कि अगले आम चुनाव में मार्क्सवादियों को पश्चिम बंगाल से अपनी कम से कम आधी सीटें खोनी पड़ेंगी। इसलिए मनमोहन सिंह सरकार के बच जाने की संभावना से पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादियों को राहत मिली है। चुनाव जल्दी होते तो उनके हाथ-पांव फूल गए होते। माकपा के लिए पश्चिम बंगाल में पैरों तले की जमीन खिसकना साधारण बात नहीं है। शुरू से ही उसकी शक्ति तीन राज्यों तक सीमित रही है। त्रिपुरा और केरल के मुकाबले पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है और यहां उन्हें अधिक सांसद जिताने का मौका मिलता है।
माकपा के इस समय लोकसभा में तैंतालीस सांसद हैं, जिनमें से छब्बीस पश्चिम बंगाल से हैं, बारह केरल से, दो त्रिपुरा से, दो तमिलनाडु से और एक आंध्र प्रदेश से। अंतर्कलह के चलते केरल में भी पार्टी की हालत अच्छी नहीं है। इसलिए अगले चुनाव में उसे सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ सकती है। पार्टी बनने के बाद 1967 में हुए आम चुनाव में उसके उन्नीस सांसद जीतकर आए थे। इस बार हो सकता है वह इतने सांसदों को भी न जिता सकें। बाकी वामपंथी दलों का भी भाग्य माकपा से जुड़ा रहता है। इसलिए अगर हवा बदली तो वामपंथियों की संख्या अगली संसद में आज से आधी भी नहीं रहेगी। इसलिए वामपंथी खेमें में यह सवाल उठना निश्चित है कि क्या परमाणु समझौते को टकराव का मुख्य मुद्दा बनाया जाना चाहिए था? इतना ही नहीं, जिस तरह यह मुद्दा उठाया गया उससे भी मार्क्सवादियों की नीयत पर सवाल उठे। दरअसल, वे भाजपा की तरह देश के नाभिकीय कार्यक्रम की स्वतंत्रता का मुद्दा तो उतनी विश्वसनीयता से उठा नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने भले ही चीन की सामरिक-वैज्ञानिक उपलब्धियों पर बधाई संदेश भेजे हों, भारत में वे हमेशा नाभिकीय परीक्षणों की निंदा करते रहे।
इसके बाद अमेरिका के साथ समझौते के विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभाव को ही मुद्दा बनाया जा सकता था। सो उन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि वह ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को समाप्त करवाने के लिए डाले जा रहे अमेरिकी दबाव का विरोध करे और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय देने के लिए गैस पाइपलाइन का समझौता करे। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि गैस पाइपलाइन ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा है, विदेश नीति का नहीं।
प्रकाश कारत की इस रणनीति पर सब वामपंथी सहमत रहे हों ऐसी बात नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एबी वर्धन की शुरू से ही यह राय थी कि परमाणु समझौते का विरोध जरूर किया जाए, पर उसे मनमोहन सिंह की सरकार पलटने का मुख्य मुद्दा न बनाया जाए। वे काफी समय तक कहते रहे कि हम समर्थन वापस लेंगे, पर आवश्यक नहीं कि सरकार गिराएं।
इसी तरह अनेक दूसरे वामपंथी नेताओं ने कहा कि परमाणु समझौते का विरोध करते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों को ही उससे टकराव का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। इसकी आधी-अधूरी कोशिश भी हुई। पर प्रकाश करात की सारी ऊर्जा भारत-अमेरिकी नाभिकीय सहयोग समाप्त करवाने में लगी रही।
करात की राजनीतिक शिक्षा छात्र आंदोलन की देन है। वे 1970 में एडिनबरा विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौटे थे और जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। 1974 से 1979 तक वे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। आपातकाल में आठ दिन जेल में रहे। 1992 में पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाए गए और 2005 में उन्हें पार्टी का महासचिव बना कर पार्टी की कमान सौंप दी गई। इसलिए उनकी समझ किताबी अधिक रही है। दूसरे दलों के नेताओं से जिस तरह का व्यक्तिगत संवाद सुरजीत बनाए रह सकते थे, करात के लिए संभव नहीं था। पर येचुरी की भूमिका कनिष्ठ ही है।
माकपा की इस अवस्था के लिए केवल प्रकाश करात को दोष देना ठीक नहीं होगा। सरकार बनाने, बदलने वाली जिस जोड़-तोड़ की राजनीति के जरिए करात अपनी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का सपना देख रहे थे, वह उन्हें उत्तराधिकार में ही मिली थी। माकपा के पिछले दोनों महासचिव उसी रास्ते पर चलते रहे थे। 1977 में कांग्रेस पहली बार केंद्र की सत्ता से हटी थी। उसी वर्ष पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादियों को सत्ता हासिल हुई थी और उसी वर्ष ईएमएस नंबूदिरीपाद पार्टी के महासचिव बने थे। देश की उन अनिश्चित परिस्थितियों में ममार्क्सवादियों को लगा था कि लोकतांत्रिक दलों के बिखराव का फायदा उठा कर वे आगे बढ़ सकते हैं। जोड़-तोड़ के उत्साह में नंबूदिरीपाद ने यहां तक कहा था कि बड़ी शत्रु कांग्रेस को हराने के लिए छोटी शत्रु भाजपा से सहयोग किया जा सकता है।
माकपा ने 1992 में नंबूदिरीपाद से कमान लेकर हरकिशन सिंह सुरजीत को सौंप दी। सुरजीत का सारा जीवन राजनीतिक जोड़-तोड़ में बीता। उन्हें अपना राजनीतिक कौशल दिखाने का मौका 1996 में मिला। लोकसभा चुनाव में भाजपा के 161 सांसद जीते और कांग्रेस के 140। उनमें से कोई सरकार नहीं बना सकता था। प्रधानमंत्री की खोज में कुछ नेताओं का ध्यान ज्योति बसु की ओर गया। पोलित ब्यूरो में सुरजीत और ज्योति बसु को छोड़कर सबने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसी राजनीतिक दुविधा के बीच देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। कांग्रेस और माकपा ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया। देवगौड़ा की सरकार ग्यारह महीने बाद समर्थन वापस लेकर कांग्रेस ने गिरा दी।
सुरजीत ने इंदर कुमार गुजराल की वैकल्पिक सरकार बनवाई, लेकिन वे भी ग्यारह महीने ही प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस लेकर आम चुनाव का रास्ता खोल दिया। इस राजनीतिक अनिश्चितता ने मार्क्सवादियों का हौसला बढ़ा दिया। ज्योति बसु ने बाद में उन्हें प्रधानमंत्री न बनने देने को पार्टी की ऐतिहासिक भूल बताया था। इस भूल को सुधारने के लिए 1998 की कलकत्ता कांग्रेस में माक्र्सवादियों ने अपना राजनीतिक कार्यक्रम संशोधित किया और यह गुंजाइश निकाल ली कि अवसर आने पर पार्टी केंद्र की सरकार में शामिल हो सकती है लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकारों की विफलता का फायदा कांग्रेस या ममार्क्सवादियों को मिलने के बजाय भाजपा को मिल गया और केंद्र में पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी।
यह दरअसल मार्क्सवादी नेतृत्व की नहीं, मार्क्सवादी सिध्दांत की कमजोरी है जिसे सभी मार्क्सवादी दियों ने तोतारटंत बना लिया है। उन्हें विश्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद से लड़ना है और भारत में वर्ग शत्रु कांग्रेस और सांप्रदायिक भाजपा से। पर भारत में उन्हें इस सरलीकृत सिध्दांत को लागू करने की राजनीतिक परिस्थितियां नहीं मिलीं। तीन राज्यों की सत्ता में आकर पार्टी वैसे ही वर्ग-संघर्ष भूल बैठी।
पिछले तीन दशकों में पार्टी ने कोई ऐसा संघर्ष नहीं किया जिसे सर्वहारा का संघर्ष कहा जा सके। हालत यह है कि उनकी राजनीति की धुरी रहे मजदूर आंदोलन में आज भाजपा से जुड़ा मजदूर संगठन पहले स्थान पर है और मार्क्सवादियों से जुड़ा मजदूर संगठन चौथे स्थान पर, यानी सबसे नीचे। किसान आंदोलन में भी उनकी कोई खास जगह नहीं है। अपने प्रभाव वाले तीन राज्यों से बाहर उनका रहा-सहा असर भी सिमट गया है। भारतीय राजनीति की धुरी हिंदी प्रदेशों में उनकी कभी कोई हैसियत नहीं रही।
मार्क्सवादी पार्टी के दिग्भ्रम की हालत यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को बेदखल करके उद्योग खड़े करना चाहती है। उद्योग खड़े करने के लिए भी उसे चीन मूल का एक विवादास्पद इंडोनेशियाई सलीम घराना घराना ही दिखाई दिया, जिसका मालिक भाग कर अमेरिका में छुपा हुआ है।
दूसरी तरफ केरल के मार्क्सवादी किसानों को खेती में मशीनों का इस्तेमाल भी नहीं करने देते कि इससे खेत मजदूर बेकार हो जाएंगे। देश की राजनीति में उन्हें इजारेदार शक्तियों से बड़ी समस्या सांप्रदायिक शक्तियां लग रही हैं। जब मनमोहन सिंह सरकार की तथाकथित सुधारवादी नीतियां सामाजिक सुरक्षा और मजदूरों के हित के सभी प्रावधानों को उलट दे रही हैं, वे मनमोहन सिंह सरकार को अपनी पीठ लादे रहे हैं। इस सब के चलते पार्टी की जड़ता बढ़ती गई है। उसका कैडर सिकुड़ता रहा है। ऐसे में बेचारे करात के पास विकल्प ही क्या है? (साभार : जनसत्ता/12 जुलाई, 2008)
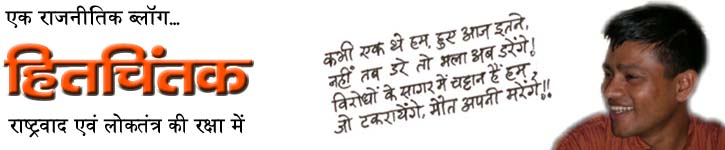
1 comment:
भगवान करे कि वामपंथ असफल हो; नहीं तो ये भारत ही को असफल कर देंगे। यदि सारा देश पश्चिम बंगाल की तरह 'प्रगति' कर जायेगा तो क्या दशा होगी?
Post a Comment