लेखिका- इन्दिरा शर्मा
पिछले कुछ सालों से भारत की राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवादी पहचान बहस का मुद्दा बन गई है। कुछ हलकों के द्वारा भारत की अक्षुण्ण राष्ट्रीय अस्मिता को नकारते हुए मार्क्सवादी और पश्चिमी विचारधारा के प्रबल प्रभाव में भारत के इतिहास और सांस्कृतिक निरंतरता को नकार कर काल्पनिक धरातल पर इसकी राष्ट्रीय पहचान को भरमाने की कोशिश कर रहा है। यह वैचारिक प्रयास बहुत हद तक कुछ लोगों को प्रभावित भी करता है। क्योंकि पिछले पचास वर्षों से भारत की राजनैतिक एवं सांस्कृतिक पहचान के बारे में उधार के तर्कों पर आधारित एकतरफा बयानबाजी का बोलबाला रहा है। और इस पर खुल कर बहस करने की जरूरत नहीं समझी गई। सैध्दांतिक पराधीनता ने विचारों को आज भी कुछ यों जकड़ रखा है कि इतिहासकार सामाजिक चिंतक आक्रांता साम्राज्यों द्वारा रचित सिध्दांत को सुलझाने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को रूढिवादी घोषित किये जाने का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक परतंत्रता का आलम यह है कि यदि बौध्दिक चिंतन का कोई वैकल्पिक प्रयास किया भी जाता है तो उस प्रयास पर नैतिकता से च्युत होने का इल्जाम लगाया जाता है और उस विचार में विश्वास करने वाले अनुयायियों को साम्प्रदायिक, कट्टरपंथी, उग्रवादी जैसे क्रूर शब्दों से नवाजा जाता है।
हिन्दुत्व की परिभाषा का पूरा ज्ञान न रखने वाले उस शब्द को अंग्रेजी के पंथ (Religion) से जोड़कर हिन्दू धर्म व्याख्या करने लगते हैं और समाज की सम्पन्न जातियों की सांस्कृतिक पहचान घोषित कर नई चर्चा करने वालों का मनोरथ भी तोड़ना चाहते हैं। यदि इस पर भी मन न भरे तो हिन्दू धर्म में निहित तथाकथित कमियों को गिनाने लगते हैं। उनके अनुसार उच्च और निम्न जातियों में विभक्त हिन्दू धर्म संकीर्ण विचारधारा वाला सिध्दांत है जिसमें आदिवासियों एवं विभिन्न प्रजातियों के लिए सद्भावना नहीं है। कहा जाता है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान सवर्ण हिन्दू की पहचान है और उसमें अन्य जातियों के लिए कोई स्थान नहीं है। देश के वनवासी और हरिजन अलग राष्ट्रीयताएं (Sub-Nationality½ हैं। भारत की ऐतिहासिक पहचान को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाये गए कदमों ने माक्र्सवादी 'विद्वानों को इतना उद्वेलित कर दिया है कि वे भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिध्दांत की दुहाई देते हुए कहने लगे हैं कि भारतीयता पर किसी एक विचारधारा का कब्जा नहीं हो सकता है न किसी एक वैचारिक समूह का। इस तर्क से उनका आशय मात्र भारत की राष्ट्रीयता और उसकी मूलभूत हिन्दू पहचान की बात करने वाले राजनैतिक दलों एवं संगठनों की आलोचना करना है। उन्हें यह डर है कि भारत पर साम्यवादी चिंतन प्रक्रिया के विरूध्द ये राजनैतिक दल अपने एकात्मक हिन्दूवाली विचारधारा की सबलता कहीं सिध्द न कर दें। जाहिर है भारत की राष्ट्रीय एकात्मता को बहस का बिन्दू बनाने से उन विचारधाराओं को ठेस पहुंचगी जो वर्षों से भारतीय संस्कृति को हेय बता रहे हैं, पुरानी जनजातियों को दास संस्कृति का परिचायक बतला रहे हैं, आर्यों के आक्रमण का झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं तथा एक देवतावादी धर्म और एकपक्षीय राजनैतिक चिंतन को भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। सेकुलरवादियों एवं मार्क्सवादियों के लिए यह काम आसान भी था क्योंकि लम्बे समय तक साम्राज्यवाद का शिकार रहा भारत का पढ़ा-लिखा अंग्रेजीदां मानस अपने अतीत से मुंह मोड़ चुका था और मैकाले की शिक्षा नीति ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता के पास अपने अतीत को समझने और जानने का साधान या तो उपलब्ध न हो या इतना दुरूह हो कि लोग अपने भौतिक आवश्यकता से परेशान होकर इस ओर रूख ही न करें। नये उद्धाटित चरमपंथी इस्लाम और ईसाई चर्चों के कट्टरपंथ की पहचान सदैव 'राजनीति और धर्म' का एकीकरण रहा है अत: 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन्ह तैसी' को चरितार्थ करते हुए उन्होंने हिन्दुत्व को भी अपने जैसा सिध्दांत मानकर पूर्वाग्रहपूर्वक उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो लोग भारतीय राष्ट्रीयता को अनेक नस्ली और धार्मिक राष्ट्रीयताओं का योग घोषित करते हैं उन्हें भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर सुधारवादी नजरिया रखने वाला हिन्दुत्व अपने विस्तार में सबसे बड़ा अवरोधक नजर आने लगा है। भारत की 'एकात्म सांस्कृतिक राष्ट्रीयता' को चुनौती इसलिए दी जाती है क्योंकि उनका बौध्दिक एवं राजनैतिक प्रपंच ही समाज के विघटनकारी प्रपंच पर खड़ा है। यदि वे भारत की सांस्कृतिक एकता स्वीकार कर लें तो फिर जातिवाद, फिरकावाद, साम्प्रदायिक तुष्टिकरण पर आधारित उनकी राजनीति ही चरमरा जाएगी। अलगाववादी राजनीति की सीधा आवश्यकता होती है विघटित राष्ट्रवाद। इसलिए कहा जाता है कि भारत कई उप-राष्ट्रीयताओं का समूह है। इस चिंतन का ऐतिहासिक तथ्यों या सत्य से कोई सरोकार नहीं है।
आधुनिक समय में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की परिकल्पना का उद्भव 18वीं शताब्दी के यूरोपीय परिवेश में हुआ है। यह राष्ट्रवाद रोमन चर्च के शिकंजे से मुक्ति की चाहत के साथ-साथ यूरोपीय संस्कृति एवं भौगोलिक पहचान के रूप में उभरा। इसी क्रम में पूंजीवाद का उदय तथा एक सुनिश्चित बाजार की चाहत इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग बन गए हैं। पाश्चात्य चिंतक कोह्न के अनुसार 1815 से 1920 के बीच यूरोप का मानचित्र तथा 1945 से 1965 के बीच एशिया और अफ्रीका का मानचित्र पुन: अंकित किया गया। इसके पहले यूरोपीय और एशियाई राज्य, नगर एवं जनपदीय समूहों के रूप में अवस्थित थे। जर्मनी तकरीबन चार सौ से ज्यादा जनपदों में तथा इटली दर्जनों जनपदों में विभक्त थे। उनका एकीकरण उन्नीसवीं सदी की घटना है जब उभरते राष्ट्रीय पूंजीवाद, साम्राज्यवादी होड़ और भाषाई, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक एकता ने उनके अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीय पहचान का बीजारोपण किया। इस प्रक्रिया में यूरोप के देशों ने भाषा, धर्म, संस्कारों तथा साझे इतिहास के आधार पर राष्ट्र की कल्पना की। आज काई जर्मनी या इटली को विभिन्न उप-राष्ट्रीयताओं का समूह तो नहीं कहता है, पर वही चिंतक भारत की सामाजिक एवं ऐतिहासिक पहचान पर प्रश्नचिह्न उठाते हैं।
सेकुलरवादियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध स्वरूप हुआ। यह अंग्रेजों के भारत पर सफलतापूर्वक शासन करने के लिए राजनैतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण के कारण ही संभव हुआ। उनके अनुसार 19वीं शताब्दी से पूर्व राजनैतिक तौर पर भारत नामक कोई देश नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद तथा उनके द्वारा शिक्षा, विज्ञान एवं दर्शन जैसे विषयों का परिचय कराकर ही भारत के संस्कृति को एक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान मिली। सत्य तो यह है कि हम अतीत काल से ही सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र हैं। यदि ऐसा न होता तो एक ही मंत्र कश्मीर में जपे जाते और कन्याकुमारी में भी उच्चरित होते। बद्रीनाथ से तिरूपति मन्दिर तक में भी वे ही मंत्र उद्गीत थे। राजनैतिक रूप से भले ही आजादी की लड़ाई के समय एक राष्ट्र की कल्पना की गई किन्तु अपने संस्कारों से हम एक राष्ट्र के रूप में बंधो हुए थे। यदि हम एक राष्ट्र नहीं होते तो अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने भी केवल उसी भाग को हिन्दुस्तान क्यों कहा जो एक सांस्कृतिक और सामाजिक परिधि में थे। अंग्रेजों ने नेपाल, बर्मा आदि भारतीय राष्ट्र का अंग क्यों नहीं माना? जबकि वे देश भी उसी के प्रभाव क्षेत्र में थे क्या वजह थी जो उन्होंने इन स्वतंत्र राज्यों को ही 'इंडिया' के रूप में स्थापित किया? स्पष्ट है पुरातनकाल से ही उन राज्यों में भारत राष्ट्र के सांस्कृतिक एवं राजनैतिक अंश विद्यमान थे। मौलिकताविहीन सेक्युलरवादी अंग्रेजीदानों का मानना था कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण ही यह था कि दोनों देशों के बीच कोई सामान्य पहचान नहीं उभर पाया। भारतीय पहचान की आड़ में पाकिस्तान के विभाजन को सांस्कृतिक रूप से अलग मानकर उसकी तरफदारी करने वाले यह भूल जाते हैं कि वह देश केवल धर्म के नाम पर सत्ता के लोलुपता के आधाार पर बना था।
कुछ लोगों का मत है कि प्रारंभिक दौर में साम्राज्यवाद का विरोधा राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष एवं स्वतंत्रता की आवश्यकता राजनैतिक कारणों से कम विचारधारा एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक था। इसलिए उस संघर्ष की पहली अभिव्यक्ति सामाजिक एवं धार्मिक सुधार थी। सबसे मुख्य प्रश्न यह था कि भारतीय समाज का सांस्कृतिक आधार क्या है? किस प्रकार हम इसका पुनर्निर्माण करें जिससे वह आधुनिक राष्ट्रों के समकक्ष रह सके। यहां छद्म सुधारवादी लोग यह भूल जाते हैं कि संस्कृति किसी राष्ट्र के निर्माण का आधार होती है जो समय, व्यक्ति, काल के अनुसार अपने में परिवर्तन लाती है और परिस्थिति के अनुसार स्वयं ही सुधारवादी रवैया अपनाती है।
आजादी के पश्चात् दो विचारधाराएं राष्ट्र निर्माण के चिंतन का आधार बन गई। एक धारा थी नेहरूवादी धारा जो पश्चिमी मॉडल के आधार पर देश का निर्माण करना चाहती थी। इस विचारधारा के वाहक भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में पश्चिमी एवं चर्च प्रचारित कुप्रचार के कारण निषेधात्मक हो गया था। मन्दिरों को ध्वस्त करने वाले महमूद गजनवी को एक महान योध्दा एवं मुस्लिम धर्म प्रचारक के रूप में स्थापित करना था तथा जातिगत वर्ग संघर्ष में उलझे हिन्दुओं खासकर दलितों को इस्लाम जैसे सेक्यूलर धार्म का उपहार देने वाले महान गुरू के रूप में दर्शाना था। यह विचारधारा सच की अनदेखी कर झूठ को महिमा मंडन करने का कुचक्र करती रही। यही दृष्टिकोण धीरे-धीरे कांग्रेस एवं उत्तारोत्तार आजादी प्राप्त कांग्रेस सरकारों का भी रहा।
इसके अतिरिक्त भारतीय इतिहास की दूसरी विचारधारा रही है जिसने हिन्दुत्व के इतिहास को उसका उचित स्थान दिलाकर तथा उसकी संस्कृति का पुनर्निमाण कर उसकी स्थापना की हैं। राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे धर्म संस्थापकों का उदाहरण हमारे सामने उपलब्ध है जिन्होंने इस्लामिक आक्रमणों एवं साम्राज्यवादी शासन की वजह से हिन्दू धर्म में आये कुरीतियों को दूर कर राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए वैदिक सभ्यता एवं दर्शन पर बल दिया।
श्री दयानंद सरस्वती ने पाप का भय दिखा कर एकमात्र त्राता के रूप में दर्शाये जेसुआ के बारे में एक श्लोक द्वारा स्पष्ट कर दिया कि आर्य समाज का एकेश्वरवाद ईसाइयों के ऐकेश्वरवाद से भिन्न है उन्होंने लिखा-
क्षणे तुष्टा, क्षणे रूष्टा, रुष्टातुष्टा क्षणे क्षणे।
अवयवस्थित चित्रस्य प्रसादोऽपि भयंकर:॥
दयानंद सरस्वती ने ईसाइयों द्वारा हिन्दू धर्म के सुधार एवं उसके भीतर परिवर्तन को बल दने के नाम पर धर्मपरिवर्तन करने के प्रपंच से चिंतित होकर ही 'शुध्दी' आंदोलन का सूत्रपात किया जिसमें किसी समय, किसी लोभ, धोखे या सत्ता के भय से अपने धर्म से विमुख हुए लोगों की पुन: हिन्दू धर्म में वापसी का प्रावधान था।
इन धर्मसंस्थापकों के प्रयासों की काट के लिए यह कहा जाने लगा कि वर्णाश्रम आधारित ऊंची जाति के वर्चस्व वाले कट्टर हिन्दुवादियों ने समाज सुधार के राष्ट्रीय आंदोलन का रूख मोड़कर राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बदल डाली और उसे सांस्कृतिक स्वरूप देकर साम्प्रदायिक रूप बना दिया। हिन्दू धर्म में परिवर्तन और सुधार का नारा देने वाले ईसाई चर्चों की कुटिल चाल भी हमें समझनी चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण बड़ी चतुराई से बार-बार हिन्दू में हीन भावना की आवृत्ति मात्र करना था। वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक स्वरूप की एक ऐसी स्वतंत्र सत्ता थी जो स्वयं में परिपूर्ण थी उसे बाहरी किसी हस्तक्षेप की या सहायता की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्वावलम्बी व्यवस्था में घुसपैठ करना आसान नहीं था। इस व्यवस्था में घुसपैठ के लिए जरूरी था ब्राह्मणों यानि वर्णाश्रम व्यवस्था के बौध्दिक पकड़ को तोड़ना और शेष वर्णों में उनके प्रति अविश्वास और असंतोष पैदा करना। बौध्दिक स्तर पर भारत के पास अकूत सम्पत्ति थी। विज्ञान, साहित्य, न्याय, मीमांसा, धार्म शास्त्र, योग शास्त्र, कृषि, व्यवसाय, विद्या, अर्थ शास्त्र, दर्शन शास्त्र जीवन विषयक भंडार भारत के पास मौजूद था तथा उसका नियामन करने के लिए विभिन्न वर्णों की संरचना की गई थी। इन सभी शास्त्रों एवं मतावलम्बियों का लक्ष्य था सत्य की खोज तथा वह खोज प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक-पृथक था। इसीलिए हिन्दू धर्म में कई पंथ समाहित थे और यही कारण भी था कि हिन्दू धर्म में धर्मपरिवर्तन की कोई अवधारणा नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी नये उद्धाटित धर्म द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करना भारत में असंभव ही था। बाहर से आये लोगों को यह वर्ण व्यवस्था समझ में भी नहीं आती थी साथ ही यह दुर्भेद्य भी लगती थी। इसीलिए अंग्रेजी चिंतकों ने इस वर्ण प्रणाली को ब्राह्मणों के अत्याचारों एवं दलितों के दलन की कहानी बनाकर प्रचलित करना शुरू किया। उसका प्रभाव दूरगामी निकला और हमारे देश में एक अमौलिक बुध्दिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण की होड़ लग गई। यह अनुकरण उन्हें सत्ता के गलियारे में ऊंची पदवी और परिवर्तन के उहापोह में खड़े समाज में सम्मान दिलाता था। इन बुध्दिजीवियों को साम्यवादी कहलाने का अधिकार मिला और वह साम्यवाद विशुध्द रूप से हिन्दुत्व विरोधी एवं विशेष पंथों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया वाला था। इन लोगों को बहुदेववाद बुरा लगता था। अपना धर्म दूसरों से हीन लगता था। काली, दुर्गा, गणेश, शिव देवताओं में आस्था करने वाले व्यक्ति अज्ञानी और निकृष्ट लगते थे। शिवाजी राणाप्रताप, बंदाबहादुर, गुरूतेग बहादुर जैसे देशभक्तों का सही चित्रण अखरने लगा। गांधीजी के अनुसार ''आजादी, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक परिवर्तन जैसी उपलब्धियां केवल समाज के धार्मिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता के आधार पर ही हो सकती है।'' परन्तु हमारा बुध्दिजीवी वर्ग पैसा कमाने की होड़ में इन वक्तव्यों को नजरअंदाज करता रहा और हिन्दुत्व को साम्प्रदायिकता की परिधि में लाने की नाकामयाब कोशिश करता रहा।
आजादी के पहले से ही इकबाल, जिन्ना, सर सैयद अहमद, अली भाइयों, जैसे मुस्लिम नेताओं ने यह प्रचारित करना शुरू किया कि यदि देश आजाद हुआ और सत्ता की बागडोर बहुसंख्यक हिन्दुओं के हाथ गई तो मुसलमानों का दमन होगा। देश के मुसलमानों में भय का माहौल बनाया गया। विघटनकारी विचारधारा ने मुसलमानों को अलग राष्ट्रीयता घोषित करा दिया। मुसलमानों के लिए यह राजनैतिक पासा फेंका गया कि उन्हें अपने धर्म के पालन व सुरक्षा के लिए नये देश की आवश्यकता होगी और इसी आधार पर पाकिस्तान की नींव रखी गई। मुस्लिम नेतृत्व यह जानता था कि उनकी यह शंका निर्मूल है। हिन्दू आक्रामक तथा जबरन वर्चस्व स्थापित करने वाली प्रजाति न थी, न है, न रहेगी।
आज पुन: जब राष्ट्रवाद के चर्चा की धुरी सांस्कृतिक पहचान है तो इन छद्म सेकुलरवादियों को अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिख रहा है। जिस झूठ की बुनियाद पर इनका विष बेल पनप रहा था अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बहस उन्हें अनाथ बनाने और उनके बौध्दिक एवं राजनीतिक प्रपंच को उजागर करने में सहायक हो रहा है।
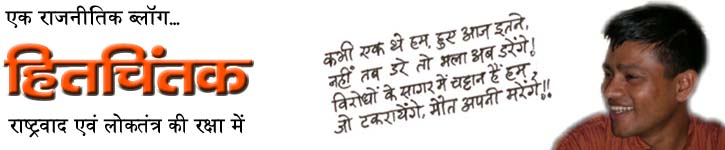
1 comment:
सास्कृतिक राष्ट्रवाद एक सम्पुर्ण विचारधारा है, और मैने अगर उसे ठीक समझा है तो वह मुसलमानो के साथ सह असितित्व मे विश्वास करती है। वह यह कहती है की जो समय गुजरा है उसमे बहुत कुछ अवांछनीय हुआ है, लेकिन उसे शुरु बिन्दु पर पहुंचाना सम्भव नही है। लेकिन, दक्षिण भारतीय मुसलमान एवम हिन्दु भाईचारे के लिए जो काम होना चाहिए उसके विपरीत काम हो रहे है। साथ ही, सास्कृतिक रास्ट्रवाद के सफलता के लिए क्रांती का सिद्धंत भी आवश्यक है।
Post a Comment