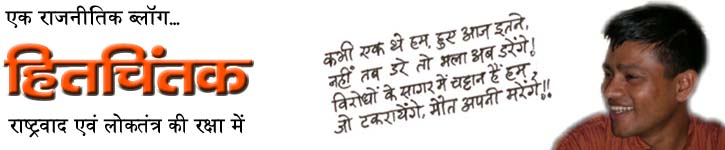लेखक - देवेन्द्र स्वरूप
3 जनवरी को बंगाल के मुख्यमंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य ने अपनी पार्टी के दैनिक मुखपत्र 'गणशक्ति' के 45वें स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित वामपंथी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि बंगाल के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकीरण आवश्यक है और औद्योगिकीरण पूंजी के बिना सम्भव नहीं है इसिलए हमें पूंजीवाद के रास्ते पर जाना होगा। बुध्ददेव ने कोई नई बात नहीं कही। वे बंगाल विधानसभा चुनाव के पूर्व ही कह चुके थे कि बंगाल में जो कुछ कर रहे हैं वह समाजवाद नहीं, पूंजीवाद है। लेकिन इस बार उन्हें बंगाल के वयोवृध्द नेता ज्योति बसु का भी खुला समर्थन मिला। 5 जनवरी को ज्योति बसु ने माकपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि औद्योगिक विकास के लिए हमें देशी व विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना होगा। हमारा शासन केवल तीन राज्यों तक सीमित है। पूरे देश में पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर हम काम कर रहे हैं इसलिए हमें भी पूंजीवाद का रास्ता अपनाना ही होगा।
क्या दो शीर्ष माकपाई नेताओं के इन उद्गारों को सोवियत रूस और माओवादी चीन में कई दशाब्दियों लम्बे मार्क्सवादी प्रयोग की विफलता की कारण-मीमांसा और विचार-मंथन में से निष्पन्न वैचारिक परिवर्तन माना जाए या केवल बंगाल में सत्ता में बने रहने की मजबूरी जन्य रणनीति? यदि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर मार्क्स, लेनिन और माओ की किताबों की तोता रटन्त से आगे बढ़कर सोवियत संघ और चीन के अनुभवों के आलोक में मार्क्सवादी विचारधारा की अवैज्ञानिकता और अपूर्णता को समझने का ईमानदार बौध्दिक प्रयास हुआ होता तो बुध्ददेव और ज्योति बसु के कथनों पर वाममोर्चे के छुटभये घटकों भाकपा, आर.एस.पी. और फार्वर्ड ब्लाक आदि की इतनी तीखी प्रतिक्रिया न होती। यहां तक कि केरल के मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानन्दन इन वक्तव्यों की खुली आलोचना न करते। शायद इस अन्तर्संवाद से बाहर निकलने के लिए ही माकपा महासचिव प्रकाश करात ने बुध्ददेव और ज्योति बसु के वक्तव्यों का समर्थन करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह मात्र रणनीति है, सैध्दांतिक परिवर्तन नहीं। समाजवाद पर हमारी निष्ठा अडिग है, वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। केन्द्र में सत्ता में आये बिना हम पूरे भारत को समाजवाद के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रणनीति के तौर पर हम पूंजीवाद को अपना सकते हैं। रणनीति बदल सकती है, लक्ष्य नहीं, सैध्दांतिक अधिष्ठान नहीं। करात ने त्वरित आलोचना के लिए आर.एस.पी. को फटकार भी लगाई।
आर.एस.पी. के नेता के. पंकजाक्षन ने कहा था कि मैंने माक्र्सवाद की किसी किताब में नहीं पढ़ा कि औद्योगिक विकास के लिए पूंजीवाद जरूरी है। पूर्व सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने निजी पूंजी के बिना ही औद्योगिक ढांचा खड़ा कर दिया था। माकपा से निष्कासित केरल के एम.वी. राघवन ने, जिन्होंने कम्युनिस्ट माक्र्सवादी पार्टी नाम से नया मंच बनाया है, ज्योति बसु व बुध्ददेव की आलोचना करते हुए कहा कि यदि माकपा समझती है कि समाजवाद का कोई भविष्य नहीं है तो उसे स्वयं को भंग कर देना चाहिए। एक अन्य मार्क्सवादी ने कहा कि माकपा को अपना नाम पूंजीवादी कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए।
विचारधारा या अंधविश्वास?
भारतीय कम्युनिस्टों में सिंगूर, नंदीग्राम, तस्लीमा, रिजवानुर रहमान आदि प्रसंगों को लेकर जो बहस चल रही है उसे पढ़कर लगता है कि मार्क्सवाद उनके लिए वैज्ञानिक विचारधारा से अधिक एक अंधविश्वास बन गया है। यह अंधविश्वास केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है तो बड़े-बड़े कम्युनिस्ट बौध्दिकों में भी गहरा बैठा हुआ है। बंगाल सरकार के संरक्षण में माकपाई कार्यकर्ताओं द्वारा नंदीग्राम में किसानों के नरमेध से उद्वेलित राजेन्द्र यादव, जो हंस के संपादक हैं, के इन शब्दों को पढ़िये, 'कुछ लोगों की असफलताओं के कारण छोड़कर विरोधी खेमे में चले जाना हमारा धर्म नहीं है। हमें आज भी वाम-विचारधारा में अटूट विश्वास है, क्योंकि मानव-इतिहास में आज भी वही सबसे विकसित अजेय विचारधारा है। चूंकि सभी विचारधाराओं में वही सबसे वैज्ञानिक है...' (हंस, दिसम्बर, 2007)
यहां सवाल खड़ा होता है कि किसी विचारधारा की वैज्ञानिकता की कसौटी क्या है? मार्क्सवाद का दार्शनिक अधिष्ठान द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को माना जाता है। मानव सभ्यता की मूल प्रेरणा आर्थिक कही गई है। क्या विज्ञान की पिछले डेढ़ सौ साल की प्रगति के आलोक में इस सिध्दांत को वैज्ञानिक कहा जा सकता है? माक्र्स ने मानव सभ्यता की इतिहास यात्रा को आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामंतयुग और पूंजीवादी युगों में विभाजित करते हुए भविष्यवाणी की कि पूंजीवाद के विनाश के बीज उसके भीतर ही विद्यमान हैं और अपने चरम पर पहुंचकर वह नए साम्यवादी युग को जन्म देगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की मृत्यु अवश्यम्भावी है, मार्क्सवादियों को केवल उस दिन को नजदीक लाना है, इसके लिए सर्वहारा को संगठित करके क्रांति का बिगुल बजाना है। माक्र्स की इतिहास दृष्टि यदि वैज्ञानिक होती तो माक्र्सवादी क्रांति को सबसे पहले सर्वाधिक विकसित पूंजीवादी देशों जैसे ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी या फ्रांस में होना चाहिए था। किन्तु इन देशों में मार्क्सवादी क्रांति होना तो दूर, उनका पूंजीवाद ही अब रूस और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों पर हावी हो गया है, माक्र्सवाद को उन्होंने पूरी तरह तिलांजलि दे दी है। माक्र्सवाद की वैज्ञानिकता तो उसी दिन धराशायी हो गई थी जब लेनिन ने असंतुष्ट रूसी सिपाहियों के सहारे सत्ता परिवर्तन को मार्क्सवाद प्रेरित क्रांति का आवरण पहना दिया था। रूस में तब तक पूंजीवाद प्रारंभिक चरण में था, इसके बाद चीन में माओ के नेतृत्व में जब सत्ता-परिवर्तन हुआ तब वहां पूंजीवाद प्रसववेदना से ही गुजर रहा था। माक्र्स ने नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। किन्तु आज दृश्य क्या है? उन्हें एकता के सूत्र में बांधने का ठेका जिन मार्क्सवादियों पर है वे स्वयं ही बीसियों टुकड़ों में बिखर गये हैं और प्रत्येक अपने को सच्चा मार्क्सवादी कहता है। क्या किसी वैज्ञानिक विचारधारा के इतने अर्थ हो सकते हैं? वैज्ञानिक सत्य एक होता है, वह सार्वकालिक, सार्वभौमिक होता है।
सच तो यह है कि भारतीय कम्युनिस्टों को माक्र्सवाद की समझ लेनिन, स्टालिन और माओ के रास्ते से मिली है। यदि लेनिन ने रूस के सत्ता-परिवर्तन को मार्क्सवादी क्रांति का आवरण न पहनाया होता और 'सर्वहारा के अधिनायकवाद' के मुखौटे में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही को स्थापित न किया होता, जार सम्राटों द्वारा निर्मित विशाल रूसी साम्राज्य के अपार साधनों के बल पर अपनी विदेश नीति को विश्व क्रांति का रूप न दिया होता, रूस की जनता को भूखों रखकर मुत प्रचार-साहित्य से पूरी दुनिया को न पाट दिया होता तो शायद माक्र्सवाद कुछ किताबी बौध्दिकों की बहस तक सिमटा रह जाता।
भारतीय कम्युनिस्टों के गहरे अंधविश्वास का ही उदाहरण है कि जब रूस की जनता स्टालिन और लेनिन की व्यक्ति-पूजा को पूरी तरह दफना चुकी है, चीन की जनता और सरकार माओ का नाम तक नहीं लेना चाहती, भारत के कम्युनिस्ट अभी भी लेनिन और माओ का झंडा उठाये घूम रहे हैं। लेनिन की अंध-भक्ति के कारण वे मार्क्सवादी क्रांति का एकमात्र लक्ष्य सत्ता पर कब्जा जमाना समझ बैठे हैं। मार्क्सवादी शब्दावरण में सत्ता को पाना, उस पर टिके रहने को ही वे क्रांति कहते हैं। उनके लिए सत्ता ही क्रांति है, क्रांति का अन्तिम लक्ष्य सत्ता है। रूस और चीन के अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया कि कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकवाद जनजीवन पर राज्य का और राज्य पर अपने शिकंजे को अधिकाधिक सुदृढ़ करता जाता है। मार्क्स के इस कथन को वह पूरी तरह भूल जाता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने का उद्देश्य शोषण विहीन समतामूलक समाजजीवन की आदर्श स्थिति उत्पन्न करना है, यह स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य स्वयं ही अस्तित्वहीन हो जाएगा। किन्तु इन दोनों देशों का अनुभव कहता है कि शोषण विहीन समतामूलक जीवन तो वहां खड़ा हुआ नहीं, स्वयं कम्युनिस्ट शासक ही शोषण और विषमता का स्रोत बन गये किन्तु अधिनायकवादी सत्ता-तन्त्र उत्तरोत्तर अपना शिकंजा कसता गया। चीन ने मार्क्सवाद और माओवाद को तो तिलांजलि दे दी किन्तु अधिनायकवाद शासन तंत्र को बनाए रखा है।
औद्योगिक दृष्टि से रेगिस्तान बना बंगाल
सिंगूर-नंदीग्राम और तस्लीमा प्रकरणों के बाद बंगाल में तीस वर्ष लम्बे कम्युनिस्ट शासन का जो रूप सामने आया है उसे देखकर कुछ मार्क्सवादी बुध्दिजीवी और कलाकार भी चिललित हो उठे हैं। संसदीय लोकतंत्र के चौखटे के भीतर शासन करने वाले दल का चरित्र इतना हिंसक, भ्रष्टाचारी और सत्ताप्रेमी हो सकता है, यह वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। किन्तु इसके लिए वे बंगाल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ही दोषी मान रहे हैं, किन्तु मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति अपनी अडिग निष्ठा का ढिंढोरा पीट रहे हैं। कई बार भारतीय कम्युनिस्टों की मार्क्सवाद के प्रति अंध श्रध्दा और व्यक्ति पूजा को देख कर उस मुस्लिम मानसिकता का स्मरण हो आता है जो इस्लाम के नाम पर होने वाली प्रत्येक हिंसा और बर्बरता को गैर इस्लामी कह कर अपना समाधान कर लेता है और मुस्लिम मानसिकता के दो मूल स्रोतों- कुरान और पैगम्बर मुहमद के प्रति अन्ध श्रध्दा लेकर चलता है, उनकी तनिक भी आलोचना सहन नहीं कर पाता। इसी प्रकार भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्स के प्रत्येक शब्द को अन्तिम सत्य मान कर चलते हैं, और प्रत्येक उलझन के समय माक्र्स या लेनिन के उध्दरणों की तोता रटन्त करते रहते हैं।
क्या प. बंगाल का अनुभव यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनवाद ने बंगाल को औद्योगिक दृष्टि से रेगिस्तान बना दिया और अब सत्ता में टिके रहने की मजबूरी ने माकपाई मुख्यमंत्री बुध्ददेव को पूंजी आकर्षित करने के लिए ट्रेड यूनियनवाद पर अंकुश लगाने को बाध्य कर दिया है। नंदीग्राम पर 10,000 पार्टी कैडरों की फौज के आक्रमण और पाशविक बल के द्वारा वहां की जमीनों और घरों पर कब्जा करने की घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में शासन-तंत्र और पार्टी का भेद मिट चुका है शासन-तंत्र और पार्टी तंत्र एक रूप हो चुके हैं और मिलकर जनता का उत्पीड़न व शोषण कर रहे हैं। इसे पार्टी अधिनायकवाद नहीं तो क्या कहें? यह अधिनायकवाद जनता के लिए नहीं, केवल पार्टी के लिये है। इसके कारण पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार और विलासिता को बढ़ावा मिला है। दिल्ली से प्रकाशित मेल टाइम्स (8 जनवरी) में आलोक बनर्जी ने पार्टी सूत्रों से अपने सम्बंध के आधार पर जानकारी दी है कि बंगाल में माकपा चुनावों पर 200-250 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि खर्च करती है। 30 वर्ष लम्बे कम्युनिस्ट शासन की अजेयता से आतंकित उद्योग और व्यापार क्षेत्र उन्हें खुलकर पैसा दे रहा है। राज्यभर में पुराने जीर्ण-शीर्ण कार्यालयों का पुनर्निर्माण पंच सितारा भवनों में हो गया है। सुदूर गांवों में भी तीन मंजिले भवन बन गये हैं। जो कामरेड तीस साल पहले साइकिलों पर चला करते थे, वे अब एयर कन्डीशन्ड गाड़ियों में घूमते हैं। नंदीग्राम नरमेध के बाद मीडिया ने पार्टी के चरित्र को पूरी तरह नंगा कर दिया है। जिससे बंगाल का मध्यम वर्ग उद्वेलित हो उठा है। उधर कट्टरपंथियों के दबाव में तस्लीमा को राज्य से खदेड़ने के निर्णय ने पार्टी के छद्म सेकुलरवाद और उदार चेहरे पर से नकाब उठा दिया है। नंदीग्राम में मुस्लिम बहुसंख्या होने के कारण वह प्रश्न भी मुस्लिम प्रश्न बन गया है। सच्चर रपट में भी बंगाल के मुसलमानों की स्थिति खराब बतायी गई है। इस प्रकार नंदीग्राम, तस्लीमा, सच्चर रपट और रिजवानुर कांड ने माकपा के सामने 20 प्रतिशत मुस्लिम वोट बैंक को बचाये रखने की गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। मेल टाइम्स की रपट के अनुसार माकपा सांसद मुहम्मद सलीम ने पार्टी कामरेडों की बंद कमरे की मीटिंग में चेतावनी दी कि यदि हमने इस्लाम की आलोचना की तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री बुध्ददेव भी इस बात से सहमत थे।
अधिनायकवाद
इसलिए बंगाल में सत्ता को टिकाए रखने की त्रिसूत्री रणनीति बनाई गई है। एक तो बंगाली मध्यम वर्ग को शान्त करने के लिए औद्योगिक विकास में तेजी की जाए। उसके लिए देशी-विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए पूंजीवाद का उद्धोष किया जाए। दूसरे, मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए कट्टरपंथी मुस्लिम नेतृत्व को प्रसन्न किया जाए। तीसरे, विपक्ष में एकता न पैदा होने दी जाए। हाल ही में सिंगूर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित बालागढ़ उपचुनाव में, जो माकपा का परंपरागत गढ़ रहा है, माकपा बड़ी मुश्किल से सीट बचा पायी, जीत का अन्तर बहुत कम हो गया। यदि वहां विपक्ष ने एक्यबध्द होकर मजबूत प्रत्याशी खड़ा किया होता तो माकपा की हार सुनिश्चित थी। इतने पर भी माकपा की साख कमजोर हुई है। वाम मोर्चे के घटक उसे आंखें दिखाने लगे हैं। ममता बनर्जी की ओर झुकने लगे हैं। किन्तु बंगाल में विपक्षी एकता सोनिया पार्टी व भाजपा के बिना पूरी नहीं मानी जा सकती। सोनिया पार्टी केन्द्र में सत्ता खोने के भय से माकपा को नाराज नहीं करना चाहती और भाजपा के प्रति मुस्लिम मन में इतना जहर भर दिया गया है कि संयुक्त मोर्चे में भाजपा के प्रवेश करते ही माकपा का प्रचार तंत्र मुस्लिम भावनाओं को भड़काने में जुट जाएगा। वोट बैंक राजनीति के इन अन्तर्विरोधों से कैसे पार पाया जाए, राष्ट्रीय एकता के उपासकों के लिए यही आज चिन्ता का मुख्य विषय है। बंगाल को माकपा के भ्रष्ट अधिनायकवाद से मुक्त कराने के लिए तात्कालिक दलीय स्वार्थ से ऊपर उठकर दूरगामी रणनीति ही आज की आवश्यकता है।
इसके साथ ही चुनावी राजनीति से आगे बढ़कर कम्युनिस्ट बुध्दिजीवियों के सामने बौध्दिक चुनौती खड़ा करने की बड़ी आवश्यकता है। बौध्दिक क्षेत्र में माक्र्सवाद पैसा, पद, प्रतिष्ठा और सुविधाएं दिलाने वाली गिरोह बन्दी का पर्याय बन गया है। जन जीवन से कटे, बुध्दि-विलास में मगन वामपंथी बौध्दिक मार्क्स की व्यक्ति-पूजा और पार्टी अनुशासन के प्रति अंधनिष्ठा से बंधे हुए हैं। मार्क्सवाद को लेनिन का मुख्य योगदान यह रहा कि उसने 'सर्वहारा के अधिनायकवाद' को 'लोकतांत्रिक केन्द्रवाद' के शब्दाडम्बर में 'पार्टी अधिनायकवाद' का रूप दे दिया और 'पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती' जैसे सूत्र वाक्य के द्वारा पार्टी को भगवान की जगह बैठा दिया। इसलिए बड़े श्रेष्ठ मार्क्सवादी बुध्दिजीवी भी मार्क्स या लेनिन के वाक्यों की तोतारटन्त में शर्म अनुभव नहीं करते और बौध्दिक अहंकार में चूर रहते हैं। अंध भक्ति और अहंकार कितनी दूर तक जा सकता है इसका नमूना राजेन्द्र यादव की इन पंक्तियों में देखिए। वे लिखते हैं :
'सोवियत यूनियन की लाख बुराइयों के बावजूद यह भी सच है कि दुनिया में जहां भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जमीनी संघर्ष हुए हैं उनकी एकमात्र प्रेरणा मार्क्सवाद ही रहा है। ... आज भी लाखों बुध्दिजीवियों और जुझारू जनता की प्राणशक्ति मार्क्सवाद ही है।' (हंस, दिसम्बर, 2007)
कोई राजेन्द्र जी से पूछे कि यदि यही सच है तो बंगाल, त्रिपुरा और केरल के बाहर कम्युनिस्ट पार्टियां जनाधार शून्य क्यों हैं? इस दिल्ली शहर में मार्क्सवादी प्रोफेसरों, पत्रकारों, साहित्यकारों और रंगकर्मियों की इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी दिल्ली नगर निगम में एक सीट जीतने लायक भी जनाधार उनके पास क्यों नहीं है?
Wednesday, 23 January 2008
Saturday, 19 January 2008
रंगनाथ मिश्रा आयोग के पीछे का राजनैतिक षडयंत्र
लेखक: डा0 कुलदीप चन्द अग्निहोत्री
भारत सरकार भारतीय मजहबों को त्याग कर ईसाई और मुसलमान समाज में चले गए व्यक्तियों की जाति तलाशने के काम में जुटी हुई है। लेकिन समस्या यह है कि इस देश में जोर जबरदस्ती या लालच से भारतीय या हिन्दू समाज के लोगों को इस्लामी समाज के घेरे में लाने की कवायद काफी लंबे अरसे से हो रही है। इसकी शुरूआत मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों के पहले ही शुरू हो गई थी। ये लगभग सातवीं-आठवीं शताब्दी की घटनाएं हैं। उसके बाद लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक और मुगल जैसी अनेक इस्लामी सल्तनतें इस देश में स्थापित हुईं और हिन्दू समाज से इस्लामी समाज की होर जाने का सिलसिला भी चलता रहा। इस्लामी समाज में जाति व्यवस्था नहीं है। इसलिए पंथ परिवर्तन के बाद उनकी जाति इस्लामी समाज में ही विलीन हो गई। यही प्रक्रिया बाद में भारत में पुर्तगाल, डच और अंग्रेजों के आने के बाद ईसाई समाज की स्थापना में हुई। हिन्दू समाज या भारतीय समाज के लोग ईसाई समाज में भी जाने लगे और वहां भी जाति व्यवस्था न होने के कारण उनकी पूर्व जाति ईसाई समाज में ही विलीन हो गई। यह तेरह शताब्दियों की कथा है और 13 शताब्दियों से निरंतर चल रही है।
21वीं शताब्दी में भारत सरकार भारतीय पंथ छोड़कर ईसाई या मुस्लिम समाज में चले गये लोगों की जाति की तलाश कर रही है। आठवीं शताब्दी में मुसलमान बन गए भारतीयों या हिन्दुओं को शायद अब अपनी उस जाति का पता भी नहीं होगा क्योंकि व्यवहार में वह लुप्त हो गई थी। परंतु भारत सरकार उनका पता लगाने के हठ पर अड़ी हुई है और यह हठ भी बड़ा अजीब है। सरकार उनकी जाति का पता लगाकर उनको सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने के लिए अड़ी हुई है और आश्चर्य की बात है कि जिन मौलवियों ने और पादरियों ने, इमामों ने और बिशपों ने कभी यह घोषणा की थी कि हमारे समाज में कोई जाति नहीं है। अब वही पादरी और बिशप अपने समाज में जाति तलाश रहे हैं और इतना ही नहीं, जाति है- इसके हठ पर भी अड़े हुए हैं।
इस पूरी रणनीति में सोनिया गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार इमामों और बिशपों के साथ खड़ी हो गई हैं। उसने इसी रणनीति के अंतर्गत उडीसा के एक सज्जन रंगनाथ मिश्र, जो कभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश भी रह चुके हैं और बाद में कांग्रेस की कृपा से 6 साल राज्यसभा का सुख भी भोग चुके हैं, की अगुवाई में आयोग की स्थापना कर दी और जैसा कि आशंका थी आयोग ने भारत सरकार की मंशा के अनुरूप ही यह सिफारिश कर दी है कि भारतीय पंथों को त्यागकर इस्लामी या ईसाई समाज में गए लोगों को भी अनुसूचित जातियों के भारतीयों के समान ही आरक्षण मिलना चाहिए।
ऊपर से देखने पर यह लगता है कि ईसाई अथवा इस्लामी समाज की सारी कवायद सरकारी नौकरियों में कुछ चंद स्थान पाने की है या फिर कुछ शिक्षा संस्थानों में कुछ छात्रों के भर्ती हो जाने की है। लेकिन ऊपर से यह षडयंत्र जितना सतही दिखाई देता है भीतर से उतना ही गहरा है। यह एक प्रकार से भारत की राज्यसत्ता पर कब्जा करने के लिए ईसाई और इस्लामी समाज द्वारा रची गई संयुक्त रणनीति है। जिसका संचालन पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी और उसके अदृश्य आका कर रहे लगते हैं। मुद्दा अत्यंत स्पष्ट है। एक बार यदि सिध्दांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि ईसाई अथवा इस्लामी समाज में भी जातियां हैं और उन जातियों में से भी कुछ को अनुसूचित श्रेणी में स्वीकार किया जाता है तो आगे सत्ता पर कब्जा करने के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। रिकार्ड के लिए रंगनाथ मिश्रा ने पहला अवरोध तो हटा ही दिया है। आयोग ने ईसाई और मुस्लिम समाज में अनुसूचित जातियों की कल्पना को यथार्थ मान लेने का आग्रह किया है।
भारतीय संविधान में, संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए हैं। यदि ईसाई और मुस्लिम समाज में भी अनुसूचित जातियों की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है तो जाहिर है कि दलित श्रेणियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा की इन सीटों पर ईसाई या मुसलमान पंथ के लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। ईसाई और मुस्लिम समाज को इससे दोहरा लाभ होगा। वे साधारण सीटों पर तो चुनाव लड़ ही सकेंगे इसके साथ ही वे आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे और जैसी भारत में राजनैतिक कारणों से मौलवी और पादरी की एकजुटता दिखाई दे रही है उसमें यह भी संभव है कि भविष्य में ये दोनों मिलकर एक रणनीति के अनुसार चुनाव लड़ें। केरल जैसे प्रदेश में जहां ईसाइयों और मुसलमानों की संख्या पर्याप्त है वहां इन पंथों के लोगों को यदि अनुसूचित जाति का लाभ भी दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि यह मिलकर केरल में सत्ता संभालने की स्थिति में आ सकते हैं । ऐसा प्रयोग कमोवेश असम और पश्चिमी बंगाल में भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड भी इस प्रयोग के अनोखे परिणाम दे सकता है। जिन शक्तियों ने अब जब सोनिया गांधी को केन्द्र में स्थापित कर दिया है वही शक्तियां राज्यों में इस्लामी और ईसाई पंथियों को सत्ता केन्द्रों तक पहुंचाने में जुटी हैं। रंगनाथ मिश्र आयोग उसी लंबे षडयंत्र की पहली कड़ी है। यदि इसको प्रारंभ में ही न तोड़ा गया तो भविष्य में इसके भयावह परिणाम निकल सकते हैं।
इसका एक और साइडइफेक्ट भी होगा। भारतीय समाज की दलित जातियों में इससे निराशा उत्पन्न होगी। आज तक उन्होंने इन विदेशी पंथों का जिस साहस और उत्साह से सामना किया है। उसमें निश्चय ही गिरावट आएगी। यह ध्यान रखना होगा कि मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ जो व्यापक संघर्ष हुए उनमें ज्यादा योगदान इन्हीं तथाकथित दलित जातियों का रहा है। इतने प्रलोभनों और भय के बावजूद दलित जातियों ने अपनी परंपरा और विरासत को नहीं त्यागा। वे व्यापक हिन्दू समाज के भीतर रहकर ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही। संकट की इन घड़ियों में इन तथाकथित दलित जातियों के जो बंधु अपनी बिरादरी छोड़कर ईसाई समाज या मुस्लिम समाज में चले गए उन्हें बिरादरी ने हिकारत की नजर से ही देखा। मध्यकालीन युग में तो उनका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार अब उन लोगों के साथ खड़ी नजर आ रही है जो संघर्ष काल में और संकट काल में अपनी बिरादरी को छोड़ गए थे।
जो संकट में और मुस्लिम आक्रांताओं के काल में और पादरियों के युग में भी अटल खड़े रहे उनके हितों पर सरकार कुठाराघात कर रही है। इससे संकट काल में लड़ने का भारतीय समाज का संकल्प टूटेगा और वह हतोत्साहित होगा। इसमें सोनिया गांधी को ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि शायद सोनिया गांधी की भारत में स्थापना ही उस संकल्प को तोड़ने के लिए हुई है जिसके बलबूते भारत आक्रमणों की इन अनेक शताब्दियों को सफलता पूर्वक झेल चुका है। परंतु पंडित रंगनाथ मिश्र को क्या कहा जाए?दुर्भाग्य से भारतीय इतिहास में रंगनाथ मिश्रों की भी परंपरा रही है। (नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
भारत सरकार भारतीय मजहबों को त्याग कर ईसाई और मुसलमान समाज में चले गए व्यक्तियों की जाति तलाशने के काम में जुटी हुई है। लेकिन समस्या यह है कि इस देश में जोर जबरदस्ती या लालच से भारतीय या हिन्दू समाज के लोगों को इस्लामी समाज के घेरे में लाने की कवायद काफी लंबे अरसे से हो रही है। इसकी शुरूआत मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों के पहले ही शुरू हो गई थी। ये लगभग सातवीं-आठवीं शताब्दी की घटनाएं हैं। उसके बाद लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक और मुगल जैसी अनेक इस्लामी सल्तनतें इस देश में स्थापित हुईं और हिन्दू समाज से इस्लामी समाज की होर जाने का सिलसिला भी चलता रहा। इस्लामी समाज में जाति व्यवस्था नहीं है। इसलिए पंथ परिवर्तन के बाद उनकी जाति इस्लामी समाज में ही विलीन हो गई। यही प्रक्रिया बाद में भारत में पुर्तगाल, डच और अंग्रेजों के आने के बाद ईसाई समाज की स्थापना में हुई। हिन्दू समाज या भारतीय समाज के लोग ईसाई समाज में भी जाने लगे और वहां भी जाति व्यवस्था न होने के कारण उनकी पूर्व जाति ईसाई समाज में ही विलीन हो गई। यह तेरह शताब्दियों की कथा है और 13 शताब्दियों से निरंतर चल रही है।
21वीं शताब्दी में भारत सरकार भारतीय पंथ छोड़कर ईसाई या मुस्लिम समाज में चले गये लोगों की जाति की तलाश कर रही है। आठवीं शताब्दी में मुसलमान बन गए भारतीयों या हिन्दुओं को शायद अब अपनी उस जाति का पता भी नहीं होगा क्योंकि व्यवहार में वह लुप्त हो गई थी। परंतु भारत सरकार उनका पता लगाने के हठ पर अड़ी हुई है और यह हठ भी बड़ा अजीब है। सरकार उनकी जाति का पता लगाकर उनको सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने के लिए अड़ी हुई है और आश्चर्य की बात है कि जिन मौलवियों ने और पादरियों ने, इमामों ने और बिशपों ने कभी यह घोषणा की थी कि हमारे समाज में कोई जाति नहीं है। अब वही पादरी और बिशप अपने समाज में जाति तलाश रहे हैं और इतना ही नहीं, जाति है- इसके हठ पर भी अड़े हुए हैं।
इस पूरी रणनीति में सोनिया गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार इमामों और बिशपों के साथ खड़ी हो गई हैं। उसने इसी रणनीति के अंतर्गत उडीसा के एक सज्जन रंगनाथ मिश्र, जो कभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश भी रह चुके हैं और बाद में कांग्रेस की कृपा से 6 साल राज्यसभा का सुख भी भोग चुके हैं, की अगुवाई में आयोग की स्थापना कर दी और जैसा कि आशंका थी आयोग ने भारत सरकार की मंशा के अनुरूप ही यह सिफारिश कर दी है कि भारतीय पंथों को त्यागकर इस्लामी या ईसाई समाज में गए लोगों को भी अनुसूचित जातियों के भारतीयों के समान ही आरक्षण मिलना चाहिए।
ऊपर से देखने पर यह लगता है कि ईसाई अथवा इस्लामी समाज की सारी कवायद सरकारी नौकरियों में कुछ चंद स्थान पाने की है या फिर कुछ शिक्षा संस्थानों में कुछ छात्रों के भर्ती हो जाने की है। लेकिन ऊपर से यह षडयंत्र जितना सतही दिखाई देता है भीतर से उतना ही गहरा है। यह एक प्रकार से भारत की राज्यसत्ता पर कब्जा करने के लिए ईसाई और इस्लामी समाज द्वारा रची गई संयुक्त रणनीति है। जिसका संचालन पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी और उसके अदृश्य आका कर रहे लगते हैं। मुद्दा अत्यंत स्पष्ट है। एक बार यदि सिध्दांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि ईसाई अथवा इस्लामी समाज में भी जातियां हैं और उन जातियों में से भी कुछ को अनुसूचित श्रेणी में स्वीकार किया जाता है तो आगे सत्ता पर कब्जा करने के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। रिकार्ड के लिए रंगनाथ मिश्रा ने पहला अवरोध तो हटा ही दिया है। आयोग ने ईसाई और मुस्लिम समाज में अनुसूचित जातियों की कल्पना को यथार्थ मान लेने का आग्रह किया है।
भारतीय संविधान में, संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए हैं। यदि ईसाई और मुस्लिम समाज में भी अनुसूचित जातियों की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है तो जाहिर है कि दलित श्रेणियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा की इन सीटों पर ईसाई या मुसलमान पंथ के लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। ईसाई और मुस्लिम समाज को इससे दोहरा लाभ होगा। वे साधारण सीटों पर तो चुनाव लड़ ही सकेंगे इसके साथ ही वे आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे और जैसी भारत में राजनैतिक कारणों से मौलवी और पादरी की एकजुटता दिखाई दे रही है उसमें यह भी संभव है कि भविष्य में ये दोनों मिलकर एक रणनीति के अनुसार चुनाव लड़ें। केरल जैसे प्रदेश में जहां ईसाइयों और मुसलमानों की संख्या पर्याप्त है वहां इन पंथों के लोगों को यदि अनुसूचित जाति का लाभ भी दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि यह मिलकर केरल में सत्ता संभालने की स्थिति में आ सकते हैं । ऐसा प्रयोग कमोवेश असम और पश्चिमी बंगाल में भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड भी इस प्रयोग के अनोखे परिणाम दे सकता है। जिन शक्तियों ने अब जब सोनिया गांधी को केन्द्र में स्थापित कर दिया है वही शक्तियां राज्यों में इस्लामी और ईसाई पंथियों को सत्ता केन्द्रों तक पहुंचाने में जुटी हैं। रंगनाथ मिश्र आयोग उसी लंबे षडयंत्र की पहली कड़ी है। यदि इसको प्रारंभ में ही न तोड़ा गया तो भविष्य में इसके भयावह परिणाम निकल सकते हैं।
इसका एक और साइडइफेक्ट भी होगा। भारतीय समाज की दलित जातियों में इससे निराशा उत्पन्न होगी। आज तक उन्होंने इन विदेशी पंथों का जिस साहस और उत्साह से सामना किया है। उसमें निश्चय ही गिरावट आएगी। यह ध्यान रखना होगा कि मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ जो व्यापक संघर्ष हुए उनमें ज्यादा योगदान इन्हीं तथाकथित दलित जातियों का रहा है। इतने प्रलोभनों और भय के बावजूद दलित जातियों ने अपनी परंपरा और विरासत को नहीं त्यागा। वे व्यापक हिन्दू समाज के भीतर रहकर ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही। संकट की इन घड़ियों में इन तथाकथित दलित जातियों के जो बंधु अपनी बिरादरी छोड़कर ईसाई समाज या मुस्लिम समाज में चले गए उन्हें बिरादरी ने हिकारत की नजर से ही देखा। मध्यकालीन युग में तो उनका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार अब उन लोगों के साथ खड़ी नजर आ रही है जो संघर्ष काल में और संकट काल में अपनी बिरादरी को छोड़ गए थे।
जो संकट में और मुस्लिम आक्रांताओं के काल में और पादरियों के युग में भी अटल खड़े रहे उनके हितों पर सरकार कुठाराघात कर रही है। इससे संकट काल में लड़ने का भारतीय समाज का संकल्प टूटेगा और वह हतोत्साहित होगा। इसमें सोनिया गांधी को ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि शायद सोनिया गांधी की भारत में स्थापना ही उस संकल्प को तोड़ने के लिए हुई है जिसके बलबूते भारत आक्रमणों की इन अनेक शताब्दियों को सफलता पूर्वक झेल चुका है। परंतु पंडित रंगनाथ मिश्र को क्या कहा जाए?दुर्भाग्य से भारतीय इतिहास में रंगनाथ मिश्रों की भी परंपरा रही है। (नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
Friday, 18 January 2008
अपने ही देश में हुए पराये

लेखक: डा. विवेक कुमार
कश्मीर घाटी में पहले छोटे-बड़े गैर मुस्लिम व्यापारियों को भगाया गया, फिर सदियों से रह रहे कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, अब पिछले दिनों गैर कश्मीरी मजदूरों पर गाज गिराई गई जो अभी भी निरंतर जारी है। जैस ए मुहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने घाटी में रह रहे गैर कश्मीरी श्रमिकों को एक सप्ताह के अंदर-अंदर घाटी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। इस अल्टीमेटम के पश्चात गैर-कश्मीरी श्रमिकों में भगदड़ सी मच गइ। उनका बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो चुका है। घाटी से बाहर जाने वाली बसों में जगह पाने के लिये श्रीनगर बस स्टैंड पर गैर कश्मीरी श्रमिकों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं।
एक ओर गैर कश्मीरी-श्रमिकों को भगाने की मुहिम है, दूसरी ओर पर्यटकों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। श्रीनगर में एक पर्यटक बस में धमाका किया गया, जिससे चार गुजराती, जो घाटी में सैर करने के लिये आये थे, मारे गये। अमरनाथ यत्रियों पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। कश्मीर में गैर-कश्मीरी श्रमिकों की संख्या लगभग तीन लाख है। वे पिछले कई वर्षों से कश्मीर की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बने हुए हैं। आतंकी संगठनों के अल्टीमेटम के पश्चात इनका घाटी में रहना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। श्रीनगर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस के एक अधिकारी के अनुसार अब तक हजारों गैर कश्मीरी श्रमिक घाटी छोड़ चुके हैं। गैर-कश्मीरी श्रमिकों को भगाने का जहरीला अभियान तो सर्वप्रथम हुरियत के सैयद गिलानी ने दिया था, जैश और हिजबुल ने इसे हवा ही नहीं दी बल्कि इस को तुरंत लागू करवाने के लिये फतवा भी निकाल दिया।
घाटी में गैर-कानूनी श्रमिक निर्माण कार्यों से जुड़े हुए हैं, रेहड़ियों पर दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें और साग-सब्जी बेचकर अपना पेट पालते हैं। यह सब आतंकवादियों को स्वीकार नहीं क्योंकि उनकी नजर में यह गरीब लोग अमीर कश्मीरियों को लूट रहे हैं। क्षेत्रवाद की यह समस्या कश्मीर घाटी में तो है ही असम में भी गैर असमियों के विरूध्द अभियान जारी है। गैर असमियों की हत्याएं हो रही हैं उनका अपहरण हो कर फिरौतियां वसूली जा रही हैं और उन्हें राज्य से पलायन के लिये विवश किया जा रहा है। सबसे अधिक निशाने पर वहां बिहारी श्रमिक और मारवाड़ी सेठ हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों नागालैंड और मिजोरम में जहां ईसाइयों का बोलबाला है वहां भारत के किसी दूसरे राज्य से आया व्यक्ति न तो घर बना सकता है और न ही मंदिर आदि। जो लोग वहां रहते भी हैं वे अपमान और प्रताड़ना का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दीवाली जैसे त्यौहार मनाने का कोई भी साहस नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में शिवसेना उत्तर भारतीयो को भगाने के लिये झंडा उठाए फिर रही हैं।
फिर भी हम अपने आप को धोखा देकर यह दावा कर रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से कटक तक भारत एक है जब कि कटु सत्य यह है कि भारत महान के कई क्षेत्रों में भारतीय परायो की तरह रहे हैं या फिर उन्हें पराया बना दिया गया है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? केवल हमारी सरकार। काश! पंडित नेहरू ने जम्मू-कश्मीरी को विशेष दर्जा देने की शेख अब्दुल्ला की मांग के आगे नतमस्तक होने से पूर्व इसके दूरगामी दुष्परिणामों की कल्पना की होती। यदि कांग्रेस सरकार की मूर्खताओं को बाद में आने वाली सरकारों ने कुछ सुधार लिया होता तो शायद लोग अपने ही देश में पराये नहीं हुए होते।
पिछले कुछ समय से पी.डी.पी. यह मांग करती आ रही है कि जम्मू-कश्मीर से सेना हटाई जाये। बाद में मुफती और उनकी पुत्री महबूबा ने यह भी धमकी दे डाली कि केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से सेना नहीं हटाई तो वे गठबंधन सरकार से बाहर निकल आयेगी। पी0डी0पी0 की इस मांग तथा धमकी पर सभी को हैरानी हुई थी क्योंकि सबसे पहले यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने उठाई थी और उसके बाद हुर्रियत का गरमपंथी अलगाववादी ग्रुप यह मांग उठाने लगा और अब पी0डी0पी0 ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाना शुरू कर दिया है। उसके चार मंत्री 28 फरवरी से तीन माह तक प्रदेश कैबिनेट की बैठकों का बहिष्कार करते रहे।
प्रदेश की सुरक्षा स्थितियों को देखते हुये भाजपा, नेशनल कान्फ्रैंस, पैंथर्स पार्टी तथा बड़ी संख्या में लोग वहां से सेना तथा सुरक्षा बलों को हटाए जाने के विरूध्द आवाज उठाते रहे हैं। गठबंधन सरकार बनाये रखने के चक्कर में पी0डी0पी0 की इस मांग के सामने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टैण्ड कुछ स्पष्ट न होने के कारण समस्या को और जटिल बना दिया है। हां! कुछ दिन पूर्व वहां के मुख्यमंत्री गुलाम नवी आजाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश की सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए सेना हटाना उचित नहीं है। एक तरफ पी0डी0पी0 नेता अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हैं। भारतीय नेताओं का यह दोहरा व्यवहार कब तक चलेगा?
स्थितियां विषम होने तथा उनसे देश को पहुंचने वाली हानि को देखते हुए कोई भी सरकार बड़े संकोच के साथ सेना तैनात करती है। सेना तथा सुरक्षा बलों के जवान बड़े परिश्रम से स्थितियों पर नियंत्रण करते हैं, आतंकवादियों तथा घुसपैठियों की धर-पकड़ करते हैं तथा इस काम में बहुत से जवान शहीद तथा घायल होते हैं। जब वे स्थिति नियंत्रण करने में सफल होते हैं तो सेना हटाओ की मांग जोर पकड़ने लगती है, हालात बिल्कुल ठीक हो जाने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेना का हटाया जाना ही उचित है परन्तु उससे पूर्व नहीं।
जिस प्रकार माओवादियों ने नेपाल में अपने पैर जमा लेने के बाद नेपाल की सीमा से लगते हुए भारत के 14 जिलों तथा अन्य 23 जिलों में भी पैर पसारना आरंभ कर दिया है, आगामी समय के लिये यह एक खतरे की घण्टी लग रही है। कुछ जिलों में समांतर सरकार चलाने का माओवादियों का खेल शुरू हो चका है। गांव-गांव में समस्त पुरूषों को जंगलों में ट्रेनिंग के लिये ले जाना माओवादियों के लिए आम बात हो गई हैं। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, विहार आदि में माओवादी, असम, नागालैंड, अरूणाचल, मिजोरम आदि ने क्रिश्चियन मिशनरी तथा माओवादी तथा नेपाल-बंगलादेश अदि को केन्द्र मानकर पाकिस्तान की आई0 एस0 आई0, जैश ए मुहम्मद तथा हिजबुल आदि तथा अन्य प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्रों द्वारा भारत को तोड़ने की कई कोशिशें युध्दस्तर पर चल रही हैं। इन कोशिशों के साथ-साथ चीन की विस्तारवादी-साम्राज्यवादी शक्ति भी तिब्बत पर काबिज होने के पश्चात तथा 1962 में भारत पर हजार वर्गमील क्षेत्र अपने अधीन करने के पश्चात अब उसकी नजर उत्तरपूर्व के पांचों राज्यों पर दिख रही है। पिछले दिनों अरूणाचल के एक भाग में चीन की सेना घुस आई थी। भारत की प्रतिरक्षा क्षमता अब कुछ ठीक होने के कारण वो वहां से खदेड़ दिये गये परन्तु चीन ने नक्शे के उस भूभाग को अपना क्षेत्र दिखाकर भारत को आगाह कर दिया है। चीन स्पष्ट रूप से कहता रहा है कि तिब्बत (हथेली) को प्राप्त कर लिया है अब उसे हथेली के साथ लगी पांच उंगलियां (असम, नागालैंड, अरूणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा) को भी प्राप्त करना है। क्या भारत मां के अंग कटने का यह क्रम कभी समाप्त होगा या जैसे ब्रह्म भारत गया व्रहद् भारत गया, 1947 का भारत गया, 1962 का भारत गया, अब क्या कश्मीर, उत्तरपूर्व तथा अन्य कई भाग जाने को तैयार नहीं बैठे? क्या केन्द्र की कोई सरकार इन प्रश्नों का उत्तर देगी? शायद नहीं। इनके पास कुछ उत्तर होता तो शायद यह सारे प्रश्न आज खड़े ही न होते।
कश्मीर घाटी तथा बाद में जम्मू प्रांत में हुए हिन्दुओं के पलायन से, अब पिछले दिनों नागालैंड से निकाले गये भारतीयों से तथा माओवादियों के प्रभाव वाले क्षेत्र से हो रहे पलायन से तथा आईएसआई के खतरनाक इरादों से और कुछ दिन पूर्व अलकायदा द्वारा कश्मीर में जारी एक टेप से तथा भीतर में पनप रहे कई प्रकार के असंतोष से निपटने के लिये केन्द्र में एक राष्ट्रवादी सोच तथा दृढ़ संकल्प वाली सरकार ही इन प्रश्नों का उत्तर शायद दे पाये। (नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
कश्मीर घाटी में पहले छोटे-बड़े गैर मुस्लिम व्यापारियों को भगाया गया, फिर सदियों से रह रहे कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, अब पिछले दिनों गैर कश्मीरी मजदूरों पर गाज गिराई गई जो अभी भी निरंतर जारी है। जैस ए मुहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने घाटी में रह रहे गैर कश्मीरी श्रमिकों को एक सप्ताह के अंदर-अंदर घाटी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। इस अल्टीमेटम के पश्चात गैर-कश्मीरी श्रमिकों में भगदड़ सी मच गइ। उनका बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो चुका है। घाटी से बाहर जाने वाली बसों में जगह पाने के लिये श्रीनगर बस स्टैंड पर गैर कश्मीरी श्रमिकों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं।
एक ओर गैर कश्मीरी-श्रमिकों को भगाने की मुहिम है, दूसरी ओर पर्यटकों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। श्रीनगर में एक पर्यटक बस में धमाका किया गया, जिससे चार गुजराती, जो घाटी में सैर करने के लिये आये थे, मारे गये। अमरनाथ यत्रियों पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। कश्मीर में गैर-कश्मीरी श्रमिकों की संख्या लगभग तीन लाख है। वे पिछले कई वर्षों से कश्मीर की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बने हुए हैं। आतंकी संगठनों के अल्टीमेटम के पश्चात इनका घाटी में रहना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। श्रीनगर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस के एक अधिकारी के अनुसार अब तक हजारों गैर कश्मीरी श्रमिक घाटी छोड़ चुके हैं। गैर-कश्मीरी श्रमिकों को भगाने का जहरीला अभियान तो सर्वप्रथम हुरियत के सैयद गिलानी ने दिया था, जैश और हिजबुल ने इसे हवा ही नहीं दी बल्कि इस को तुरंत लागू करवाने के लिये फतवा भी निकाल दिया।
घाटी में गैर-कानूनी श्रमिक निर्माण कार्यों से जुड़े हुए हैं, रेहड़ियों पर दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें और साग-सब्जी बेचकर अपना पेट पालते हैं। यह सब आतंकवादियों को स्वीकार नहीं क्योंकि उनकी नजर में यह गरीब लोग अमीर कश्मीरियों को लूट रहे हैं। क्षेत्रवाद की यह समस्या कश्मीर घाटी में तो है ही असम में भी गैर असमियों के विरूध्द अभियान जारी है। गैर असमियों की हत्याएं हो रही हैं उनका अपहरण हो कर फिरौतियां वसूली जा रही हैं और उन्हें राज्य से पलायन के लिये विवश किया जा रहा है। सबसे अधिक निशाने पर वहां बिहारी श्रमिक और मारवाड़ी सेठ हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों नागालैंड और मिजोरम में जहां ईसाइयों का बोलबाला है वहां भारत के किसी दूसरे राज्य से आया व्यक्ति न तो घर बना सकता है और न ही मंदिर आदि। जो लोग वहां रहते भी हैं वे अपमान और प्रताड़ना का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दीवाली जैसे त्यौहार मनाने का कोई भी साहस नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में शिवसेना उत्तर भारतीयो को भगाने के लिये झंडा उठाए फिर रही हैं।
फिर भी हम अपने आप को धोखा देकर यह दावा कर रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से कटक तक भारत एक है जब कि कटु सत्य यह है कि भारत महान के कई क्षेत्रों में भारतीय परायो की तरह रहे हैं या फिर उन्हें पराया बना दिया गया है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? केवल हमारी सरकार। काश! पंडित नेहरू ने जम्मू-कश्मीरी को विशेष दर्जा देने की शेख अब्दुल्ला की मांग के आगे नतमस्तक होने से पूर्व इसके दूरगामी दुष्परिणामों की कल्पना की होती। यदि कांग्रेस सरकार की मूर्खताओं को बाद में आने वाली सरकारों ने कुछ सुधार लिया होता तो शायद लोग अपने ही देश में पराये नहीं हुए होते।
पिछले कुछ समय से पी.डी.पी. यह मांग करती आ रही है कि जम्मू-कश्मीर से सेना हटाई जाये। बाद में मुफती और उनकी पुत्री महबूबा ने यह भी धमकी दे डाली कि केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से सेना नहीं हटाई तो वे गठबंधन सरकार से बाहर निकल आयेगी। पी0डी0पी0 की इस मांग तथा धमकी पर सभी को हैरानी हुई थी क्योंकि सबसे पहले यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने उठाई थी और उसके बाद हुर्रियत का गरमपंथी अलगाववादी ग्रुप यह मांग उठाने लगा और अब पी0डी0पी0 ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाना शुरू कर दिया है। उसके चार मंत्री 28 फरवरी से तीन माह तक प्रदेश कैबिनेट की बैठकों का बहिष्कार करते रहे।
प्रदेश की सुरक्षा स्थितियों को देखते हुये भाजपा, नेशनल कान्फ्रैंस, पैंथर्स पार्टी तथा बड़ी संख्या में लोग वहां से सेना तथा सुरक्षा बलों को हटाए जाने के विरूध्द आवाज उठाते रहे हैं। गठबंधन सरकार बनाये रखने के चक्कर में पी0डी0पी0 की इस मांग के सामने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टैण्ड कुछ स्पष्ट न होने के कारण समस्या को और जटिल बना दिया है। हां! कुछ दिन पूर्व वहां के मुख्यमंत्री गुलाम नवी आजाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश की सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए सेना हटाना उचित नहीं है। एक तरफ पी0डी0पी0 नेता अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हैं। भारतीय नेताओं का यह दोहरा व्यवहार कब तक चलेगा?
स्थितियां विषम होने तथा उनसे देश को पहुंचने वाली हानि को देखते हुए कोई भी सरकार बड़े संकोच के साथ सेना तैनात करती है। सेना तथा सुरक्षा बलों के जवान बड़े परिश्रम से स्थितियों पर नियंत्रण करते हैं, आतंकवादियों तथा घुसपैठियों की धर-पकड़ करते हैं तथा इस काम में बहुत से जवान शहीद तथा घायल होते हैं। जब वे स्थिति नियंत्रण करने में सफल होते हैं तो सेना हटाओ की मांग जोर पकड़ने लगती है, हालात बिल्कुल ठीक हो जाने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेना का हटाया जाना ही उचित है परन्तु उससे पूर्व नहीं।
जिस प्रकार माओवादियों ने नेपाल में अपने पैर जमा लेने के बाद नेपाल की सीमा से लगते हुए भारत के 14 जिलों तथा अन्य 23 जिलों में भी पैर पसारना आरंभ कर दिया है, आगामी समय के लिये यह एक खतरे की घण्टी लग रही है। कुछ जिलों में समांतर सरकार चलाने का माओवादियों का खेल शुरू हो चका है। गांव-गांव में समस्त पुरूषों को जंगलों में ट्रेनिंग के लिये ले जाना माओवादियों के लिए आम बात हो गई हैं। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, विहार आदि में माओवादी, असम, नागालैंड, अरूणाचल, मिजोरम आदि ने क्रिश्चियन मिशनरी तथा माओवादी तथा नेपाल-बंगलादेश अदि को केन्द्र मानकर पाकिस्तान की आई0 एस0 आई0, जैश ए मुहम्मद तथा हिजबुल आदि तथा अन्य प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्रों द्वारा भारत को तोड़ने की कई कोशिशें युध्दस्तर पर चल रही हैं। इन कोशिशों के साथ-साथ चीन की विस्तारवादी-साम्राज्यवादी शक्ति भी तिब्बत पर काबिज होने के पश्चात तथा 1962 में भारत पर हजार वर्गमील क्षेत्र अपने अधीन करने के पश्चात अब उसकी नजर उत्तरपूर्व के पांचों राज्यों पर दिख रही है। पिछले दिनों अरूणाचल के एक भाग में चीन की सेना घुस आई थी। भारत की प्रतिरक्षा क्षमता अब कुछ ठीक होने के कारण वो वहां से खदेड़ दिये गये परन्तु चीन ने नक्शे के उस भूभाग को अपना क्षेत्र दिखाकर भारत को आगाह कर दिया है। चीन स्पष्ट रूप से कहता रहा है कि तिब्बत (हथेली) को प्राप्त कर लिया है अब उसे हथेली के साथ लगी पांच उंगलियां (असम, नागालैंड, अरूणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा) को भी प्राप्त करना है। क्या भारत मां के अंग कटने का यह क्रम कभी समाप्त होगा या जैसे ब्रह्म भारत गया व्रहद् भारत गया, 1947 का भारत गया, 1962 का भारत गया, अब क्या कश्मीर, उत्तरपूर्व तथा अन्य कई भाग जाने को तैयार नहीं बैठे? क्या केन्द्र की कोई सरकार इन प्रश्नों का उत्तर देगी? शायद नहीं। इनके पास कुछ उत्तर होता तो शायद यह सारे प्रश्न आज खड़े ही न होते।
कश्मीर घाटी तथा बाद में जम्मू प्रांत में हुए हिन्दुओं के पलायन से, अब पिछले दिनों नागालैंड से निकाले गये भारतीयों से तथा माओवादियों के प्रभाव वाले क्षेत्र से हो रहे पलायन से तथा आईएसआई के खतरनाक इरादों से और कुछ दिन पूर्व अलकायदा द्वारा कश्मीर में जारी एक टेप से तथा भीतर में पनप रहे कई प्रकार के असंतोष से निपटने के लिये केन्द्र में एक राष्ट्रवादी सोच तथा दृढ़ संकल्प वाली सरकार ही इन प्रश्नों का उत्तर शायद दे पाये। (नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
Thursday, 17 January 2008
मार्क्सवादियों की हिंदी मंडली
लेखक- शंकर शरण
अभी किसी संगोष्ठी में एक जाने-माने हिंदी मार्क्सवादी ने कहा कि दुनिया में हर जगह सबसे बड़े राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट ही हुए हैं। यह भी कि हर राजनीतिक प्रणाली तानाशाही होती है अत: कम्युनिस्ट शासनों को अलग से तानाशाही कहना ठीक नहीं। उनके अनुसार मार्क्सवाद का लक्ष्य वही था जो पहले भारतीय शास्त्रों में सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया:... के रूप में कहा गया। उन्होंने दस मिनट के अंदर ऐसी अनेक बेजोड़ बातें कहीं। इससे पता चलता है कि आखिर हिंदी वाले मार्क्सवादी कैसे बिना किसी शंका-शर्म के मार्क्सवाद का बिल्ला आज भी लहराते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता भयंकर अंधविश्वास और घोर अज्ञान में डूबी है। वे मार्क्सीय विचार का म नहीं जानते, मगर प्रतिष्टिंत मार्क्सवादी हैं! इनके ही भरोसे हिंदी के विद्यार्थी मार्क्सवादी या उसके हमदर्द बनते रहे। इस तरह यह अज्ञानी संप्रदाय हिंदी समाज को डुबा रहा है।
-- यह बड़ी मोटी सी बात है कि इस्लाम की तरह मार्क्सीय विचार में भी अंतर्राष्ट्रीयतावाद एक मूल सिध्दांत है। इसमें भी राष्ट्रवाद को सदैव एक दोष या भटकाव माना गया। इसीलिए कम्युनिस्टों की आपसी बहस में राष्ट्रवादी कहलाना गाली जैसा रहा है। कार्ल मार्क्स के शब्दों में, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। जब देश ही नहीं, तो देशभक्ति कैसी। लेनिन ने द्वितीय इंटरनेशनल को खारिज कर 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इसीलिए बनाया था क्योंकि उनके ख्याल में यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियां राष्ट्रवादी हो गई थीं। पश्चिमी में अपने देश के खिलाफ सोवियत संघ के लिए जासूसी करने वाले अधिकांश लोग संबंधित देशों के कम्युनिस्ट ही थे। भारत में भी, कम्युनिस्टों ने 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन से द्रोह एवं अंग्रेजों से सहयोग सोवियत संघ को मदद पहुँचाने की चाह से किया। फिर 1943 में (मुस्लिम आत्मनिर्णय का अधिकार कह कर) भारत के विभाजन का मौलिक सिध्दांत कम्युनिस्ट पार्टी ने ही दिया था। उसके लिए गढ़ी गई विस्तृत अधिकारी थीसिस क्या राष्ट्रवाद का दस्तावेज था। उस एक थीसिस ने भारत को जितना तबाह किया, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं, किंतु हिंदी मार्क्सवादी इस घोर-सांप्रदायिक अतीत के बावजूद धर्म-निरपेक्ष हैं! भारतीय कम्युनिस्टों के लिए 1942 और 1943 कोई पहला या अंतिम राष्ट्र-विरोधी कारनामा नहीं था। उससे पहले भी उनकी नीतियाँ कोमिंटर्न या स्तालिन के कहने पर तय होती थीं।
-- राष्ट्रीय नेताओं या कांग्रेस का चरित्र हमारे कम्युनिस्ट अपनी अक्ल से नहीं, अपने रूसी या ब्रिटिश कामरेडों की बुध्दि से तय करते रहे। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही कम्युनिस्ट भी काम करते थे। उससे वे निकाले क्यों गए। इसलिए कि कोमिंटर्न की लाइन के अनुरूप वे छल से कांग्रेस का नेतृत्व हड़पने के लिए उद्योग कर रहे थे, न कि राष्ट्रीय आंदोलन को मदद देने के लिए। इसी तरह 1962 में चीनी आक्रमण का बचाव करने के लिए ही कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुई। जो लोग अलग होकर माकपा (सीपीएम) बने, उन्होंने कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयता के नशे में नेहरू सरकार को ही दोषी बताया। यह न मानने के कारण ही भाकपा (सीपीआई) को राष्ट्रवादी भटकाव की शिकार दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी कहकर दो दशक तक निंदित किया गया। वस्तुत: पूरे एशिया में कम्युनिस्ट आंदोलन का ग्राफ दिखाता है कि राष्ट्रवादी भावनाओं से दूर होने के कारण ही वह लोगों की सहानुभूति खोता गया। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपने देश के राष्ट्रवादियों के साथ केवल एक छोटी अवधि तक ही रहीं। वह भी कोमिंटर्न के इशारे पर ही। इसी दौर में उन्हें कुछ लोकप्रियता भी मिली। लेकिन चूँकि राष्ट्रवाद उनकी निष्ठा नहीं थी, इसलिए जैसे-जैसे यह साफ होता गया, लोग उनसे दूर होते गए।
-- कम्युनिस्टों को देश से कभी मतलब न था, उन्हें हर हाल में केवल विश्व में साम्यवादी सत्ता के लिए जोड़-तोड़ षडयंत्र करना था। इसीलिए वे देश की चिंता से कभी एकाकार नहीं हुए। अंतर्राष्ट्रीयतावादी फिक्र में उनका मुख्य शत्रु अमेरिका और एकमात्र पितृभूमि सोवियत संघ या लाल चीन था। अपना देश उनकी गिनती में हमेशा बाद में आता था। सोवियत संघ के समीकरणों से उनकी नीतियाँ बनती थीं, न कि अपने देश-हित के लिए। जब बार-बार अनुभव से जनता ने यह समझ लिया, तब से लोकतांत्रिक देशों में कम्युनिस्टों की स्थिति एक सीमित संप्रदाय की हो गई। जिस पर देश-हित के लिए कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। केवल भारतीय कम्युनिस्टों ने मुस्लिम आत्मनिर्णय के नाम पर देश को नहीं तोड़ा। जर्मनी, कोरिया और यमन में भी उन्होंने अपने-अपने देशों का विखंडन किया। स्पष्टंत: उनके लिए वर्ग-संघर्ष के समक्ष राष्ट्रीय एकता, अखंडता या सहमति का कोई अर्थ न था। मगर सैध्दांतिक, व्यावहारिक तथ्यों, अनुभवों से अनजान हिंदी का मार्क्सवादी कम्युनिस्टों को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मान उनका भक्त बना हुआ है! उसके लिए सबका कल्याण ही मार्क्सवाद है। उसके लिए निजी संपत्ति का खात्मा, पूँजीपति वर्ग का विनाश, वर्ग-युध्द, क्रांतिकारी हिंसा आदि संकल्पनाओं का अस्तित्व नहीं। कितनी हैरत की बात है कि जो सिध्दांत डंके की चोट पर मानवता के एक हिस्से को खूँरेजी से मिटाने की बात करता है उसे कोई सबका कल्याण चाहने वाला बताए! 1989 में पूर्वी यूरोप में जनता ने तमाम कम्युनिस्ट तानाशाहियों को रातो-रात गद्दी से खींच उतारा। उनसे लोगों को कितनी घृणा थी, इसके रोचक दृश्य सारी दुनिया ने टेलीविजन पर देखे, मगर हिंदी मार्क्सवादी के लिए सभी शासन तानाशाही हैं।
-- हिंदी मार्क्सवादी के लिए सभा-संगठन की आजादी, मुक्त प्रेस, स्वतंत्र न्यायालय, वयस्क मताधिकार आदि के होने या न होने में कोई अंतर नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में मार्क्सवादी मंडली हर कहीं, हर विषय पर अनर्गल प्रवचन देती दिखती है। उसे किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं। बस उसके बारे में कुछ-न-कुछ मान लेने की जरूरत है। कुछ न जानकर भी सर्व-ज्ञानी होने का अंदाज- ऐसा विचित्र दृश्य हिंदी मार्क्सवादी जगत के सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने अपनी सदिच्छाओं को मार्क्सवादी पर आरोपित कर उसे बाजार में चलाया, लेकिन जैसा कि निर्मल वर्मा ने कहीं लिखा है कि जिन्होंने मार्क्स, लेनिन आदि के लेखन को सचमुच पढ़ने-समझने का कष्टं किया, वे निश्चित रूप से मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन से दूर होते गए। हिंदी बौध्दिकता में आज भी मार्क्सवाद की प्रतिष्ठा का रहस्य इसी टिप्पणी में छिपा हुआ है।
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।
अभी किसी संगोष्ठी में एक जाने-माने हिंदी मार्क्सवादी ने कहा कि दुनिया में हर जगह सबसे बड़े राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट ही हुए हैं। यह भी कि हर राजनीतिक प्रणाली तानाशाही होती है अत: कम्युनिस्ट शासनों को अलग से तानाशाही कहना ठीक नहीं। उनके अनुसार मार्क्सवाद का लक्ष्य वही था जो पहले भारतीय शास्त्रों में सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया:... के रूप में कहा गया। उन्होंने दस मिनट के अंदर ऐसी अनेक बेजोड़ बातें कहीं। इससे पता चलता है कि आखिर हिंदी वाले मार्क्सवादी कैसे बिना किसी शंका-शर्म के मार्क्सवाद का बिल्ला आज भी लहराते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता भयंकर अंधविश्वास और घोर अज्ञान में डूबी है। वे मार्क्सीय विचार का म नहीं जानते, मगर प्रतिष्टिंत मार्क्सवादी हैं! इनके ही भरोसे हिंदी के विद्यार्थी मार्क्सवादी या उसके हमदर्द बनते रहे। इस तरह यह अज्ञानी संप्रदाय हिंदी समाज को डुबा रहा है।
-- यह बड़ी मोटी सी बात है कि इस्लाम की तरह मार्क्सीय विचार में भी अंतर्राष्ट्रीयतावाद एक मूल सिध्दांत है। इसमें भी राष्ट्रवाद को सदैव एक दोष या भटकाव माना गया। इसीलिए कम्युनिस्टों की आपसी बहस में राष्ट्रवादी कहलाना गाली जैसा रहा है। कार्ल मार्क्स के शब्दों में, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। जब देश ही नहीं, तो देशभक्ति कैसी। लेनिन ने द्वितीय इंटरनेशनल को खारिज कर 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इसीलिए बनाया था क्योंकि उनके ख्याल में यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियां राष्ट्रवादी हो गई थीं। पश्चिमी में अपने देश के खिलाफ सोवियत संघ के लिए जासूसी करने वाले अधिकांश लोग संबंधित देशों के कम्युनिस्ट ही थे। भारत में भी, कम्युनिस्टों ने 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन से द्रोह एवं अंग्रेजों से सहयोग सोवियत संघ को मदद पहुँचाने की चाह से किया। फिर 1943 में (मुस्लिम आत्मनिर्णय का अधिकार कह कर) भारत के विभाजन का मौलिक सिध्दांत कम्युनिस्ट पार्टी ने ही दिया था। उसके लिए गढ़ी गई विस्तृत अधिकारी थीसिस क्या राष्ट्रवाद का दस्तावेज था। उस एक थीसिस ने भारत को जितना तबाह किया, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं, किंतु हिंदी मार्क्सवादी इस घोर-सांप्रदायिक अतीत के बावजूद धर्म-निरपेक्ष हैं! भारतीय कम्युनिस्टों के लिए 1942 और 1943 कोई पहला या अंतिम राष्ट्र-विरोधी कारनामा नहीं था। उससे पहले भी उनकी नीतियाँ कोमिंटर्न या स्तालिन के कहने पर तय होती थीं।
-- राष्ट्रीय नेताओं या कांग्रेस का चरित्र हमारे कम्युनिस्ट अपनी अक्ल से नहीं, अपने रूसी या ब्रिटिश कामरेडों की बुध्दि से तय करते रहे। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही कम्युनिस्ट भी काम करते थे। उससे वे निकाले क्यों गए। इसलिए कि कोमिंटर्न की लाइन के अनुरूप वे छल से कांग्रेस का नेतृत्व हड़पने के लिए उद्योग कर रहे थे, न कि राष्ट्रीय आंदोलन को मदद देने के लिए। इसी तरह 1962 में चीनी आक्रमण का बचाव करने के लिए ही कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुई। जो लोग अलग होकर माकपा (सीपीएम) बने, उन्होंने कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयता के नशे में नेहरू सरकार को ही दोषी बताया। यह न मानने के कारण ही भाकपा (सीपीआई) को राष्ट्रवादी भटकाव की शिकार दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी कहकर दो दशक तक निंदित किया गया। वस्तुत: पूरे एशिया में कम्युनिस्ट आंदोलन का ग्राफ दिखाता है कि राष्ट्रवादी भावनाओं से दूर होने के कारण ही वह लोगों की सहानुभूति खोता गया। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपने देश के राष्ट्रवादियों के साथ केवल एक छोटी अवधि तक ही रहीं। वह भी कोमिंटर्न के इशारे पर ही। इसी दौर में उन्हें कुछ लोकप्रियता भी मिली। लेकिन चूँकि राष्ट्रवाद उनकी निष्ठा नहीं थी, इसलिए जैसे-जैसे यह साफ होता गया, लोग उनसे दूर होते गए।
-- कम्युनिस्टों को देश से कभी मतलब न था, उन्हें हर हाल में केवल विश्व में साम्यवादी सत्ता के लिए जोड़-तोड़ षडयंत्र करना था। इसीलिए वे देश की चिंता से कभी एकाकार नहीं हुए। अंतर्राष्ट्रीयतावादी फिक्र में उनका मुख्य शत्रु अमेरिका और एकमात्र पितृभूमि सोवियत संघ या लाल चीन था। अपना देश उनकी गिनती में हमेशा बाद में आता था। सोवियत संघ के समीकरणों से उनकी नीतियाँ बनती थीं, न कि अपने देश-हित के लिए। जब बार-बार अनुभव से जनता ने यह समझ लिया, तब से लोकतांत्रिक देशों में कम्युनिस्टों की स्थिति एक सीमित संप्रदाय की हो गई। जिस पर देश-हित के लिए कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। केवल भारतीय कम्युनिस्टों ने मुस्लिम आत्मनिर्णय के नाम पर देश को नहीं तोड़ा। जर्मनी, कोरिया और यमन में भी उन्होंने अपने-अपने देशों का विखंडन किया। स्पष्टंत: उनके लिए वर्ग-संघर्ष के समक्ष राष्ट्रीय एकता, अखंडता या सहमति का कोई अर्थ न था। मगर सैध्दांतिक, व्यावहारिक तथ्यों, अनुभवों से अनजान हिंदी का मार्क्सवादी कम्युनिस्टों को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मान उनका भक्त बना हुआ है! उसके लिए सबका कल्याण ही मार्क्सवाद है। उसके लिए निजी संपत्ति का खात्मा, पूँजीपति वर्ग का विनाश, वर्ग-युध्द, क्रांतिकारी हिंसा आदि संकल्पनाओं का अस्तित्व नहीं। कितनी हैरत की बात है कि जो सिध्दांत डंके की चोट पर मानवता के एक हिस्से को खूँरेजी से मिटाने की बात करता है उसे कोई सबका कल्याण चाहने वाला बताए! 1989 में पूर्वी यूरोप में जनता ने तमाम कम्युनिस्ट तानाशाहियों को रातो-रात गद्दी से खींच उतारा। उनसे लोगों को कितनी घृणा थी, इसके रोचक दृश्य सारी दुनिया ने टेलीविजन पर देखे, मगर हिंदी मार्क्सवादी के लिए सभी शासन तानाशाही हैं।
-- हिंदी मार्क्सवादी के लिए सभा-संगठन की आजादी, मुक्त प्रेस, स्वतंत्र न्यायालय, वयस्क मताधिकार आदि के होने या न होने में कोई अंतर नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में मार्क्सवादी मंडली हर कहीं, हर विषय पर अनर्गल प्रवचन देती दिखती है। उसे किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं। बस उसके बारे में कुछ-न-कुछ मान लेने की जरूरत है। कुछ न जानकर भी सर्व-ज्ञानी होने का अंदाज- ऐसा विचित्र दृश्य हिंदी मार्क्सवादी जगत के सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने अपनी सदिच्छाओं को मार्क्सवादी पर आरोपित कर उसे बाजार में चलाया, लेकिन जैसा कि निर्मल वर्मा ने कहीं लिखा है कि जिन्होंने मार्क्स, लेनिन आदि के लेखन को सचमुच पढ़ने-समझने का कष्टं किया, वे निश्चित रूप से मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन से दूर होते गए। हिंदी बौध्दिकता में आज भी मार्क्सवाद की प्रतिष्ठा का रहस्य इसी टिप्पणी में छिपा हुआ है।
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।
तसलीमा नसरीन और मार्क्सवाद का नकली चेहरा
वर्ष 2007 के अन्त में सत्ता के गलियारों में जिन मुद्दों ने खासी हलचल मचाई उनमे बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन को लेकर उठा विवाद खासा अहम रहा। उपरी तौर पर भले ही यह मामला शांत लग रहा हो मगर हकीकत में यह शांति क्षणिक है। बंगाल के मार्क्सवादियों ने तसलीमा को लेकर जो चिंगारी भड़काई है वह किसी भी वक्त भङक सकती है। इसी बात को लेकर केन्द्र की सत्ता पर काबिज कुछ कथित धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले नेता बहुत अधिक चिंतित हैं।
अपने देश से निकाले जाने के बाद तसलीमा ने यह सोच कर भारत में शरण लेने का फैसला किया था कि कम से कम यहाँ उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रह सकेगी। कोलकाता आकर उन्होंने समझा कि उन्हें उनका घर मिल गया। दुनिया भर के साहित्य-संस्कृति प्रेमियों के लिए कोलकाता हमेशा से आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस शहर में आज भी वैसी बहुत सी चीजें विद्यमान हैं जो यहाँ आने वालों को अपनी जङों की ओर मुङने की प्रेरणा देती हैं। मुक्त चिंतन और बेबाक अभिव्यक्ति यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है। इस शहर की सांस्कृतिक विशेषताओं को उदाहरण देकर समझाना बहुत कठिन है। लेकिन तसलीमा के शहर में आने के बाद से ये विशेष ताएँ धूमिल होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान दौर में राजनीति संस्कृति से ज्यादा ताकतवर है। कोलकाता में तसलीमा भी कुत्सित राजनीति की शिकार हुई।
प. बंगाल में पिछले तीस वर्षों से सत्ता का नेतृत्व कर रहे मार्क्सवादियों को जब ऐसा लगा कि नन्दीग्राम और सिंगूर मामलों के कारण उनकी जागीर छिन सकती है, तो उन्होंने एक ऐसे मुद्दे की तलाश शुरु की जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके ताकि, नन्दीग्राम में पार्टी कैडरों द्वारा चलाया जा रहा खूनी अभियान किसी की नजर में न आ सके। इसके लिए उस वक्त तसलीमा से बेहतर कोई मुद्दा नहीं था। सुनियोजित तरीके से यह मुद्दा भड़का और ऐसा भड़का कि उसे संभालने में सबसे ज्यादा तकलीफ भड़काने वालों को ही हुई। विगत 21 नवंबर को तसलीमा को लेकर कोलकाता में जो कुछ हुआ उसे देख कर देश-विदेश के वे बुध्दिजीवी अचम्भित थे जो कोलकाता की खूबियों को जानते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में कोलकाता को मुक्तचिंतन की सरजमीं माना जाता है। उस घटना के बाद जिस प्रकार प. बंगाल सरकार ने तसलीमा को कोलकाता छोङने के लिए विवश किया वह मुक्तचिंतन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति माक्र्सवादियों की कुण्ठा को उजागर करता है। एक कपङे में कोलकाता से जयपुर पहुँची तसलीमा को इस बात से भी अन्जान रखा गया कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और यह सब हुआ मुट्ठी भर धर्मांन्धों की उच्छृंखलता के कारण। तसलीमा को लेकर अचानक कोलकाता में ऐसी परिस्थिति का सृजन किया गया जिसे नियंत्रित करने के लिए सेना बुलानी पङी और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाने पङे। आनन-फानन में राज्य सरकार ने तसलीमा को सुरक्षा देने में असमर्थता प्रकट कर दी और तसलीमा को शहर छोङना पङा। कोलकाता से जयपुर और फिर वहाँ से दिल्ली का अज्ञातवास। इतनी खींचतान से परेशान तसलीमा ने बाद में अपनी लेखनी पर खेद प्रकट किया। कई लोगों ने कहा - तसलीमा हार चुकी हैं। लेकिन सही मायनो में इस पूरे प्रकरण से पराजय तसलीमा की नहीं हुई बल्कि पराजित हुई प. बंगाल की मार्क्सवादी सरकार। जो सरकार एक शरणार्थी को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही हो उसे पराजित ही माना जाएगा। लेकिन राज्य सरकार को अपनी पराजय का अहसास तक नहीं है। यहाँ के माक्र्सवादी तसलीमा को कोलकाता से बाहर कर इस खुशफहमी के शिकार हैं कि इससे उनका मुसलमान वोट बैंक जो नन्दीग्राम के कारण खिसक चुका था कुछ हद तक मजबूत होगा। लेकिन वे इस बात से बेखबर हैं कि तसलीमा को कोलकाता से बाहर करने की जल्दबाजी में उन्होंने जो कदम उठाए उनसे सरकार की छवि को कितना नुकसान पहुँचा है।
तसलीमा को मीडिया और उनके आलोचकों ने विवादास्पद लेखिका का खिताब दिया है। वे विवादास्पद क्यों है? सिर्फ इसलिए कि इस्लाम को लेकर उनकी सोच औरों से अलग है। लेकिन इस बात से सभी सहमत होंगे कि किसी भी विषय-वस्तु को देखने, समझने और उसका विश्लेषण करने का हर आदमी का तरीका अलग-अलग होता है। तसलीमा नसरीन एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने अपनी लेखनी में उन मुद्दों को मुक्तचिंतन से जोङने की कोशिश की है जिन पर उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। किसी भी मुद्दे पर दुनिया के हर आदमी की राय एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन सभी को अपनी राय जाहिर करने का हक तो है। यदि तसलीमा को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है तो उन्हें विवादास्पद कहा जाना कहाँ तक उचित है? कोई लेखक क्या लिख रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह देखना है कि उसकी लेखनी में कलात्मक अनुशासन है या नहीं। तसलीमा ने अपनी लेखनी में कम से कम इस अनुशासन का पालन जरूर किया है। कला जगत की जानी-मानी हस्ती चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आङ में कलात्मक अनुशासन की सारी हदें तोङ दी थी। इसके बावजूद उन्हें कभी विवादास्पद चित्रकार नहीं कहा गया।
शायद माकपा नेता अभी भी इस गलतफहमी में हैं कि जनता को झूठ का आईना दिखाकर सच पर पर्दा डाला जा सकता है। वे जनता को भ्रमित करने की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। तसलीमा प्रकरण भी उनकी इसी रणनीति का एक हिस्सा था। लेकिन इस कोशिश में उनकी अपनी कमजोरिया ही उजागर हुई। सरकार के लिए इससे बङी विफलता और क्या होगी कि वह कुछ सौ लोगों की धमकियों से डर गई। तसलीमा को बांग्लादेश में भी इस तरह की धमकियों का सामना करना पङा था। लेकिन वे भयभीत नहीं हुई। भयभीत हुई वहाँ की सरकार, और अब प. बंगाल की मार्क्सवादी सरकार। इस सरकार ने आतातायियों की भीड़ के समक्ष आत्मसमर्पण कर खुद अपनी औकात दिखा दी। बेसहारों को सहारा देने का दम भरने वाले मार्क्सवादियों के लिए यह बड़े शर्म का विषय है।
संतोष कुमार मधुप (नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
अपने देश से निकाले जाने के बाद तसलीमा ने यह सोच कर भारत में शरण लेने का फैसला किया था कि कम से कम यहाँ उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रह सकेगी। कोलकाता आकर उन्होंने समझा कि उन्हें उनका घर मिल गया। दुनिया भर के साहित्य-संस्कृति प्रेमियों के लिए कोलकाता हमेशा से आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस शहर में आज भी वैसी बहुत सी चीजें विद्यमान हैं जो यहाँ आने वालों को अपनी जङों की ओर मुङने की प्रेरणा देती हैं। मुक्त चिंतन और बेबाक अभिव्यक्ति यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है। इस शहर की सांस्कृतिक विशेषताओं को उदाहरण देकर समझाना बहुत कठिन है। लेकिन तसलीमा के शहर में आने के बाद से ये विशेष ताएँ धूमिल होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान दौर में राजनीति संस्कृति से ज्यादा ताकतवर है। कोलकाता में तसलीमा भी कुत्सित राजनीति की शिकार हुई।
प. बंगाल में पिछले तीस वर्षों से सत्ता का नेतृत्व कर रहे मार्क्सवादियों को जब ऐसा लगा कि नन्दीग्राम और सिंगूर मामलों के कारण उनकी जागीर छिन सकती है, तो उन्होंने एक ऐसे मुद्दे की तलाश शुरु की जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके ताकि, नन्दीग्राम में पार्टी कैडरों द्वारा चलाया जा रहा खूनी अभियान किसी की नजर में न आ सके। इसके लिए उस वक्त तसलीमा से बेहतर कोई मुद्दा नहीं था। सुनियोजित तरीके से यह मुद्दा भड़का और ऐसा भड़का कि उसे संभालने में सबसे ज्यादा तकलीफ भड़काने वालों को ही हुई। विगत 21 नवंबर को तसलीमा को लेकर कोलकाता में जो कुछ हुआ उसे देख कर देश-विदेश के वे बुध्दिजीवी अचम्भित थे जो कोलकाता की खूबियों को जानते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में कोलकाता को मुक्तचिंतन की सरजमीं माना जाता है। उस घटना के बाद जिस प्रकार प. बंगाल सरकार ने तसलीमा को कोलकाता छोङने के लिए विवश किया वह मुक्तचिंतन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति माक्र्सवादियों की कुण्ठा को उजागर करता है। एक कपङे में कोलकाता से जयपुर पहुँची तसलीमा को इस बात से भी अन्जान रखा गया कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और यह सब हुआ मुट्ठी भर धर्मांन्धों की उच्छृंखलता के कारण। तसलीमा को लेकर अचानक कोलकाता में ऐसी परिस्थिति का सृजन किया गया जिसे नियंत्रित करने के लिए सेना बुलानी पङी और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाने पङे। आनन-फानन में राज्य सरकार ने तसलीमा को सुरक्षा देने में असमर्थता प्रकट कर दी और तसलीमा को शहर छोङना पङा। कोलकाता से जयपुर और फिर वहाँ से दिल्ली का अज्ञातवास। इतनी खींचतान से परेशान तसलीमा ने बाद में अपनी लेखनी पर खेद प्रकट किया। कई लोगों ने कहा - तसलीमा हार चुकी हैं। लेकिन सही मायनो में इस पूरे प्रकरण से पराजय तसलीमा की नहीं हुई बल्कि पराजित हुई प. बंगाल की मार्क्सवादी सरकार। जो सरकार एक शरणार्थी को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही हो उसे पराजित ही माना जाएगा। लेकिन राज्य सरकार को अपनी पराजय का अहसास तक नहीं है। यहाँ के माक्र्सवादी तसलीमा को कोलकाता से बाहर कर इस खुशफहमी के शिकार हैं कि इससे उनका मुसलमान वोट बैंक जो नन्दीग्राम के कारण खिसक चुका था कुछ हद तक मजबूत होगा। लेकिन वे इस बात से बेखबर हैं कि तसलीमा को कोलकाता से बाहर करने की जल्दबाजी में उन्होंने जो कदम उठाए उनसे सरकार की छवि को कितना नुकसान पहुँचा है।
तसलीमा को मीडिया और उनके आलोचकों ने विवादास्पद लेखिका का खिताब दिया है। वे विवादास्पद क्यों है? सिर्फ इसलिए कि इस्लाम को लेकर उनकी सोच औरों से अलग है। लेकिन इस बात से सभी सहमत होंगे कि किसी भी विषय-वस्तु को देखने, समझने और उसका विश्लेषण करने का हर आदमी का तरीका अलग-अलग होता है। तसलीमा नसरीन एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने अपनी लेखनी में उन मुद्दों को मुक्तचिंतन से जोङने की कोशिश की है जिन पर उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। किसी भी मुद्दे पर दुनिया के हर आदमी की राय एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन सभी को अपनी राय जाहिर करने का हक तो है। यदि तसलीमा को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है तो उन्हें विवादास्पद कहा जाना कहाँ तक उचित है? कोई लेखक क्या लिख रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह देखना है कि उसकी लेखनी में कलात्मक अनुशासन है या नहीं। तसलीमा ने अपनी लेखनी में कम से कम इस अनुशासन का पालन जरूर किया है। कला जगत की जानी-मानी हस्ती चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आङ में कलात्मक अनुशासन की सारी हदें तोङ दी थी। इसके बावजूद उन्हें कभी विवादास्पद चित्रकार नहीं कहा गया।
शायद माकपा नेता अभी भी इस गलतफहमी में हैं कि जनता को झूठ का आईना दिखाकर सच पर पर्दा डाला जा सकता है। वे जनता को भ्रमित करने की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। तसलीमा प्रकरण भी उनकी इसी रणनीति का एक हिस्सा था। लेकिन इस कोशिश में उनकी अपनी कमजोरिया ही उजागर हुई। सरकार के लिए इससे बङी विफलता और क्या होगी कि वह कुछ सौ लोगों की धमकियों से डर गई। तसलीमा को बांग्लादेश में भी इस तरह की धमकियों का सामना करना पङा था। लेकिन वे भयभीत नहीं हुई। भयभीत हुई वहाँ की सरकार, और अब प. बंगाल की मार्क्सवादी सरकार। इस सरकार ने आतातायियों की भीड़ के समक्ष आत्मसमर्पण कर खुद अपनी औकात दिखा दी। बेसहारों को सहारा देने का दम भरने वाले मार्क्सवादियों के लिए यह बड़े शर्म का विषय है।
संतोष कुमार मधुप (नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
Saturday, 12 January 2008
भारतीय नवजागरण के अग्रदूत : स्वामी विवेकानंद

भारतीय नवजागरण का अग्रदूत यदि स्वामी विवेकानेद को कहा जाय, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने सदियों की गुलामी में जकड़े भारतवासी को मुक्ति का रास्ता सुझाया। जन-जन के मन में भारतीय होने के गर्व का बोध कराया। उन्होंने मानव समाज को अन्याय, शोषण और कुरीतियों के खिलाफ उठ खड़े होने का साहस प्रदान किया और पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में दिशाभ्रमित भारतीय नौजवानों के मन-मस्तिष्क में स्वदेश-प्रेम एवं हिन्दुत्व-जीवन दर्शन के प्रति अगाध विश्वास पैदा किया। अपनी विद्वतापूर्ण एवं तर्क आधारित भाषण से दुनिया भर के बुध्दिजीवियों के बीच भारत के प्रति एक जिज्ञासा पैदा की। भारत की एक अनोखे ढंग से व्याख्या की। उन्होंने भारतीय बौध्दिक क्रांति का सूत्रपात किया। स्वामी विवेकानंद ने उद्धोष किया कि समस्त संसार हमारी मातृभूमि का ऋणी है। स्वामीजी ने अध्यात्म को अंधविश्वास एवं कालबाह्य हो चुके कर्मकांड से मुक्त कराया एवं हिन्दुत्व की युगानुकूल व्याख्या की तथा अध्यात्म को मानव के सर्वांगीण विकास का केन्द्र-बिन्दु बताया।
भारतवर्ष में 'गुरू-शिष्य' की अभिनव परंपरा रही है। हम सब जानते है कि छत्रपति शिवाजी, सम्राट चन्द्रगुप्त, प्रभु श्री रामचन्द्र जैसे कर्मशील एवं प्रतापी योध्दाओं के निर्माण और सफलता के पीछे समर्थ गुरू रामदास, चाणक्य, विश्वामित्र जैसे गुरूजनों का स्नेह और आशीर्वाद का अप्रतिम योगदान रहा है। ठीक इसी प्रकार कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के स्नेहिल सान्निध्य और आशीर्वाद से स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति एवं हिन्दू धर्म का प्रचार करके संसार का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया।
स्वामी विवेकानंद के जीवन में शिकागो धर्म सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस सत्रह दिन के धर्म सम्मेलन ने इस तीस वर्षीय हिन्दू संन्यासी को जगत में सुविख्यात कर दिया। 11 सितंबर, 1893 से प्रारंभ हुए इस सम्मेलन में उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। भाषण प्रारंभ करते हुए जैसे ही उनके मधुर कंठ से 'अमरीकी निवासी बहनों और भाइयों' संबोधन निकला, सभा भवन काफी देर तक तालियों से गूंजता रहा। वहां उपस्थित हजारों प्रतिनिधि इस आत्मीय संबोधन को सुनकर अभिभूत हो गए। सवामीजी ने आगे कहा-' मुझको ऐसे धमार्वलंबी होने का गौरव है, जिसने संसार को 'सहिष्णुता' तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया।.......सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धार्मिक उन्माद हमारी इस पृथ्वी पर काफी समय तक राज कर चुके है। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी थक गई है। इस उन्माद ने अनेक बार मानव रक्त से पृथ्वी को सींचा है, सभ्यताएं नष्ट कर डाली है तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला है। यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका भी समय आ गया है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो घंटे आज इस सभा के सम्मान के लिए बजाए गए, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों तथा मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद सिध्द होंगे।'
स्वामीजी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। वे स्वदेश-प्रेम को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसलिए भारत की स्वाधीनता के लिए निरंतर युवा-वर्ग को अपने बौध्दिक आख्यायनों से जगाते रहे। उनकी रचनाओं को पढ़कर नवयुवकों में स्वाधीनता प्राप्त करने की तीव्र प्रेरणा जागृत हुई। क्रांतिकारियों के बीच वे सर्वमान्य आदर्श रहे। उनके जीवन कर्म से प्रभावित होकर अनेक क्रांतिकारी, अंग्रेजों के अत्याचार से क्रुध्द हो उनकी हत्या कर देते तथा हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते। स्वामीजी ने कहा-'आगामी पचास वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार-केन्द्र होगा और वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सब व्यर्थ के देवताओं को कुछ समय तक के लिए हमारे मन से लुप्त हो जाने दो। हमारी जाति-स्वरूप केवल यही एक देवता है जो जाग रहा है। जिसके हर जगह हाथ है, हर जगह पैर है, हर जगह कान है, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। दूसरे सब देवता सो रहे है। हम क्यों इन व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़े और उस देवता की, उस विराट की, पूजा क्यों न करे जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे है। जब हम उसकी पूजा कर लेंगे तभी हम सभी देवताओं की पूजा करने योग्य बनेंगे।
आज समाज-जीवन में जो विकृतियां पनप रही है, उसके बारे में उन्होंने काफी पहले सावधान कर दिया था। आज यह सहज ही देखने को मिल रहा है कि विश्वविद्यालयों, कैम्पसों में ड्रग-ड्रिंक-डिस्को की कचरा संस्कृति में सराबोर आज का युवक स्व-विस्मृति के कगार पर है। उन्होंने पाश्चात्य जीवन शैली के अंधानुकरण को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा था, 'ऐ भारत! यही तेरे लिए एक भयानक खतरे की बात है-तुम्हें पाश्चात्य जातियों की नकल करने की इच्छा ऐसी प्रबल होती जा रही है कि भले-बुरे का निश्चय अब विचार-बुध्दि, शास्त्र या हिताहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव और आचार की प्रशंसा करे या जिसे न चाहे, वही अच्छा है और वे जिसकी निंदा करे तथा जिसे न चाहे, वही बुरा! खेद है, इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय भला और क्या होगा? यह कथन आज भी प्रासंगिक लगता है।
स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों पर अपना ध्यान तो रखते ही थे साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी होने वाले सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों का अध्ययन और विचार करते थे। उन दिनों समाजवाद के विचार बड़ी तेजी से फैल रहे थे। उनका मानना था कि 'भारत को समाजवाद-विषयक अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने से पहले यह आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य निहित है, उन्हें इन सब ग्रंथों के पृष्ठों के बाहर लाकर, मठोें की चहारदीवारियां भेदकर, वनों की नीरवता से दूर लाकर, कुछ संप्रदाय-विशेषों के हाथों से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दावानल के समान सारे देश को चारों ओर से लपेट लें-उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सब जगह फैल जाए- हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र वे धधक उठें।'
स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों व रचनाओं से जन-जन में प्रबल इच्छाशक्ति व स्वाभिमान तो जगाया ही, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य को पाने में एक सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता हुई। वे 'संघे शक्ति कलौयुगे' के सूत्र की महत्ता को भलीभांति जानते थे। वे चाहते थे कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में आम जन भी हाथ बंटाये। 1 मई, 1897 के दिन उन्होंने स्वामी रामकृष्ण देव के कुछ शिष्यों के सम्मुख एक योजना रखी। उन्होंने कहा कि 'विश्व के कई देशों का भ्रमण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमें पवित्र धर्म एवं गुरूदेव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाना ही होगा।' आज सर्वविदित है कि देश के कोने-कोने में 'रामकृष्ण मिशन' द्वारा संचालित सैकड़ों अस्पताल, विद्यालय व सेवाकार्य राष्ट्र के नवोन्मेष व परम वैभव प्राप्त करने की दृष्टि से अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।
स्वामीजी ने मात्र 39 वर्ष की आयु में ही अपना भौतिक देह त्याग दिया और इतनी कम उम्र में ही अनथक प्रवास करते हुए एक बेहतर भारत व विश्व के निर्माण के लिए निरंतर सक्रिय रहे। अपने जीवन का क्षण-क्षण मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने सशक्त और समृध्दिशाली भारत का जो सपना देखा, उसे आज भी अनेक राष्ट्रवादी संस्थाएं पूरा करने में जुटी हुई हैं। ऐसे वक्तृत्व व कर्तृत्व के धनी एवं तेजस्विता के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जन-जन के आदर्श पुरूष है। उनका संपूर्ण जीवन-कर्म व विचार हम सबके लिए पाथेय है।
भारतवर्ष में 'गुरू-शिष्य' की अभिनव परंपरा रही है। हम सब जानते है कि छत्रपति शिवाजी, सम्राट चन्द्रगुप्त, प्रभु श्री रामचन्द्र जैसे कर्मशील एवं प्रतापी योध्दाओं के निर्माण और सफलता के पीछे समर्थ गुरू रामदास, चाणक्य, विश्वामित्र जैसे गुरूजनों का स्नेह और आशीर्वाद का अप्रतिम योगदान रहा है। ठीक इसी प्रकार कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के स्नेहिल सान्निध्य और आशीर्वाद से स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति एवं हिन्दू धर्म का प्रचार करके संसार का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया।
स्वामी विवेकानंद के जीवन में शिकागो धर्म सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस सत्रह दिन के धर्म सम्मेलन ने इस तीस वर्षीय हिन्दू संन्यासी को जगत में सुविख्यात कर दिया। 11 सितंबर, 1893 से प्रारंभ हुए इस सम्मेलन में उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। भाषण प्रारंभ करते हुए जैसे ही उनके मधुर कंठ से 'अमरीकी निवासी बहनों और भाइयों' संबोधन निकला, सभा भवन काफी देर तक तालियों से गूंजता रहा। वहां उपस्थित हजारों प्रतिनिधि इस आत्मीय संबोधन को सुनकर अभिभूत हो गए। सवामीजी ने आगे कहा-' मुझको ऐसे धमार्वलंबी होने का गौरव है, जिसने संसार को 'सहिष्णुता' तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया।.......सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धार्मिक उन्माद हमारी इस पृथ्वी पर काफी समय तक राज कर चुके है। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी थक गई है। इस उन्माद ने अनेक बार मानव रक्त से पृथ्वी को सींचा है, सभ्यताएं नष्ट कर डाली है तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला है। यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका भी समय आ गया है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो घंटे आज इस सभा के सम्मान के लिए बजाए गए, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों तथा मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद सिध्द होंगे।'
स्वामीजी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। वे स्वदेश-प्रेम को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसलिए भारत की स्वाधीनता के लिए निरंतर युवा-वर्ग को अपने बौध्दिक आख्यायनों से जगाते रहे। उनकी रचनाओं को पढ़कर नवयुवकों में स्वाधीनता प्राप्त करने की तीव्र प्रेरणा जागृत हुई। क्रांतिकारियों के बीच वे सर्वमान्य आदर्श रहे। उनके जीवन कर्म से प्रभावित होकर अनेक क्रांतिकारी, अंग्रेजों के अत्याचार से क्रुध्द हो उनकी हत्या कर देते तथा हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते। स्वामीजी ने कहा-'आगामी पचास वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार-केन्द्र होगा और वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सब व्यर्थ के देवताओं को कुछ समय तक के लिए हमारे मन से लुप्त हो जाने दो। हमारी जाति-स्वरूप केवल यही एक देवता है जो जाग रहा है। जिसके हर जगह हाथ है, हर जगह पैर है, हर जगह कान है, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। दूसरे सब देवता सो रहे है। हम क्यों इन व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़े और उस देवता की, उस विराट की, पूजा क्यों न करे जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे है। जब हम उसकी पूजा कर लेंगे तभी हम सभी देवताओं की पूजा करने योग्य बनेंगे।
आज समाज-जीवन में जो विकृतियां पनप रही है, उसके बारे में उन्होंने काफी पहले सावधान कर दिया था। आज यह सहज ही देखने को मिल रहा है कि विश्वविद्यालयों, कैम्पसों में ड्रग-ड्रिंक-डिस्को की कचरा संस्कृति में सराबोर आज का युवक स्व-विस्मृति के कगार पर है। उन्होंने पाश्चात्य जीवन शैली के अंधानुकरण को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा था, 'ऐ भारत! यही तेरे लिए एक भयानक खतरे की बात है-तुम्हें पाश्चात्य जातियों की नकल करने की इच्छा ऐसी प्रबल होती जा रही है कि भले-बुरे का निश्चय अब विचार-बुध्दि, शास्त्र या हिताहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव और आचार की प्रशंसा करे या जिसे न चाहे, वही अच्छा है और वे जिसकी निंदा करे तथा जिसे न चाहे, वही बुरा! खेद है, इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय भला और क्या होगा? यह कथन आज भी प्रासंगिक लगता है।
स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों पर अपना ध्यान तो रखते ही थे साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी होने वाले सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों का अध्ययन और विचार करते थे। उन दिनों समाजवाद के विचार बड़ी तेजी से फैल रहे थे। उनका मानना था कि 'भारत को समाजवाद-विषयक अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने से पहले यह आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य निहित है, उन्हें इन सब ग्रंथों के पृष्ठों के बाहर लाकर, मठोें की चहारदीवारियां भेदकर, वनों की नीरवता से दूर लाकर, कुछ संप्रदाय-विशेषों के हाथों से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दावानल के समान सारे देश को चारों ओर से लपेट लें-उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सब जगह फैल जाए- हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र वे धधक उठें।'
स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों व रचनाओं से जन-जन में प्रबल इच्छाशक्ति व स्वाभिमान तो जगाया ही, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य को पाने में एक सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता हुई। वे 'संघे शक्ति कलौयुगे' के सूत्र की महत्ता को भलीभांति जानते थे। वे चाहते थे कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में आम जन भी हाथ बंटाये। 1 मई, 1897 के दिन उन्होंने स्वामी रामकृष्ण देव के कुछ शिष्यों के सम्मुख एक योजना रखी। उन्होंने कहा कि 'विश्व के कई देशों का भ्रमण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमें पवित्र धर्म एवं गुरूदेव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाना ही होगा।' आज सर्वविदित है कि देश के कोने-कोने में 'रामकृष्ण मिशन' द्वारा संचालित सैकड़ों अस्पताल, विद्यालय व सेवाकार्य राष्ट्र के नवोन्मेष व परम वैभव प्राप्त करने की दृष्टि से अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।
स्वामीजी ने मात्र 39 वर्ष की आयु में ही अपना भौतिक देह त्याग दिया और इतनी कम उम्र में ही अनथक प्रवास करते हुए एक बेहतर भारत व विश्व के निर्माण के लिए निरंतर सक्रिय रहे। अपने जीवन का क्षण-क्षण मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने सशक्त और समृध्दिशाली भारत का जो सपना देखा, उसे आज भी अनेक राष्ट्रवादी संस्थाएं पूरा करने में जुटी हुई हैं। ऐसे वक्तृत्व व कर्तृत्व के धनी एवं तेजस्विता के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जन-जन के आदर्श पुरूष है। उनका संपूर्ण जीवन-कर्म व विचार हम सबके लिए पाथेय है।
Thursday, 10 January 2008
माओ के जुल्मों की कहानी

माओ-त्से तुंग को 20 वीं सदी का एक ऐसा निर्मम नेता माना जाता है जिसने अहम तथा सत्ता लिप्सा के चलते न केवल 7 करोड़ लोगों की हत्या करवाई बल्कि 'किसानों की क्रान्ति' के नाम पर चीन को दमन चक्र की चक्की में बुरी तरह से पीसा। वह विश्व राजनीति में एक ऐसे कुटिल नेता के रूप में छाया रहा जिसने 'पंचशील व हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के नारे की आड़ में भारत की पीठ में छुरा घोंपा।
माओ के बारे में दो लेखकों, जुंग चांग तथा जॉन हालीडे, द्वारा लिखित पुस्तक 'माओ-दि अननोन स्टोरी' में जो तथ्य दिए गए हैं उन्होंने माओ के क्रान्तिकारी स्वरूप बारे व्याप्त मिथों को तोड़ा है। जुंग चांग 14 वर्ष की आयु से रैड ब्रिगेड के सदस्य रहे तथा उन्होंने माओ के बारे में काफी कुछ निकट से जाना था।
भारतीय राजनीतिक विश्लेषक ब्रह्म चेलानी ने माओ की इस जीवनी की समीक्षा करते हुए जो लिखा वह चौंकाने वाला है। हम पाठकों की जानकारी के लिए उसके कुछ प्रमुख अंशों को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :
''माओ-त्से तुंग द्वारा साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद के विरुध्द लड़ी गई लड़ाई और उसमें प्राप्त जीत ने उन्हें चीन में सर्वोच्च नेता बना दिया।''
माओ ने नरसंहार के मामले में इस सदी के हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी जैसे क्रूर तानाशाहों को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्रान्ति के दौरान हुई हिंसा को छोड़ दें तो शांति काल में माओ ने 7 करोड़ लोगों की हत्याएं करवाईं। ये हत्याएं क्रान्ति विरोधी होने के आरोप में की गईं।
माओ के लिए मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं था। 1959-61 के मध्य जो भीषण अकाल पड़ा उसे माओ निर्मित माना जाता है तथा इसमें 3.80 करोड़ लोग भूख से मरे। जब लोग भूख से मर रहे थे तब माओ कमसिन लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाने में व्यस्त था।
माओ की कुटिलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों ने क्रांति में और च्वांग काई शेक को सत्ता से हटाने में साथ दिया उन्हीं में से अनेक लोगों के विरुध्द माओ ने 1957 में 'सुधारवादी अभियान' चलाया। अभियान के अन्तर्गत कई लोगों पर मुकदमे चलाए गए व उन्हें दंडित किया गया। इसी 'विश्वासघाती' प्रवृत्तिा के कारण माओ ने अपनी चौथी पत्नी को विभिन्न आरोपों में जेल में डलवा दिया जहां 1991 में उसने आत्महत्या कर ली।
माओ ने सत्ता में आते ही 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने की योजना बनाई और रूसी नेता स्टालिन से कहा कि चीनी सेनाएं तिब्बत पर हमला करने जा रही हैं, सोवियत वायुसेना उसके लिए वहां गोला-बारूद आदि पहुंचा कर सहायता करे। इस प्रकार माओ की इस युध्द में रूस को भी शामिल करने की योजना थी।
माओ ने 1962 में भारत पर हमला करने के लिए एक ऐसे समय को चुना जब विश्व का ध्यान अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य आसन्न टकराव की ओर लगा था। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा में अमेरिका की ओर लक्ष्य करती हुई अपनी मधयम दूरी की मिसाइलें तैनात कर दी थीं। माओ को क्यूबा में मिसाइलें तैनात किए जाने की पूर्व सूचना ख्रुश्चेव से मिल गई थी, जिन्होंने युध्द छिड़ने की स्थिति में चीन से सहायता मांगी थी। माओ ने सूचना का लाभ उठाने के लिए तत्कालीन सोवियत राजदूत को बुलाकर कहा - चीन द्वारा भारत पर हमला किए जाने की स्थिति में मास्को को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। बताया जाता है कि ख्रुश्चेव ने भी अपनी हितसाधक कूटनीति अपनाते हुए माओ को आश्वासन दिया कि वह भारत को मिग-21 लड़ाकू विमान देने के वायदे को पूरा करने में विलम्ब करेंगे और इस प्रकार युध्द में चीन का साथ देंगे।
माओ के बारे में दो लेखकों, जुंग चांग तथा जॉन हालीडे, द्वारा लिखित पुस्तक 'माओ-दि अननोन स्टोरी' में जो तथ्य दिए गए हैं उन्होंने माओ के क्रान्तिकारी स्वरूप बारे व्याप्त मिथों को तोड़ा है। जुंग चांग 14 वर्ष की आयु से रैड ब्रिगेड के सदस्य रहे तथा उन्होंने माओ के बारे में काफी कुछ निकट से जाना था।
भारतीय राजनीतिक विश्लेषक ब्रह्म चेलानी ने माओ की इस जीवनी की समीक्षा करते हुए जो लिखा वह चौंकाने वाला है। हम पाठकों की जानकारी के लिए उसके कुछ प्रमुख अंशों को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :
''माओ-त्से तुंग द्वारा साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद के विरुध्द लड़ी गई लड़ाई और उसमें प्राप्त जीत ने उन्हें चीन में सर्वोच्च नेता बना दिया।''
माओ ने नरसंहार के मामले में इस सदी के हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी जैसे क्रूर तानाशाहों को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्रान्ति के दौरान हुई हिंसा को छोड़ दें तो शांति काल में माओ ने 7 करोड़ लोगों की हत्याएं करवाईं। ये हत्याएं क्रान्ति विरोधी होने के आरोप में की गईं।
माओ के लिए मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं था। 1959-61 के मध्य जो भीषण अकाल पड़ा उसे माओ निर्मित माना जाता है तथा इसमें 3.80 करोड़ लोग भूख से मरे। जब लोग भूख से मर रहे थे तब माओ कमसिन लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाने में व्यस्त था।
माओ की कुटिलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों ने क्रांति में और च्वांग काई शेक को सत्ता से हटाने में साथ दिया उन्हीं में से अनेक लोगों के विरुध्द माओ ने 1957 में 'सुधारवादी अभियान' चलाया। अभियान के अन्तर्गत कई लोगों पर मुकदमे चलाए गए व उन्हें दंडित किया गया। इसी 'विश्वासघाती' प्रवृत्तिा के कारण माओ ने अपनी चौथी पत्नी को विभिन्न आरोपों में जेल में डलवा दिया जहां 1991 में उसने आत्महत्या कर ली।
माओ ने सत्ता में आते ही 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने की योजना बनाई और रूसी नेता स्टालिन से कहा कि चीनी सेनाएं तिब्बत पर हमला करने जा रही हैं, सोवियत वायुसेना उसके लिए वहां गोला-बारूद आदि पहुंचा कर सहायता करे। इस प्रकार माओ की इस युध्द में रूस को भी शामिल करने की योजना थी।
माओ ने 1962 में भारत पर हमला करने के लिए एक ऐसे समय को चुना जब विश्व का ध्यान अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य आसन्न टकराव की ओर लगा था। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा में अमेरिका की ओर लक्ष्य करती हुई अपनी मधयम दूरी की मिसाइलें तैनात कर दी थीं। माओ को क्यूबा में मिसाइलें तैनात किए जाने की पूर्व सूचना ख्रुश्चेव से मिल गई थी, जिन्होंने युध्द छिड़ने की स्थिति में चीन से सहायता मांगी थी। माओ ने सूचना का लाभ उठाने के लिए तत्कालीन सोवियत राजदूत को बुलाकर कहा - चीन द्वारा भारत पर हमला किए जाने की स्थिति में मास्को को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। बताया जाता है कि ख्रुश्चेव ने भी अपनी हितसाधक कूटनीति अपनाते हुए माओ को आश्वासन दिया कि वह भारत को मिग-21 लड़ाकू विमान देने के वायदे को पूरा करने में विलम्ब करेंगे और इस प्रकार युध्द में चीन का साथ देंगे।
माओ ने उस समय चतुर रणनीति अपनाते हुए अमेरिका से यह आश्वासन भी लिया था कि च्यांग काई शेक फार्मोसा (अब ताईवान) से चीन की मुख्य भूमि के विरुध्द कभी किसी प्रकार की आक्रामक कार्यवाही नहीं करेगा। माओ ने इस प्रकार प्रशांत क्षेत्र से कोई मोर्चा न खुलने को सुनिश्चित करते हुए भारत पर आक्रमण करने की ओर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित किया। इस युध्द में भारत की बुरी तरह हार हुई तथा नेहरू को ऐसा सदमा पहुंचा जो उनके लिए जानलेवा सिध्द हुआ। नेहरू जिस तरह विकासशील देशों के नेता के रूप में उभर रहे थे वह माओ को पसंद नहीं था तथा वह इस क्षेत्र में नेतृत्व के लिए उन्हें अपना प्रतिद्वन्द्वी मानता था।
ख्रुश्चेव व माओ की दोस्ती भी लम्बे समय तक नहीं चली। अमेरिका व सोवियत संघ में समझौते के बाद ख्रुश्चेव ने क्यूबा से मिसाइलें हटा लीं और माओ से दोस्ती तोड़ ली, जिस पर माओ ने तिलमिलाते हुए कहा था ''ख्रुश्चेव अमेरिका के हाथों बिक गया।'' असल में माओ की इच्छा थी कि अमेरिका व सोवियत यूनियन परमाणु युध्द द्वारा नष्ट हो जाएं और चीन एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया पर राज करे।
अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि माओ का चीन किस प्रकार मानवाधिकारों के हनन व दमनचक्र में लगा हुआ है, इसके बावजूद वह उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाने में लगा था। 1971 के बांग्लादेश युध्द के समय अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर ने चीनी नेताओं से सम्पर्क कर कहा था कि वे उत्तार में भारत के विरुध्द मोर्चा खोल कर पाकिस्तान की सहायता करें, लेकिन सोवियत संघ की घुड़की के कारण चीन की तब ऐसा करने की हिम्मत न हुई।
निक्सन सरकार के लिए चीन के दरवाजे खोलने में किसिंगर की चीन दोस्ती व माओ तथा उनकी कम्युनिस्ट सरकार ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह बाहर से घृणा और भीतर से अपने हित साधने का कुटिल खेल था। माओ की 'ऊंची छलांग' व 'सांस्कृतिक क्रांति' के नाम पर हुई हिंसा तथा माओ के उत्ताराधिकारियों द्वारा व 'सांस्कृतिक क्रांति' के नाम पर हुई हिंसा तथा माओ के उत्ताराधिकारियों द्वारा तिनानमिन चौक में लोकतंत्र समर्थक छात्रों के नरसंहार के बाद आज चीन उसी अमेरिका के साथ पूंजीवादी मार्ग पर चल पड़ा है जिसका वह हमेशा विरोध करता था।
जुंग चांग और जॉन हालीडे की पुस्तक में माओ के चरित्र और जीवन बारे में जो तथ्य प्रकाशित किए गए हैं वह स्पष्ट करते हैं कि माओ जैसे नेता किस तरह पूरी कौम को अपनी सनक का शिकार बना देते हैं।
विश्व राजनीति में महत्वाकांक्षी नेताओं के लिए मित्रता व विश्वसनीयता का कोई मोल नहीं होता। भारत के प्रति मैत्री का राग अलापने वाले कई नेता अपने हित साधने के लिए भारत के विरुध्द माओ का साथ देने के लिए चल पड़े थे। आज यह नेता नहीं रहे, लेकिन इतिहास की यह कटु वास्तविकताएं दुनिया को काफी समय तक झकझोरती रहेंगी। (साभार : पंजाब केसरी)
Wednesday, 9 January 2008
साध्वी ऋतंभरा की हुंकार

गत 30 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित ऐतिहासिक रामसेतु रक्षा महासम्मेलन में साध्वी ऋतंभरा, प्रणेता, वात्सल्य ग्राम (वृंदावन) का उदबोधन-
इस देश का प्राणाधार हैं श्री राम। वे हमारी आस्थाओं और जन-जन की निष्ठाओं में बसते हैं। वे पंचवटी की छांव में मिलते हैं, अंगद के पांव में मिलते हैं, अनसुइया की मानवता में मिलते हैं और मां सीता की पावनता में दृष्टिगोचर होते हैं। राम मंदिर के फेरों में नहीं शबरी के झूठे बेरों में मिलते हैं। देख सकते हो तो देखो, सारा हिन्दू जनमानस भगवान राम से आलोकित और संचालित होता है।
अपने पुरखों और संस्कृति को नकारने से बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। आज जैसी स्थिति बनी है वैसी स्थिति पहले भी आई थी जब अयोध्या में प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर पराभवी युग का प्रतीक सबकी आस्थाओं को चुनौती दे रहा था। 6 दिसम्बर 1992 को हिन्दू समाज की शक्ति के आगे वह प्रतीक देखते ही देखते ओझल हो गया। लेकिन आज परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं। रामसेतु को तोड़ना निशाचरी चिंतन है, आसुरी प्रवृत्ति है। रामसेतु केवल एक सेतु नहीं हमारी आस्था का दर्पण है। इसे ध्वस्त करने वालों के विरुध्द संकल्पित होकर प्रतिकार का शंख गुंजाना होगा, राजकाज के लिए सभी को आगे आना होगा।
करुणा हमारा स्वभाव है लेकिन जब कोई हमारी आस्थाओं को चुनौती देता है तो हम षडंत्रों के संहारी बनकर मंत्रों का नवनिर्माण करते हैं, जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। ये देश राम का है, परिवेश राम का है, हम सब राम के हैं। तुम हिन्दू हो, जिन्होंने नक्षत्रों को संज्ञा दी है, जिन्होंने दधीचि बनकर अपनी हड्डियां राष्ट्र को समर्पित की हैं। तुम हिन्दू हो, जिन्होंने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया था, जिन्होंने स्वाभिमान के लिए अपने पुत्रों को दीवार में चिनवाया था। तुम हिन्दू हो, जिन्होंने युध्दों की चुनौतियां भी स्वीकार कर ली थीं, फांसी को फंदे को चूमा था, लेकिन मां भारती के स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए अपने यौवन को न्योछावर किया था। हिन्दुओ, तुमने अन्दमान की काली कोठरी में पत्थरों पर अपने रक्त के शौर्य की कहानियां लिखी थीं। हिन्दुओ, तुमने घास की रोटियां खाई थीं लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा था। हिन्दुओ, तुमने हरिश्चंद्र बनकर मणिकर्णिका घाट पर अपना कर्तव्य निभाया था, अपने सम्मुख अपने पुत्र की लाश लिए खड़ी पत्नी को देखकर भी तुम विचलित नहीं हुए थे। हिन्दुओ, तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर किया राष्ट्र के लिए, समाज, धर्म, संस्कृति के लिए। हम अपने लिए जीना जानते ही नहीं, हम अपनों के लिए जीना जानते हैं। हमने कण-कण में राम का दर्शन किया है। हम सारी दुनिया में वात्सल्य लुटाने वाले हैं। लेकिन आज अपनी धरती पर अपनी सहिष्णुता के कारण अपमानित होने को विवश हुए हैं। अपनी धरती पर शरणार्थी बन जाने का दंश एक हिन्दू से ज्यादा कौन जानता है? अपने ही देश के अंदर केसर की क्यारियों में बारूद पैदा की गई, हमारे ही देश के टुकड़े-टुकड़े करके तुष्टीकरण की राजनीति को परवान चढ़ाया गया। हम देखते रहे। और आज स्थिति यह हो गई कि लोग हमारे राम को नकारने की धृष्टता करने लगे हैं। इस देश में जब तक आसुरी ताकतें रहेंगी वंदनीय का वंदन नहीं होगा, दण्डनीयों का दण्ड नहीं होगा। इसलिए हिन्दू समाज को संतों का आदेश है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां कातिलों की मुक्ति के विधान नहीं रचे जाएंगे, अपितु देश के अंदर आतंकवादियों को सूली पर चढ़ाया जाएगा।
कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहां
आज देशद्रोही भी महान हो गया यहां।
इक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया,
कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया।
कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां,
जो उजाड़ता रहा है मेहंदी, मांग, रोलियां।
जो सदा वतन की लाज को उघाड़ता रहा,
और भारती का मानचित्र फाड़ता रहा।
जो नकारता रहा है देश के विधान को,
थूकने की चीज मानता था संविधान को।
इसके सर पे ताज धरके हो रही है आरती,
रो रहा है देशप्रेम, रो रही है भारती।
जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे,
और देश द्रोहियों को गोलियों से भून दे,
ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए,
देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए।
महात्मा गांधी ने इस देश की बागडोर पं. नेहरू के हाथों में न सौंपकर यदि सरदार पटेल के हाथों में सौंपी होती तो भारत, भारत के रूप में भारतीयता के गीत गाता दिखाई देता। उस समय हम चूके। लेकिन आज पुन: देश हमसे कुछ मांग रहा है। राम से प्रेम रखने वाले धर्मयोध्दाओं रामद्रोहियों के प्रतिकार का संकल्प करो। उन पाषाणों का स्मरण करो जो 'राम' नाम अंकित कर सागर की छाती पर तैराए गए थे, उस गिलहरी का स्मरण करो जो सेतु निर्माण में अपना किंचित योगदान देने आई थी। प्रभु राम ने भी गिलहरी के उस प्रयास को देखकर प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरा था। इसलिए हिन्दुओ, अपने छोटे-छोटे प्रयत्नों से बिखरी शक्ति को संगठित करो। क्रंदन नहीं, हुंकार भरो हिन्दुओ।
जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से,
जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से,
वो सनातन क्या मिटेगा मनमोहन की सरकार से
इस सत्य सनातन संस्कृति की जड़ें गहरी हैं, जिन्हें हमने अपनी श्रध्दा से सींचा है। इसलिए हिन्दू समाज रामसेतु रक्षार्थ संकल्पित हो।
Monday, 7 January 2008
दर्जनों माओवादी नेता प्रेम संबंधों के कारण पकडे गए
पटना। माओवादियों की प्रेरणा माने जाने वाली कवियित्री कल्पना बोस की एक कविता है- प्यार में नदी मत बनो/ बन सको तो बाढ बनकर आओ/ मैं उसके प्रबल आवेग से निराशा के बांध तोड दूंगी- लेकिन बिहार में माओवादी प्रेम में नदी की तरह बह ही नहीं रहे, बर्फ की तरह पिघल भी रहे हैं। इसका फायदा पुलिस को मिल रहा है। पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार और झारखंड के दर्जनों माओवादी नेता अपने प्रेम संबंधों के कारण पकडे गए हैं।
अपने कैडरों के दिल के रोग से परेशान भाकपा माओवादी ने हाल ही में इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। पुलिस मुख्यालय की ही गुप्तचर शाखा के एक रिकार्ड के अनुसार पार्टी की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने अपने सर्कुलर संख्या 2/07 में विवाहेतर संबंधों को प्रतिबंधित करते हुए सदस्यों को इससे बचने की सलाह दी है। इसके अलावे संगठन ने अपने मुखपत्र लाल चिनगारी के एक अंक में भी सदस्यों को ऐसे मामलों में न फंसने की सलाह दी है। इसके बावजूद सदस्यों की कौन कहे नक्सलियों के बडे नेता भी इस चक्कर में फंसते जा रहे हैं। हाल में नक्सली संगठनों के कई सदस्य अपने विवाहेतर संबंधों को लेकर चर्चा में रहे हैं तो कुछ युवा सदस्यों पर एक साथ कई लडकियों से इश्क लडाने के आरोप भी लगे हैं। नक्सली संगठन के कई सदस्य लडकियों के चक्कर में पकडकर पुलिस के हत्थे चढ चुके हैं। संगठन के जोनल कमांडर बेतिया के रहने वाले सूरज मोची गत 28 सितंबर कों मसौढी अनुमंडल क्षेत्र में एक लडकी के घर से इसी चक्कर में पकडे गए। पटना में पकडे गए तुषार भटटाचार्या भी हरियाणा की एक महिला के साथ अवैध संबंधों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पटना में पकडे गए माओवादी सब जोनल कमांडर छठू जगत के भाई प्रफुल्ल भगत के बारे में भी पुलिस इसी तरह के कई आरोप लगाती है।
पुलिस मुख्यालय सूत्रों के अनुसार प्रफुल्ल जमीन से बेदखल लोगों को कब्जा दिलाने का सब्जबाग दिखाता था और उनके घर की लडकियों का यौन शोषण करता था। इस तरह के मामले पडोसी राज्य झारखंड में भी पाए गए हैं। लेखक- प्रियरंजऩ, साभार- हिन्दुस्तान, 7 जनवरी, 2008
अपने कैडरों के दिल के रोग से परेशान भाकपा माओवादी ने हाल ही में इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। पुलिस मुख्यालय की ही गुप्तचर शाखा के एक रिकार्ड के अनुसार पार्टी की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने अपने सर्कुलर संख्या 2/07 में विवाहेतर संबंधों को प्रतिबंधित करते हुए सदस्यों को इससे बचने की सलाह दी है। इसके अलावे संगठन ने अपने मुखपत्र लाल चिनगारी के एक अंक में भी सदस्यों को ऐसे मामलों में न फंसने की सलाह दी है। इसके बावजूद सदस्यों की कौन कहे नक्सलियों के बडे नेता भी इस चक्कर में फंसते जा रहे हैं। हाल में नक्सली संगठनों के कई सदस्य अपने विवाहेतर संबंधों को लेकर चर्चा में रहे हैं तो कुछ युवा सदस्यों पर एक साथ कई लडकियों से इश्क लडाने के आरोप भी लगे हैं। नक्सली संगठन के कई सदस्य लडकियों के चक्कर में पकडकर पुलिस के हत्थे चढ चुके हैं। संगठन के जोनल कमांडर बेतिया के रहने वाले सूरज मोची गत 28 सितंबर कों मसौढी अनुमंडल क्षेत्र में एक लडकी के घर से इसी चक्कर में पकडे गए। पटना में पकडे गए तुषार भटटाचार्या भी हरियाणा की एक महिला के साथ अवैध संबंधों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पटना में पकडे गए माओवादी सब जोनल कमांडर छठू जगत के भाई प्रफुल्ल भगत के बारे में भी पुलिस इसी तरह के कई आरोप लगाती है।
पुलिस मुख्यालय सूत्रों के अनुसार प्रफुल्ल जमीन से बेदखल लोगों को कब्जा दिलाने का सब्जबाग दिखाता था और उनके घर की लडकियों का यौन शोषण करता था। इस तरह के मामले पडोसी राज्य झारखंड में भी पाए गए हैं। लेखक- प्रियरंजऩ, साभार- हिन्दुस्तान, 7 जनवरी, 2008
Saturday, 5 January 2008
विदेशी भाषा और भारतीय भाषाओं के मीडिया की प्राथमिकताएं
लेखक : डा. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री
भारत में मीडिया की दो समांतर धाराएं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। एक धारा है विदेशी भाषा के मीडिया की और दूसरी धारा है भारतीय भाषाओं के मीडिया की। भारत में विदेशी भाषा का मीडिया मुख्य तौर पर अंग्रेजी भाषा तक ही सीमित है। पुदुच्चेरी और में फ्रांसीसी भाषा का भी थोड़ा बहुत मीडिया है और गोआ दमन दीव में पुर्तगाली भाषा की कुछ पत्र-पत्रिकाएं भी निकलती हैं। गोवा से प्रकाशित पुर्तगाली दैनिक 'ओ हेराल्डो' पिछले कुछ दिनों से अब अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा है। भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता में सभी भारतीय भाषाओं की शमूलियत है।
पिछले दिनों की तीन घटनाओं को आधार बनाकर विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषा के मीडिया की प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। ये तीन घटनाएं हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव, रामसेतु आंदोलन, विशेषकर 30 दिसंबर को दिल्ली में रामेश्वरम रामसेतु रक्षा मंच की ओर से की गई विशाल राष्ट्रीय महासभा और उड़ीसा के कंधमाल जिला में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी महाराज पर क्रिसमस के दिन ईसाई संगठनों द्वारा किया गया घातक आक्रमण। इन तीनों घटनाओं का मीडिया में विवरण जिस प्रकार छपा या छप रहा है वह अपने आप में विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषा के मीडिया की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। गुजरात के विधानसभा के चुनावों की घटना और उड़ीसा में स्वामी जी पर आक्रमण की घटना का विश्लेषण दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी एवं गुजरात/उड़ीसा से प्रकाशित गुजराती और उड़िया भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण को आधार बनाया गया है। जबकि रामसेतु की विशाल राष्ट्रीय सभा के लिए दिल्ली से ही प्रकाशित अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों को आधार बनाया गया है। दिल्ली में तीन प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के हिन्दी संस्करण भी नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान और जनसत्ता के नाम से निकलते हैं। ये समाचार पत्र ज्यादातर अंग्रेजी संस्करणों के अनुवाद पर ही आधारित है और अपने मूल अंग्रेजी अखबार की रसगंध को हिन्दी भाषा में परोसने को दोयम दर्जे का प्रयास है। इसलिए इन तीनों हिन्दी अखबारों का शुमार उनके अंग्रेजी संस्करणों में ही कर लिया है। अलग से उन्हें भारतीय भाषा के मीडिया में शामिल नहीं किया गया है।
सबसे पहले गुजरात के विधानसभा के चुनावों की घटना का विश्लेषण करें। उस काल के दो महीने के निम्न चार अंग्रेजी अखबारों, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और दि हिन्दू को विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और इसी प्रकार गुजरात से प्रकाशित गुजराती भाषा के अखबारों-संदेश, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, जय हिन्द और प्रभात को आधार बनाया गया है। उस विश्लेषण के आधार पर निम्न निष्कर्ष सहज ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस विश्लेषण में अंग्रेजी और गुजराती के उपरोक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित संपादक के नाम पत्रों को भी शामिल किया गया है।
निष्कर्ष :- अंग्रेजी भाषा के उपरोक्त समाचार पत्रों के आधार पर
1. नरेन्द्र मोदी घोर सांप्रदायिक व्यक्ति है।
2. वे गुजरात में मुसलमानों का विरोध करते हैं।
3. गुजरात में सरकार द्वारा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है।
4. सोहराबुद्दीन की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु राज्य सरकार द्वारा किया गया एक कत्ल ही है।
5. मोदी की दृष्टि में मुसलमान आतंकवादी है जबकि ऐसा नहीं है।
6. मोदी गुजरात को हिन्दू और मुस्लिम के आधार पर बांट रहे हैं।
7. मोदी हिन्दुत्व का एजेंडा लागू कर रहे हैं।
8. नरेन्द्र मोदी जनजातिय क्षेत्रों में चर्च और इस्लाम का कार्य दूभर कर रहे हैं।
9. नरेन्द्र मोदी तानाशाह है।
10. नरेन्द्र मोदी अफजल गुरु और सोहराबुद्दीन का प्रश्न उठाकर मुसलमानों को अन्यायपूर्ण ढंग से बदनाम कर रहे हैं।
इसके विपरीत गुजराती भाषा के मीडिया के आधार पर निम्न निष्कर्ष सहज ही निकलते हैं।
1. नरेन्द्र मोदी ने गुजरात से आतंकवाद को समाप्त किया है।
2. नरेन्द्र मोदी के सख्त प्रशासन के कारण ही आतंकवादी गुजरात में घुसने और कोई घटना करने से घबराते हैं।
3. सोहराबुद्दीन की घटना के बाद दूसरे आतंकवादी गुजरात में कोई वारदात करने से डरने लगे।
4. तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुसलमानों और आतंकवादियों को शह भी देती हैं और वोट की खातिर उनका तुष्टिकरण भी करती है। लेकिन मोदी वोट की खातिर किसी का तुष्टिकरण नहीं करते।
5. आतंकवाद से मुकाबला सख्ती से किया जा सकता है तुष्टिकरण से नहीं। गुजरात इस विषय में राह दिखा रहा है।
6. अफजल गुरू को फांसी न देकर कांग्रेस और सीपीएम मुसलमानों को राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करते हुए भी प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है।
इन दोनों निष्कर्षों के अवलोकन से प्रश्न उठता है कि एक ही घटना पर विदेशी भाषा का मीडिया और भारतीय भाषाओं का मीडिया लगभग परस्पर विरोधी खेमे में ही खड़ा क्याें दिखाई देता है? ऐसा क्यों है कि सोहराबुद्दीन की मुठभेड़ की घटना को लेकर गुजराती भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार अलग प्रकार से करते हैंघ् इसका मुख्य कारण विभिन्न मुद्दों और विभिन्न स्थितियों को लेकर अंग्रेजी मीडिया की मानसिकता जिस धरातल पर अवस्थित है वह गुजराती भाषा के मीडिया से या फिर भारतीय भाषा के मीडिया से बिल्कुल अलग है। एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय भाषाओं के मीडिया और विदेशी भाषाओं के मीडिया के पाठक वर्ग भी लगभग अलग-अलग ही है। भारतीय भाषाओं के मीडिया का पाठक आम आदमी है जिसमें खबर की भूख दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। विदेशी भाषा के मीडिया का वर्ग खास आदमी है, उसकी संख्या सीमित है परंतु उसका प्रभाव ज्यादा है। विभिन्न मुद्दों से संबंधित अवधारणाओं के स्तर पर भी ये दोनों पाठक वर्ग काफी अलग-अलग है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिकता को लेकर इन दोनों वर्गों की अवधारणा में जमीन आसमान का फर्क है। विदेशी भाषा के मीडिया का पाठक वर्ग ऐसी जगहों पर रहता है जहां आदमी-आदमी के बीच संपर्क भी कम है और संबंधों के स्तर पर एक और औपचारिकता बनी रहती है। इन स्थानों पर भीड़ कम है स्थान ज्यादा है। एक खुलापन भी है। आपसी संपर्क और संबंध न्यूनतम स्तर पर ही विद्यमान है। इसलिए इस वर्ग के लिए सांप्रदायिकता किताबों में पढ़ा हुआ शब्द है जिसको उसके समग्र रूप में देखपाना इनके लिए संभव ही नहीं है। यदि और ढंग से कहें तो कहा जा सकता है यह पाठक वृंद गांधीनगर का पाठक वृंद है। इसके विपरीत भारतीय भाषाओं के अथवा गुजराती भाषाओं के मीडिया का पाठक वृंद ठेठ अहमदाबाद में रहता है। उसके लिए सांप्रदायिकता महज कागज पर छपा हुआ शब्द नहीं है बल्कि नित्यप्रति के परस्पर व्यवहार और अनुभव के भीतर से उपजा और निर्मित एक यथार्थ है। उस यथार्थ में सोहराबुद्दीन नित्यप्रति मूर्त रूप में घूमता है। अफजल गुरू भी घूमता है। उनकी ऑंखें घूरती हैं और कर्म भय पैदा करते हैं। इस सांप्रदायिकता के बीच में से ही उसे नित्यप्रति गुजरना है। इसलिए उससे वह बच भी नहीं सकता। ये नित्यप्रति की संकरी गलियां हैं। जहां सांप्रदायिकता से नित्य-नित्य मुठभेड़ होती है। इन पाठकों का क्रोध इस बात से उपजता है। यह सांप्रदायिक चेहरा कभी हाजी मस्तान के रूप में प्रकट होता है, कभी दाऊद अब्राहिम के रूप में प्रकट होता है, कभी सोहराबुद्दीन के रूप में प्रकट होता है और कभी अफजल गुरू के रूप में प्रकट होता है। कभी यह तस्लीमुद्दीन बनकर आता है और कभी ईश्रतजहां बनकर रात्रि के अंधकार में निशाचरों की तरह घूमता है। राज्यसत्ता इन निशाचरों से वोट की खातिर हाथ मिला लेती है। आम आदमी का यह पाठक वर्ग इस मिलते हुए हाथ को देखता भी है और उससे सहमता भी है। आम आदमी का इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि सोहराबुद्दीन को किसने मारा और कैसे मारा? उसके मरने की खबर पर वह राहत महसूस करता है जैसे गली-मोहल्ले में घूमता हुआ कोई पागल कुत्ता मरता है तो लोग खुश होते हैं कि जीवन सुरक्षित हो गया है। लेकिन जब जीवजंतुओं के प्रति करूणा की वकालत करने वाला कोई संगठन पागल कुत्ते को मारने के खिलाफ अभियान चला दे तो स्वभाविक है यह पाठक वृंद अभियान चलाने वालों की ओर आश्चर्य भरी नजरों से ही देखेगा। विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषाओं के मीडिया की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण के अलग होने का रहस्य भी यही है। दूर से बैठकर पागल कुत्ते के प्रति करूणा की मांग करना एक बात है और उस कुत्ते के साथ रहते हुए एक दिन उसे मरा हुआ देखकर भयमुक्त होने के एहसास से प्रसन्न होना दूसरी बात है। अंग्रेजी भाषा का मीडिया इस देश में घट रही घटनाओं को दूर बैठकर केवल द्रष्टा के रूप में देखता है और भारतीय भाषाओं का मीडिया उन स्थितियों को भोक्ता के रूप में देखता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। पहले मीडिया का पाठक केवल द्रष्टा है और दूसरे मीडिया का पाठक स्वयं भोक्ता है।
रामसेतु बचाने के लिए दिल्ली में विशाल राष्ट्रीय महासभा-दूसरी घटना 30 दिसंबर 2007 को दिल्ली के स्वर्णजयंती पार्क में रामसेतु को बचाने के लिए की गई विशाल राष्ट्रीय महासभा है। इस सभा में देश के प्रत्येक हिस्से से लाखों लोगों ने शिरकत की। लद्दाख से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक के लोग आए थे। केरल से लेकर पंजाब तक से लोग स्वयं अपना किराया खर्च कर इस राष्ट्रीय सभा में भागीदारी करने के लिए आए थे। हजारों दिल्लीवासी भक्तिभाव से इन रामभक्तों के लिए भोजन तैयार करने में लगे हुए थे। अनेक मोहल्लों में रामभक्तों को रोक-रोक कर लोग आग्रहपूर्वक फल खाने को दे रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम की रपट विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषा के मीडिया में बिल्कुल ही अलग-अलग प्रकार से हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रपट इस प्रकार की थी कि लाखों लोगों के आ जाने से दिल्लीवासियों को बहुत कष्ट हुआ, सड़कों पर जाम लग गया और लोग रविवार का आनंद नहीं मना सके। दिल्ली शोर शराबे को माहौल में डूब गई। परिवहन व्यवस्था में अफरा-तफरी मच गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक करोड़ की आबादी वाले दिल्ली प्रदेश में से किसी एक महिला से इस राष्ट्रीय सभा के बारे में पूछा भी। उसने कहा कि मैं हर रविवार को मेट्रो से अपनी बहन को मिलने के लिए शाहदरा जाती हूँ लेकिन इस अव्यवस्था के कारण नहीं जा सकी। रपट का स्वर कुछ ऐसा था कि इस महिला के अपनी बहन से न मिल पाने के कारण इस राष्ट्रीय महा सभा ने बड़ा ही अहित किया है। एक अन्य अंग्रेजी अखबार ने मानो एक बहुत बड़ा रहस्योद्धाटन किया। एक सज्जन ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे। टिकट लेना उनकी आदत में शुमार नहीं था। वे टीटी को कुछ पैसे देकर सुखपूर्वक यात्रा करूँगा यह सोच कर चले थे। लेकिन रामसेतु पर हो रही इस राष्ट्रीय सभा में भाग लेने वालों की भीड़ के कारण टीटी इन सज्जन की सहायता नहीं कर सके। अंग्रेजी अखबार के अनुसार इस राष्ट्रीय सभा के कारण जनता को हो रहे कष्ट की यह पराकाष्ठा है।
इसके विपरीत दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों पंजाब केसरी और दैनिक जागरण की रपट का स्वर बिल्कुल भिन्न था। इनके अनुसार इस राष्ट्रीय सभा से सारी दिल्ली राममय हुई। रामभक्तों का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े हजारों दिल्लीवासी। दिल्ली में जगह-जगह उनका स्वागत हो रहा था और लोग उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था में संलग्न थे। दिल्ली की भारतीय भाषाओं के अखबारों ने तो कई दिन पहले से ही खबरें देनी शुरू कर दी थी कि इस राष्ट्रीय सभा में भाग लेने के लिए आ रहे रामभक्तों का स्वागत करने के लिए दिल्ली के लोग किस प्रकार की तैयारियाँ कर रहे हैं।
इन दोनों रपटों को पढ़ने के बाद प्रश्न पैदा होता है कि क्या कारण है एक ही घटना पर रपट देते हुए मीडिया का एक वर्ग कहता है कि इससे दिल्ली के लोग प्रसन्न हो रहे हैं और दूसरा वर्ग कहता है कि इससे दिल्ली के लोगों का कष्ट बढ़ रहा है। इसका कारण भी उसी मानसिकता में खोजना होगा जो विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषा के मीडिया के पाठक वर्ग को अलग-अलग करती है। विदेशी भाषा के मीडिया का पाठक वर्ग नई कालोनियों में है। डिफे न्स कालोनी, डीएलएफ कालोनी में है, अंसल प्लाजा में है, टीडीआई में है और सरकारी बाबुओं में है। (बाबुओं से हमारा अभिप्राय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से है।) जैसा कि ऊपर हमने संकेत किया है कि दोनों वर्गों की अवधारणाओं में स्पष्ट ही अंतर है। एक वर्ग ऐसा है जो प्रात: काल ब्रह्ममुहर्त में समीप के मंदिर में हो रही आरती को सुनकर प्रसन्न होता है और दूसरा वर्ग ऐसा है जो उसी आरती को सुनकर नाक भौं सिकोड़ता है कि इससे सुबह की नींद में खलल पड़ता है। यह वही वर्ग है जो रामजन्मभूमि पर मंदिर बनाने को नकार कर वहां एकता के लिए पार्क बनाने का सुझाव देता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि पार्क से उपजी एकता एक ही खुरचन में खत्म हो जाती है । आरती से उपजी एकता लंबे अरसे तक चलती है। अंग्रेजी अखबारों और भारतीय भाषाओं के अखबारों द्वारा इस राष्ट्रीय महा सभा पर की गई रपट उनकी प्राथमिकता भी निश्चित करती है। अंग्रेजी मीडिया के लिए भारतीयता से जुड़ी चीजें और क्रियाकलाप अंग्रेजों द्वारा स्थापित सभ्यता और जीवन पध्दति में खलल पैदा करती है।
उड़ीसा के कंधमाल की घटना-उड़ीसा के कंधमाल में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी महाराज पर 24 दिसंबर को ईसाई संगठनों ने घातक आक्रमण कर दिया। स्वामी जी घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। स्वभाविक ही उड़ीसा के लोगों में इस पर प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने 4 घंटे का शांतिपूर्ण बंद रखा। गुस्से में आए कुछ लोगों ने चर्च की कुछ झोपड़ियां भी जला दीं। इन झोपड़ियों पर सलीव का निशान भी लगा हुआ था। इसलिए इनको चर्च का जलाना कहा गया। ब्राह्मणी गांव में ईसाइयों ने दो सौ लोगों के घर जला दिए। इस घटना की रपट अंग्रेजी मीडिया और उड़िया भाषा के मीडिया में बिल्कुल अलग-अलग प्रकार से आनी प्रारंभ हुई और अभी तक आ रही है। दिल्ली में स्थित लगभग विदेशी भाषा का समग्र मीडिया (एक आध अपवाद को छोड़कर) की रपट का मुख्य स्वर निम्न प्रकार से सारणीबध्द किया जा सकता है।
1. उड़ीसा में ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है और चर्च फूंके जा रहे हैं।
2. सरकार ईसाइयों की रक्षा करने में बुरी तरह असफल रही है।
इसके विपरीत उड़ीसा के उड़िया भाषी समाचार पत्रों यथा-संवाद, समाज, धरित्री, प्रजातंत्र, अमरी कथा, उड़ीसा भास्कर, पर्यवेक्षक इत्यादि में कंधमाल की घटना को लेकर जो रपटें छप रही है उनका मुख्य स्वर निम्न प्रकार से है।
1. ईसाई मिशनरियां व्यापक स्तर पर उड़ीसा के जनजातीय लोगों के घरों को जला रही है। लोगों को धमकाया जा रहा है।
2. मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है ।
3. सरकार उड़ीसा के लोगों की ईसाई मिशनरियों के आक्रमणों से रक्षा नहीं कर पा रही।
4. ईसाई मिशनरियों के इशारे पर एक सांसद इन आक्रमणों को भड़का रहा है।
5. माओवादी और चर्च उड़ीसा के लोगों पर आक्रमण करने में आपस में मिल गए हैं।
6. जनजाति के लोगों पर आधुनिक हथियारों से आक्रमण किये जा रहे हैं।
विदेशी भाषा के मीडिया की प्राथमिकताएं और भारतीय भाषाओं के मीडिया की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए जब किसी मंदिर में लोग भजन कीर्तन के लिए एकत्रित होते हैं तो भारतीय भाषा के मीडिया के लिए यह भक्ति का ज्वार उमडना है लेकिन अंग्रेजी मीडिया के लिए यह शोर शराबा और सामान्य जीवन में होने वाला खलल है। उसका कारण शायद भारत में अंग्रेजों के शासन काल से ही खोजना होगा। अग्रेजों के लिए मंदिर के भीड खलल भी है और खतरा भी है। उसी मानसिकता को आज तक विदेशी भाषा अंग्रेजी का मीडिया ढो रहा है और इसी प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी मीडिया किसी भी घटना की रपट करता है।
इस मानसिकता और प्राथमिकता का एक और कारण भी है । जिन दिनों अंग्रेज इस देश पर राज करते थे, वे यहां के भारतीय समाज को अपने लिए खतरा समझते थे और मुस्लिम समाज एवं ईसाई समाज को अपना पक्षधर मानते थे। इसलिए बहुसंख्यक भारतीय समाज का कोई भी कृत्य उनकी दृष्टि में निंदनीय और ईसाई व मुस्लिम समाज के लिए खतरनाक माना जाता था। अंग्रेजी मीडिया आज भी उसी मानसिकता को ढो रहा है। यही कारण है कि गुजरात का जननिर्णय,रामसेतु को लेकर हुई राष्ट्रीय महासभा और उडिया अस्मिता के लिए संघर्षरत ओडिया लोग अंग्रेजी मीडिया की दृष्टि में खतरनाक कृत्य हैं और मुस्लिम व ईसाई समाज के हितों के विपरीत हैं ।
सारत: विदेशी भाषा के मीडिया की जडें ब्रिटिश शासनकाल की मानसिकता में गहरे धंसी हुई हैं। इसके विपरीत भारतीय भाषाओं के मीडिया की जडें उसी संघर्ष में से उपजी हैं जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आम भारतीय ने किया था ।
(नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
भारत में मीडिया की दो समांतर धाराएं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। एक धारा है विदेशी भाषा के मीडिया की और दूसरी धारा है भारतीय भाषाओं के मीडिया की। भारत में विदेशी भाषा का मीडिया मुख्य तौर पर अंग्रेजी भाषा तक ही सीमित है। पुदुच्चेरी और में फ्रांसीसी भाषा का भी थोड़ा बहुत मीडिया है और गोआ दमन दीव में पुर्तगाली भाषा की कुछ पत्र-पत्रिकाएं भी निकलती हैं। गोवा से प्रकाशित पुर्तगाली दैनिक 'ओ हेराल्डो' पिछले कुछ दिनों से अब अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा है। भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता में सभी भारतीय भाषाओं की शमूलियत है।
पिछले दिनों की तीन घटनाओं को आधार बनाकर विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषा के मीडिया की प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। ये तीन घटनाएं हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव, रामसेतु आंदोलन, विशेषकर 30 दिसंबर को दिल्ली में रामेश्वरम रामसेतु रक्षा मंच की ओर से की गई विशाल राष्ट्रीय महासभा और उड़ीसा के कंधमाल जिला में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी महाराज पर क्रिसमस के दिन ईसाई संगठनों द्वारा किया गया घातक आक्रमण। इन तीनों घटनाओं का मीडिया में विवरण जिस प्रकार छपा या छप रहा है वह अपने आप में विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषा के मीडिया की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। गुजरात के विधानसभा के चुनावों की घटना और उड़ीसा में स्वामी जी पर आक्रमण की घटना का विश्लेषण दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी एवं गुजरात/उड़ीसा से प्रकाशित गुजराती और उड़िया भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण को आधार बनाया गया है। जबकि रामसेतु की विशाल राष्ट्रीय सभा के लिए दिल्ली से ही प्रकाशित अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों को आधार बनाया गया है। दिल्ली में तीन प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के हिन्दी संस्करण भी नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान और जनसत्ता के नाम से निकलते हैं। ये समाचार पत्र ज्यादातर अंग्रेजी संस्करणों के अनुवाद पर ही आधारित है और अपने मूल अंग्रेजी अखबार की रसगंध को हिन्दी भाषा में परोसने को दोयम दर्जे का प्रयास है। इसलिए इन तीनों हिन्दी अखबारों का शुमार उनके अंग्रेजी संस्करणों में ही कर लिया है। अलग से उन्हें भारतीय भाषा के मीडिया में शामिल नहीं किया गया है।
सबसे पहले गुजरात के विधानसभा के चुनावों की घटना का विश्लेषण करें। उस काल के दो महीने के निम्न चार अंग्रेजी अखबारों, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और दि हिन्दू को विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और इसी प्रकार गुजरात से प्रकाशित गुजराती भाषा के अखबारों-संदेश, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, जय हिन्द और प्रभात को आधार बनाया गया है। उस विश्लेषण के आधार पर निम्न निष्कर्ष सहज ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस विश्लेषण में अंग्रेजी और गुजराती के उपरोक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित संपादक के नाम पत्रों को भी शामिल किया गया है।
निष्कर्ष :- अंग्रेजी भाषा के उपरोक्त समाचार पत्रों के आधार पर
1. नरेन्द्र मोदी घोर सांप्रदायिक व्यक्ति है।
2. वे गुजरात में मुसलमानों का विरोध करते हैं।
3. गुजरात में सरकार द्वारा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है।
4. सोहराबुद्दीन की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु राज्य सरकार द्वारा किया गया एक कत्ल ही है।
5. मोदी की दृष्टि में मुसलमान आतंकवादी है जबकि ऐसा नहीं है।
6. मोदी गुजरात को हिन्दू और मुस्लिम के आधार पर बांट रहे हैं।
7. मोदी हिन्दुत्व का एजेंडा लागू कर रहे हैं।
8. नरेन्द्र मोदी जनजातिय क्षेत्रों में चर्च और इस्लाम का कार्य दूभर कर रहे हैं।
9. नरेन्द्र मोदी तानाशाह है।
10. नरेन्द्र मोदी अफजल गुरु और सोहराबुद्दीन का प्रश्न उठाकर मुसलमानों को अन्यायपूर्ण ढंग से बदनाम कर रहे हैं।
इसके विपरीत गुजराती भाषा के मीडिया के आधार पर निम्न निष्कर्ष सहज ही निकलते हैं।
1. नरेन्द्र मोदी ने गुजरात से आतंकवाद को समाप्त किया है।
2. नरेन्द्र मोदी के सख्त प्रशासन के कारण ही आतंकवादी गुजरात में घुसने और कोई घटना करने से घबराते हैं।
3. सोहराबुद्दीन की घटना के बाद दूसरे आतंकवादी गुजरात में कोई वारदात करने से डरने लगे।
4. तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुसलमानों और आतंकवादियों को शह भी देती हैं और वोट की खातिर उनका तुष्टिकरण भी करती है। लेकिन मोदी वोट की खातिर किसी का तुष्टिकरण नहीं करते।
5. आतंकवाद से मुकाबला सख्ती से किया जा सकता है तुष्टिकरण से नहीं। गुजरात इस विषय में राह दिखा रहा है।
6. अफजल गुरू को फांसी न देकर कांग्रेस और सीपीएम मुसलमानों को राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करते हुए भी प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है।
इन दोनों निष्कर्षों के अवलोकन से प्रश्न उठता है कि एक ही घटना पर विदेशी भाषा का मीडिया और भारतीय भाषाओं का मीडिया लगभग परस्पर विरोधी खेमे में ही खड़ा क्याें दिखाई देता है? ऐसा क्यों है कि सोहराबुद्दीन की मुठभेड़ की घटना को लेकर गुजराती भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार अलग प्रकार से करते हैंघ् इसका मुख्य कारण विभिन्न मुद्दों और विभिन्न स्थितियों को लेकर अंग्रेजी मीडिया की मानसिकता जिस धरातल पर अवस्थित है वह गुजराती भाषा के मीडिया से या फिर भारतीय भाषा के मीडिया से बिल्कुल अलग है। एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय भाषाओं के मीडिया और विदेशी भाषाओं के मीडिया के पाठक वर्ग भी लगभग अलग-अलग ही है। भारतीय भाषाओं के मीडिया का पाठक आम आदमी है जिसमें खबर की भूख दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। विदेशी भाषा के मीडिया का वर्ग खास आदमी है, उसकी संख्या सीमित है परंतु उसका प्रभाव ज्यादा है। विभिन्न मुद्दों से संबंधित अवधारणाओं के स्तर पर भी ये दोनों पाठक वर्ग काफी अलग-अलग है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिकता को लेकर इन दोनों वर्गों की अवधारणा में जमीन आसमान का फर्क है। विदेशी भाषा के मीडिया का पाठक वर्ग ऐसी जगहों पर रहता है जहां आदमी-आदमी के बीच संपर्क भी कम है और संबंधों के स्तर पर एक और औपचारिकता बनी रहती है। इन स्थानों पर भीड़ कम है स्थान ज्यादा है। एक खुलापन भी है। आपसी संपर्क और संबंध न्यूनतम स्तर पर ही विद्यमान है। इसलिए इस वर्ग के लिए सांप्रदायिकता किताबों में पढ़ा हुआ शब्द है जिसको उसके समग्र रूप में देखपाना इनके लिए संभव ही नहीं है। यदि और ढंग से कहें तो कहा जा सकता है यह पाठक वृंद गांधीनगर का पाठक वृंद है। इसके विपरीत भारतीय भाषाओं के अथवा गुजराती भाषाओं के मीडिया का पाठक वृंद ठेठ अहमदाबाद में रहता है। उसके लिए सांप्रदायिकता महज कागज पर छपा हुआ शब्द नहीं है बल्कि नित्यप्रति के परस्पर व्यवहार और अनुभव के भीतर से उपजा और निर्मित एक यथार्थ है। उस यथार्थ में सोहराबुद्दीन नित्यप्रति मूर्त रूप में घूमता है। अफजल गुरू भी घूमता है। उनकी ऑंखें घूरती हैं और कर्म भय पैदा करते हैं। इस सांप्रदायिकता के बीच में से ही उसे नित्यप्रति गुजरना है। इसलिए उससे वह बच भी नहीं सकता। ये नित्यप्रति की संकरी गलियां हैं। जहां सांप्रदायिकता से नित्य-नित्य मुठभेड़ होती है। इन पाठकों का क्रोध इस बात से उपजता है। यह सांप्रदायिक चेहरा कभी हाजी मस्तान के रूप में प्रकट होता है, कभी दाऊद अब्राहिम के रूप में प्रकट होता है, कभी सोहराबुद्दीन के रूप में प्रकट होता है और कभी अफजल गुरू के रूप में प्रकट होता है। कभी यह तस्लीमुद्दीन बनकर आता है और कभी ईश्रतजहां बनकर रात्रि के अंधकार में निशाचरों की तरह घूमता है। राज्यसत्ता इन निशाचरों से वोट की खातिर हाथ मिला लेती है। आम आदमी का यह पाठक वर्ग इस मिलते हुए हाथ को देखता भी है और उससे सहमता भी है। आम आदमी का इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि सोहराबुद्दीन को किसने मारा और कैसे मारा? उसके मरने की खबर पर वह राहत महसूस करता है जैसे गली-मोहल्ले में घूमता हुआ कोई पागल कुत्ता मरता है तो लोग खुश होते हैं कि जीवन सुरक्षित हो गया है। लेकिन जब जीवजंतुओं के प्रति करूणा की वकालत करने वाला कोई संगठन पागल कुत्ते को मारने के खिलाफ अभियान चला दे तो स्वभाविक है यह पाठक वृंद अभियान चलाने वालों की ओर आश्चर्य भरी नजरों से ही देखेगा। विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषाओं के मीडिया की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण के अलग होने का रहस्य भी यही है। दूर से बैठकर पागल कुत्ते के प्रति करूणा की मांग करना एक बात है और उस कुत्ते के साथ रहते हुए एक दिन उसे मरा हुआ देखकर भयमुक्त होने के एहसास से प्रसन्न होना दूसरी बात है। अंग्रेजी भाषा का मीडिया इस देश में घट रही घटनाओं को दूर बैठकर केवल द्रष्टा के रूप में देखता है और भारतीय भाषाओं का मीडिया उन स्थितियों को भोक्ता के रूप में देखता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। पहले मीडिया का पाठक केवल द्रष्टा है और दूसरे मीडिया का पाठक स्वयं भोक्ता है।
रामसेतु बचाने के लिए दिल्ली में विशाल राष्ट्रीय महासभा-दूसरी घटना 30 दिसंबर 2007 को दिल्ली के स्वर्णजयंती पार्क में रामसेतु को बचाने के लिए की गई विशाल राष्ट्रीय महासभा है। इस सभा में देश के प्रत्येक हिस्से से लाखों लोगों ने शिरकत की। लद्दाख से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक के लोग आए थे। केरल से लेकर पंजाब तक से लोग स्वयं अपना किराया खर्च कर इस राष्ट्रीय सभा में भागीदारी करने के लिए आए थे। हजारों दिल्लीवासी भक्तिभाव से इन रामभक्तों के लिए भोजन तैयार करने में लगे हुए थे। अनेक मोहल्लों में रामभक्तों को रोक-रोक कर लोग आग्रहपूर्वक फल खाने को दे रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम की रपट विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषा के मीडिया में बिल्कुल ही अलग-अलग प्रकार से हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रपट इस प्रकार की थी कि लाखों लोगों के आ जाने से दिल्लीवासियों को बहुत कष्ट हुआ, सड़कों पर जाम लग गया और लोग रविवार का आनंद नहीं मना सके। दिल्ली शोर शराबे को माहौल में डूब गई। परिवहन व्यवस्था में अफरा-तफरी मच गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक करोड़ की आबादी वाले दिल्ली प्रदेश में से किसी एक महिला से इस राष्ट्रीय सभा के बारे में पूछा भी। उसने कहा कि मैं हर रविवार को मेट्रो से अपनी बहन को मिलने के लिए शाहदरा जाती हूँ लेकिन इस अव्यवस्था के कारण नहीं जा सकी। रपट का स्वर कुछ ऐसा था कि इस महिला के अपनी बहन से न मिल पाने के कारण इस राष्ट्रीय महा सभा ने बड़ा ही अहित किया है। एक अन्य अंग्रेजी अखबार ने मानो एक बहुत बड़ा रहस्योद्धाटन किया। एक सज्जन ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे। टिकट लेना उनकी आदत में शुमार नहीं था। वे टीटी को कुछ पैसे देकर सुखपूर्वक यात्रा करूँगा यह सोच कर चले थे। लेकिन रामसेतु पर हो रही इस राष्ट्रीय सभा में भाग लेने वालों की भीड़ के कारण टीटी इन सज्जन की सहायता नहीं कर सके। अंग्रेजी अखबार के अनुसार इस राष्ट्रीय सभा के कारण जनता को हो रहे कष्ट की यह पराकाष्ठा है।
इसके विपरीत दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों पंजाब केसरी और दैनिक जागरण की रपट का स्वर बिल्कुल भिन्न था। इनके अनुसार इस राष्ट्रीय सभा से सारी दिल्ली राममय हुई। रामभक्तों का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े हजारों दिल्लीवासी। दिल्ली में जगह-जगह उनका स्वागत हो रहा था और लोग उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था में संलग्न थे। दिल्ली की भारतीय भाषाओं के अखबारों ने तो कई दिन पहले से ही खबरें देनी शुरू कर दी थी कि इस राष्ट्रीय सभा में भाग लेने के लिए आ रहे रामभक्तों का स्वागत करने के लिए दिल्ली के लोग किस प्रकार की तैयारियाँ कर रहे हैं।
इन दोनों रपटों को पढ़ने के बाद प्रश्न पैदा होता है कि क्या कारण है एक ही घटना पर रपट देते हुए मीडिया का एक वर्ग कहता है कि इससे दिल्ली के लोग प्रसन्न हो रहे हैं और दूसरा वर्ग कहता है कि इससे दिल्ली के लोगों का कष्ट बढ़ रहा है। इसका कारण भी उसी मानसिकता में खोजना होगा जो विदेशी भाषा के मीडिया और भारतीय भाषा के मीडिया के पाठक वर्ग को अलग-अलग करती है। विदेशी भाषा के मीडिया का पाठक वर्ग नई कालोनियों में है। डिफे न्स कालोनी, डीएलएफ कालोनी में है, अंसल प्लाजा में है, टीडीआई में है और सरकारी बाबुओं में है। (बाबुओं से हमारा अभिप्राय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से है।) जैसा कि ऊपर हमने संकेत किया है कि दोनों वर्गों की अवधारणाओं में स्पष्ट ही अंतर है। एक वर्ग ऐसा है जो प्रात: काल ब्रह्ममुहर्त में समीप के मंदिर में हो रही आरती को सुनकर प्रसन्न होता है और दूसरा वर्ग ऐसा है जो उसी आरती को सुनकर नाक भौं सिकोड़ता है कि इससे सुबह की नींद में खलल पड़ता है। यह वही वर्ग है जो रामजन्मभूमि पर मंदिर बनाने को नकार कर वहां एकता के लिए पार्क बनाने का सुझाव देता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि पार्क से उपजी एकता एक ही खुरचन में खत्म हो जाती है । आरती से उपजी एकता लंबे अरसे तक चलती है। अंग्रेजी अखबारों और भारतीय भाषाओं के अखबारों द्वारा इस राष्ट्रीय महा सभा पर की गई रपट उनकी प्राथमिकता भी निश्चित करती है। अंग्रेजी मीडिया के लिए भारतीयता से जुड़ी चीजें और क्रियाकलाप अंग्रेजों द्वारा स्थापित सभ्यता और जीवन पध्दति में खलल पैदा करती है।
उड़ीसा के कंधमाल की घटना-उड़ीसा के कंधमाल में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी महाराज पर 24 दिसंबर को ईसाई संगठनों ने घातक आक्रमण कर दिया। स्वामी जी घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। स्वभाविक ही उड़ीसा के लोगों में इस पर प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने 4 घंटे का शांतिपूर्ण बंद रखा। गुस्से में आए कुछ लोगों ने चर्च की कुछ झोपड़ियां भी जला दीं। इन झोपड़ियों पर सलीव का निशान भी लगा हुआ था। इसलिए इनको चर्च का जलाना कहा गया। ब्राह्मणी गांव में ईसाइयों ने दो सौ लोगों के घर जला दिए। इस घटना की रपट अंग्रेजी मीडिया और उड़िया भाषा के मीडिया में बिल्कुल अलग-अलग प्रकार से आनी प्रारंभ हुई और अभी तक आ रही है। दिल्ली में स्थित लगभग विदेशी भाषा का समग्र मीडिया (एक आध अपवाद को छोड़कर) की रपट का मुख्य स्वर निम्न प्रकार से सारणीबध्द किया जा सकता है।
1. उड़ीसा में ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है और चर्च फूंके जा रहे हैं।
2. सरकार ईसाइयों की रक्षा करने में बुरी तरह असफल रही है।
इसके विपरीत उड़ीसा के उड़िया भाषी समाचार पत्रों यथा-संवाद, समाज, धरित्री, प्रजातंत्र, अमरी कथा, उड़ीसा भास्कर, पर्यवेक्षक इत्यादि में कंधमाल की घटना को लेकर जो रपटें छप रही है उनका मुख्य स्वर निम्न प्रकार से है।
1. ईसाई मिशनरियां व्यापक स्तर पर उड़ीसा के जनजातीय लोगों के घरों को जला रही है। लोगों को धमकाया जा रहा है।
2. मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है ।
3. सरकार उड़ीसा के लोगों की ईसाई मिशनरियों के आक्रमणों से रक्षा नहीं कर पा रही।
4. ईसाई मिशनरियों के इशारे पर एक सांसद इन आक्रमणों को भड़का रहा है।
5. माओवादी और चर्च उड़ीसा के लोगों पर आक्रमण करने में आपस में मिल गए हैं।
6. जनजाति के लोगों पर आधुनिक हथियारों से आक्रमण किये जा रहे हैं।
विदेशी भाषा के मीडिया की प्राथमिकताएं और भारतीय भाषाओं के मीडिया की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए जब किसी मंदिर में लोग भजन कीर्तन के लिए एकत्रित होते हैं तो भारतीय भाषा के मीडिया के लिए यह भक्ति का ज्वार उमडना है लेकिन अंग्रेजी मीडिया के लिए यह शोर शराबा और सामान्य जीवन में होने वाला खलल है। उसका कारण शायद भारत में अंग्रेजों के शासन काल से ही खोजना होगा। अग्रेजों के लिए मंदिर के भीड खलल भी है और खतरा भी है। उसी मानसिकता को आज तक विदेशी भाषा अंग्रेजी का मीडिया ढो रहा है और इसी प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी मीडिया किसी भी घटना की रपट करता है।
इस मानसिकता और प्राथमिकता का एक और कारण भी है । जिन दिनों अंग्रेज इस देश पर राज करते थे, वे यहां के भारतीय समाज को अपने लिए खतरा समझते थे और मुस्लिम समाज एवं ईसाई समाज को अपना पक्षधर मानते थे। इसलिए बहुसंख्यक भारतीय समाज का कोई भी कृत्य उनकी दृष्टि में निंदनीय और ईसाई व मुस्लिम समाज के लिए खतरनाक माना जाता था। अंग्रेजी मीडिया आज भी उसी मानसिकता को ढो रहा है। यही कारण है कि गुजरात का जननिर्णय,रामसेतु को लेकर हुई राष्ट्रीय महासभा और उडिया अस्मिता के लिए संघर्षरत ओडिया लोग अंग्रेजी मीडिया की दृष्टि में खतरनाक कृत्य हैं और मुस्लिम व ईसाई समाज के हितों के विपरीत हैं ।
सारत: विदेशी भाषा के मीडिया की जडें ब्रिटिश शासनकाल की मानसिकता में गहरे धंसी हुई हैं। इसके विपरीत भारतीय भाषाओं के मीडिया की जडें उसी संघर्ष में से उपजी हैं जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आम भारतीय ने किया था ।
(नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
पाकिस्तान की राजनीति का रक्तरंजित इतिहास
लेखक- संतोष कुमार मधुप
पाकिस्तान की स्थापना से लेकर आज तक इस देश की राजनीति हिंसा और रक्तपात की बुनियाद पर चलती रही है। लियाकत अली से लेकर बेनजीर भुट्टो तक सभी इसी रक्तरंजित राजनीति के शिकार हुए हैं। वर्षों से हत्या और आतंक पाकिस्तान की राजनीति का अभिन्न अंग बना हुआ है। वहाँ जनतांत्रिक चेतना और मूल्यबोध बहुत पहले लुप्त हो चुके हैं। 1947 में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ के लोगों को यह समझाने की कोशिश की थी कि शांति, प्रेम, भाईचारा और लोकतांत्रिक भावना इस्लामी विचारधारा से जुङे हुए हैं, अत: पाकिस्तान की राजनीति को लेकर चिन्ता का कोई कारण नहीं है। लेकिन जिन्ना का यह भरोसा अधिक दिनो तक कायम नहीं रह सका और खुद उनके उपर भी जानलेवा हमला हुआ। हालाँकि उस हमले के पीछे अन्य तरह के कारण थे। दरअसल पाकिस्तान के बहुत से लोग विभाजन से खुश नहीं थे। बहुतों ने अपना सब कुछ खोकर पाकिस्तान में आश्रय लिया था। उस पर तत्कालीन राजनेताओं की महात्वाकांक्षा और सत्ता लोलुपता ने पाकिस्तान की राजनीति को शुरु में ही अस्थिर कर दिया। पाकिस्तान को जन्म के साथ मिली राजनीतिक अस्थिरता की सौगात के कारण राजनीतिक द्वेष बढता रहा और हिंसा होती रही।
इस हिंसा के पहले शिकार बने लियाकत अली। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जनसभा को संबोधित करने गए लियाकत अली की गोली मार कर हत्या कर दी गई। जिन्ना की तरह वे भी एक सुखी और समृध्द पाकिस्तान की कल्पना करते थे और उन्होंने भारत के साथ कुछ समझौते भी किए थे। कट्टरवादी उनकी राजनीति पसन्द नहीं करते थे। उन्हें पता था कि लोकतांत्रिक तरीके से लियाकत अली को हटाना संभव नहीं है इसलिए उन्होंने बंदूक का सहारा लिया। उसके बाद से पाकिस्तान में अधिनायकवाद और सैन्य शासन का दौर प्रारंभ हुआ। 1954 में अयूब खान द्वारा सत्ता हथिया लिए जाने के साथ ही पाकिस्तान में सैन्य शासन का नया सिलसिला शुरु हुआ। अयूब खान के बाद 1969 में याहिया खान ने सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन दो सालों बाद उन्हें सत्ता छोङनी पङी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल की लेकिन उनके शासन काल में भी सामरिक और सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होती रही। परिणामस्वरूप जनरल जियाउल हक ने उनका तख्ता पलट कर एक बार फिर पाकिस्तान की सत्ता पर सेना का एकाधिकार कायम कर लिया। 4 अप्रैल 1979 को सुनियोजित तरीके से एक पुराने कत्ल के मामले में मुकदमा चला कर भुट्टो को फाँसी दे दी गई। जियाउल हक का अन्त भी सुखद नहीं रहा और 16 नवम्बर 1988 को रहस्यमय तरीके से एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर पाकिस्तान की सेना और गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के साथ-साथ अमेरिका की सीआईए और रूस की केजीबी की ओर भी शक की उंगली उठी थी। लेकिन उनकी मौत आज तक रहस्य बना हुआ है।
इसी दौरान पाकिस्तान की राजनीति में बेनजीर भुट्टो का अभ्युदय हुआ। 1988 के आम चुनाव में उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और बेनजीर देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन वे अधिक दिनो तक सत्ता नहीं संभाल सकी और अल्पावधि में ही भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों के कारण उन्हें कुर्सी छोङनी पङी। उनके पति आसिफ अली जरदारी को अपहरण के मामले में गिरतार कर लिया गया। उसके बाद हुए चुनाव नवाज शरीफ की पार्टी विजयी रही और वे प्रधानमंत्री बने। बेनजीर को अगले तीन सालों तक विपक्ष में बैठना पङा। 1993 के आम चुनाव में एक बार फिर पीपीपी की जीत हुई और बेनजीर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रही। लेकिन एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई और इस बार पति जरदारी के साथ बेनजीर को भी रिश्वतखोरी के मामले में जेल जाना पडा।
1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तखता पलट कर लोकतंत्र का मखौल उङाते हुए पाकिस्तान में पुन: सामरिक शासन स्थापित किया। नवाज शरीफ को दर-बदर कर मुशर्रफ लंदन में रह रही बेनजीर को भी गिरतारी का भय दिखाते रहे। मुशर्रफ के शासन में हुए आम चुनाव में 382 में से 80 सीटें मिली लेकिन बेनजीर देश लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। क्योंकि मुशर्रफ ने पाकिस्तान लौटते ही उन्हें सलाखों के पीछे डालने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वर्ष 2007 में बेनजीर और मुशर्रफ के बीच समझौते के सुर सुनाई पङे। बेनजीर ने इस्लामाबाद के लाल मस्जिद में कट्टरपंथियों के खिलाफ मुशर्रफ की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। ऐसा कर उन्होंने कट्टरपंथियों की नाराजगी जरूर मोल ले ली पर इससे उनकी पाकिस्तान वापसी का रास्ता भी साफ हो गया। आखिरकार 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर वापस लौटीं और पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में नया जोश उमर पङा। लेकिन इसके साथ ही उनकी जान लेने की कोशिशें भी शुरु हो गई।
पाकिस्तान आगमन के साथ ही उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में वे खुद तो बच गईं लेकिन उनके स्वागत में खङे सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई। आखिरकार 27 दिसम्बर 2007 को बेनजीर भी पाकिस्तान की खूनी राजनीति की शिकार हो गई। उनकी हत्या में मुशर्रफ या उनकी सरकार का हाथ था या नहीं यह कहना मुश्किल है, परन्तु जिस तरह उनकी मौत के कारणों को लेकर नए-नए रहस्य पैदा किए गए उससे भयानक राजनीतिक षडयंत्र की बू आ रही है। गौरतलब है कि उसी दिन एक और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के काफिले पर भी गोलिया दागी गई। खुद नवाज शरीफ ने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। पाकिस्तान पूरी तरह से कृत्रिम अराजकता का शिकार है। यहाँ बैलेट की बजाए बुलेट पर भरोसा करने की परम्परा रही है। बेनजीर खूनी सियासत की शिकार होने वाली पहली या आखिरी शख्स नहीं थीं। यह सिलसिला चलता रहेगा। पता नहीं कब तक।
(नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
पाकिस्तान की स्थापना से लेकर आज तक इस देश की राजनीति हिंसा और रक्तपात की बुनियाद पर चलती रही है। लियाकत अली से लेकर बेनजीर भुट्टो तक सभी इसी रक्तरंजित राजनीति के शिकार हुए हैं। वर्षों से हत्या और आतंक पाकिस्तान की राजनीति का अभिन्न अंग बना हुआ है। वहाँ जनतांत्रिक चेतना और मूल्यबोध बहुत पहले लुप्त हो चुके हैं। 1947 में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ के लोगों को यह समझाने की कोशिश की थी कि शांति, प्रेम, भाईचारा और लोकतांत्रिक भावना इस्लामी विचारधारा से जुङे हुए हैं, अत: पाकिस्तान की राजनीति को लेकर चिन्ता का कोई कारण नहीं है। लेकिन जिन्ना का यह भरोसा अधिक दिनो तक कायम नहीं रह सका और खुद उनके उपर भी जानलेवा हमला हुआ। हालाँकि उस हमले के पीछे अन्य तरह के कारण थे। दरअसल पाकिस्तान के बहुत से लोग विभाजन से खुश नहीं थे। बहुतों ने अपना सब कुछ खोकर पाकिस्तान में आश्रय लिया था। उस पर तत्कालीन राजनेताओं की महात्वाकांक्षा और सत्ता लोलुपता ने पाकिस्तान की राजनीति को शुरु में ही अस्थिर कर दिया। पाकिस्तान को जन्म के साथ मिली राजनीतिक अस्थिरता की सौगात के कारण राजनीतिक द्वेष बढता रहा और हिंसा होती रही।
इस हिंसा के पहले शिकार बने लियाकत अली। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जनसभा को संबोधित करने गए लियाकत अली की गोली मार कर हत्या कर दी गई। जिन्ना की तरह वे भी एक सुखी और समृध्द पाकिस्तान की कल्पना करते थे और उन्होंने भारत के साथ कुछ समझौते भी किए थे। कट्टरवादी उनकी राजनीति पसन्द नहीं करते थे। उन्हें पता था कि लोकतांत्रिक तरीके से लियाकत अली को हटाना संभव नहीं है इसलिए उन्होंने बंदूक का सहारा लिया। उसके बाद से पाकिस्तान में अधिनायकवाद और सैन्य शासन का दौर प्रारंभ हुआ। 1954 में अयूब खान द्वारा सत्ता हथिया लिए जाने के साथ ही पाकिस्तान में सैन्य शासन का नया सिलसिला शुरु हुआ। अयूब खान के बाद 1969 में याहिया खान ने सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन दो सालों बाद उन्हें सत्ता छोङनी पङी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल की लेकिन उनके शासन काल में भी सामरिक और सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होती रही। परिणामस्वरूप जनरल जियाउल हक ने उनका तख्ता पलट कर एक बार फिर पाकिस्तान की सत्ता पर सेना का एकाधिकार कायम कर लिया। 4 अप्रैल 1979 को सुनियोजित तरीके से एक पुराने कत्ल के मामले में मुकदमा चला कर भुट्टो को फाँसी दे दी गई। जियाउल हक का अन्त भी सुखद नहीं रहा और 16 नवम्बर 1988 को रहस्यमय तरीके से एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर पाकिस्तान की सेना और गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के साथ-साथ अमेरिका की सीआईए और रूस की केजीबी की ओर भी शक की उंगली उठी थी। लेकिन उनकी मौत आज तक रहस्य बना हुआ है।
इसी दौरान पाकिस्तान की राजनीति में बेनजीर भुट्टो का अभ्युदय हुआ। 1988 के आम चुनाव में उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और बेनजीर देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन वे अधिक दिनो तक सत्ता नहीं संभाल सकी और अल्पावधि में ही भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों के कारण उन्हें कुर्सी छोङनी पङी। उनके पति आसिफ अली जरदारी को अपहरण के मामले में गिरतार कर लिया गया। उसके बाद हुए चुनाव नवाज शरीफ की पार्टी विजयी रही और वे प्रधानमंत्री बने। बेनजीर को अगले तीन सालों तक विपक्ष में बैठना पङा। 1993 के आम चुनाव में एक बार फिर पीपीपी की जीत हुई और बेनजीर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रही। लेकिन एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई और इस बार पति जरदारी के साथ बेनजीर को भी रिश्वतखोरी के मामले में जेल जाना पडा।
1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तखता पलट कर लोकतंत्र का मखौल उङाते हुए पाकिस्तान में पुन: सामरिक शासन स्थापित किया। नवाज शरीफ को दर-बदर कर मुशर्रफ लंदन में रह रही बेनजीर को भी गिरतारी का भय दिखाते रहे। मुशर्रफ के शासन में हुए आम चुनाव में 382 में से 80 सीटें मिली लेकिन बेनजीर देश लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। क्योंकि मुशर्रफ ने पाकिस्तान लौटते ही उन्हें सलाखों के पीछे डालने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वर्ष 2007 में बेनजीर और मुशर्रफ के बीच समझौते के सुर सुनाई पङे। बेनजीर ने इस्लामाबाद के लाल मस्जिद में कट्टरपंथियों के खिलाफ मुशर्रफ की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। ऐसा कर उन्होंने कट्टरपंथियों की नाराजगी जरूर मोल ले ली पर इससे उनकी पाकिस्तान वापसी का रास्ता भी साफ हो गया। आखिरकार 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर वापस लौटीं और पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में नया जोश उमर पङा। लेकिन इसके साथ ही उनकी जान लेने की कोशिशें भी शुरु हो गई।
पाकिस्तान आगमन के साथ ही उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में वे खुद तो बच गईं लेकिन उनके स्वागत में खङे सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई। आखिरकार 27 दिसम्बर 2007 को बेनजीर भी पाकिस्तान की खूनी राजनीति की शिकार हो गई। उनकी हत्या में मुशर्रफ या उनकी सरकार का हाथ था या नहीं यह कहना मुश्किल है, परन्तु जिस तरह उनकी मौत के कारणों को लेकर नए-नए रहस्य पैदा किए गए उससे भयानक राजनीतिक षडयंत्र की बू आ रही है। गौरतलब है कि उसी दिन एक और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के काफिले पर भी गोलिया दागी गई। खुद नवाज शरीफ ने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। पाकिस्तान पूरी तरह से कृत्रिम अराजकता का शिकार है। यहाँ बैलेट की बजाए बुलेट पर भरोसा करने की परम्परा रही है। बेनजीर खूनी सियासत की शिकार होने वाली पहली या आखिरी शख्स नहीं थीं। यह सिलसिला चलता रहेगा। पता नहीं कब तक।
(नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
बिहार: नक्सलियों का बढ़ता आतंक
लेखक-नवल निराला
बिहार में नक्सली गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों ने बिहार में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। 10 दिसम्बर की रात वैशाली के सुक्की में नक्सलियों ने हमलाकर तीन लोगों की हत्या कर दी। जमुई में नक्सलियों द्वारा दो व्यवसायियों तथा शिवहर में एक दफादार की हत्या के साथ ही देव (औरंगाबाद) में चौकीदार को अपहृत कर पीटने, गया में डायनामाइट से किसानों के घर उड़ाने, लखीसराय में रेल पटरी को क्षतिग्रस्त करने तथा रून्नी सैदपुर (सीतामढ़ी) की ताजा घटना से स्पष्ट है कि राज्य में नक्सली तेजी से पांव पसार रहे हैं। इससे पूर्व गोपालगंज स्टेशन कांड, मनियापुर (राजेपुर) कांड, मसही (सारण) कांड, सीतामढ़ी का रीगा कांड तथा पूर्वी चंपारण का चर्चित मधुबन कांड बिहार में नक्सलियों के बढ़ते दु:साहस का परिचायक है। उपरोक्त सभी घटनाओं में बिहार पुलिस नक्सलियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई करने में विफल रही है। यद्यपि रीगा में तैनात सशस्त्र बलों ने वहां घटना को नाकाम कर दिया था तथा नक्सली अपने मंसूबे में पूरी तरह असफल रहे थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि राज्य में जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की पुनरावृति हो जाये, तो कोई आश्चर्य नहीं। रीगा कांड में जिस तरह खुफिया तंत्र की विफलता उजागर हुई, उससे इस तरह की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। मालूम हो कि जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में नक्सली पूरे जेल पर कब्जा कर वहां बंद अपने साथियों को भगा ले गये थे। तब नक्सलियों के साथ ही जेल में बंद अन्य अपराधी भी जेल से भाग निकलने में सफल हुए थे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे सीमावर्ती जिले इन दिनों नक्सलियों के निशाने पर हैं। इन जिलों में बढ़ी नक्सली गतिविधियों तथा उनकी कारगुजारियों से पुलिस के साथ ही इलाके के लोग भी दहशत में हैं। इन इलाकों में नक्सलियों द्वारा पोस्टर चिपकाकर लोगों को धमकी देने की घटना आम हो गयी है।
दो दशक पूर्व उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर का मुसहरी तथा मीनापुर प्रखंड ही नक्सलियों का केन्द्र हुआ करता था। लेकिन इस दौरान नक्सलियों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने कार्यक्षेत्र का व्यापक विस्तार किया है। अब वे मुजफ्फरपुर से निकलकर पश्चिम में नरकटियागंज से लेकर पूर्व में सीतामढ़ी तक फैल गये हैं।
नरकटियागंज, मोतिहारी, रक्सौल, घोड़ासहान, आदापुर, वैरगनियां, ढेंग, मेजरगंज, पुरनहिया, शिवहर, सोनबरसा तथा सीतामढ़ी माओवादियों के आसान लक्ष्य बने हैं। गत वर्षों में पूर्वी चंपारण का मधुबन कांड, शिवहर के पुरनहिया तथा पिपराही में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ तथा वैशाली- जंदाहा बैंक लूट कांड की घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। इनमें मधुबन कांड एक बड़ी घटना थी। तब नक्सलियों के मुखालफत के कारण सांसद सीताराम सिंह उनके निशाने पर थे। यद्यपि उस घटना में सीताराम सिंह को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह उनके आवास, बैंक तथा थाने पर नक्सलियों ने भारी उत्पात मचाकर लूट-पाट, हिंसा की, वह दिल दहला देने वाली थी।
इन दिनों नेपाल से सटा सीमावर्ती इलाका भी नक्सलियों के लिए अभ्यारण्य बन गया है। जहां सीमा पार के माओवादियों से भी उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। भारत तथा नेपाल, दोनों तरफ के माओवादियों में आपसी तालमेल है। भारत-नेपाल सीमा के खुली रहने का लाभ भी इन माओवादियों को मिल रहा है। नेपाल में शाही सेनाओं द्वारा सख्ती किये जाने पर नेपाली माओवादी भारतीय सीमाओं में आ छुपते हैं और बिहार पुलिस द्वारा धर-पकड़ तेज की जाती है, तब यहां के माओवादी सीमा पार भाग जाते हैं। इसके अलावा इन माओवादियों के तार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड के नक्सलियों से भी जुड़े बताये जाते हैं। जहां से इनको भारी समर्थन के साथ ही हथियारों की भी आपूर्ति होती है।
बहरहाल, बिहार का सीमावर्ती इलाका नक्सलियों का केन्द्र बना हुआ है। नक्सली तथा माओवादी आये दिन नई-नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस कारण पुलिस प्रशासन के साथ ही आम जनता भी दहशत में है। सरकार को चाहिए कि वह अपने खुफिया तंत्र के जाल को और अधिक विकसित करे। साथ ही, नक्सलियों की धर-पकड़ तथा उनके साथ कठोरता की कार्रवाई अनवरत चलती रहनी चाहिए। साभार- पांचजन्य
बिहार में नक्सली गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों ने बिहार में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। 10 दिसम्बर की रात वैशाली के सुक्की में नक्सलियों ने हमलाकर तीन लोगों की हत्या कर दी। जमुई में नक्सलियों द्वारा दो व्यवसायियों तथा शिवहर में एक दफादार की हत्या के साथ ही देव (औरंगाबाद) में चौकीदार को अपहृत कर पीटने, गया में डायनामाइट से किसानों के घर उड़ाने, लखीसराय में रेल पटरी को क्षतिग्रस्त करने तथा रून्नी सैदपुर (सीतामढ़ी) की ताजा घटना से स्पष्ट है कि राज्य में नक्सली तेजी से पांव पसार रहे हैं। इससे पूर्व गोपालगंज स्टेशन कांड, मनियापुर (राजेपुर) कांड, मसही (सारण) कांड, सीतामढ़ी का रीगा कांड तथा पूर्वी चंपारण का चर्चित मधुबन कांड बिहार में नक्सलियों के बढ़ते दु:साहस का परिचायक है। उपरोक्त सभी घटनाओं में बिहार पुलिस नक्सलियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई करने में विफल रही है। यद्यपि रीगा में तैनात सशस्त्र बलों ने वहां घटना को नाकाम कर दिया था तथा नक्सली अपने मंसूबे में पूरी तरह असफल रहे थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि राज्य में जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की पुनरावृति हो जाये, तो कोई आश्चर्य नहीं। रीगा कांड में जिस तरह खुफिया तंत्र की विफलता उजागर हुई, उससे इस तरह की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। मालूम हो कि जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में नक्सली पूरे जेल पर कब्जा कर वहां बंद अपने साथियों को भगा ले गये थे। तब नक्सलियों के साथ ही जेल में बंद अन्य अपराधी भी जेल से भाग निकलने में सफल हुए थे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे सीमावर्ती जिले इन दिनों नक्सलियों के निशाने पर हैं। इन जिलों में बढ़ी नक्सली गतिविधियों तथा उनकी कारगुजारियों से पुलिस के साथ ही इलाके के लोग भी दहशत में हैं। इन इलाकों में नक्सलियों द्वारा पोस्टर चिपकाकर लोगों को धमकी देने की घटना आम हो गयी है।
दो दशक पूर्व उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर का मुसहरी तथा मीनापुर प्रखंड ही नक्सलियों का केन्द्र हुआ करता था। लेकिन इस दौरान नक्सलियों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने कार्यक्षेत्र का व्यापक विस्तार किया है। अब वे मुजफ्फरपुर से निकलकर पश्चिम में नरकटियागंज से लेकर पूर्व में सीतामढ़ी तक फैल गये हैं।
नरकटियागंज, मोतिहारी, रक्सौल, घोड़ासहान, आदापुर, वैरगनियां, ढेंग, मेजरगंज, पुरनहिया, शिवहर, सोनबरसा तथा सीतामढ़ी माओवादियों के आसान लक्ष्य बने हैं। गत वर्षों में पूर्वी चंपारण का मधुबन कांड, शिवहर के पुरनहिया तथा पिपराही में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ तथा वैशाली- जंदाहा बैंक लूट कांड की घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। इनमें मधुबन कांड एक बड़ी घटना थी। तब नक्सलियों के मुखालफत के कारण सांसद सीताराम सिंह उनके निशाने पर थे। यद्यपि उस घटना में सीताराम सिंह को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह उनके आवास, बैंक तथा थाने पर नक्सलियों ने भारी उत्पात मचाकर लूट-पाट, हिंसा की, वह दिल दहला देने वाली थी।
इन दिनों नेपाल से सटा सीमावर्ती इलाका भी नक्सलियों के लिए अभ्यारण्य बन गया है। जहां सीमा पार के माओवादियों से भी उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। भारत तथा नेपाल, दोनों तरफ के माओवादियों में आपसी तालमेल है। भारत-नेपाल सीमा के खुली रहने का लाभ भी इन माओवादियों को मिल रहा है। नेपाल में शाही सेनाओं द्वारा सख्ती किये जाने पर नेपाली माओवादी भारतीय सीमाओं में आ छुपते हैं और बिहार पुलिस द्वारा धर-पकड़ तेज की जाती है, तब यहां के माओवादी सीमा पार भाग जाते हैं। इसके अलावा इन माओवादियों के तार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड के नक्सलियों से भी जुड़े बताये जाते हैं। जहां से इनको भारी समर्थन के साथ ही हथियारों की भी आपूर्ति होती है।
बहरहाल, बिहार का सीमावर्ती इलाका नक्सलियों का केन्द्र बना हुआ है। नक्सली तथा माओवादी आये दिन नई-नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस कारण पुलिस प्रशासन के साथ ही आम जनता भी दहशत में है। सरकार को चाहिए कि वह अपने खुफिया तंत्र के जाल को और अधिक विकसित करे। साथ ही, नक्सलियों की धर-पकड़ तथा उनके साथ कठोरता की कार्रवाई अनवरत चलती रहनी चाहिए। साभार- पांचजन्य
मनमोहन सिंह युग प्रवर्तक अथवा विदेश नीति के विध्वंसक
लेखक : रामजी प्रसाद सिंह
अमेरिका के साथ आणविक संधि कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक जुआ खेला है। अगर ये सफल हो गया तो वे एक युग प्रवर्तक माने जाएंगे अथवा भारत की विदेश नीति के विध्वसंक के रूप में उनकी निंदा की जाएगी। अमेरिका के साथ भारत का संबध कभी भी ज्यादा मधुर नहीं रहा। नेहरू युग में जब भारत नवनिर्माण की नींव डालने के महाअभियान का सूत्रपात कर रहा था, तब अमेरिका के साथ दो महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, एक पीएल-480 के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति का समझौता और दूसरा तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए सवंर्धित यूरोनियम(ईंधन) देने का समझौता। खाद्ययान देने के समझौते को जिस तरह से लागू किया गया, उसके कारण भारत को 1964-67 के अकाल का सामना करने में मदद अवश्य मिली, लेकिन इससे अमेरिका को होने वाली आय का जिस प्रकार से उपयोग किया गया, उससे भारत को काफी नुकसान हुआ। उस धन का उपयोग कर अमेरिका ने भारत में कुछ राजनीतिक दलों की मदद कर अपने पक्ष में जनमत तैयार करने की चेष्टा की। ठेठ भाषा में कहा जाएगा कि इस धन का उपयोग कर अमेरिका ने भारत के राजनेताओं और जनमत बनाने वाले बुध्दिजीवियों को खरीदने की चेष्टा की। निश्चित रूप से अमेरिका भारत की विदेश नीति को प्रभावित करना चाहता था। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की निर्गुटता की नीति को अमेरिका ध्वस्त करना चाहता था। उसे लगता था कि भारत की निर्गुटता की विदेश नीति का झुकाव सोवियत संघ की ओर है। यानि जो हमारा दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। इसलिए उसने भारत की प्राकृतिक आपदाओं (सुखे और बाढ़) का फायदा उठा कर अत्यंत लोकप्रिय प्रधानंमत्री जवाहर लाल नेहरू को कमजोर करने की ठान ली।
नेहरू काल में भारत में अणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। आणविक उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में भी बहुविध प्रयास शुरू हो चुके थे। परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार के अनुसंधान शुरू हो चुके थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में कृषि, औषधी-विज्ञान और उद्योग के विकास के लिए परमाणु उर्जा के उपयोग पर व्यापक कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। 1956 में भारत की पहली परमाणु शोध भट्टी 'अप्सरा' चालू हो चुकी थी। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम और भारी जल का उपयोग कर 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन आरंभ हो गया था। देश की पहली परमाणु उर्जा भट्टी (संवर्धित यूरेनियम पर अधारित) की स्थापना तारापुर में की गई थी। इसके लिए 200 मेगावाट की दो परमाणु भट्टियां एक अमेरिकी फर्म से खरीदी गई थी। इसके लिए ईंधन की आपूर्ति अमेरिका करने के लिए वचनबध्द था। उसने ईंधन भेजना भी शरू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप इसे रिएक्टर ने 1 अप्रैल 1969 से काम करना शुरू कर दिया था। किंतु दो साल के अंदर अमेरिका ने संवंर्धित यूरेनियम की सप्लाई की मात्रा में कमी कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को उस बिजली घर को चालू रखने के लिए उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता बहुत घटानी पड़ गई।
इंदिरा सरकार में विदेशमंत्री के रूप में श्री नरसिम्हा राव इस विषय पर बात करने के लिए अमेरिका गए, किंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इस विषय पर उन्होंने बड़े ही कूटनीतिक भाषा में लोकसभा को बताया कि तारापुर बिजली घर को संर्विधत यूरेनियम देने के बारे में अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ, था उसकी अकाल मृत्यु हो गई, किंतु तरीके से उसको दफन किया जाना बाकी है।
इसके बाद इंदिरा सरकार सावधान हो गई और अपने आतंरिक साधनों से परमाणु उर्जा की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वैकल्पिक ईंधन की खोज शरू हो गई। तमिलनाडु के कल्पकम्म में 500 मेगावाट की क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिडर रिएक्टर तैयार किया गया, जिसमें प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद चौथा परमाणु उर्जा संयत्र उत्तर प्रदेश के नरौला में और पांचवा गुजरात के कतरापुर में स्थापित किया गया। साथ ही यूरेनियम का खनन और निस्कस्कण्र के अलावा भारत ने प्रयुक्त परमाणु कचरे को दोबारा इस्तेमाल में लाने की तकनीक भी प्राप्त कर ली। परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन का पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने के बाद 11 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने राजस्थान के पोखरण की मरूभूमि में पहला परमाणु विस्फोट कर संसार को हैरान कर दिया। यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य परमाणु हथियार बनाने का कदापि नहीं था, तथापि अमेरिका ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, इसके कारण परमाणु उपकरण बनाने वाले अन्य देशों ने भी भारत को मदद देना बंद कर दिया। किंतु भारत ने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने वैज्ञानिकों की बदौलत परमाणु हथियार बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली।
1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक साथ पांच परमाणु विस्फोट कर दुनिया को बता दिया कि भारत संसार का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गया है। अटल सरकार ने परमाणु विस्फोटों की शृंखला में पंद्रह टन की क्षमता के हाइड्रोजन बम का भी विस्फोट किया था। फिर भी अमेरिका या संसार की दुसरी महाशक्तियों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की पंक्ति में शामिल नहीं किया है। यद्यपि भारत ने बार-बार संसार को आश्वस्त किया कि वो अपने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल निर्माण, विकास और शांति के लिए करेगा। भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी देश पर हमला करने के लिए आरंभ नहीं किया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां तक कहा कि भारत अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल केवल जवाबी हमले के तौर पर करेगा, किंतु भारत की इस सदाशयता की इस नीति पर अमेरिका या किसी अन्य महाशक्ति की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। उल्टे भारत पर आणविक अप्रसार संधि और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए तरह-तरह के दवाब डालने की कोशिश जारी रही।
सन् 1977 के बाद भारत में कई बार अल्पजीवी सरकार बनी। परंतु किसी ने देश की विदेश नीति अथवा आणविक नीति में किसी प्रकार का परिर्वतन करना स्वीकार नहीं किया। महाशक्तियों के कड़े प्रतिबंध के बावजूद भारत अपनी नीति पर डटा रहा। इसी बीच अमेरिका पर अलकायदा के हमले के फलस्वरूप अमेरिका को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा और भारत को आतंकवाद विरोधी विश्व की लड़ाई में अपना भागीदार बनाने के सिवा उसे कोई और विकल्प दिखाई नहीं पड़ा। नतीजा उसे अपनी आर्थिक, राजनीतिक और विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा और भारत के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग का हाथ बढ़ाना पड़ा। भारत-अमेरिका परमाणु संधि इसी की ताजी कड़ी है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस पर आमादा हैं। किंतु अफगानिस्तान और इराक में मुंह की खाने के बाद उनका अमेरिका की राजनीति पर प्रभुत्व समाप्त प्राय हो गया है। अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। उसमें निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार सफल होता दिख रहा है। उसके बाद इस संधि का क्या रूप होगा, यह कहना मुश्किल है। किंतु हर सुबह रात की कहानी बता देता है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जिनका संसद में बहुतम है, भारत अमेरिका आणविक संधि से असहमत हैं। इसलिए आज बुश के दवाब में आकर वे इस संधि पर अपनी मुहर लगा भी दें। तो भी यह पूरी तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति पद हासिल करने के बाद भी वे समझौते पर ईमानदारी से अमल करेंगे।
अगर अमेरिका पीछे हटने लगेगा तो आणविक उपकरणों की सप्लाई करने वाले 44 अन्य देशों के भी पैर लड़खड़ाने लगेंगे। ऐसी अवस्था में भारत को सतत् जागरूक रहना होगा और अमेरिका के भरोसे अपनी कोई योजना बनाने से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा, और वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखना होगा।
अमेरिका ने अपनी आणविक नीति में भारत के लिए विशेष छूट दी है, ये सही है। किंतु इसके पीछे हो सकता है कि वह एशिया में अपनी शक्ति संचय करना चाहता है। ये भी संभव है कि वो चीन के मुकाबले भारत को खड़ा करने की कूटनीतिक चाल चल रहा हो। यह भी संभव है कि अफगानिस्तान मोर्चे पर पाकिस्तान से उसकी जो उम्मीदें थीं, वह पूरी नहीं हुईं, इसके कारण अब वो भारत को अपने आगोश में लेने की तैयारी कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि वह एशिया में नया शक्ति संतुलन पैदा करना चाहता हो। यह भी संभव है वो कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान को लड़ा कर दोनों को बर्बाद करना चाहता हो।
अमेरिका यदि भारत के प्रति मैत्री और सहयोग का संबंध बढ़ाना चाहता, तो सबसे पहले उसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए आगे बढ़कर भारत को उसका न्यायपूर्ण अधिकार दिलाने का प्रयास करता। क्योंकि ये सर्वविदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूनर्गठन की रिपोर्ट आई तो अमेरिका ने दो टूक कहा कि वो सुरक्षा परिषद के विस्तार की स्थिति में जर्मनी और जापान को इसकी सदस्यता दिलाने का प्रयास करेगा। यूएन के महासचिव के चुनाव के समय अमेरिका ने भारत के शशि थरूर की तुलना में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान-की-मून का समर्थन किया।
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत को अमेरिका से सदैव सावधान रहना चाहिए। भारत को निर्गुटता की अपनी विदेश नीति को धारदार बनाकर महाशक्तियों की होड़ से अपने को दूर रखकर ही देश की आधारशिला को मजबूत करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
(नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
अमेरिका के साथ आणविक संधि कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक जुआ खेला है। अगर ये सफल हो गया तो वे एक युग प्रवर्तक माने जाएंगे अथवा भारत की विदेश नीति के विध्वसंक के रूप में उनकी निंदा की जाएगी। अमेरिका के साथ भारत का संबध कभी भी ज्यादा मधुर नहीं रहा। नेहरू युग में जब भारत नवनिर्माण की नींव डालने के महाअभियान का सूत्रपात कर रहा था, तब अमेरिका के साथ दो महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, एक पीएल-480 के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति का समझौता और दूसरा तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए सवंर्धित यूरोनियम(ईंधन) देने का समझौता। खाद्ययान देने के समझौते को जिस तरह से लागू किया गया, उसके कारण भारत को 1964-67 के अकाल का सामना करने में मदद अवश्य मिली, लेकिन इससे अमेरिका को होने वाली आय का जिस प्रकार से उपयोग किया गया, उससे भारत को काफी नुकसान हुआ। उस धन का उपयोग कर अमेरिका ने भारत में कुछ राजनीतिक दलों की मदद कर अपने पक्ष में जनमत तैयार करने की चेष्टा की। ठेठ भाषा में कहा जाएगा कि इस धन का उपयोग कर अमेरिका ने भारत के राजनेताओं और जनमत बनाने वाले बुध्दिजीवियों को खरीदने की चेष्टा की। निश्चित रूप से अमेरिका भारत की विदेश नीति को प्रभावित करना चाहता था। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की निर्गुटता की नीति को अमेरिका ध्वस्त करना चाहता था। उसे लगता था कि भारत की निर्गुटता की विदेश नीति का झुकाव सोवियत संघ की ओर है। यानि जो हमारा दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। इसलिए उसने भारत की प्राकृतिक आपदाओं (सुखे और बाढ़) का फायदा उठा कर अत्यंत लोकप्रिय प्रधानंमत्री जवाहर लाल नेहरू को कमजोर करने की ठान ली।
नेहरू काल में भारत में अणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। आणविक उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में भी बहुविध प्रयास शुरू हो चुके थे। परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार के अनुसंधान शुरू हो चुके थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में कृषि, औषधी-विज्ञान और उद्योग के विकास के लिए परमाणु उर्जा के उपयोग पर व्यापक कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। 1956 में भारत की पहली परमाणु शोध भट्टी 'अप्सरा' चालू हो चुकी थी। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम और भारी जल का उपयोग कर 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन आरंभ हो गया था। देश की पहली परमाणु उर्जा भट्टी (संवर्धित यूरेनियम पर अधारित) की स्थापना तारापुर में की गई थी। इसके लिए 200 मेगावाट की दो परमाणु भट्टियां एक अमेरिकी फर्म से खरीदी गई थी। इसके लिए ईंधन की आपूर्ति अमेरिका करने के लिए वचनबध्द था। उसने ईंधन भेजना भी शरू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप इसे रिएक्टर ने 1 अप्रैल 1969 से काम करना शुरू कर दिया था। किंतु दो साल के अंदर अमेरिका ने संवंर्धित यूरेनियम की सप्लाई की मात्रा में कमी कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को उस बिजली घर को चालू रखने के लिए उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता बहुत घटानी पड़ गई।
इंदिरा सरकार में विदेशमंत्री के रूप में श्री नरसिम्हा राव इस विषय पर बात करने के लिए अमेरिका गए, किंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इस विषय पर उन्होंने बड़े ही कूटनीतिक भाषा में लोकसभा को बताया कि तारापुर बिजली घर को संर्विधत यूरेनियम देने के बारे में अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ, था उसकी अकाल मृत्यु हो गई, किंतु तरीके से उसको दफन किया जाना बाकी है।
इसके बाद इंदिरा सरकार सावधान हो गई और अपने आतंरिक साधनों से परमाणु उर्जा की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वैकल्पिक ईंधन की खोज शरू हो गई। तमिलनाडु के कल्पकम्म में 500 मेगावाट की क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिडर रिएक्टर तैयार किया गया, जिसमें प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद चौथा परमाणु उर्जा संयत्र उत्तर प्रदेश के नरौला में और पांचवा गुजरात के कतरापुर में स्थापित किया गया। साथ ही यूरेनियम का खनन और निस्कस्कण्र के अलावा भारत ने प्रयुक्त परमाणु कचरे को दोबारा इस्तेमाल में लाने की तकनीक भी प्राप्त कर ली। परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन का पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने के बाद 11 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने राजस्थान के पोखरण की मरूभूमि में पहला परमाणु विस्फोट कर संसार को हैरान कर दिया। यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य परमाणु हथियार बनाने का कदापि नहीं था, तथापि अमेरिका ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, इसके कारण परमाणु उपकरण बनाने वाले अन्य देशों ने भी भारत को मदद देना बंद कर दिया। किंतु भारत ने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने वैज्ञानिकों की बदौलत परमाणु हथियार बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली।
1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक साथ पांच परमाणु विस्फोट कर दुनिया को बता दिया कि भारत संसार का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गया है। अटल सरकार ने परमाणु विस्फोटों की शृंखला में पंद्रह टन की क्षमता के हाइड्रोजन बम का भी विस्फोट किया था। फिर भी अमेरिका या संसार की दुसरी महाशक्तियों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की पंक्ति में शामिल नहीं किया है। यद्यपि भारत ने बार-बार संसार को आश्वस्त किया कि वो अपने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल निर्माण, विकास और शांति के लिए करेगा। भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी देश पर हमला करने के लिए आरंभ नहीं किया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां तक कहा कि भारत अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल केवल जवाबी हमले के तौर पर करेगा, किंतु भारत की इस सदाशयता की इस नीति पर अमेरिका या किसी अन्य महाशक्ति की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। उल्टे भारत पर आणविक अप्रसार संधि और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए तरह-तरह के दवाब डालने की कोशिश जारी रही।
सन् 1977 के बाद भारत में कई बार अल्पजीवी सरकार बनी। परंतु किसी ने देश की विदेश नीति अथवा आणविक नीति में किसी प्रकार का परिर्वतन करना स्वीकार नहीं किया। महाशक्तियों के कड़े प्रतिबंध के बावजूद भारत अपनी नीति पर डटा रहा। इसी बीच अमेरिका पर अलकायदा के हमले के फलस्वरूप अमेरिका को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा और भारत को आतंकवाद विरोधी विश्व की लड़ाई में अपना भागीदार बनाने के सिवा उसे कोई और विकल्प दिखाई नहीं पड़ा। नतीजा उसे अपनी आर्थिक, राजनीतिक और विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा और भारत के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग का हाथ बढ़ाना पड़ा। भारत-अमेरिका परमाणु संधि इसी की ताजी कड़ी है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस पर आमादा हैं। किंतु अफगानिस्तान और इराक में मुंह की खाने के बाद उनका अमेरिका की राजनीति पर प्रभुत्व समाप्त प्राय हो गया है। अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। उसमें निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार सफल होता दिख रहा है। उसके बाद इस संधि का क्या रूप होगा, यह कहना मुश्किल है। किंतु हर सुबह रात की कहानी बता देता है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जिनका संसद में बहुतम है, भारत अमेरिका आणविक संधि से असहमत हैं। इसलिए आज बुश के दवाब में आकर वे इस संधि पर अपनी मुहर लगा भी दें। तो भी यह पूरी तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति पद हासिल करने के बाद भी वे समझौते पर ईमानदारी से अमल करेंगे।
अगर अमेरिका पीछे हटने लगेगा तो आणविक उपकरणों की सप्लाई करने वाले 44 अन्य देशों के भी पैर लड़खड़ाने लगेंगे। ऐसी अवस्था में भारत को सतत् जागरूक रहना होगा और अमेरिका के भरोसे अपनी कोई योजना बनाने से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा, और वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखना होगा।
अमेरिका ने अपनी आणविक नीति में भारत के लिए विशेष छूट दी है, ये सही है। किंतु इसके पीछे हो सकता है कि वह एशिया में अपनी शक्ति संचय करना चाहता है। ये भी संभव है कि वो चीन के मुकाबले भारत को खड़ा करने की कूटनीतिक चाल चल रहा हो। यह भी संभव है कि अफगानिस्तान मोर्चे पर पाकिस्तान से उसकी जो उम्मीदें थीं, वह पूरी नहीं हुईं, इसके कारण अब वो भारत को अपने आगोश में लेने की तैयारी कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि वह एशिया में नया शक्ति संतुलन पैदा करना चाहता हो। यह भी संभव है वो कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान को लड़ा कर दोनों को बर्बाद करना चाहता हो।
अमेरिका यदि भारत के प्रति मैत्री और सहयोग का संबंध बढ़ाना चाहता, तो सबसे पहले उसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए आगे बढ़कर भारत को उसका न्यायपूर्ण अधिकार दिलाने का प्रयास करता। क्योंकि ये सर्वविदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूनर्गठन की रिपोर्ट आई तो अमेरिका ने दो टूक कहा कि वो सुरक्षा परिषद के विस्तार की स्थिति में जर्मनी और जापान को इसकी सदस्यता दिलाने का प्रयास करेगा। यूएन के महासचिव के चुनाव के समय अमेरिका ने भारत के शशि थरूर की तुलना में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान-की-मून का समर्थन किया।
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत को अमेरिका से सदैव सावधान रहना चाहिए। भारत को निर्गुटता की अपनी विदेश नीति को धारदार बनाकर महाशक्तियों की होड़ से अपने को दूर रखकर ही देश की आधारशिला को मजबूत करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
(नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
Thursday, 3 January 2008
हिन्दुत्व और विकास के समन्वय की जीत
लेखक- विजय कुमार
यों तो भारत में साल भर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं; पर गुजरात के विधानसभा चुनावों ने देश-विदेश में जितनी सुर्खियां बटोरीं; इस पर जितनी और जैसी टिप्पणियां हुईं, उसके आगे अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव भी फीका लगता है। अब तो वहां के परिणाम भी आ चुके हैं। इनमें स्पष्टत: भाजपा की विजय और कांग्रेस की पराजय हुई है। दूसरे शब्दों में इसे यों भी कह सकते हैं कि वहां नरेन्द्र मोदी की जीत और सोनिया गांधी की पराजय हुई है। बाकी दलों और नेताओं की चर्चा करना उचित नहीं है, क्योंकि गर्बी गुजरात की जनता ने सबको शीशा दिखा दिया है। 117 स्थान जीतकर नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो सत्ता के स्वप्न देख रही कांग्रेस 59 स्थानों के साथ अपनी चोटों को ही सहलाने में लगी है।
वैसे तो इन्हीं दिनों हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए; पर चर्चा सब ओर गुजरात की ही थी। इसे मोदी की कुशल रणनीति ही कहना होगा कि उन्होंने चुनाव को अपने और सोनिया गांधी के बीच का जनमत संग्रह बना दिया। उनकी टीम ने संचार की आधुनिक तकनीक का सदुपयोग कर 'जीतेगा गुजरात' का नारा गढ़ा, जो जन-जन के मन में घर कर गया। इसके विपरीत सोनिया और राहुल दूसरों के लिखे भाषण ही पढ़ते रहे। इस कारण ही 'मौत के सौदागर' जैसी असंसदीय और अशालीन टिप्पणी चर्चा में आयी।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूरे देश और विश्व में फैल रहे मुस्लिम आतंकवाद की आलोचना करने की बजाय गुजरात में हिन्दू आतंकवाद पनपने की बात की। इसी प्रकार मनमोहन सिंह की दंगों की पुन: जांच की टिप्पणी ने आग में घी का काम किया। लोग समझ गये कि कांग्रेस वाले यहां फिर आग लगाना चाहते हैं। अब कांग्रेसी मान रहे हैं कि इन टिप्पणियों के कारण उन्हें भारी हानि हुई है। कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर आये नौ विधायकों को टिकट दिया; इससे भी जनता में गलत संदेश गया और उसने उनमें से आठ को हराकर हिसाब बराबर कर लिया।
जर्मन समाजशास्त्री मैक्सवेबर के अनुसार 'यदि चमत्कारी नेतृत्व हो, तो नेता और जनता के बीच सीधा संवाद होता है और बिचौलिये अप्रासंगिक हो जाते हैं।' नरेन्द्र मोदी ने इसे सत्य सिध्द कर दिखाया है। यहां तक कि राजनाथ सिंह और लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी जब नरेन्द्र मोदी के साथ मंच पर उपस्थित होते थे, तो जनता उनके बदले मोदी को ही सुनना पसंद करती थी। उनकी भाषण शैली, गुजरात के गौरव की चर्चा और गत पांच वर्ष की उपलब्धियों ने मिलकर वह समां बांधा कि जनता ने थोक में कमल के सामने वाले बटन को ही दबाना उचित समझा।
चुनाव के दिनों में अपने आश्वासन और उपलब्धियों की चर्चा तो सब करते हैं; पर मोदी की उपलब्धियां प्रत्यक्ष दिखाई देती थीं। गुजरात में सड़कों का जाल, शहर ही नहीं तो गांवो तक में बिजली की हर समय उपलब्धता, दंगा रहित प्रदेश और भूकम्पग्रस्त क्षेत्र का चहुंमुखी विकास, विदेशी निवेश की वर्षा, आतंकवादियों पर नियन्त्रण आदि के लिए बहुत कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गुजरात मूलत: व्यापारी प्रवृत्ति के लोगों का राज्य है। ऐसे लोग शांत वातावरण पसंद करते हैं। नरेन्द्र मोदी ने यह वातावरण प्रदेश को दिया, इसीलिए जनता ने उन्हें और भाजपा को विजयी बनाया।
मोदी और भाजपा ने यह भी समझा कि अनेक विधायकों के प्रति उनके क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। इसलिए उन्होंने लगभग 100 नये चेहरों को मैदान में उतारा और इसका परिणाम अच्छा ही मिला। दूसरी और कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नेता ही नहीं था। मोदी के विरुध्द लड़ाने के लिए भी केन्द्र सरकार के एक मंत्री दिनशा पटेल को बलि का बकरा बनाया गया।
इस चुनाव की एक विशेषता यह भी थी कि इस बार नरेन्द्र मोदी को बाहर के साथ-साथ अंदर से भी चुनौती मिल रही थी। भाजपा के केशूभाई पटेल, सुरेश मेहता, काशीराम राणा जैसे बड़े नेता ही उनका विरोध कर रहे थे। इसे मीडिया और कांग्रेस ने खूब उछाला, उन्होंने तो यहां तक झूठा प्रचार किया कि रा0स्व0संघ, विहिप और भारतीय किसान संघ जैसे बड़े संगठन भी मोदी के विरोध में हैं; पर मोदी चुपचाप चुनाव प्रचार में लगे रहे। फलत: वे इस अग्निपरीक्षा में सफल हुए और विरोधियों के मुख पर कालिख ही लगी। अपवादस्वरूप मध्य गुजरात को यदि छोड़ दें, तो शेष सारे राज्य में उन्हें अच्छी सफलता मिली। लोगों ने जाति-बिरादारी से ऊपर उठकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया।
जहां तक इस चुनाव के राष्ट्रीय परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभाव की बात है, तो इससे जहां भाजपा और नरेन्द्र मोदी की छवि उज्जवल हुई है, वहां कांग्रेस और सोनिया गांधी की छवि को दाग लगा है। कांग्रेस ने अपने तीनों सर्वोच्च नेताओं (सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह) को मैदान में उतारा; पर उनके सब हथकंडे विफल हुए। इससे संप्रग गठबंधन को भी झटका लगा है। कुछ दल तो अभी से कांग्रेस को आंखें दिखाने लगे हैं।
इसका आगामी लोकसभा चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। उस समय प्रधानमंत्री पद के दो प्रबल दावेदार होंगे। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और भाजपा की ओर से लालकृष्ण आडवाणी। वैसे इस पद के सपने मायावती भी देख रही हैं। कुछ लोग नरेन्द्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तुत करने की बात उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी युवा हैं, उन्होंने राजनीति और प्रशासन दोनों स्थानों पर अपनी उपयोगिता सिध्द की है। अत: उन्हें गुजरात तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। इन तर्कों में काफी वजन है; पर इसका निर्णय को भाजपा को ही करना है।
नरेन्द्र मोदी को अब अत्यधिक सावधान होने की आवश्यकता है। उनके शत्रु अब और अधिक तैयारी से वार करने का प्रयास करेंगे। विदेशियों के हाथों बिके हुए समाचार पत्र और दूरदर्शन चैनल उनकी छवि को नष्ट करने तथा भाजपा और उनके बीच दरार डालने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हिन्दुत्व और भाजपा से अलग 'मोदीत्व' शब्द गढ़ा गया है। वे बार-बार कह रहे हैं कि यह भाजपा की नहीं मोदी की जीत है। यद्यपि इसके दूसरे पक्ष के रूप में यदि यह कहा जाए कि गुजरात की हार कांग्रेस की नहीं सोनिया गांधी की हार है, तो वे मुंह पर ताला लगा लेते हैं।
मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भले ही व्यंग्य बाणों और गर्वोक्तियों का प्रयोग किया हो; पर अब उन्हें शांत रहकर प्रदेश के विकास में ही लगना होगा। यदि वे अन्य राजनेताओं की भांति चमचों से घिर गये, यदि उनके मन में थोड़ा भी अहंकार उत्पन्न हो गया, तो फिर उनका पतन होते देर नहीं लगेगी। यद्यपि उन्होंने विधायक दल का नेता चुने जाते समय भावुक होकर भाजपा संगठन को सर्वोच्च बताया, उनका यह व्यवहार आवश्स्त करता है कि वे सत्ता और संगठन में पहले से भी अच्छा समन्वय बनाकर चलेंगे।
जहां तक यह प्रश्न है कि गुजरात चुनाव में किसकी जीत हुई, तो यह हिन्दुत्व, विकास, संगठन और नरेन्द्र मोदी की समन्वित जीत है। हिन्दुत्व और विकास परस्पर पूरक हैं। पश्चिमी लोकतंत्र अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की बात करता है। 51 प्रतिशत लोगों के हित के लिए 49 प्रतिशत के हितों की बलि चढ़ा देना वहां अनुचित नहीं माना जाता; पर हिन्दुत्व 'सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया' का पक्षधर है। वह केवल मानव ही नहीं, तो पशु, पक्षी, जलचर, नभचर अर्थात सब प्राणियों के हित की कामना करता है। इतना ही नहीं, वह इससे आगे बढ़कर संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड का भला चाहता है। इसलिए गुजरात की जीत हिन्दुत्व के पक्षधरों की जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं। (नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
यों तो भारत में साल भर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं; पर गुजरात के विधानसभा चुनावों ने देश-विदेश में जितनी सुर्खियां बटोरीं; इस पर जितनी और जैसी टिप्पणियां हुईं, उसके आगे अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव भी फीका लगता है। अब तो वहां के परिणाम भी आ चुके हैं। इनमें स्पष्टत: भाजपा की विजय और कांग्रेस की पराजय हुई है। दूसरे शब्दों में इसे यों भी कह सकते हैं कि वहां नरेन्द्र मोदी की जीत और सोनिया गांधी की पराजय हुई है। बाकी दलों और नेताओं की चर्चा करना उचित नहीं है, क्योंकि गर्बी गुजरात की जनता ने सबको शीशा दिखा दिया है। 117 स्थान जीतकर नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो सत्ता के स्वप्न देख रही कांग्रेस 59 स्थानों के साथ अपनी चोटों को ही सहलाने में लगी है।
वैसे तो इन्हीं दिनों हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए; पर चर्चा सब ओर गुजरात की ही थी। इसे मोदी की कुशल रणनीति ही कहना होगा कि उन्होंने चुनाव को अपने और सोनिया गांधी के बीच का जनमत संग्रह बना दिया। उनकी टीम ने संचार की आधुनिक तकनीक का सदुपयोग कर 'जीतेगा गुजरात' का नारा गढ़ा, जो जन-जन के मन में घर कर गया। इसके विपरीत सोनिया और राहुल दूसरों के लिखे भाषण ही पढ़ते रहे। इस कारण ही 'मौत के सौदागर' जैसी असंसदीय और अशालीन टिप्पणी चर्चा में आयी।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूरे देश और विश्व में फैल रहे मुस्लिम आतंकवाद की आलोचना करने की बजाय गुजरात में हिन्दू आतंकवाद पनपने की बात की। इसी प्रकार मनमोहन सिंह की दंगों की पुन: जांच की टिप्पणी ने आग में घी का काम किया। लोग समझ गये कि कांग्रेस वाले यहां फिर आग लगाना चाहते हैं। अब कांग्रेसी मान रहे हैं कि इन टिप्पणियों के कारण उन्हें भारी हानि हुई है। कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर आये नौ विधायकों को टिकट दिया; इससे भी जनता में गलत संदेश गया और उसने उनमें से आठ को हराकर हिसाब बराबर कर लिया।
जर्मन समाजशास्त्री मैक्सवेबर के अनुसार 'यदि चमत्कारी नेतृत्व हो, तो नेता और जनता के बीच सीधा संवाद होता है और बिचौलिये अप्रासंगिक हो जाते हैं।' नरेन्द्र मोदी ने इसे सत्य सिध्द कर दिखाया है। यहां तक कि राजनाथ सिंह और लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी जब नरेन्द्र मोदी के साथ मंच पर उपस्थित होते थे, तो जनता उनके बदले मोदी को ही सुनना पसंद करती थी। उनकी भाषण शैली, गुजरात के गौरव की चर्चा और गत पांच वर्ष की उपलब्धियों ने मिलकर वह समां बांधा कि जनता ने थोक में कमल के सामने वाले बटन को ही दबाना उचित समझा।
चुनाव के दिनों में अपने आश्वासन और उपलब्धियों की चर्चा तो सब करते हैं; पर मोदी की उपलब्धियां प्रत्यक्ष दिखाई देती थीं। गुजरात में सड़कों का जाल, शहर ही नहीं तो गांवो तक में बिजली की हर समय उपलब्धता, दंगा रहित प्रदेश और भूकम्पग्रस्त क्षेत्र का चहुंमुखी विकास, विदेशी निवेश की वर्षा, आतंकवादियों पर नियन्त्रण आदि के लिए बहुत कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गुजरात मूलत: व्यापारी प्रवृत्ति के लोगों का राज्य है। ऐसे लोग शांत वातावरण पसंद करते हैं। नरेन्द्र मोदी ने यह वातावरण प्रदेश को दिया, इसीलिए जनता ने उन्हें और भाजपा को विजयी बनाया।
मोदी और भाजपा ने यह भी समझा कि अनेक विधायकों के प्रति उनके क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। इसलिए उन्होंने लगभग 100 नये चेहरों को मैदान में उतारा और इसका परिणाम अच्छा ही मिला। दूसरी और कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नेता ही नहीं था। मोदी के विरुध्द लड़ाने के लिए भी केन्द्र सरकार के एक मंत्री दिनशा पटेल को बलि का बकरा बनाया गया।
इस चुनाव की एक विशेषता यह भी थी कि इस बार नरेन्द्र मोदी को बाहर के साथ-साथ अंदर से भी चुनौती मिल रही थी। भाजपा के केशूभाई पटेल, सुरेश मेहता, काशीराम राणा जैसे बड़े नेता ही उनका विरोध कर रहे थे। इसे मीडिया और कांग्रेस ने खूब उछाला, उन्होंने तो यहां तक झूठा प्रचार किया कि रा0स्व0संघ, विहिप और भारतीय किसान संघ जैसे बड़े संगठन भी मोदी के विरोध में हैं; पर मोदी चुपचाप चुनाव प्रचार में लगे रहे। फलत: वे इस अग्निपरीक्षा में सफल हुए और विरोधियों के मुख पर कालिख ही लगी। अपवादस्वरूप मध्य गुजरात को यदि छोड़ दें, तो शेष सारे राज्य में उन्हें अच्छी सफलता मिली। लोगों ने जाति-बिरादारी से ऊपर उठकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया।
जहां तक इस चुनाव के राष्ट्रीय परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभाव की बात है, तो इससे जहां भाजपा और नरेन्द्र मोदी की छवि उज्जवल हुई है, वहां कांग्रेस और सोनिया गांधी की छवि को दाग लगा है। कांग्रेस ने अपने तीनों सर्वोच्च नेताओं (सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह) को मैदान में उतारा; पर उनके सब हथकंडे विफल हुए। इससे संप्रग गठबंधन को भी झटका लगा है। कुछ दल तो अभी से कांग्रेस को आंखें दिखाने लगे हैं।
इसका आगामी लोकसभा चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। उस समय प्रधानमंत्री पद के दो प्रबल दावेदार होंगे। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और भाजपा की ओर से लालकृष्ण आडवाणी। वैसे इस पद के सपने मायावती भी देख रही हैं। कुछ लोग नरेन्द्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तुत करने की बात उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी युवा हैं, उन्होंने राजनीति और प्रशासन दोनों स्थानों पर अपनी उपयोगिता सिध्द की है। अत: उन्हें गुजरात तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। इन तर्कों में काफी वजन है; पर इसका निर्णय को भाजपा को ही करना है।
नरेन्द्र मोदी को अब अत्यधिक सावधान होने की आवश्यकता है। उनके शत्रु अब और अधिक तैयारी से वार करने का प्रयास करेंगे। विदेशियों के हाथों बिके हुए समाचार पत्र और दूरदर्शन चैनल उनकी छवि को नष्ट करने तथा भाजपा और उनके बीच दरार डालने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हिन्दुत्व और भाजपा से अलग 'मोदीत्व' शब्द गढ़ा गया है। वे बार-बार कह रहे हैं कि यह भाजपा की नहीं मोदी की जीत है। यद्यपि इसके दूसरे पक्ष के रूप में यदि यह कहा जाए कि गुजरात की हार कांग्रेस की नहीं सोनिया गांधी की हार है, तो वे मुंह पर ताला लगा लेते हैं।
मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भले ही व्यंग्य बाणों और गर्वोक्तियों का प्रयोग किया हो; पर अब उन्हें शांत रहकर प्रदेश के विकास में ही लगना होगा। यदि वे अन्य राजनेताओं की भांति चमचों से घिर गये, यदि उनके मन में थोड़ा भी अहंकार उत्पन्न हो गया, तो फिर उनका पतन होते देर नहीं लगेगी। यद्यपि उन्होंने विधायक दल का नेता चुने जाते समय भावुक होकर भाजपा संगठन को सर्वोच्च बताया, उनका यह व्यवहार आवश्स्त करता है कि वे सत्ता और संगठन में पहले से भी अच्छा समन्वय बनाकर चलेंगे।
जहां तक यह प्रश्न है कि गुजरात चुनाव में किसकी जीत हुई, तो यह हिन्दुत्व, विकास, संगठन और नरेन्द्र मोदी की समन्वित जीत है। हिन्दुत्व और विकास परस्पर पूरक हैं। पश्चिमी लोकतंत्र अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की बात करता है। 51 प्रतिशत लोगों के हित के लिए 49 प्रतिशत के हितों की बलि चढ़ा देना वहां अनुचित नहीं माना जाता; पर हिन्दुत्व 'सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया' का पक्षधर है। वह केवल मानव ही नहीं, तो पशु, पक्षी, जलचर, नभचर अर्थात सब प्राणियों के हित की कामना करता है। इतना ही नहीं, वह इससे आगे बढ़कर संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड का भला चाहता है। इसलिए गुजरात की जीत हिन्दुत्व के पक्षधरों की जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं। (नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
Wednesday, 2 January 2008
उड़ीसा से आ रहे संकेतों को सुनो
लेखक : कुलदीप चन्द अग्निहोत्री
उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने 1956 में मजहब परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया था। उड़ीसा का अनेक क्षेत्र जनजाति बहुल हैं और चर्च जनजातियों को ईसा की शरण में ले जाने के लिए अंग्रेजों के वक्त से ही प्रयास कर रहा है। ब्रिटिश काल में ईसा की शरण में लाने का अर्थ ब्रिटिश सत्ताधारियों की शरण में ही लाना था। इसलिए यह एक प्रकार से अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को निष्क्रिय करने का अप्रत्यक्ष प्रयास भी था। चर्च के इस आक्रमण ने जनजातिय क्षेत्र के लोगों को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, विरासत और पूर्वजों के और नजदीक ही नहीं ला दिया बल्कि उससे भावात्मक लगाव को भी बढ़ाया। मनोवैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या यूं की जा सकती है कि जब किसी संस्कृति का अस्तित्व खतरे में पड़ता है तो उससे जुड़े हुए लोग खतरे को सूँघकर इक्ट्ठे ही नहीं हो जाते बल्कि उनके अन्य छोटे-मोटे मतभेद इस आसान खतरे के कारण समाप्त हो जाते हैं। उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में भी चर्च को लेकर ऐसा ही हो रहा है।
चर्च ने जनजातिय क्षेत्र के लोगों की इस एकता और प्रतिरोध से लड़ने के लिए जो रणनीति बनाई वह केवल उड़ीसा के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए भी खतरनाक कही जा सकती है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने विदेशी स्रोतों को सक्रिय करते हुए ज्यादा धन की माँग की और आशा के अनुरूप चर्च को विदेशों से अरबों रूपये की सहायता आनी शुरू हो गई। यदि भारत सरकार इस विषय पर कोई श्वेत पत्र प्रकाशित करें तो यह भयावह स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। द्वितीय चर्च ने दिल्ली में सरकार के भीतर और बाहर उस वर्ग को पकड़ा जिस वर्ग के लिए चर्च की अवैध गतिविधियों के विरोध का अर्थ ही हिन्दू सांप्रदायिकता है। उनके लिए आतंकवाद, चर्च और इस्लाम से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि का प्रयोग यदि कोई भारतीय या भारतीय संगठन करता है तो वह हिन्दू सांप्रदायिकता ही है। कांग्रेस और सीपीएम में इस अवधारणा को लेकर आश्चर्यजनक रूप से समानता देखी जा सकती है। गुजरात में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में लोकनिर्णय पर टिप्पणी करते हुए सीपीएम ने स्पष्ट ही कहाकि इस देश की मिट्टी में अभी भी भारतीय संप्रदाय की जड़ें गहरी जमी हुई है। उसे उखाड़ने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी लगभग इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना था कि अफजल गुरू के लिए फांसी की मांग करना हिन्दू आतंकवाद है। जाहिर है चर्च को सीपीएम की यह रणनीति बहुत ही ज्यादा अनुकूल पड़ती है। इसलिए तीनों आश्चर्यजनकर रूप से एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं। उड़ीसा के मामले में ऐसा ही हो रहा है। अब जब उड़ीसा के लोग खासकर जनजाति क्षेत्रों के लोग चर्च की अभारतीयकरण की नीति के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं तो कांग्रेस और सीपीएम स्पष्ट ही अपने नकाब उतारकर चर्च के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है। इन दोनों के लिए उड़ीसा के जनजाति क्षेत्र के लोग हिन्दू आतंकवादी है और इस हिन्दू आतंकवाद से चर्च की रक्षा करना जरूरी हो गया है। चर्च इनके लिए पवित्रता का प्रतीक है। क्योंकि चर्च इनको ठोस रूप से वोटें मुहैय्या करवा सकता है।
उड़ीसा के कंधमाल जिला में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती पर ईसाई एजेण्टों द्वारा किए गए आक्रमणों को इसी परिदृश्य में देखना होगा। लक्ष्मणानंद सरस्वती उड़ीसा की अस्मिता के प्रतीक है। वे ओडिया भाषा संस्कृति और परंपरा के संरक्षण की बात कहते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए अपना सारा जीवन होम दिया है। न उन्हें विधायक बनना है, न सांसद बनना है, न उन्हें रहने के लिए महलों की जरूरत है, न खाने के लिए छत्तीस प्रकार के व्यंजनों की । वे महात्मा गांधी की तरह उड़ीसा के ग्राम-ग्राम में झोंपड़ी में और जनजाति के लोगों के घरों में पिछले 45 वर्षों से घूम रहे हैं। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती एक प्रकार से उड़ीसा का सांस्कृतिक प्रवाह है। वे मधुर ओडिया भाषा में कीर्तन करते हैं। उत्कल प्रदेश की मिट्टी के गीत गाते हैं । उनमें उत्कल प्रदेश की रंग-गंध बसी है। चर्च जानता है कि यह उत्कल अस्मिता और उत्कल गंध उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए चर्च ने शायद भारत में निर्णायक लड़ाई करने का निर्णय कर लिया है। इसीलिए उसने स्वामी जी पर क्रिसमस के दिन ही प्रहार किया है। लेकिन यह लड़ाई लड़ने से पूर्व चर्च ने अपनी मोर्चा बंदी भी सख्त प्रकार से की हुई है। यह लड़ाई शुरू करने से पहले उसने सत्ता के केन्द्र पर सोनिया गांधी को स्थापित कर दिया है। सीपीएम को साथ ले लिया है और मीडिया के एक वर्ग को इस कार्य के लिए योजना पूर्वक प्रशिक्षित कर दिया। इस पूरी मोर्चाबंदी के बाद चर्च ने उड़ीसा से अपना नया अभियान शुरू किया है। मीडिया के लिए यह आक्रमण उत्कल अस्मिता के प्रतीक स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती पर न होकर हिन्दू गुण्डों द्वारा चर्च पर किजा जा रहा आक्रमण है। कांग्रेस, सीपीएम और मीडिया के लिए उड़िसा का जनजातिय समाज असामाजिक तत्व है जो चर्चों को जला रहा है। ब्रिटिश शासकों की दृष्टि में जनजातिय समाज असभ्य और बर्बर था। कांग्रेस और सीपीएम की दृष्टि में यह समाज हिन्दू गुंडागर्दी का प्रतीक है। यदि दिग्विजय सिंह की माने तो भारत में हिन्दू आतंकवाद प्रारंभ हो चुका है। आश्चर्य नहीं होगा यदि कल भारत सरकार स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को हिन्दू आतंकवादी घोषित कर दे । जहां तक सीपीएम का प्रश्न है उसके लिए हर भगवाधारी सांप्रदायिक है और चर्च व अफजल गुरू धर्मनिरपेक्षता के उत्कृष्ट प्रतीक है। यह सब उस समय हो रहा है जब गुजरात में लोगों ने कांग्रेस और सीपीएम की इस संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टि का मुंहतोड़ उत्तर दिया है।
उड़ीसा से स्पष्ट संकेत आ रहे हैं। उड़ीसा के लोग अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इधर कांग्रेस और सीपीएम भी मोर्चा संभाल रही है। जैसे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा है कि गुजरात के लोक निर्णय से यह आशा फिर बंधी है कि भारत और भारतीयता की लड़ाई अभी पूरी तरह हारी नहीं है। वह फिर जीती जा सकती है इसकी संभावना बढ़ गई है। चर्च ने इस लड़ाई को अब उड़ीसा में लड़ने का निर्णय किया है। भारत के सब लोगों को उड़ीसा के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा।
(नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने 1956 में मजहब परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया था। उड़ीसा का अनेक क्षेत्र जनजाति बहुल हैं और चर्च जनजातियों को ईसा की शरण में ले जाने के लिए अंग्रेजों के वक्त से ही प्रयास कर रहा है। ब्रिटिश काल में ईसा की शरण में लाने का अर्थ ब्रिटिश सत्ताधारियों की शरण में ही लाना था। इसलिए यह एक प्रकार से अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को निष्क्रिय करने का अप्रत्यक्ष प्रयास भी था। चर्च के इस आक्रमण ने जनजातिय क्षेत्र के लोगों को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, विरासत और पूर्वजों के और नजदीक ही नहीं ला दिया बल्कि उससे भावात्मक लगाव को भी बढ़ाया। मनोवैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या यूं की जा सकती है कि जब किसी संस्कृति का अस्तित्व खतरे में पड़ता है तो उससे जुड़े हुए लोग खतरे को सूँघकर इक्ट्ठे ही नहीं हो जाते बल्कि उनके अन्य छोटे-मोटे मतभेद इस आसान खतरे के कारण समाप्त हो जाते हैं। उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में भी चर्च को लेकर ऐसा ही हो रहा है।
चर्च ने जनजातिय क्षेत्र के लोगों की इस एकता और प्रतिरोध से लड़ने के लिए जो रणनीति बनाई वह केवल उड़ीसा के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए भी खतरनाक कही जा सकती है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने विदेशी स्रोतों को सक्रिय करते हुए ज्यादा धन की माँग की और आशा के अनुरूप चर्च को विदेशों से अरबों रूपये की सहायता आनी शुरू हो गई। यदि भारत सरकार इस विषय पर कोई श्वेत पत्र प्रकाशित करें तो यह भयावह स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। द्वितीय चर्च ने दिल्ली में सरकार के भीतर और बाहर उस वर्ग को पकड़ा जिस वर्ग के लिए चर्च की अवैध गतिविधियों के विरोध का अर्थ ही हिन्दू सांप्रदायिकता है। उनके लिए आतंकवाद, चर्च और इस्लाम से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि का प्रयोग यदि कोई भारतीय या भारतीय संगठन करता है तो वह हिन्दू सांप्रदायिकता ही है। कांग्रेस और सीपीएम में इस अवधारणा को लेकर आश्चर्यजनक रूप से समानता देखी जा सकती है। गुजरात में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में लोकनिर्णय पर टिप्पणी करते हुए सीपीएम ने स्पष्ट ही कहाकि इस देश की मिट्टी में अभी भी भारतीय संप्रदाय की जड़ें गहरी जमी हुई है। उसे उखाड़ने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी लगभग इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना था कि अफजल गुरू के लिए फांसी की मांग करना हिन्दू आतंकवाद है। जाहिर है चर्च को सीपीएम की यह रणनीति बहुत ही ज्यादा अनुकूल पड़ती है। इसलिए तीनों आश्चर्यजनकर रूप से एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं। उड़ीसा के मामले में ऐसा ही हो रहा है। अब जब उड़ीसा के लोग खासकर जनजाति क्षेत्रों के लोग चर्च की अभारतीयकरण की नीति के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं तो कांग्रेस और सीपीएम स्पष्ट ही अपने नकाब उतारकर चर्च के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है। इन दोनों के लिए उड़ीसा के जनजाति क्षेत्र के लोग हिन्दू आतंकवादी है और इस हिन्दू आतंकवाद से चर्च की रक्षा करना जरूरी हो गया है। चर्च इनके लिए पवित्रता का प्रतीक है। क्योंकि चर्च इनको ठोस रूप से वोटें मुहैय्या करवा सकता है।
उड़ीसा के कंधमाल जिला में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती पर ईसाई एजेण्टों द्वारा किए गए आक्रमणों को इसी परिदृश्य में देखना होगा। लक्ष्मणानंद सरस्वती उड़ीसा की अस्मिता के प्रतीक है। वे ओडिया भाषा संस्कृति और परंपरा के संरक्षण की बात कहते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए अपना सारा जीवन होम दिया है। न उन्हें विधायक बनना है, न सांसद बनना है, न उन्हें रहने के लिए महलों की जरूरत है, न खाने के लिए छत्तीस प्रकार के व्यंजनों की । वे महात्मा गांधी की तरह उड़ीसा के ग्राम-ग्राम में झोंपड़ी में और जनजाति के लोगों के घरों में पिछले 45 वर्षों से घूम रहे हैं। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती एक प्रकार से उड़ीसा का सांस्कृतिक प्रवाह है। वे मधुर ओडिया भाषा में कीर्तन करते हैं। उत्कल प्रदेश की मिट्टी के गीत गाते हैं । उनमें उत्कल प्रदेश की रंग-गंध बसी है। चर्च जानता है कि यह उत्कल अस्मिता और उत्कल गंध उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए चर्च ने शायद भारत में निर्णायक लड़ाई करने का निर्णय कर लिया है। इसीलिए उसने स्वामी जी पर क्रिसमस के दिन ही प्रहार किया है। लेकिन यह लड़ाई लड़ने से पूर्व चर्च ने अपनी मोर्चा बंदी भी सख्त प्रकार से की हुई है। यह लड़ाई शुरू करने से पहले उसने सत्ता के केन्द्र पर सोनिया गांधी को स्थापित कर दिया है। सीपीएम को साथ ले लिया है और मीडिया के एक वर्ग को इस कार्य के लिए योजना पूर्वक प्रशिक्षित कर दिया। इस पूरी मोर्चाबंदी के बाद चर्च ने उड़ीसा से अपना नया अभियान शुरू किया है। मीडिया के लिए यह आक्रमण उत्कल अस्मिता के प्रतीक स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती पर न होकर हिन्दू गुण्डों द्वारा चर्च पर किजा जा रहा आक्रमण है। कांग्रेस, सीपीएम और मीडिया के लिए उड़िसा का जनजातिय समाज असामाजिक तत्व है जो चर्चों को जला रहा है। ब्रिटिश शासकों की दृष्टि में जनजातिय समाज असभ्य और बर्बर था। कांग्रेस और सीपीएम की दृष्टि में यह समाज हिन्दू गुंडागर्दी का प्रतीक है। यदि दिग्विजय सिंह की माने तो भारत में हिन्दू आतंकवाद प्रारंभ हो चुका है। आश्चर्य नहीं होगा यदि कल भारत सरकार स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को हिन्दू आतंकवादी घोषित कर दे । जहां तक सीपीएम का प्रश्न है उसके लिए हर भगवाधारी सांप्रदायिक है और चर्च व अफजल गुरू धर्मनिरपेक्षता के उत्कृष्ट प्रतीक है। यह सब उस समय हो रहा है जब गुजरात में लोगों ने कांग्रेस और सीपीएम की इस संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टि का मुंहतोड़ उत्तर दिया है।
उड़ीसा से स्पष्ट संकेत आ रहे हैं। उड़ीसा के लोग अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इधर कांग्रेस और सीपीएम भी मोर्चा संभाल रही है। जैसे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा है कि गुजरात के लोक निर्णय से यह आशा फिर बंधी है कि भारत और भारतीयता की लड़ाई अभी पूरी तरह हारी नहीं है। वह फिर जीती जा सकती है इसकी संभावना बढ़ गई है। चर्च ने इस लड़ाई को अब उड़ीसा में लड़ने का निर्णय किया है। भारत के सब लोगों को उड़ीसा के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा।
(नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)
Subscribe to:
Comments (Atom)