लेखक- विष्णुकान्त शास्त्री
मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं यह नहीं मानता कि 15 अगस्त, 1947 को भारत एक नया राष्ट्र बन गया। सच तो यह है कि ऐसा मानने वाले बहुत विरले हैं।
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वाधीनता के बाद 24 जनवरी 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा था ''हमें अपनी उस विरासत और अपने उन पूर्वजों पर गर्व है जिन्होंने भारत को बौध्दिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता प्रदान की। आप इस अतीत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी यह महसूस होता है कि आप भी इसके साझीदार और उत्तराधिकारी हैं? क्या आप भी उस पर गौरवान्वित होते हैं, जो आपका भी उतना ही है जितना मेरा अथवा आप उसे अपना ही समझते हैं?'' उनको स्पष्ट अपेक्षा थी कि उन सब विद्यार्थियों को भी प्राचीन भारत की उपलब्धियों के लिए गौरव का अनुभव करना चाहिए। इस निरूपण से यह साफ हो जाता है कि स्वाधीन भारत प्राचीन भारत का ही विकसित आधुनिक रूप है।
मैं समझता हूं कि अपने राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के पहले हमें अपने पारम्परिक स्वरूप को पहचानना चाहिए। हमें उस स्वरूप को हृदयंगम करना चाहिए जो परिस्थितियों के दबाव में रूपत: बाहर से तो बदलता रहता है किन्तु भीतर से अपरिवर्तित रहा है। हम परम्परा के आधारभूत चिंतन मनन और जीवन में उसके प्रतिफलन को समझने की चेष्टा करें।
राजधर्म और राजनीति
महाभारत में कहा गया है कि धारण करने की शक्ति के कारण धर्म, धर्म होता है। धर्म वही है जो प्रजा धारण करे। अत: निश्चित सिध्दांत यही है कि जो धारण शक्ति से संयुक्त है वही धर्म है। यहीं कुछ चर्चा संस्कृति की भी कर ली जाये। संस्कृति अर्थात् 'सम्यक कृति'। इससे यह ध्वनि निकलती है कि जो कृति को सम्यक रूप से सुधार दे वह संस्कृति है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृति शब्द कल्चर का अनुवाद है। यह ठीक नहीं है। हम जो कुछ करते हैं, जिस प्रकार का वैयक्तिक, पारिवारिक या सामाजिक जीवन जीते हैं, उसको निरन्तर सुधारते रहने की प्रक्रिया ही संस्कृति है।
अपनी संस्कृति की एक आधारभूत विशेषता की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि अपने अपने उपास्य की उत्कृष्टता सिध्द करने के हठाग्रह के कारण धार्मिक विद्वेष उत्पन्न होता है। भारतीय संस्कृति ने इस विकृति के निराकरण के लिए एक अद्भुत स्थापना की है। ऋग्वेद में कहा गया है कि 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' अर्थात परमसत्ता एक ही है जिसे विद्वान विविधा नामों से पुकारते हैं। अत: इनके लिए विवाद करना व्यर्थ है।
इस मान्यता के कारण भारत में बड़ी हद तक साम्प्रदायिक समरसता बनी रही। सम्राट हर्षवर्धन, शिव, सूर्य और बुध्द तीनों की उपासना करते थे। एक ही परिवार के भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न इष्ट देवों की पूजा करते हुए प्रेमपूर्वक साथ-साथ रहते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने इसे भारतीय संस्कृति का भेदक लक्षण घोषित करते हुए इसको 'भी वाद' की संज्ञा दी हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम सब श्रध्दापूर्वक चल रहे हैं तो भगवान तक मेरा रास्ता भी पहुंचेगा और तुम्हारा तथा उसका रास्ता भी पहुंचेगा। यह 'भी वाद' यदि सभी धर्मावलंबियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो धार्मिक संघर्ष का मूलोच्छेद हो जाए। परन्तु अभी इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि विनोबा भावे के अनुसार यहूदी, ईसाई और इस्लाम 'ही वाद' धर्म हैं। यह भी यहां जोड़ दूं कि बाबा विनोबा भावे के अनुसार मार्क्सवादी भी 'ही वादी' ही हैं। वे भी सबों पर अपना सिध्दांत थोपने के हठाग्रही हैं।
समग्र मानव जीवन के मंगल का विधान करने वाली हमारी सांस्कृतिक चेतना ने जिस भारतीय समाज और राष्ट्र का निर्माण किया उनमें राजनीति की भूमिका को महत्वपूर्ण तो माना गया है किन्तु उसे सर्वोपरि नहीं माना गया है। धर्मधिष्ठित राजनीति का ही हमारे देश में सम्मान था। भारतीय चेतना ने आदर्श शासक के रूप में श्रीराम को ही स्वीकार किया है, जिनकी प्रशस्ति में कहा गया है, 'रामो विग्रहवान धर्म:' राम तो मूर्तिमान धर्म ही है।
राजनीति कभी सत्यमयी, कभी मिथ्यामयी, कभी कठोर, कभी प्रियभाषिणी, कभी हिंसामयी, कभी दयालु, कभी लोभी, कभी उदार, कभी अत्यंत खर्चीली, कभी अत्याधिक अर्जनशील होती है। राजनीति वस्तुत: कल्याणकारी तभी होती है जब वह सच्चे राजधर्म पर आधारित होती है, जिसका एक प्रधान लक्षण यह है कि राजा पार्थिव व्रत का निर्वाह करे अर्थात् उसी प्रकार बिना किसी भेदभाव के सारी प्रजा का समानभाव से पालन करे जिस प्रकार पृथ्वी सब प्राणियों को समान भाव से धारण करती है। इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय धर्म व राज्य को मजहबी राज्य या थियोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें जाति, भाषा, उपासना पध्दति आदि के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं किया जाता था।
संस्कृतिपरक भारतीय राष्ट्रवाद
यह तथ्य भी उल्लेख्य है कि प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास में मनु, रघु, श्रीराम, युधिष्ठिर, अशोक, विक्रमादित्य आदि कुछ ही ऐसे चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पर शासन किया था। अन्यथा भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग स्वाधीन राज्य थे। हमारा इतिहास साक्षी है कि राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न राज्यों में विभक्त होते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टि से पूरा भारतवर्ष एक देश माना जाता था। देश के किसी भी कोने में बैठ कर पुण्य कार्य करने वाला व्यक्ति जल को शुध्द करने के लिए देश के विभिन्न भागों में बहने वाली सात पवित्र नदियों का आह्वान करता था, जो परंपरा आज तक चली आ रही है।
यह ठीक है कि राजनीति को कम महत्व देने का दंड भी हम लोगों को भोगना पड़ा है। जब विदेशी शक्तियां राज्यों पर आक्रमण करती थीं तो देश भर के सभी राज्य मिल कर उनका प्रतिरोध नहीं करते थे। फलत: एक-एक करके वे राज्य विपन्न होते रहे और हमें पराधीनता का अभिशाप भोगना पड़ा। अब हम इस ओर भी सावधान रह कर अपने को राजनीतिक दृष्टि से भी अजेय बनायें, यही अभीष्ट है। जो हो, अपने विचारक्रम को ऐतिहासिक दृष्टि से आगे बढ़ाने पर यह लक्षित किया जा सकता है कि जब तुर्क आये, पठान आये, मुगल आये और केन्द्रीय राज्य क्षमता छिन गयी, तब भी हमारी संस्कृति ने ही सारे देश को एक मानने की दृष्टि को अक्षुण्ण रखा।
यह दिवालोक की भांति स्पष्ट है कि धार्मिक कट्टरता को लांघ कर साधाना और साहित्य के क्षेत्र में पठान-मुगल काल में ही भारतीय संस्कृति की उदारता को मुसलमान भाई अपना रहे थे। दाराशिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाना भी इसी धारा की कड़ी है। यह देश का दुर्भाग्य ही है कि औरंगजेब की मजहबी कट्टरता ने इस धारा को अवरूध्द करना चाहा पर फिर भी मंदगति से ही सही वह धारा प्रवाहित होती रही। संत प्राणनाथजी ने समन्वय की दृष्टि से औरंगजेब को पत्र भी लिखा और अपने सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण के निराकार रूप की उपासना का प्रवर्तन किया। संगीत, चित्रकला एवं नृत्य के क्षेत्र में भी आदान प्रदान चलता रहा। यह उदार समन्वयी धारा निश्चय ही भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गौरवपूर्ण उपलब्धि है।
1857 में अंग्रेजों के विरूध्द छेड़े गये प्रथम स्वाधीनता संग्राम के पूर्व जनसंघर्ष की चेतना जगाने के लिए रोटी के साथ-साथ कमल को प्रतीक के रूप में चुनना, हमारी सांस्कृतिक चेतना के कारण ही संभव हो सका था। इस संग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर हिन्दू और मुसलमान अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए लड़े थे। दुर्भाग्य से इस स्वातंत्र्य समर के विफल होने के बाद जनता में व्यापक हताशा फैल गयी। राष्ट्र को इस हताशा से उबारने के लिए पुन: एक बार हमारी सांस्कृतिक चेतना ही सक्रिय हुई। राजा राम मोहन राय, श्री रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि दयानन्द सरस्वती, श्री अरविन्द, स्वामी रामतीर्थ आदि महापुरूषों ने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्षों को उभार कर और विकृतियों को नकार कर पुन: देश में नवजीवन का संचार किया। इस सांस्कृतिक जागरण का एक सुफल यह भी हुआ कि पाश्चात्य ज्ञान-विभान और जीवन मूल्यों के अंधानुकरण के अतिरेकों से मुक्त होकर भारतीय प्रबुध्द चित्र ने भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान आदि के स्वस्थ समन्वय पर बल दिया। इस सांस्कृतिक जागरण की फलश्रुति ही थे भारतीय स्वाधीनता के सहिंस और अहिंसा आन्दोलन। आरंभ में इन आन्दोलनों को सभी भारतीयों का समर्थन प्राप्त था। किन्तु कालान्तर में अंग्रेजों की कूटनीति के कारण कट्टरपंथी मुसलमान इनसे कटते गये। दुर्भाग्य की बात है कि ''सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा'' लिखने वाले अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का बीजारोपण किया और एक समय के हिन्दू मुस्लिम एकता के समर्थक, नरमपंथी नेता कायदे आजम जिन्ना अंग्रेजों की कूटनीति को सफल करते हुए पाकिस्तान के जनक बने। मजहब के आधार पर जिस पाकिस्तान की सृष्टि हुई थी वह 1971 में टूट गया। स्वाधीन बांग्लादेश इस बात का प्रमाण है कि मजहब के नाम पर बने पाकिस्तान की नींव कितनी खोखली थी। बचे-खुचे पाकिस्तान में भी पंजाबी, सिंधी, बलूची, पख्तून, मुहाजिर के भेद उग्र होते जा रहे हैं। मुहाजिरों के नेता अल्ताफ हुसैन ने तो साफ-साफ कह दिया है कि पाकिस्तान का निर्माण ऐतिहासिक भूल थी। इसलिए उसने ''सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा'' फिर से गाना शुरू कर दिया है।
इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि उपासना पध्दति एवं सामाजिक रीति-नीति की भिन्नताओं के बावजूद साझी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को हम लोग और दृढ़ करें।
एकात्म भारतीय संस्कृति
संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी संस्कृति ने दूसरे देशों की संस्कृतियों से आदान-प्रदान न किया हो। आधुनिक युग में यह प्रक्रिया और भी तेज हो गयी है। फिर भी दुनिया का कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है जो अपनी संस्कृति को सामासिक संस्कृति कहता हो। अत: हमें अकुंठ चित्त से अपने देश की संस्कृति को सीधे भारतीय संस्कृति ही कहना चाहिए।
(एकात्म मानववाद अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सेमिनार में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री द्वारा दिए गए भाषण से संकलित है।)
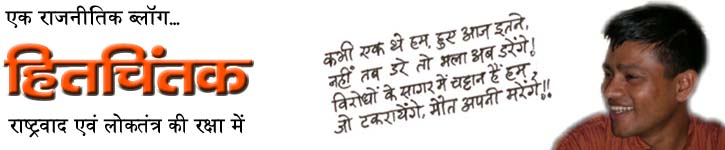
3 comments:
in lekhanshon ko sabhi rashtra ke swayambhu karnadharon ko preshit karen. rashtra, rashtravaad aur bhaartiyta ki inki avdharna ko sahi disha dena behad aavshyak hai. Poori na sahi, kuch hi sahi, ye lekh unhen maarg dikhhayega.
देश मै आज जिस तरह का माहोल है उससे सामान्य जन अपनी भूमिका को लेकर आशंकित है,युवा तो बुरी तरह से भ्रमित है !कई युवको को मैंने कहते सुना है "भाड़ मै जाय देश ,देश ने हमे दिया क्या है "देश भक्तो की श्रंखला वाले इस देश मै ये कपूत कहा से आ गये ? तो इनके जनक है- देश का स्वार्थी व अक्षम नेतृत्व !देशवासियों को दिशा देने वाले माध्यमो का आपसी प्रति स्पर्धा मै खुद ही दिशा भटक जाना है !देश के नेतृत्व करने वालो की कोई स्पष्ट नीति नहीं है ,और विलासिता का सुख भोगते -भोगते ,आपत्ति के समय भी वे, विलासिता के मद में चूर ऐसे ब्यान देते है जो जनमानस के आहत मन को कचोट जाते है फिर रही सही कसर मीडिया पूरी कर देता ,उस आहत और कचोट गये मन पर मिर्च,और नमक छिड़क कर (उस ब्यान को बार -बार दिखा कर ) !क्या लोकतंत्र के इस चोथे स्तम्भ के कर्तव्य की इतिश्री मात्र इसमें है की वो देश के सभी लूट -मार ,बलात्कार ,खून- खराबा,हत्या ,बम्ब धमाके ही दिन भर दिखाते रहे !क्या देश मै कही कोई सकारात्मक कार्य नहीं हो रहा जो ,देश के युवाओ के सामने "आदर्श ' बने, और उनकी भ्रमित सोच को परिवर्तित करे!
@भारतीय चेतना ने आदर्श शासक के रूप में श्रीराम को ही स्वीकार किया है, जिनकी प्रशस्ति में कहा गया है, 'रामो विग्रहवान धर्म:' राम तो मूर्तिमान धर्म ही है।
बहुत अच्छा लेख है.
Post a Comment