सच को राजनीति में लोग दो तरीकों से देखते हैं। एक तरीका वह है जिसमें लोग समझते हैं कि जोर से और बार-बार दुहराने से झूठ ही सच में परिवर्तित हो जाता है। कांग्रेस सहित अन्य वामपंथी दल ''गोयबल्स'' की इसी विचारधारा को सिर माथे लगाते हैं। जबकि दूसरा तरीका विशुध्द भारतीय है जो मानता है 'सत्यमेव जयते' यानि कुछ भी हो सत्य की ही विजय होती है। अंधोरे का कुहासा चाहे जितना लम्बा हो, उसे सच की एक किरण चीर कर रख देती है। यह रास्ता लम्बा परन्तु कारगर है। यह एक विशुध्द भारतीय अवधारणा है। भारतीय शब्द का प्रयोग मैं यहां जानबूझ कर कर रहा हूं।
आज भारतीय राजनीति की यह बड़ी भारी विडम्बना है कि जैसे ही आप इस देश की मिट्टी और मूल की बात करने लगते हैं तो लोगों की भौंहें कमान होने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी बात करके हम भारतीय समाज के एक वर्ग विशेष को दरकिनार कर रहे हैं। परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग न तो भारत को समझते हैं और न ही उसकी संस्कृति को। इस देश की भूमि पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी पंथ का हो इस देश के मूल और मिट्टी के प्रति आभारी हो इस आग्रह में दुराग्रह कहां है? संसार के सभी देश ऐसा आग्रह अपने देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों से करते रहे हैं परन्तु वहां कोई 'सेक्युलरवादी' हंगामा खड़ा नहीं करता। वहां राष्ट्र और संस्कृति की बात की जा रही है और उस पर कुठाराघात करने वालों से निपटने की तैयारियां चल रही हैं परन्तु भारत में सारा मामला यहां अटका है कि भारतीय संस्कृति 'एकमेव' हो या 'बहुल'।
पाश्चात्य विचारधारा में पोषित लोग अंग्रेजों के बहकावे में आकर यह मान बैठे कि भारत एक 'धर्मशाला' है, जहां हर कोई आकर अपना खूंटा ठोक सकता है। ऐसा कहने से अंग्रेजों को अपना राज्य 'वैध' कहने में सहायता मिलती थी। उन्होंने इसी दृष्टि से भारतीय संस्कृति को देखा। वैसे भी पश्चिम की दृष्टि इतनी बहिर्मुखी है कि वह चाह कर भी भारतीय संस्कृति के भीतर की एकात्मकता को नहीं पहचान सकती थी। पश्चिम की निगाह बाहर से भीतर की नहीं बल्कि भीतर से बाहर की यात्रा करती है।
अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को 'अनेक संस्कृति' मान लिया यह तो उनके स्वार्थों और अज्ञानता के चलते समझ में आता है। परन्तु वही अज्ञानता जब गोरी चमड़ी के बजाय 'भूरी चमड़ी' के लोग प्रदर्शिित करने लगते हैं तो आश्चर्य के साथ उन पर तरस भी आता है। भारतीय संस्कृति की तुलना हम 'हिन्द महासागर' से कर सकते हैं जिसमें अनेक नदियां गिरती हैं परन्तु उनमें विलीन हो जाने के बाद कौन बता सकता है कि यह गंगा का पानी है और यह कावेरी का। इस सच्चाई से मुंह मोड़ने का परिणाम यह है कि आज भी हम भारतीय मूल्यों और संस्कारों को भारतीय राजनीति में वह स्थान नहीं दिला पाये जो उसका होना चाहिए।
पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के दबाव के चलते संविधान की रचना होते समय भारतीय मूल्यों और अवधारणाओं की चर्चा से बचा गया। इसका एक कारण यह भी था कि मुस्लिम कहीं नाराज न हो जाये। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वे लोग भारतीय संस्कृति के आदर्शों की गहराई को नहीं समझ पाये। स्वामी विवेकानन्द ने जिस भारतीय संस्कृति की गर्जना शिकागो में की थी वह भारत में ही कांग्रेसी सुर में मिमियाने लगी। यह भारतीय संस्कृति की नहीं बल्कि कांग्रेसी दृष्टि की कमी थी और यह आज भी बरकरार है।
हमारी दृष्टि भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित है और इस पर हमें गर्व है। 'संस्कृति' और 'राष्ट्र' दोनों हमारे लिए आराध्य हैं। हम देश को विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं। यहां पर बहुत से लोग यह कहते हैं कि फिर हमें विकास के अलावा सभी मुद्दों को त्याग देना चाहिए। ऐसा करके वे सभी अपनी नादानी ही प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो यह है कि विश्व का कोई भी देश अपनी संस्कृति पर गर्व किए बिना विकसित हो नहीं सकता। अपनी विरासत पर गर्व किए बिना देश के लोगों में वह आत्मविश्वास नहीं पैदा होता जो जापान को 'जापान' बनाता है।
भारतीय सांस्कृतिक अवधारणा तो विश्व के सबसे ऊंचे मानदंडों पर आधारित है। फिर उसे अपनाने में संकोच क्यों? इसलिए अपने मूल्यों और संस्कारों को हमें प्रतिष्ठा दिलानी ही होगी। यह प्रतिष्ठा मात्र शब्दों से नहीं, हमारे कार्यकलापों से पैदा होगी। तब हम में ऐसा आत्मविश्वास पैदा होगा कि हमारा भारतीय विकसित भारत हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा विकास, बिना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नहीं आ सकता। यदि मान भी लें कि यह संभव भी हो जाये तो भारतीय संस्कृति के संस्कारों के बिना उस विकास की दिशा एक ''मिसगाइडेड मिसाइल'' की तरह होगी जो विकास को विनाश में बदल देगी।
जिस प्रकार शरीर बिना आत्मा के निरर्थक है उसी प्रकार संस्कृति से रहित देश में निष्प्राण हो जाता है। संस्कृति से हीन होने पर जीवन मूल्यों में गिरावट आती है और जब मूल्यों का ह्रास होता है तो मनुष्य पतन की ओर अग्रसर होता है। यहाँ हमें भलीभांति समझना होगा कि संस्कृति कोई संकुचित शब्द नहीं है। उसकी व्यापकता में ही उसका महत्व है। इसलिए कि हमने व्यापकता की हर पराकाष्ठा को छू लिया।
यह भारतीय संस्कृति ही है जो मनुष्य को परमात्मा की सर्वोत्तम कृति तो मानती ही है उसके साथ पशुओं के प्रति भी दया का भाव रखती है। यह भारत देश की संस्कृति ही है जहां पर राजकुमार सिध्दार्थ अपने भाई द्वारा घायल किए गये पक्षी को सौंपने से इंकार कर देते हैं। ''यदि हम दूसरों को जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है।'' पशु-पक्षियों के प्रति दया और उदारता के ऐसे उदाहरण भला किस देश की संस्कृति ने प्रस्तुत किये हैं ?
हमारे देश में ही सबसे पहले 'अतिथि देवो भव' कहकर अतिथि को ईश्वर का सम्मान दिया गया और नारी को देवी मानकर उसकी पूजा की गयी। राज्य और राष्ट्र को एक मानने और समझने वाले ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का आदर्श नहीं समझ सकते क्योंकि इस भाव को वही समझ सकता है जो राज्य की शक्ति के ऊपर उठकर 'राष्ट्र' के सद्भाव और विस्तार को समझ सके। 'राज्य' राजनीति के इर्द-गिर्द सिमट जाता है जबकि 'राष्ट्र' राजनीति की संकुचित अवधारणा को तोड़कर एक 'राष्ट्र नीति' या पध्दति को विकसित करता है जहां पर हर सत्ता परिवर्तन बेमानी हो जाता है।
भारत देश मूलत: संस्कृति प्रधान है। यह इस संस्कृति का ही जादू है कि यूनान, मिस्र और रोम नक्शे से मिट गये पर भारत का अस्तित्व या यूं कहें भारतीयता बनी रही। हर दौर में यहां पर संस्कृति बार-बार अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती रही। इसका कारण सिर्फ इतना है कि हम भारतीयों ने इस देश की मिट्टी, नदियों, पर्वतों, मैदानों, पठारों परम्पराओं, देवी, देवताओं से ऐसा तारतम्य स्थापित कर लिया है कि कोई बाहरी ताकत इसको प्रभावित करने की चाहे जितनी भी चेष्टा कर ले, हम अपनी जड़ों को विस्मृत नहीं करते।
इस देश में समस्या तब खड़ी होती है जब कुछ लोग निहित स्वार्थों के कारण समग्र दृष्टि रखने के बजाय स्थूल दृष्टि रखकर बाह्य रूप के आधार पर पाले खींचना प्रारम्भ कर देते हैं। उनका आग्रह दुराग्रह में बदल जाता है और वे जोर-जोर से भारत को 'बहुसंस्कृति' का देश कहना प्रारम्भ कर देते हैं। गोया भारतीय संस्कृति न हुई कोई मसालेदार व्यंजन हो गई जिसमें एक मसाला इस संस्कृति का है तो दूसरा किसी और का। यह प्रवृत्ति खतरनाक है और उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कथित बौध्दिक वर्ग इस प्रवृत्ति के खतरों को समझ नहीं पा रहा है।
राजनीति के चलते भारत की संस्कृति को ही विकृत रूप में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से इस देश की जड़ों को खोदना है। ऐसी ही दृष्टि भारतीय समाज को 'बहुसंख्यक' और 'अल्पसंख्यक' की श्रेणी में रखती है। इस देश में रहने वाले सभी लोग भारत की सन्तान हैं जो भी भारत भूमि को मां कहता है, ज्ञान को सरस्वती कहता है और राष्ट्र को वन्दनीय मानता है वह भारत का सच्चे अर्थों में पुत्र है। भारतीय अवधारणा यह है कि वह सभी प्रत्यक्ष-परोक्ष विचार एवं वस्तुएं जिनसे जीवन मिला है या जिनसे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने में सहायता मिलती है वे सब वन्दनीय हैं। भारतीय संस्कृति ने हमें वैदिक काल से ही यह विचार दिया है और यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पांच हजार वर्ष पूर्व था।
(लेखक भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है)
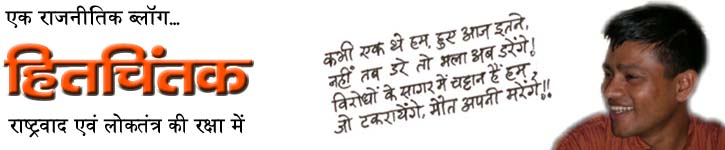
1 comment:
www.prakharhindu.blogspot.com.....
हमारे हिन्दू शूरवीरों ने जिस योजनाबद्ध तरीके से एक राष्ट्रीय कलंक को 6 दिसम्बर 1992 को धोया उस योजना के पीछे दो सत्ता के लालची लोगों का हाथ था। एक ने तो सत्ता का पूर्ण सुख भोग लिया पर दूसरा अभी भी कतार में है। यह व्यक्ति 13 दिसम्बर 2001 की घटना के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार है। इस सत्तालोलुप व्यक्ति को आजकल भारत के प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री के नाम से भी जाना जा रहा है। असल में इसने भारत भूमि पर राज करने के लिए हिन्दुत्व का भी जमके सहारा लिया अपना उल्लू सीधा किया पर अब बदले माहौल को देखकर सेक्युलरवाद की राह पकड़ अपनी स्वार्थसिद्धि की कामना कर रखता है।
यदि यह हाल है आदर्शवादी और इमानदार माने जाने वाले नेताओं का तो तमाम सेक्युलरवादियों और अन्य दलों के नेताओं से कोई भी आशा रखना मूर्खता ही है।
....www.prakharhindu.blogspot.com
Post a Comment