बृजेश ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। वह हिन्दी में कामकाज, लिखना-पढ़ना कर सकता था लेकिन आज के माहौल और हर अवसर पर लगे अंग्रेजी के ताले ने उसे इतना बेबस और हताश कर दिया कि उसे लगा अब जीवन बेकार है। वह लड़ सकता था। हो सकता है लड़ना चाहता भी हो, लेकिन जब चारों ओर हर कोई यह सलाह देने के लिए तत्पर हो कि 'जिंदगी में क्या करोगे अगर अंग्रेजी नहीं सीखी-चपरासी भी नहीं बन सकते' तो शायद वह और निराश हो गया होगा। आश्चर्य की बात यह है कि इस आत्महत्या पर न हिन्दी वालों में कोई कंपन हुआ, न ही किसी भी अन्य भाषा के पत्र में या चैनल पर इस विषय पर उस तरह की बहसें हुईं जैसी प्राय: सामाजिक सरोकारों से जुड़े क्रुध्द और बुध्दमना पत्रकार किसी आंदोलनकारी की भूमिका में किया करते हैं। भारत के अंग्रेजी अखबार भारतीय ही चलाते हैं लेकिन उनकी कोशिश यह रहती है कि वह अधिक से अधिक स्वयं को उस सांचे और आंच का प्रतिरुप दिखाते रहें जो लंदन वाले यहां के गली कूचों में छोड़ गए या वे अब भी फ्लीट स्ट्रीट से दिखाते रहते हैं।
बृजेश की आत्महत्या भारतीय भाषाओं के क्षरण की शोकांतिका है। लेकिन ग्लानि उसे हो जिसके भीतर सत्व बचा हो। देश की शोकांतिका राष्ट्रीय समाज के मर्म स्थल के रेतीले पठारों जैसी सूखती जा रही उस नदी का संकेत देती है जिसे संस्कृति भी कहा जाता है। इस समय माहौल यह है कि चैनलों और अखबारों में हिन्दी की हत्या का आनंदोत्सव बड़े गर्व और दंभ के साथ मनाया जा रहा है और कहा जाता है कि जो हिन्दी को हिन्दी के रुप में बनाए रखने के पक्षधर हैं वे बैलगाड़ी युग के पगलाए हुए संदर्भहीन जीवाश्म हैं जो बदलते समय की चाल के अनुसार स्वयं को बदलने से इनकार कर रहे हैं। यह कहते हुए हिन्दी के अखबार अब अंग्रेजी में निकलने लगे हैं, जिसमें हिन्दी का भी देवनागरी में उपयोग होता है। शुध्दता के पक्षधर वैसे ही गाली और तिरस्कार पाते हैं जैसे 'ग' से गणपति के पक्षधर 'ग' से गधा पढ़ाने के सेकुलर पक्षधरों से आघात सहते रहे हैं।
भाषा जीवन, संस्कार, सभ्यता और समाज की वैश्विक दृष्टि का पहला परिचय होता है। देश के क्षरण से पहले भाषा मरती है। भाषा का खत्म होना उन तमाम अवयवों के शिथिल और प्राणहीन होते जाने का लक्षण है जिसे राष्ट्रीयता का पार्किंसन भी कह सकते हैं। इसके परिणाम अनेक रुपों में दिखते हैं। आत्मदैन्य, आत्मविस्मृति, आत्म तिरस्कार में भौंडा आनंद और अपने से इतनी घृणा कि हमलावर आततायी बर्बरों के अनाचार को दैवदत्त कृपा मानते हुए उनके अनुचर बनने में गौरव और कृतार्थता अनुभव करने लगते हैं। खेत खलिहान में फसल रोपते और काटते समय, कुएं की मेंड़ पर पानी भरते समय, विद्यालय में, घर के भीतर या यात्रा के समय , पूजा के समय, यज्ञोपवीत संस्कार, सप्तपदी और अंतिम संस्कार के समय जो भाषा बोली और समझी जाती है उस भाषा का तिरस्कार और उसे धीरे-धीरे खत्म करने का प्रयास यदि राज्यसत्ता और उस सत्ता को चुनने वाले घटक मिलकर करने लगें तो भविष्य कैसा होगा? हिन्दी, संस्कृत तथा सभी भारतीय भाषाओं के प्रति हेय दृष्टि का संवर्ध्दन हर वह व्यक्ति कर रहा है जो आज धन, बौध्दिकता और प्रभाव में संपन्न है एवं वर्तमान प्रचलित एवं लोकमान्य मापदंडों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ऐसे किसी भी परिवार में अपनी घरेलू भाषा, गीत, संस्कार, प्राचीन पुस्तकों का पठन पाठन और सम्मान कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है, यह रहस्य की बात नहीं रह गई है बल्कि सबको ठीक उसी प्रकार से दिख रहा है जैसे दीवार पर लिखी इबारत दिखती है। इसलिए जिन कांवेंट स्कूलों में अक्सर त्योहारों की छुट्टी न होना, बिंदी न लगाने या चूड़ी न पहनकर आने की शिकायतें, संपादक के नाम रीढ़हीन गुस्साए पत्रों में दिखती हैं, ऐसे किसी भी विद्यालय से कभी संस्कृतिनिष्ठ धीरोदात्त व्यक्ति ने दृढ़ता से अपने बच्चे निकाले हों, ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं?
खंडित आजादी के बाद भी देश सिकुड़ता ही गया, उसी अनुपात में जिस अनुपात में भारतीय भाषा का विस्तार और सम्मान सिकुड़ता गया। अब कश्मीर से भारतीय देशभक्त सिकुड़कर जम्मू तक आए। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं क्या हुआ? कश्मीर से कश्मीरी भाषा को निकाला गया। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कश्मीरी भाषा कश्मीर की राजभाषा नहीं है, वहां की राजभाषा है अरबी लिपि में लिखी जाने वाली वह उर्दू जिसका कश्मीर, कश्मीरियत, कश्मीर के इतिहास और संस्कृति से कोई आत्मीय रिश्ता रहा ही नहीं। अगर कुछ रहा तो सिर्फ यह कि जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश ने उर्दू में अलगाववादी, विभाजनकारी पाकिस्तान परस्तों को गोला बारुद और लड़ने का सामान दिया ठीक वैसे ही कश्मीर पर उर्दू थोपे जाने के बाद वहां की मूल संस्कृति, परंपरा, इतिहास और उस सबका प्रतिनिधि करने वाले हिन्दुओं को ही नहीं बल्कि एक साथ रहने वाले सांझी विरासत के मुसलमानों को भी आहत किया गया। यानी जमीन सिकुड़ी, भाषा को बहिष्कृत किया और फिर देशभक्तों को तिरस्कृत कर पलायन पर मजबूर किया गया। उधर अरुणाचल पर निरंतर खतरे की तलवार लटकती आ रही है। आज जिससे भी आप पूछिए, पूर्वांचल में ऐसा कौन सा द्वीप अभी शेष है जहां शासन, सुशासन, गांव-नगरों में आज भी जयहिंद का नारा सम्मान से उच्चारा जाता है, तो एक ही जवाब होगा-अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में आज भी हिन्दी जीवित है। वहां के कामकाज, सामान्य व्यवहार, बाजार और यहां तक कि अरुणाचली जनजातियों के घरों और गांवों में भी हिन्दी में ही व्यवहार सामान्य बात है। लेकिन अब अरुणाचल पर भी खतरा मंडराने लगा है और ईसाई मिशनरी जहां-जहां अरुणाचल में अलगाव की आग को हवा दे रहे हैं वहां-वहां रोमन लिपि और रोमन भाषा बढ़ रही है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारतीय भाषाओं का बहिष्कार और अपमान पहले हुआ और उसके बाद भारत से अलग होने की मांग उठी। यही भारतीयता का सिकुड़ना और विलुप्त होना है, जो राम मंदिर के विरोध में राम की अर्चना कर रहे उन्हीं लोगों को खड़ा कर देता है जो सत्ता के लिए सेकुलर होते हैं और धन-धान्य का व्यापार बढ़ाने के लिए घर के प्राइवेट रुम में अत्यंत धार्मिक और पूजापाठी।
जिनका अपने में विश्वास नहीं और जो द्रोपदी के चीरहरण को किसी खेल का सामान्य दृश्य मानकर जीवन व्यापार चलाते रहते हैं वही रामसेतु भंजन में कुछ भी असामान्य नहीं देखते।
भाषा और संस्कार वह जमीन है जो राष्ट्र को आधार देती है। राष्ट्र जंगल, नदियों, पहाड़ों और बस्तियों में श्मशान घाटों का समुच्चय नहीं होता, वह भूधरों का ऐसा खंड हो सकता है जहां लोग वैसे ही रहते हों जैसे मवेशी चराने वाले किसी भी हरे भरे मैदान को देखकर वहां सुबह मवेशी छोड़ देते हैं और शाम को मवेशियों का दूध निकाल लेते हैं या भेड़ों की ऊन काट लेते हैं। वे पैदा हुए हैं इसलिए जीने का साधन ढूंढना ही पड़ता है और मर जाएंगे तो न उस जमीन से रिश्ता होगा जहां जिए थे और न ही वहां के दर्द से वेदना का कोई सरोकार पैदा कर पाएंगे। यही लोग भाषा, भूषा और भावना के भंजक होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। भौगोलिक जमीन गई तो न प्रतिशोध की आवाज उठी, न प्रतिकार का संकल्प गूंजा। अब सांस्कृतिक जमीन घट रही है, दूर हो रही है और वहां गजनी और गोरियों के तम्बू तन गए हैं, फिर भी तानसेन दरबार में गा रहे हैं और वाजिद अली शाह की रूमानियत के गीतों का इश्क बदस्तूर जारी है। हमें समझाया जा रहा है 'विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, भारतीय सेठों के बैंक खाते दुनिया में सबसे बड़े और ऊंचे हुए हैं। देखो, हम सबसे अमीर हो गए। हमारी अभिनेत्रियां भी दुनिया भर में प्रसिध्द हो रही हैं, होटलों, बाजारों और घटिया से घटिया जगहों पर भी उनके पोस्टर लगे हैं, फिल्मों की सीडियां बिक रही हैं। देखो, हम कितना बढ़ रहे हैं।' यह बढ़ना किसका बढ़ना है? क्या कोई यह सवाल नहीं उठाएगा? यहां के सेठों के पास पैसा बाबर, औरंगजेब या मैकाले के समय क्या कम था और यहां की नौटंकियां और नृत्य क्या कम लोकप्रिय थे? पर भारत कहां था?
भारत तो तिल-तिलकर जल रहा था। जिन्हें उसकी जलन से पीड़ा हुई वे स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, भगत सिंह और डा. हेडगेवार बने। जिन्हें उस समय भी सब कुछ सामान्य लग रहा वे शहर कोतवाल या भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले बने। उन्हें इसमें कुछ भी खराब नहीं लगा, स्वाभाविक ही था।
वही लोग रामसेतु तोड़े जाने पर न उद्वेलित होते हैं न परेशान। पत्थर ही तो हैं। आज तक किसी ने नहीं तोड़ा, आज तोड़ रहे हैं तो क्या हुआ? ये वही लोग थे जो सीता के अपहरण पर भी परेशान नहीं हुए और रावण की लंका में रोज का व्यापार, खाना पीना, आमोद-प्रमोद करते रहे। सीता अगर अशोक वाटिका में थी, तो थी। सीता जैसी अनेक स्त्रियों का रावण अपहरण करता आ रहा था। रावण स्त्री जाति के प्रति भोगवादी दृष्टि रखने वाला अहंकारी, बलशाली राजा था तो क्या हुआ? क्या इससे किसी को पीड़ा होनी चाहिए थी? आमतौर पर सोचा जाए तो सभी को रावण के इस व्यवहार के प्रति विद्रोही बनना चाहिए। लेकिन उस समय मेघनाथ और कुंभकरण थे और इस समय बालू और करुणानिधि हैं। बालू और करुणानिधि अपने मन में यह मानकर चल रहे हैं कि वे जो जानते हैं, समझते हैं और कर रहे हैं, वही ठीक है। इसलिए एक अनपढ़ उच्छिष्ट जीवी की तरह वे किसी ऊल जलूल उध्दरण और बकवास को वाल्मीकि की रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अंश बता देते हैं या शपथ पत्र दे देते हैं कि राम थे ही नहीं। और दीवाली, दशहरे पर राम का पूजन करते हुए रामसेतु तोड़ने की साजिश में उसी आनंद के साथ शामिल होते हैं जिस आनंद से वे रात में दीवाली पूजन करते हैं। ऐसे लोगों का पतन और पराजय सुनिश्चित करनी है, राम की सेना में शामिल होना है और यही कार्य अयोध्या आगमन की पूर्व पीठिका बन सकता है-और कुछ नहीं।
इसलिए राम योध्दा होने का अर्थ है अपनी भारतीयता और रामभक्ति और अपने मनुष्यत्व की साधना करना। राम योध्दा होने का अर्थ यह भी है कि एक जिद्द लेकर अपने चतुर्दिक समझौतावादियों के सलेटी और स्याह रंग को भस्म करते जाना। जो समझौता करे, झुके या बीच का रास्ता खोजे वह सिर्फ धिक्कार के योग्य है। अयोध्या की दीपावली भारत का दीपोत्सव तभी बन सकती है जब राम योध्दा राक्षसों को परास्त कर घर लौटें।
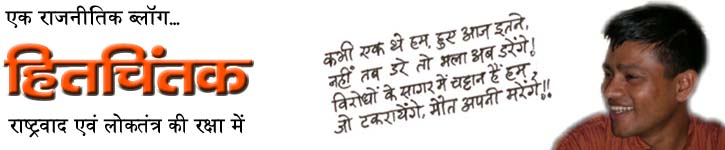
2 comments:
यह दुखद धटना मीडिया के लिए ख़बर नहीं बन पाई...काफी शर्मनाक हैं हम सब के लिए...
सत्य है किसी भी देश की भाषा और संस्कृति ही राष्ट्र का प्राण होती है इसके बिना अखंडता की बात करना पत्तों को पानी पिलाने जैसा ही है
Post a Comment