
लेखक- स्वपन दासगुप्ता
भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के मामले में यह अटपटा समय है। पिछले दिनों गार्जियन में एक निर्वासित बर्मी और थाईलैंड स्थित इरावेडी मैगजीन के संपादक आंग जा ने जो कुछ लिखा वह बेशक भारतीयों को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने लिखा-बर्मा के नेता अभी भी यह मानते हैं कि उन्हें अपने शासन को जारी रखने के लिए चीन, भारत और रूस का सहयोग मिलता रहेगा।- दो नैतिकताविहीन राष्ट्रों के साथ भारत को रखा जाना अपने आप में एक खराब अनुभव है। यह तब और अधिक कष्टप्रद हो जाता है जब नई दिल्ली को दमनकारी सैन्य जुंटा को समर्थन देता हुआ देखा जाता है। यह विडंबना ही है कि महात्मा गांधी का देश बर्मा में लोकतांत्रिक आंदोलन का दमन कर रही जुंटा के खिलाफ लामबंद होने की पश्चिमी जगत की कोशिशों में सुर नहीं मिला रहा।
यदि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले नेल्सन मंडेला को भारत का समर्थन मिल सकता है और ऐसा कर नई दिल्ली गांधी की विरासत पर गौरवान्वित हो सकती है तो अब बर्मा में एक ऐसी साहसी महिला की बात है जो आंसू बहा रही है और अपने देश में लोकतंत्र के समर्थन में बौद्ध भिक्षुओं के मौन प्रदर्शन को खुद भी मौन रहकर देख रही है। बर्मा की राजधानी यांगून में आंग सान सू की अपने घर में नजरबंद हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए उनकी लड़ाई अप्रतिम है। लोकतंत्र के लिए एक और प्रतिबद्ध संघर्ष के रूप में सू की ने यह लड़ाई भले ही दो दशक पहले आरंभ की हो, लेकिन आज यह साहसी और दृढ़ विचारों वाली महिला जीवंत गांधी के रूप में नजर आ रही है। बर्मा की घटनाओं ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक गंभीर धर्म संकट उपस्थित कर दिया है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि प्रत्येक भारतीय का हृदय नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी तथा उसकी नजरबंद नेता के साथ है। आंग सान सू की का पालन-पोषण, उनकी शिक्षा तथा उनके मूल्य हर तरह से उन्हें हमारे अपने बीच की महिला बनाते हैं। बावजूद इसके पिछले एक दशक में सिर्फ जार्ज फर्नाडीज ही आंग सान सू की के पक्ष में खुलकर और निरंतरता से बोले हैं।
भारतीयों के लिए सू की और 74 वर्षीय वरिष्ठ जनरल थान श्वे के बीच कोई चयन ही नहीं है। यह अच्छाई और बुराई के बीच एक साधारण लड़ाई है-दुर्गा और महिषासुर के बीच प्राचीन युद्ध की तरह। वैसे भारत के सतर्क और देखो और प्रतीक्षा करो वाले दृष्टिकोण के समर्थन में दिए जाने वाले तर्को को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। 1990 के दशक के आरंभ में भारत ने बर्मा में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में अपनी गर्दन फंसा ली थी और इसके परिणाम उसे भुगतने पड़s थे। बर्मा के जनरलों ने सीमा पार के क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे नगा, मणिपुरी और असमी विद्रोहियों की ओर से आंखें फेर ली थीं। भारत और बर्मा के बीच संबंधों में आए तनाव का फायदा उठाते हुए चीन ने वहां अपनी जड़ें मजबूत करने में देर नहीं लगाई। 1990 के दशक के मध्य से आरंभ हुए धैर्यपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों के बाद ही नई दिल्ली क्षति की भरपाई कर करने में सफल रही। व्यापारिक उपस्थिति के साथ-साथ पूर्वी सीमा को सुरक्षित बनाने में बर्मा का सहयोग फिर से हासिल करने के लिए भारत को जो कीमत चुकानी पड़ी वह थी लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मामले में पूर्ण खामोशी। यह सही है कि भारत चीन की पकड़ को पूरी तरह विफल करने में सफल नहीं रहा है] लेकिन इतना तो है ही कि भारत की बर्मा में अर्थपूर्ण उपस्थिति है। अपने मतलब के लिए ही सही, लेकिन जुंटा भी पारस्परिक हितों पर आधारित समझबूझ में पीछे नहीं हटी। अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश और ब्रिटिश प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन सैन्य जुंटा के खिलाफ अपनी नाराजगी के प्रति भले ही ईमानदार हों, सच्चाई यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय संघ के बर्मा में कोई महत्वपूर्ण, सामरिक और व्यापारिक हित नहीं जुड़े हैं। लिहाजा सऊदी अरब और पाकिस्तान के विपरीत बर्मा की सैन्य जुंटा के खिलाफ वे सख्त कदम उठा सकते हैं। सू की के आंदोलन की मौलिक सराहना और सैन्य शासन की आमतौर पर होने वाली निंदा को छोड़ दिया जाए तो पश्चिम का बर्मा से कोई सीधा लेना-देना नहीं है। बर्मा में लोकतंत्र के प्रति पश्चिमी जगत की संवेदनशीलता का ज्यादा मतलब दरअसल चीन के कारण है। कोंडोलिजा राइस या डेविड मिलिबैंड मानें या न मानें, लेकिन सच यह है कि बर्मा का घटनाक्रम एशिया में चीन के वर्चस्व को लेकर उभरी चिंताओं से जुड़ा हुआ है। यह कम विचित्र नहीं है कि बर्मा के मामले में भारत और पश्चिम के हितों में काफी कुछ समानता है। भारत आदर्श रूप में बर्मा में ऐसा शासन चाहेगा जो भले ही पश्चिम समर्थक हो, लेकिन चीन से दूर रहे। ऐसा कोई शासन यदि भारत में शिक्षित आंग सान सू की के नेतृत्व में कायम होता है तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। हालांकि बर्मा में लोकतंत्र की लड़ाई में फंसने से पहले भारत को दो बातों पर आश्वस्त होना होगा।
पहला यह कि भारत को इस पर सुनिश्चित होना होगा कि लोकतंत्र समर्थक आंदोलन वास्तव में सफल हो अर्थात सैन्य शासन जन दबाव के आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाए। यदि लोकतंत्र के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन एक बार फिर कुचल दिया जाता है तो जुंटा उन देशों से पूरी कीमत वसूलेगी जो इस आंदोलन के समर्थन में होंगे। फिलहाल संकेत बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। दूसरे, सैन्य जुंटा के असामयिक पतन से बर्मा में केंद्रीय शासन कमजोर होगा और पूरी आशंका है कि चीन इस मौके का फायदा उठाकर स्थानीय विद्रोहियों को अपना समर्थन देना आरंभ कर देगा। बर्मा में कोई भी अस्थिरता भारत में उत्तार-पूर्व के बागियों को नए अवसर उपलब्ध करा सकती है। क्या तब पश्चिमी जगत भारत की मदद के लिए आगे आएगा। अपने हितों के लिए भारत को एक स्थिर और आत्मविश्वासी बर्मा की आवश्यकता है, जो चीन को दूर रख सके। हमारी आतंरिक बहस को उस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए जिससे यह उद्देश्य हासिल किया जा सके। बाकी सब धोखा है।(साभार- दैनिक जागरण)
भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के मामले में यह अटपटा समय है। पिछले दिनों गार्जियन में एक निर्वासित बर्मी और थाईलैंड स्थित इरावेडी मैगजीन के संपादक आंग जा ने जो कुछ लिखा वह बेशक भारतीयों को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने लिखा-बर्मा के नेता अभी भी यह मानते हैं कि उन्हें अपने शासन को जारी रखने के लिए चीन, भारत और रूस का सहयोग मिलता रहेगा।- दो नैतिकताविहीन राष्ट्रों के साथ भारत को रखा जाना अपने आप में एक खराब अनुभव है। यह तब और अधिक कष्टप्रद हो जाता है जब नई दिल्ली को दमनकारी सैन्य जुंटा को समर्थन देता हुआ देखा जाता है। यह विडंबना ही है कि महात्मा गांधी का देश बर्मा में लोकतांत्रिक आंदोलन का दमन कर रही जुंटा के खिलाफ लामबंद होने की पश्चिमी जगत की कोशिशों में सुर नहीं मिला रहा।
यदि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले नेल्सन मंडेला को भारत का समर्थन मिल सकता है और ऐसा कर नई दिल्ली गांधी की विरासत पर गौरवान्वित हो सकती है तो अब बर्मा में एक ऐसी साहसी महिला की बात है जो आंसू बहा रही है और अपने देश में लोकतंत्र के समर्थन में बौद्ध भिक्षुओं के मौन प्रदर्शन को खुद भी मौन रहकर देख रही है। बर्मा की राजधानी यांगून में आंग सान सू की अपने घर में नजरबंद हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए उनकी लड़ाई अप्रतिम है। लोकतंत्र के लिए एक और प्रतिबद्ध संघर्ष के रूप में सू की ने यह लड़ाई भले ही दो दशक पहले आरंभ की हो, लेकिन आज यह साहसी और दृढ़ विचारों वाली महिला जीवंत गांधी के रूप में नजर आ रही है। बर्मा की घटनाओं ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक गंभीर धर्म संकट उपस्थित कर दिया है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि प्रत्येक भारतीय का हृदय नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी तथा उसकी नजरबंद नेता के साथ है। आंग सान सू की का पालन-पोषण, उनकी शिक्षा तथा उनके मूल्य हर तरह से उन्हें हमारे अपने बीच की महिला बनाते हैं। बावजूद इसके पिछले एक दशक में सिर्फ जार्ज फर्नाडीज ही आंग सान सू की के पक्ष में खुलकर और निरंतरता से बोले हैं।
भारतीयों के लिए सू की और 74 वर्षीय वरिष्ठ जनरल थान श्वे के बीच कोई चयन ही नहीं है। यह अच्छाई और बुराई के बीच एक साधारण लड़ाई है-दुर्गा और महिषासुर के बीच प्राचीन युद्ध की तरह। वैसे भारत के सतर्क और देखो और प्रतीक्षा करो वाले दृष्टिकोण के समर्थन में दिए जाने वाले तर्को को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। 1990 के दशक के आरंभ में भारत ने बर्मा में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में अपनी गर्दन फंसा ली थी और इसके परिणाम उसे भुगतने पड़s थे। बर्मा के जनरलों ने सीमा पार के क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे नगा, मणिपुरी और असमी विद्रोहियों की ओर से आंखें फेर ली थीं। भारत और बर्मा के बीच संबंधों में आए तनाव का फायदा उठाते हुए चीन ने वहां अपनी जड़ें मजबूत करने में देर नहीं लगाई। 1990 के दशक के मध्य से आरंभ हुए धैर्यपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों के बाद ही नई दिल्ली क्षति की भरपाई कर करने में सफल रही। व्यापारिक उपस्थिति के साथ-साथ पूर्वी सीमा को सुरक्षित बनाने में बर्मा का सहयोग फिर से हासिल करने के लिए भारत को जो कीमत चुकानी पड़ी वह थी लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मामले में पूर्ण खामोशी। यह सही है कि भारत चीन की पकड़ को पूरी तरह विफल करने में सफल नहीं रहा है] लेकिन इतना तो है ही कि भारत की बर्मा में अर्थपूर्ण उपस्थिति है। अपने मतलब के लिए ही सही, लेकिन जुंटा भी पारस्परिक हितों पर आधारित समझबूझ में पीछे नहीं हटी। अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश और ब्रिटिश प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन सैन्य जुंटा के खिलाफ अपनी नाराजगी के प्रति भले ही ईमानदार हों, सच्चाई यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय संघ के बर्मा में कोई महत्वपूर्ण, सामरिक और व्यापारिक हित नहीं जुड़े हैं। लिहाजा सऊदी अरब और पाकिस्तान के विपरीत बर्मा की सैन्य जुंटा के खिलाफ वे सख्त कदम उठा सकते हैं। सू की के आंदोलन की मौलिक सराहना और सैन्य शासन की आमतौर पर होने वाली निंदा को छोड़ दिया जाए तो पश्चिम का बर्मा से कोई सीधा लेना-देना नहीं है। बर्मा में लोकतंत्र के प्रति पश्चिमी जगत की संवेदनशीलता का ज्यादा मतलब दरअसल चीन के कारण है। कोंडोलिजा राइस या डेविड मिलिबैंड मानें या न मानें, लेकिन सच यह है कि बर्मा का घटनाक्रम एशिया में चीन के वर्चस्व को लेकर उभरी चिंताओं से जुड़ा हुआ है। यह कम विचित्र नहीं है कि बर्मा के मामले में भारत और पश्चिम के हितों में काफी कुछ समानता है। भारत आदर्श रूप में बर्मा में ऐसा शासन चाहेगा जो भले ही पश्चिम समर्थक हो, लेकिन चीन से दूर रहे। ऐसा कोई शासन यदि भारत में शिक्षित आंग सान सू की के नेतृत्व में कायम होता है तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। हालांकि बर्मा में लोकतंत्र की लड़ाई में फंसने से पहले भारत को दो बातों पर आश्वस्त होना होगा।
पहला यह कि भारत को इस पर सुनिश्चित होना होगा कि लोकतंत्र समर्थक आंदोलन वास्तव में सफल हो अर्थात सैन्य शासन जन दबाव के आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाए। यदि लोकतंत्र के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन एक बार फिर कुचल दिया जाता है तो जुंटा उन देशों से पूरी कीमत वसूलेगी जो इस आंदोलन के समर्थन में होंगे। फिलहाल संकेत बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। दूसरे, सैन्य जुंटा के असामयिक पतन से बर्मा में केंद्रीय शासन कमजोर होगा और पूरी आशंका है कि चीन इस मौके का फायदा उठाकर स्थानीय विद्रोहियों को अपना समर्थन देना आरंभ कर देगा। बर्मा में कोई भी अस्थिरता भारत में उत्तार-पूर्व के बागियों को नए अवसर उपलब्ध करा सकती है। क्या तब पश्चिमी जगत भारत की मदद के लिए आगे आएगा। अपने हितों के लिए भारत को एक स्थिर और आत्मविश्वासी बर्मा की आवश्यकता है, जो चीन को दूर रख सके। हमारी आतंरिक बहस को उस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए जिससे यह उद्देश्य हासिल किया जा सके। बाकी सब धोखा है।(साभार- दैनिक जागरण)
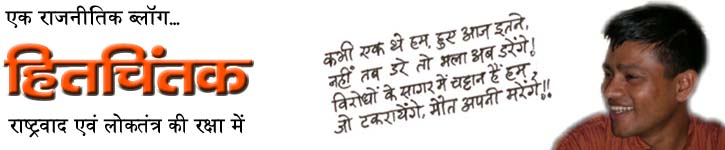
No comments:
Post a Comment