
तिब्बत के प्रश्न को सुलझाना ही होगा : इन्द्रेश कुमार
तिब्बत का प्रश्न अब उस मोड़ पर पहुँच गया है जहां यदि हम ठीक ढंग से प्रयास करें तो उसे उसकी निर्णायक परिणति तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि भारत सरकार इसमें अपनी भूमिका ठीक ढंग से अदा करती है कि नहीं ? आज इतने सालों के बाद यदि हम तिब्बत आंदोलन पर समग्रता से विचार करें तो इसके तीन पड़ाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। 1959 में दलाईलामा तिब्बत से भारत में आए थे। पंडित नेहरू के सुझाव पर दलाईलामा ने कुछ साल चीन के साथ निभाने का प्रयास भी किया क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा तो 1949-50 में ही कर लिया था । 1949 से लेकर 1959 तक का यह 10 साल का कालखंड तिब्बत के इतिहास का विनाशकारी और निराशाजनक कालखंड है। एक शक्तिशाली पड़ोसी देश चीन तिब्बत को निगल रहा था और दुनिया चुपचाप उसे देख रही थी। तिब्बत के गुलाम हो जाने से सबसे ज्यादा नुकसाना भारत को ही होने वाला था लेकिन भारत सरकार केवल चुप नहीं रही बल्कि दलाईलामा को भी चुप रहकर येनकेन प्रकारेण माओ के साथ तालमेल बनाने की सलाह देती रही। पंडित नेहरू को शायद इसमें कुछ अटपटा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि वे उस कालखंड में स्वयं भी माओ से तालमेल बिठाने का हर प्रयास कर रहे थे। वैसे इधर जो नए दस्तावेज मिल रहे हैं उनसे ऐसा आभास भी मिलता है कि पंडित नेहरू चीन के खतरे को पहचान तो रहे थे लेकिन उसका सामना करने में वे स्वयं को विवश अनुभव कर रहे थे। उनकी इस विवशता या फिर चीन पर उनके विश्वास ने भारत और तिब्बत दोनों को ही घायल किया। तिब्बत के इतिहास का यह कालखंड यदि श्रीगुरूजी माधवराव सदाशिव गोलवलकर के शब्दों में कहा जाए तो तिब्बत के साथ विश्वासघात का कालखंड है।
दूसरा कालखंड 1959 से शुरू होता है जब दलाईलामा को तिब्बत से भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। उनके साथ उनके हजारों अनुयायी भी थे। भारत ने दलाईलामा को शरण तो दी लेकिन किसी प्रकार की भी गतिविधियों की उन्हें अनुमति नहीं दी। 1962 को भरत के इतिहास का भी और तिब्बत के इतिहास का भी टर्निंग प्वाइन्ट कहा जा सकता है। चीन के आक्रमण के कारण भारत का मोह तो उससे टूटा ही साथ ही पंडित नेहरू को इस बात का पता भी चल गयाकि चीन के बारे में दलाई लामा का आकलन सही था और उनका अपना गलत । इसमें एक बात और जोड़नी जरूरी है कि इस संपूर्ण कालखंड में तिब्बत के लोगों को भारतीयों का भरपूर समर्थन प्राप्त होता रहा। देशों के इतिहास में अनेक बार ऐसा कालखंड भी आता है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद किसी प्रमुख प्रश्न पर सरकार की राय उत्तरी धु्रव की होती है और जनता की राय दक्षिणी ध्रुव की होती है । भारत के इतिहास में तिब्बत का प्रश्न ऐसा ही प्रश्न कहा जाएगा। लेकिन 1962 के बाद दलाईलामा को भारत सरकार ने कम से कम इस बात की अनुमति तो दे ही दी कि वे भारत में रहकर तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को चला सकते हैं। चाहे यह अनुमति प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार ने एक भरी पूरी सरकार का रूप ही अख्तयार कर लिया था। इस कालखंड में भारत के लगभग तमाम राजनैतिक दलों का तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को भरतपूर समर्थन मिला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनसंघ की इसमें अग्रणी भूमिका रही। संघ के उस समय के सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष आचार्य रघुवीर तिब्बत के प्रश्न को देश की विदेश नीति में प्रमुख स्थान पर ले आए थे। समाजवादी भी अपने ढंग से इस प्रश्न को लेकर भारत की जनता के बीच जा रहे थे। राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का स्मरण यहां करना उचित होगा ।
आपात्स्थिति के बाद ऐसा कालखंड आया जिसमें सरकारों ने एक बार फिर चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के नाम पर बीजिंग में दस्तख देनी शुरू कर दी। इधर दलाईलामा भी भारत सरकार का पूरा समर्थन न मिलते देखकर मध्यमार्ग अपनाने के लिए विवश हुए । अलबत्ता मध्यमार्ग से इतना लाभ अवश्य हो सकता था कि भारत सरकार यदि चाहती तो उसे तिब्बत का खुलकर समर्थन करने का एक अवसर प्राप्त हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार ने इस अवसर का भी लाभ नहीं उठाया । अलबत्ता उसकी चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने की इच्छा जरूर तेज होती गई और यह सब तब हो रहा था जब चीन पहले की तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की अपनी कोशिशों में जी-जान से जुटा हुआ था। उसने 1962 में भारत पर आक्रमण भी इसलिए किया था ताकि उसे सबक सिखाया जा सके और नेतृत्व की उसकी इच्छा का उपहास उडाया जा सके। 21वीं शताब्दी में भी चीन उसी रास्ते पर चल रहा है और भारत सरकार एक बार फिर पंडित नेहरू के रास्ते पर ही चल पड़ी है। खुदा का शुक्र है कि अभी तक साऊथ ब्लॉक में हिंदी चीनी भाई -भाई के नारे लगने शुरू नहीं हुए है। इस मरहले पर जार्ज फर्नांडिस ने जब यह कहा था कि चीन हमारा शत्रु नम्बर एक है तो वह असलियत से ही पर्दा उठा रहे थे। पर जो लोग असलियत को ढकना चाहते है उन्होंने जल्दी-जल्दी उस पर फिर पर्दा डालना शुरू कर दिया। परंतु पिछले लगभग 10 सालों से तिब्बत का प्रश्न एक बार फिर देश की मुख्य कार्यसूची में शामिल हो रहा है। भारत-तिब्बत सहयोग मंच इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उसने हाशिये पर चले गए इस प्रश्न को फिर देश की जनता के सम्मुख रखा है और नीति निर्धारकों को तिब्बत के प्रश्न से दाएं-बाएं भागने से रोकने का प्रयास किया है। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तिब्बत की गुलामी से कैलाश मानसरोवर भी गुलाम हो गया है। कैलाश मानसरोवर करोड़ों हिन्दुओं, सिखों और बौध्दों की श्रध्दा भूमि है। चीन के इतिहास में कैलाश मानसरोवर कहीं नहीं है। जबकि भारत और तिब्बत का इतिहास कैलाश मानसरोवर के बिना अधूरा है । भारत सरकार तिब्बत के प्रश्न को अपनी विदेश नीति का मुख्य मुद्दा बनाना चाहिए। तिब्बत को स्वतंत्र कराना भारत का दायित्व है, क्योंकि तिब्बत उस मूल सांस्कृतिक प्रवाह का अंग हैजिससे भारत भी उत्प्लावित हो रहा है।
तिब्बत का प्रश्न अब उस मोड़ पर पहुँच गया है जहां यदि हम ठीक ढंग से प्रयास करें तो उसे उसकी निर्णायक परिणति तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि भारत सरकार इसमें अपनी भूमिका ठीक ढंग से अदा करती है कि नहीं ? आज इतने सालों के बाद यदि हम तिब्बत आंदोलन पर समग्रता से विचार करें तो इसके तीन पड़ाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। 1959 में दलाईलामा तिब्बत से भारत में आए थे। पंडित नेहरू के सुझाव पर दलाईलामा ने कुछ साल चीन के साथ निभाने का प्रयास भी किया क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा तो 1949-50 में ही कर लिया था । 1949 से लेकर 1959 तक का यह 10 साल का कालखंड तिब्बत के इतिहास का विनाशकारी और निराशाजनक कालखंड है। एक शक्तिशाली पड़ोसी देश चीन तिब्बत को निगल रहा था और दुनिया चुपचाप उसे देख रही थी। तिब्बत के गुलाम हो जाने से सबसे ज्यादा नुकसाना भारत को ही होने वाला था लेकिन भारत सरकार केवल चुप नहीं रही बल्कि दलाईलामा को भी चुप रहकर येनकेन प्रकारेण माओ के साथ तालमेल बनाने की सलाह देती रही। पंडित नेहरू को शायद इसमें कुछ अटपटा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि वे उस कालखंड में स्वयं भी माओ से तालमेल बिठाने का हर प्रयास कर रहे थे। वैसे इधर जो नए दस्तावेज मिल रहे हैं उनसे ऐसा आभास भी मिलता है कि पंडित नेहरू चीन के खतरे को पहचान तो रहे थे लेकिन उसका सामना करने में वे स्वयं को विवश अनुभव कर रहे थे। उनकी इस विवशता या फिर चीन पर उनके विश्वास ने भारत और तिब्बत दोनों को ही घायल किया। तिब्बत के इतिहास का यह कालखंड यदि श्रीगुरूजी माधवराव सदाशिव गोलवलकर के शब्दों में कहा जाए तो तिब्बत के साथ विश्वासघात का कालखंड है।
दूसरा कालखंड 1959 से शुरू होता है जब दलाईलामा को तिब्बत से भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। उनके साथ उनके हजारों अनुयायी भी थे। भारत ने दलाईलामा को शरण तो दी लेकिन किसी प्रकार की भी गतिविधियों की उन्हें अनुमति नहीं दी। 1962 को भरत के इतिहास का भी और तिब्बत के इतिहास का भी टर्निंग प्वाइन्ट कहा जा सकता है। चीन के आक्रमण के कारण भारत का मोह तो उससे टूटा ही साथ ही पंडित नेहरू को इस बात का पता भी चल गयाकि चीन के बारे में दलाई लामा का आकलन सही था और उनका अपना गलत । इसमें एक बात और जोड़नी जरूरी है कि इस संपूर्ण कालखंड में तिब्बत के लोगों को भारतीयों का भरपूर समर्थन प्राप्त होता रहा। देशों के इतिहास में अनेक बार ऐसा कालखंड भी आता है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद किसी प्रमुख प्रश्न पर सरकार की राय उत्तरी धु्रव की होती है और जनता की राय दक्षिणी ध्रुव की होती है । भारत के इतिहास में तिब्बत का प्रश्न ऐसा ही प्रश्न कहा जाएगा। लेकिन 1962 के बाद दलाईलामा को भारत सरकार ने कम से कम इस बात की अनुमति तो दे ही दी कि वे भारत में रहकर तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को चला सकते हैं। चाहे यह अनुमति प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार ने एक भरी पूरी सरकार का रूप ही अख्तयार कर लिया था। इस कालखंड में भारत के लगभग तमाम राजनैतिक दलों का तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को भरतपूर समर्थन मिला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनसंघ की इसमें अग्रणी भूमिका रही। संघ के उस समय के सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष आचार्य रघुवीर तिब्बत के प्रश्न को देश की विदेश नीति में प्रमुख स्थान पर ले आए थे। समाजवादी भी अपने ढंग से इस प्रश्न को लेकर भारत की जनता के बीच जा रहे थे। राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का स्मरण यहां करना उचित होगा ।
आपात्स्थिति के बाद ऐसा कालखंड आया जिसमें सरकारों ने एक बार फिर चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के नाम पर बीजिंग में दस्तख देनी शुरू कर दी। इधर दलाईलामा भी भारत सरकार का पूरा समर्थन न मिलते देखकर मध्यमार्ग अपनाने के लिए विवश हुए । अलबत्ता मध्यमार्ग से इतना लाभ अवश्य हो सकता था कि भारत सरकार यदि चाहती तो उसे तिब्बत का खुलकर समर्थन करने का एक अवसर प्राप्त हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार ने इस अवसर का भी लाभ नहीं उठाया । अलबत्ता उसकी चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने की इच्छा जरूर तेज होती गई और यह सब तब हो रहा था जब चीन पहले की तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की अपनी कोशिशों में जी-जान से जुटा हुआ था। उसने 1962 में भारत पर आक्रमण भी इसलिए किया था ताकि उसे सबक सिखाया जा सके और नेतृत्व की उसकी इच्छा का उपहास उडाया जा सके। 21वीं शताब्दी में भी चीन उसी रास्ते पर चल रहा है और भारत सरकार एक बार फिर पंडित नेहरू के रास्ते पर ही चल पड़ी है। खुदा का शुक्र है कि अभी तक साऊथ ब्लॉक में हिंदी चीनी भाई -भाई के नारे लगने शुरू नहीं हुए है। इस मरहले पर जार्ज फर्नांडिस ने जब यह कहा था कि चीन हमारा शत्रु नम्बर एक है तो वह असलियत से ही पर्दा उठा रहे थे। पर जो लोग असलियत को ढकना चाहते है उन्होंने जल्दी-जल्दी उस पर फिर पर्दा डालना शुरू कर दिया। परंतु पिछले लगभग 10 सालों से तिब्बत का प्रश्न एक बार फिर देश की मुख्य कार्यसूची में शामिल हो रहा है। भारत-तिब्बत सहयोग मंच इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उसने हाशिये पर चले गए इस प्रश्न को फिर देश की जनता के सम्मुख रखा है और नीति निर्धारकों को तिब्बत के प्रश्न से दाएं-बाएं भागने से रोकने का प्रयास किया है। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तिब्बत की गुलामी से कैलाश मानसरोवर भी गुलाम हो गया है। कैलाश मानसरोवर करोड़ों हिन्दुओं, सिखों और बौध्दों की श्रध्दा भूमि है। चीन के इतिहास में कैलाश मानसरोवर कहीं नहीं है। जबकि भारत और तिब्बत का इतिहास कैलाश मानसरोवर के बिना अधूरा है । भारत सरकार तिब्बत के प्रश्न को अपनी विदेश नीति का मुख्य मुद्दा बनाना चाहिए। तिब्बत को स्वतंत्र कराना भारत का दायित्व है, क्योंकि तिब्बत उस मूल सांस्कृतिक प्रवाह का अंग हैजिससे भारत भी उत्प्लावित हो रहा है।
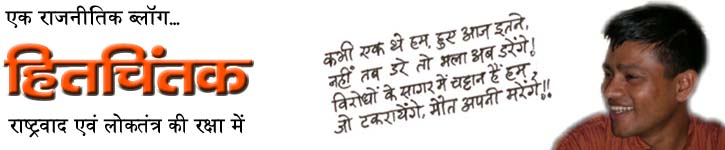
No comments:
Post a Comment